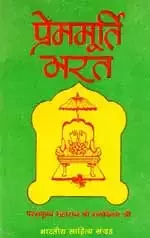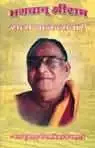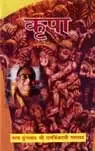|
धर्म एवं दर्शन >> प्रेममूर्ति भरत प्रेममूर्ति भरतरामकिंकर जी महाराज
|
|
||||||
भरत जी के प्रेम का तात्विक विवेचन
नर्तक ताल की गति पर ही तो नृत्य करता है। उससे ही उसकी कला ज्ञातृत्व का भी पता चलता है। चतुर कवि की लेखनी मानों उन्माद में निकली हुई वाणी को ही ताल मानकर थिरक उठती है। पर जब प्रेमी सर्वथा मौन हो जाए, सात्विक भावों का संचार भी रुक जाय, तब कवि किस आधार पर वर्णन करे?
कबिहिं अरथ आखर बल साँचा।
अनुहर ताल गतिहि नट नाचा।।
छाया और ताल का दृष्टान्त भी सकारण है। वर्णन में दो ही इन्द्रियाँ सहायक होती हैं ‘नेत्र’ और ‘कर्ण’ – देखी या सुनी हुई बात के आधार पर ही वर्णन किया जाता है। छाया नेत्र का और ताल कान का विषय है। पर यहाँ तो दोनों का ही अभाव है – शरीर की वाणी निःस्पन्द है।
“सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई” भी यहाँ नहीं कहा जा सकता है – क्योंकि ‘अहं’ न होने से सुख के अनुभविता का भी सर्वथा अभाव है। ‘मूकाऽस्वादनवत्’ या ‘गूँगे के गुड़’ का दृष्टान्त भी यहाँ असंगत है। क्योंकि गूँगे को उसके स्वाद का ज्ञान होता है, केवल वर्णन में असमर्थता है। पर यहाँ तो मन का अभा होने से रसास्वाद भी नहीं रहा। ‘निर्विकल्प समाधि’ से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि समस्त विकल्पों का नाश हो जाने पर भी ‘अंह’ का स्फुरण तो रहता ही है। पर यहाँ को अहंकार भी विस्मृत हो गया है। निस्पन्दता होते हुए भी जड़ता नहीं है, क्योंकि प्रेम तो रस-रूप हैं। आप कहेंगे फिर क्या है? पर इसे बतावे कौन? जिसका आश्रय लेकर हम कुछ कहते हैं, वे महाकवि असमर्थ हो रहे हैं। इस असमर्थता में वे अकेले नहीं। जो विश्व के रचयिता हैं, पालनकर्त्ता और संहारक हैं, सभी इस श्रेणी में आते हैं।
अगम सनेह भरत रघुबर को।
जहँ न जाइ मति बिधि हरि हर को।।
|
|||||