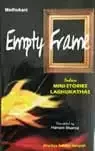|
ई-पुस्तकें >> तिरंगा हाउस तिरंगा हाउसमधुकांत
|
344 पाठक हैं |
||||||
समकालीन कहानी संग्रह
मैंने तो उठकर खिड़की ही बन्द कर ली और आदर्शवादी लीडर की तस्वीर के आगे दीवार से माथा पीट-पीटकर फूटती रही... बोल अब कैसे पालूं इन बच्चों को। अभी तो बहुत छोटे हैं इनके हाथ कैसे थमा दूं तुम्हारा झण्डा... पर उसने तो जिन्दा होते भी मेरे दर्द को न समझा अब क्या समझेगा।
गोद में उठाकर उसने पुचकारा--ठीक है बेटा मैं कल से कहीं नहीं जाऊंगी घर में ही रहूँगी...
‘पहले भी तो तुम कई बार कह चुकी हो। पिछली बार जब पिंकी के डरने की बात कही थी तब भी तो तुमने कहा था-फिर बोलो क्यों गई-’ नीरू की आंखें लाल हो गई थीं।
मैं कौन-सी अपनी खुशी से जाती हूँ बेटा-जाना पड़ता है-रोटियाँ तो चाहिए बेटा-नीरू को बाहों में लेने से फिर उसकी आंखें डबडबा आईं।
कितनी मुश्किल से नौकरी मिली थी। उन्हें मालूम हो जाता तो शायद इस नौकरी को भी स्वीकार न करते और शायद यह अच्छा ही होता।
पिताजी ने चोरी-छिपे इनकी नौकरी का प्रबंध किया था। मुझे देखकर वे बहुत दुखी होते थे। सम्पन्न और इज्जतदार घराने को देखकर ही तो उन्होंने मेरी शादी तय की थी। सब कुछ तो अच्छा देखा था लेकिन ये क्या मालूम था इनके रास्ते ही अलग हैं।
कभी भूल से भी अपने मन की कोई बात पिताजी के सामने कह देती तो उनकी आंखें भर आती थीं- क्या करें बेटी तेरे भाग्य में यही लिखा था।
यह बहन का पति कस्टम में था तो दूसरे का पति मिल का मालिक। मैं उन सबसे बड़ी होकर भी छोटी पड़ गई थी। मैं उनके साथ रहकर अपमानित होने लगी। मुझे उनसे मिलने पर संकोच होने लगा और धीरे-धीरे मैंने उनसे मिलना ही बंद कर दिया।
|
|||||