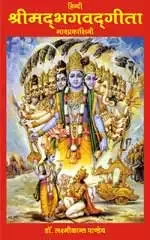|
ई-पुस्तकें >> श्रीमद्भगवद गीता - भावप्रकाशिनी श्रीमद्भगवद गीता - भावप्रकाशिनीडॉ. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय
|
411 पाठक हैं |
|||||||
गीता काव्य रूप में।
।। ॐ श्रीपरमात्मने नम:।।
अथ सोलहवाँ अध्याय : देवासुरसंपद विभाग योग
मोह हटा, चिन्ता गयी, प्रभु चरणों में नेह।।
श्री हरि पिछले प्रश्न का, करते हैं विस्तार।
दैवी, आसुर सम्पदा, का अब सुनिए सार।।
प्रभु बोले, मन की शुद्धि, ज्ञान में दृढ़ता हो, निर्भयता हो।
यदि दान, दमन, स्वाध्याय, यज्ञ, तप, निष्ठा और सरलता हो।।१।।
कोमलता, दया, शांति, लज्जा, सत्यता इन्हें धारण करना।
चंचलता, हिंसा, लोभ, क्रोध, निन्दा इन पाँचों को तजना।।२।।
हो तेज, क्षमा, धीरज, शुचिता, न मान द्रोह को करो ग्रहण।
हे भारत दैवी सम्पद है जिस जन के, उसके ये लक्षण।।३।।
सुनिए तुम हे कुन्ती नन्दन, आसुरी सम्पदा लक्षण अब।
अभिमान, दम्भ, अज्ञान, क्रोध पारुष्य-यही कहलाते सब।।४।।
दैवी सम्पद से मुक्ति मिले, आसुरी सम्पदा बन्धन दे।
तुम शोक कर रहे व्यर्थ पार्थ, तुममें तो दैवी सम्पद है।।५।।
दैवी-आसुरी भाव - ये दो, जिनमें सब प्राणी रहते हैं।
दैवी का भेद सुना तुमने, आसुरी रूप अब कहते हैं।।६।।
करणीय कौन, क्या अकरणीय, यह असुर जान ना पाते हैं।
आचार श्रेष्ठ, शुचि सत्य भाव, उनके मन में ना आते हैं।।७।।
वे कहते हैं जग को असत्य, ईश्वर ने नहीं बनाया है।
जग का कारण है काम वृत्ति, नर-नारी ने उपजाया है।।८।।
ऐसे मति मंद, न आत्म बोध, जग में रखते हैं यही दृष्टि।
ये अपने खोटे कर्मों से, यह लोक कर रहे नष्ट-भ्रष्ट।।९।।
पाखण्ड, मान, मद मत्त सदा रखते हैं अनुचित इच्छायें।
वे दुराग्रही हैं, मोहग्रस्त, दुष्कर्म करें या करवायें।।१०।।
वे अन्त समय तक रहते हैं, डूबे अनन्त चिन्ताओं में।
हैं सदा मानते ऐसे जन, सुख को विषयों के भावों में।।११।।
वे काम, क्रोध में लीन शताधिक आशा-फाँसी में जकड़े।
धन संचित हो, सुख-भोग मिले, चाहे करना दुष्कर्म पड़े।।१२।।
हैं कहते- इतना आज मिला कल और कहीं से आयेगा।
इतना धन मैंने जोड़ लिया, कुछ और अभी मिल जायेगा।।१३।।
वह शत्रु आज मैंने मारा, मारूँगा कल औरों को भी।
मैं ही ईश्वर, बलवान, सुखी, सब योग-भोग हैं मेरे ही।।१४।।
धन, जन सब मेरे पास बहुत, है कौन भला मेरे समान।
अज्ञान घेरता, वे कहते, सुख पाऊँगा कर यज्ञ-दान।।१५।।
फँसते हैं मोह जाल में जब, इस तरह भ्रमित मन हो जाता।
वह विषयासक्त काम लोलुप, फिर घोर नरक को है पाता।।१६।।
धन और मान, मद, जड़ता से, अपने को उत्तम कहते हैं।
वे नाम मात्र का दम्भ सहित, विधि हीन यज्ञ ही करते हैं।।१७।।
अभिमान, अहं, हठ, काम, क्रोध के भाव भरे उनके मन में।
सबके शरीर में नित्य व्याप्त, मुझ ईश्वर की निन्दा करते।।१८।।
मुझ प्रभु को नहीं मानते हैं, वे पापी, नीच, दुराचारी।
मेरे द्वारा वे होते हैं फिर, असुर योनि के अधिकारी।।१९।।
हे पार्थ, मूढ़ ये असुर योनि में जन्म ले रहे बार-बार।
मुझको पाने का प्रश्न नहीं, उनको नरकों के खुले द्वार।।२०।।
हैं क्रोध, कामना और लोभ, ये तीन नरक के दरवाजे।
जीवात्मा अगर बचाना हो तो इन तीनों को शीघ्र तजे।।२१।।
तम रूप तीन उन द्वारों को, जो त्याग सके कुन्तीनन्दन।
वह श्रेय मार्ग पर चल करके, फिर परमधाम में नित्य मगन।।२२।।
जो शास्त्र-बिहित कर्मों को तज, निज इच्छा से सब करता है।
सुख, सिद्धि, परम गति, इनमें से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है।।२३।।
अनुचित या उचित कर्म क्या है, शास्त्रों में इसका है विचार।
तुम शास्त्र-विहित सब कर्म करो, कर्त्तव्य-कर्म का यही सार।।२४।।
क्या दैवी क्या आसुरी, इसका है विस्तार।।
¤
|
|||||