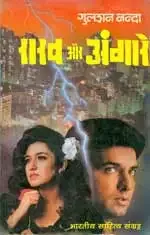|
ई-पुस्तकें >> राख और अंगारे राख और अंगारेगुलशन नन्दा
|
299 पाठक हैं |
|||||||
मेरी भी एक बेटी थी। उसे जवानी में एक व्यक्ति से प्रेम हो गया।
'पर वाबा तो अभी लौटे नहीं। देर हो गई। अब आते ही होंगे। बैठिए न!' रमेश कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला-’बावा नहीं हैं, तो क्या हुआ? तुम तो हो। परन्तु यह पीला शरीर, मलीन मुखाकृनि जैसे अरसे से बीमार ! यह सब क्या देख रहा हूं? ‘मैं तो अच्छी-भली हूं। आश्चर्य है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है।'
'चेहरा तो कुछ ऐसा ही बता रहा है..... अच्छा, कॉलेज कौन सा ज्वाइन कर रही हो?' रमेश ने टापिक बदल दी।
'घर का।'
'घर का? ’ मैं समझा नहीं।'
'मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, घर-गृहस्थी का कॉलेज अटैण्ड कर रही हूं।'
'क्यों? आखिर क्या बात है?'
'स्वास्थ्य इस काबिल नहीं कि आगे पढ़ना जारी रख सकूं।'
'अभी तो तुम कह रही थीं.... अच्छी-भली हूं!'
'मैंने झूठ कहा था.. बहुत दिनों से बीमार हूं।'
रमेश नेँ देखा उसकी आंखें सजल हो आई हैं। उसने अधिक पूछताछ करना उचित नहीं समझा। दोनों उधर ही बढ़ चले, जिधर से बाबा की आवाज उनके आने की सूचना दे रही थी। उसी रात जब शहर के घड़ियाल ने टन-टनकर दस बजाए तो रेखा के मन की धड़कन क्षण-भर के लिए रुक गई और दस वजने के साथ ही पहले से कहीं अधिक तेज हो गई।
उसने कांपती उंगलियों से रोशनदान में मोमबत्ती जलाई और थोड़ी जलने के पश्चात् ही उसे फौरन बुझा दिया। ठीक उसी समय निश्चित संकेत पर मोहन रोशनदान के पास झुका। ‘मोहन... तुम.. .आ गए।' रेखा उखड़ी हुई सांस को अधि- कार में लाते हुए बोली।
'क्या तुम्हें शंका थी?'
'नहीं, ऐसी कोई वात नहीं।'
'रेखा! मेरा मन और मस्तिष्क अब मेरे पास नहीं रहा। मैं बहुत घबराया हूं। जानती हो, परदेश में कितनी तकलीफ होती है जब तक कोई बोलने वाला, साथ देने वाला न हो।'
|
|||||