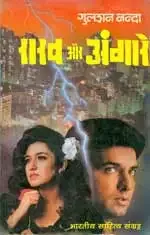|
ई-पुस्तकें >> राख और अंगारे राख और अंगारेगुलशन नन्दा
|
299 पाठक हैं |
|||||||
मेरी भी एक बेटी थी। उसे जवानी में एक व्यक्ति से प्रेम हो गया।
छह
सांझ का अंधेरा अभी फैला नहीं था कि मोहन, राणा साहब की कोठी की पिछली दीवार के साथ खड़ा मुंह से सीटी बजाने लगा। उसकी आवाज सुनकर रेखा भागी हुई आई। उलझी हुई और परेशान सूरत देखकर मोहन ने अधीर होकर पूछा- 'आज यह रूप क्या बना रखा है।'
'काम कर रही थी, आवाज सुनते ही भागी आई हूं।'
'तो क्या आज घूमने नहीं चलोगी...'
'आज न जा सकूंगी..'
'वह क्यों?’
'आज कोई अथिति आ रहे हैं.. बाबा उन्हें लेने स्टेशन गए हैं?'
‘कौन हैं वे?'
'बाबा के किसी मित्र का लड़का है.. सरकारी अफसर है और किसी काम से इस शहर में आ रहा है।'
'शीघ्र लौट जाएंगे शायद।'
'कह नहीं सकती... अभी मुझे कपड़े बदलने हैं, चाय का प्रबन्ध करना है, कल मिलूंगी..' कहकर रेखा वापस जाने लगी तो मोहन उसे रोकता हुआ बोला-’यह तो लेती जाओ।' उसने जेब से वह हार निकालकर उसकी हथेली पर दिया-’दो दिन आ न सका.. तुम सोचती रही होगी, कहीं सदा के लिए तो हार नहीं ले गया।'
'तुम्हारा है.. चाहो तो ले जाओ।'
'और मैं किसका हूं?'
'मैं क्या जानूं.... पुरुष जाति का क्या भरोसा..' रेखा मुस्कराई और आंचल छुड़ाकर भाग गई।
मोहन के संग न जाने का उसे दुःख तो था किन्तु इस दुःख ने उसके मन को यह कहकर सन्तोष दिया कि कभी-कभी किसी की प्रतीक्षा में तड़पना ही चाहिए।
जब वह दर्पण के सम्मुख कपड़े बदलकर केस संवार रही थी तो मुख पर एक अनोखी लालिमा देखकर उसका मन गुदगुदा उठा। यौवन ने सीमा का बांध तोड़ दिया और उसके हृदय में छिपी प्रसन्नता ने गुनगुनाहट का रूप धारण कर लिया। वह धीरे-धीरे मधुर स्वर में गुनगुनाने लगी।
|
|||||