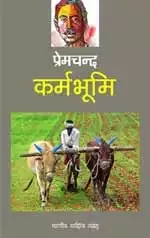|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
|||||||
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
‘वह तो तुम्हें मालूम ही है।’
‘मैं तो ऐसे आदमी से एक बार भी न बोलती।’
‘मैं भी कभी नहीं बोली।’
‘सच! बहुत बिगड़े होंगे। अच्छा, सारा वृत्तान्त कहो। सोहागरात को क्या हुआ? देखो, तुम्हें मेरी क़सम, एक शब्द भी झूठ न कहना।’
नैना माथा सिकोड़कर बोली–‘भाभी, तुम मुझे दिक़ करती हो; लेकर क़सम रखा दी। जाओ मैं कुछ नहीं बताती।’
‘अच्छा न बताओ भाई, कोई ज़बरदस्ती है!’
यह कहकर वह उठकर ऊपर चली। नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा–‘अब भाभी कहाँ जाती हो, क़सम तो रखा चुकी। बैठकर सुनती जाओ। आज तक मेरी और उसकी एक बार भी बोलचाल नहीं हुई।’
सुखदा ने चकित होकर कहा–‘अरे! सच कहो।’
नैना ने व्यथित हृदय से कहा–‘हाँ, बिलकुल सच है भाभी। जिस दिन मैं गयी उस दिन रात को गले में हार डाले, आँखें नशे से लाल, उन्मत्त की भाँति पहुँचे, जैसे कोई प्यादा असामी से महाजन के रुपये वसूल करने जाये। और मेरा घूँघट हटाते हुए बोले–मैं तुम्हारा घूँघट देखने नहीं आया हूँ, और न मुझे यह ढकोसला पसन्द है। आकर इस कुरसी पर बैठो। मैं उन दक़ियानूसी मर्दों में नहीं हूँ, जो गुड़ियों के खेल खेलते हैं। तुम्हें हँसकर मेरा स्वागत करना चाहिए था और तुम घूँघट निकाले बैठी हो, मानो तुम मेरा मुँह नहीं देखना चाहती। उनका हाथ पड़ते ही मेरी देह में जैसे किसी सर्प ने काट लिया। मैं सिर से पाँव तक सिहर उठी। इन्हें मेरी देह को स्पर्श करने का क्या अधिकार है? यह प्रश्न एक ज्वाला की भाँति मेरे मन में उठा। मेरी आँखों से आँसू गिरने लगे, वह सारे सोने के स्वप्न, जो मैं कई दिनों से देख रही थी, जैसे उड़ गये। इतने दिनों से जिस देवता की उपासना कर रही थी, क्या उसका यही रूप था! इसमें न देवत्व था, मनुष्यता थी, केवल मदांधता थी, अधिकार का गर्व था और हृदयहीन निर्लज्जता थी। मैं श्रद्धा के थाल में अपनी आत्मा का सारा अनुराग, सारा आनन्द, सारा प्रेम स्वामी के चरणों पर समर्पित करने को बैठी हुई थी। उनका यह रूप देखकर, जैसे थाल मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा और उसका धूप-दीप-नैवेद्य जैसे भूमि पर बिखर गया। मेरी चेतना का एक-एक रोम, जैसे इस अधिकार-गर्व से विद्रोह करने लगा। कहाँ था वह आत्मसमर्पण का भाव, जो मेरे अणु-अणु में व्याप्त हो रहा था। मेरे जी में आया, मैं भी कह दूँ कि तुम्हारे साथ मेरे विवाह का यह आशय नही हैं कि मैं तुम्हारी लौंडी हूँ। तुम मेरे स्वामी हो, तो मैं भी तुम्हारी स्वामिनी हूँ। प्रेम के शासन के सिवा मैं कोई दूसरा शासन स्वीकार नहीं कर सकती और न चाहती हूँ कि तुम स्वीकार करो; लेकिन जी ऐसा जल रहा था कि मैं इतना तिरस्कार भी न कर सकी। तुरन्त वहाँ से उठकर बरामदे में आ खड़ा हुई। वह कुछ देर कमरे में मेरी प्रतीक्षा करते रहे, फिर झल्लाकर उठे और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कठोर स्वर में बोली–मैं यह अपमान नहीं सह सकती।
|
|||||