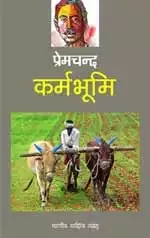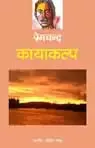|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
|||||||
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
शान्तिकुमार ने परास्त होकर कहा–‘मैं अपनी गलती को मानता हूँ सुखदा देवी। मैं तुम्हें न जानता था और इस भ्रम में था कि तुम्हारी ज्यादती है। मैं आज ही अमर को पत्र...’
सुखदा ने फिर बात काटी–‘नहीं, मैं आपसे यह प्रेरणा करने नहीं आयी हूँ और न यह चाहती हूँ कि आप उनसे मेरी ओर से दया की भिक्षा माँगे। यदि वह मुझसे दूर भागना चाहते हैं, तो मैं भी उनको बाँधकर नहीं रखना चाहती। पुरुष को जो आज़ादी मिली है, वह उसे मुबारक रहे; वह अपना तन-मन गली-गली बेचता फिरे। मैं अपने बन्धन में प्रसन्न हूँ और ईश्वर से यहीं विनती करती हूँ कि वह इस बन्धन में मुझे डाल रखे। मैं जलन या ईर्ष्या से विचलित हो जाऊँ उस दिन के पहले वह मेरा अन्त कर दे। मुझे आपसे मिलकर आज जो तृप्ति हुई, उसका प्रमाण यही है कि मैं आपसे वह बातें कह गयी, जो मैंने कभी अपनी माता से भी नहीं कहीं। बीबी आपका बखान करती थी, उससे ज़्यादा सज्जनता आप में पायी, मगर आपको मैं अकेला न रहने दूँगी। ईश्वर वह दिन लाये कि मैं इस घर में भाभी के दर्शन करूँ।’
जब दोनों रमणियाँ यहाँ से चलीं, तो डॉक्टर साहब लाठी टेकते हुए फाटक तक उन्हें पहुँचाने आये और फिर कमरे में आकर लेटे, तो ऐसा जान पड़ा कि उनका यौवन जाग उठा है। सुखदा के वेदना से भरे हुए शब्द उनके कानों में गूँज रहे थे और नैना मुन्ने को गोद में लिए जैसे उनके सम्मुख खड़ी थी।
७
उसी रात को शान्तिकुमार ने अमर के नाम खत लिखा। वह उन आदमियों में थे जिन्हें और सभी कामों के लिए समय मिलता है, ख़त लिखने के लिए नहीं मिलता। जितनी अधिक घनिष्ठता, उतनी ही बेफ़िक्री। उनकी मैत्री ख़तों से कहीं गहरी होती है। शान्तिकुमार को अमर के विषय में सलीम से सारी बातें मालूम होती रहती थीं। ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी? सकीना से उसे प्रेम हुआ इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने सुखदा पर रखी थी, पर आज सुखदा से मिलकर उन्होंने चित्र का दूसरा रुख भी देखा और सुखदा को उस ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया। खत जो लिखा, वह इतना लम्बा-चौड़ा कि एक ही पत्र में साल भर की कसर निकली गयी। अरमकान्त के जाने के बाद शहर में जो कुछ हुआ, उसकी पूरी-पूरी कैफियत बयान की और अपने भविष्य के सम्बन्ध में उसकी सलाह भी पूछी। अभी तक उन्होंने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया था। पर इस आन्दोलन के बाद से उन्हें अपने पद पर रहना कुछ जँचता न था। उनके मन में बार–बार शंका होती, जब तुम गरीबों के वकील बनते हो, तो तुम्हें क्या हक है कि तुम पाँच सौ रुपये माहवार सरकार से वसूल करो। अगर तुम गरीबों की तरह नहीं रह सकते तो ग़रीबों की वकालत करना छोड़ दो। जैसे और लोग आराम करते हैं, वैसे तुम भी मजे से खाते पीते रहो। लेकिन इस निर्द्वन्द्वता को उनकी आत्मा स्वीकार न करती थी। प्रश्न था, फिर गुज़र कैसे हो? किसी देहात में जाकर खेती करें, या क्या? यों रोटियाँ तो बिना काम किए भी चल सकती थीं, क्योंकि सेवाश्रम को क़ाफ़ी चन्दा मिलता था; लेकिन दान-वृत्ति की कल्पना ही से उनके आत्माभिमान को चोट लगती थी।
|
|||||