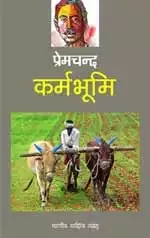|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
|||||||
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
छोटे-बड़े सभी सुखदा को पूज्य समझ रहे थे और उनकी यह भावना सुखदा में एक गर्वमय सेवा का भाव प्रदीप्त कर रही थी। कल उसने जो कुछ किया। वह एक प्रबल आवेश में किया। उसका फल क्या होगा, इसकी उसे ज़रा भी चिन्ता न थी। ऐसे अवसरों पर हानि-लाभ का विचार मन को दुर्बल बना देता है। आज यह जो कुछ कर रही थी, उसमें उसके मन का अनुराग था, सद्भाव था। उसे अब अपनी शक्ति और क्षमता का ज्ञान हो जाता है, वह नशा हो गया है; जो अपनी सुध-बुध भूलकर सेवारत हो जाता है, जैसे अपनी आत्मा को पा गयी है।
जब सुखदा नगर की नेत्री है। नगर में जाति–हित के लिए जो काम होता है, सुखदा के हाथों उसका श्रीगणेश होता है। कोई उत्सव हो, कोई परमार्थ का काम हो, कोई राष्ट्र का आन्दोलन हो, सुखदा का उसमें प्रमुख भाग होता है। उसका जी चाहे या न चाहे, भक्त लोग उसे खींच ले जाते हैं। उसकी उपस्थिति किसी जलसे की सफलता की कुँजी है। आश्चर्य यह है कि बोलने भी लगी है और उसके भाषण में चाहे भाषा–चातुर्य न हो, पर सच्चे उद्गार अवश्य होते हैं। शहर में कई सार्वजनिक संस्थाएँ हैं, कुछ सामाजिक, कुछ राजनैतिक, कुछ धार्मिक। सभी निर्जीव–सी पड़ी थीं। सुखदा के आते ही उनमें स्फूर्ति–सी आ गयी है। मादक–वस्तु बहिष्कार–सभा बरसों से बेजान पड़ी थी। न कुछ प्रचार होता था, न कोई संगठन। उसका मन्त्री एक दिन सुखदा को खींच ले गया। दूसरे ही दिन उस सभा की एक भजन–मण्डली बन गयी। कई उपदेशक निकल आये, कई महिलाएँ घर-घर प्रचार करने के लिए तैयार हो गयीं और मुहल्ले-मुहल्ले पंचायतें बनने लगीं। एक नए जीवन की सृष्टि हो गयी।
अब सुखदा को ग़रीबों की दुर्दशा का यथार्थ रूप देखने के अवसर मिलने लगे। अब तक इस विषय में जो कुछ ज्ञात था, वह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित था। आँखों से देखकर उसे ज्ञात हुआ, देखने और सुनने में बड़ा अन्तर है। शहर की उन अँधेरी, तंग गलियों में, जहाँ वायु और प्रकाश का कभी गुज़र ही न होता था, जहाँ की ज़मीन ही नहीं, दीवारें भी सीली रहती थीं, जहाँ दुर्गन्ध के मारे नाक फटती थी, भारत की कमाऊ सन्तान रोग और दरिद्रता के पैरों तले दबी हुई अपने क्षीण जीवन को मृत्यु के हाथों से छीनने में प्राण दे रही थी। उसे अब मालूम हुआ कि अमरकान्त को धन और विलास से जो विरोध था, यह कितना यथार्थ था। उसे खुद अब उस मकान में रहते, अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनते, अच्छे-अच्छे पदार्थ खाते ग्लानि होती। नौकरों से काम लेना उसने छोड़ दिया। अपनी धोती ख़ुद छाँटती थी, घर में झाडू खुद लगाती। वह जो आठ बजे सोकर उठती थी, अब मुँह-अँधेरे उठती और घर के काम-काज में लग जाती। नैना तो अब उसकी पूजा-सी करती थी। लालाजी अपने घर की यह दशा देख-देख कुढ़ते थे, पर करते क्या? सुखदा के यहाँ तो अब नित्य दरबार-सा लगा रहता था। बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े विद्वान आते रहते थे। इसलिए वह अब बहू से कुछ दबते थे। गृहस्थी के जंजाल से अब उनका मन ऊबने लगा था। जिस घर में उनसे किसी को सहानुभूति न हो, उस घर में कैसे अनुराग होगा? जहाँ अपने विचारों का राज हो, वहीं अपना घर है। जो अपने विचारों को मानते हों, वही अपने सगे हैं। यह घर अब उनके लिए सराय–मात्र था। सुखदा या नैना, दोनों ही से कुछ कहते उन्हें डर लगता था।
|
|||||