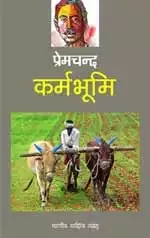|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
|||||||
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
तीसरे दिन लालाजी उठ बैठे। सुखदा दिन-भर तो उनके पास रही। संध्या समय उनसे बिदा माँगी। लालाजी स्नेह-भरी आँखों से देखकर बोले–‘मैं जानता कि तुम मेरी तीमारदारी ही के लिए आयी हो तो दस-पाँच दिन और पड़ा रहता बहू। मैंने तो जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कुछ अनुचित हुआ हो तो उसे क्षमा करो।’
सुखदा का जी हुआ मान त्याग दे, पर इतना कष्ट उठाने के बाद जब अपनी गृहस्थी कुछ-कुछ जम चली थी, यहाँ आना कुछ अच्छा न लगता था। फिर, वहाँ वह स्वामिनी थी। घर का संचालन उसके अधीन था। वहाँ की एक-एक वस्तु में अपनापन भरा हुआ था। एक-एक तृण में उसका स्वाभिमान झलक रहा था। एक-एक वस्तु में उसका अनुराग अंतित था। एक-एक वस्तु पर उसकी आत्मा की छाप थी, मानो उसकी आत्मा ही प्रत्यक्ष हो गयी हो। यहाँ की कोई वस्तु उसके अभिमान की वस्तु न थी। उसकी स्वामिनी कल्पना सब कुछ होने पर भी तुष्टि का आनन्द न पाती थी। पर लालाजी को समझाने के लिए किसी युक्ति की ज़रूरत थी। बोली–‘यह आप क्या कहते है दादा, हम लोग आपके बालक हैं। आप जो कुछ उपदेश या ताड़ना देंगे, वह हमारे ही भले के लिए देंगे। मेरा जी तो जाने को नहीं चाहता, लेकिन अकेले मेरे चले आने से क्या होगा? मुझे खुद शर्म आती है कि दुनिया क्या कह रही होगी। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा, सबको घसीट लाऊँगी। जब तक आदमी कुछ दिन ठोकरें नहीं खा लेता, उसकी आँखें नहीं खुलतीं। मैं एक बार रोज़ आकर आपका भोजन बना जाया करूँगी। कभी बीबी चली आयेंगी, कभी मैं चली आऊँगी।’
उस दिन से सुखदा का यही नियम हो गया। वह सवेरे यहाँ चली आती और लालाजी को भोजन कराके लौट जाती। फिर खुद भोजन करके बालिका विद्यालय चली जाती। तीसरे पहर जब अमरकान्त खादी बेचने चला जाता, तो वह नैना को लेकर फिर आ जाती और दो-तीन घण्टे रहकर चली जाती। कभी-कभी खुद रेणुका के पास जाती, तो नैना को यहाँ भेज देती। उसके स्वाभिमान में कोमलता थी, अगर कुछ जलन थी तो वह कब की शीतल हो चुकी थी। वृद्ध पिता को कोई कष्ट हो, यह उससे न देखा जाता था।
इन दिनों उसे जो बात सबसे ज़्यादा खटकती थी, वह अमरकान्त का सिर पर खादी लादकर चलना था। वह कई बार इस विषय पर उनसे झगड़ा कर चुकी थी, पर उसके कहने से वह और जिद पकड़ लेता था। इसलिए उसने कहना-सुनना छोड़ दिया था, पर एक दिन घर जाते समय उसने अमरकान्त को खादी की गट्ठर लिए देख लिया। उस मुहल्ले की एक महिला भी उसके साथ थी। सुखदा मानो धरती में गड़ गयी।
अमर ज्यों ही घर आया, उसने यही विषय छेड़ दिया– ‘ मालूम तो हो गया कि तुम बड़े सत्यवादी हो। दूसरों के लिए भी कुछ रहने दोगे, या सब तुम्हीं ले लोगे। अब तो संसार में परिश्रम का महत्व सिद्ध हो गया। अब तो बकचा लादना छोड़ो। तुम्हें शर्म न आती हो, लेकिन तुम्हारी इज़्ज़त के साथ मेरी इज़्ज़त भी तो बँधी हुई है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम यों मुझे अपमानित करते फिरो।’
अमर तो कमर कसे तैयार था ही। बोला– ‘यह तो मैं जानता हूँ कि मेरा अधिकार कहीं कुछ नहीं है, लेकिन क्या पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे अधिकारों की भी कहीं सीमा है, या वह असीम हैं?’
|
|||||