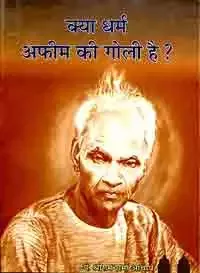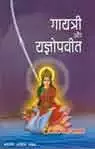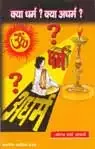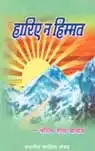|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> क्या धर्म अफीम की गोली है ? क्या धर्म अफीम की गोली है ?श्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
क्या धर्म अफीम की गोली है ?
धर्म का उद्देश्य-व्यक्तित्व का परिष्कार
मनुष्य जीवन में सुख-शांति की उपलब्धि के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक एवं उपयोगी तत्त्व है, उसे लोग धर्म के नाम से जानते हैं। सदाचार एवं कर्तव्यपालन की प्रेरणा, ‘जिओ और जीने दो' का संदेश धर्म की आत्मा के पर्याय हैं। धर्म का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की प्रकृति, गुण, कर्म एवं स्वभाव है। कवींद्र-रवींद्र ने इसकी शाश्वत अनुभूति कर अभिव्यक्त किया है कि-'धर्म अंतः प्रकृति है, वही समस्त वस्तुओं का ध्रुव सत्य है। धर्म ही चरम लक्ष्य है, जो हमारे अंदर कार्य करता है। अतएव यह कहा जा सकता है। कि जिस पथ पर चलकर अपने अभीष्ट की उपलब्धि संभव हो उसे ही धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म का उद्देश्य मानव जीवन को पथभ्रष्ट होने से बचाना है। इसलिए धर्म को जीवन का प्राण ही कहना चाहिए। धर्म का अभाव मनुष्य को पशु से भी गया बीता बना देता है, बल्कि अधार्मिक व्यक्ति को पशु कहना, पशु का अपमान करना है; क्योंकि पशु का भी तो अपना धर्म होता है, जिसे पाशविक धर्म कहा जाता है, किंतु मनुष्य यदि मानवीय धर्म का पालन नहीं करता अथवा अपने धर्म-कर्तव्य का परित्याग कर देता है तो उसे हेय दृष्टि से ही देखा जाता है। समादरणीय व्यक्ति अथवा सम्मान के अधिकारी व्यक्ति वही हैं, जो धर्म-कर्तव्य से विमुख नहीं हैं। शास्त्रोक्ति है-जो धर्म का पालन करता है उसकी धर्म ही रक्षा करता है, पर जो उसे नष्ट कर देता है, उसका नष्ट किया हुआ धर्म ही नाश कर देता है।'' इस सिद्धांत में दो मत नहीं हो सकते। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है। वह श्री समृद्धियों एवं विभूतियों से वंचित हो जाता है। दु:ख, दारिद्र्य एवं दुर्भाग्य धर्म विमुख के संगी-सहचर बन जाते हैं। नारकीय यंत्रणा की अग्नि में वे सतत जलते एवं येन केन प्रकारेण' जिंदगी के दिन पूरे करते रहते हैं।
धर्म का निवास वहाँ होता है, जहाँ सदाचार एवं कर्तव्यपालन का समादर किया जाता है, इसलिए सदाचार एवं कर्तव्यपालन को धर्म के प्रधान प्रतीक कहना अतिशयोक्ति न होगी। धर्म की भव्य संरचना हेतु मानवोचित आदर्शों एवं उत्तरदायित्वों को सुचारु रूप से संपादित करने की महती आवश्यकता होती है।
आस्तिकता, उपासना, शास्त्र-श्रवण, पूजा-पाठ, कथा-कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, व्रत, उपवास, नियम, संयम, तीर्थयात्रा, पर्व एवं संस्कार आदि समस्त प्रक्रियाएँ धर्म भावना को परिपक्व करने के उद्देश्य से विनिर्मित हुई हैं, ताकि मनुष्य उपने जीवन के महारिपुओंवासना एवं तृष्णा, लोभ, मोह तथा आकर्षणों एवं प्रलोभनों से मुक्त होकर अपने कर्तव्य-पथ पर अबाध गति से अग्रसर हो सके। साथ ही यदि वह इन धर्म के साधनों को साध्य मान बैठने की गलती कर लेता है, तो उसके समस्त धार्मिक कर्मकांड, जो धर्म के कलेवर मात्र हैं-धर्म के प्राण से कोसों दूर ले जाते हैं। कलेवर अपने आप में पूर्ण नहीं है, कलेवर का महत्त्व प्राण से है और प्राण का कलेवर से। सुस्पष्ट है कि दोनों एकदूसरे के परस्पर पूरक हैं। साधन और साध्य का एकदूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। साधन को मात्र साधन ही समझा जाए, साधनोचित महत्त्व ही प्रदान किया जाए।
ईश्वर की सत्ता सर्वव्यापक, निष्पक्ष, न्यायकारी तथा सुनिश्चित कर्मफल प्रदान करने वाली, सृष्टि की नियामक एवं नियंत्रक है। उसकी अनुभूति अपने इर्द-गिर्द करना ही इस चिंतन, मनन, ध्यान एवं भजन का उद्देश्य है। पाप कर्मों के दंड से भयभीत रहें और मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर उसके कठोर प्रतिफल का ध्यान रखते हुए अनीति एवं अन्याय न करें। उपासक अथवा धर्मभीरु के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता है कि उसकी ईश्वरीय न्याय और कर्मफल की सुनिश्चितता में आस्था हो, अन्यथा उसकी समस्त भक्ति भावना निरर्थक ही सिद्ध होगी। धर्म कर्मों से जो स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, देवकृपा, सुख-शांति, समृद्धि, साक्षात्कार आदि लाभ होते हैं, वह केवल उन्हीं के लिए संभव हैं, जिन्होंने धर्म के मर्म एवं उसके वास्तविक स्वरूप को भली भाँति समझ लिया है, साथ ही उसे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप प्रदान कर अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र को उज्ज्वल बनाया है। समस्त विभूतियाँ भले ही वे लौकिक या लोकोत्तर हों, सदाचार द्वारा ही सुलभ होती हैं। यही कारण है कि धर्म को सदाचार का प्रेरणोत्पादक तत्त्व माना गया है। यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि धर्म विभूति एवं सुख-शांति का जनक है। सदाचार के प्रति अनास्थावान होकर कोई व्यक्ति मात्र बाह्य क्रियाकलापों से सुख-शांति का स्वप्न देखे तो उसे मात्र दिवास्वप्न की संज्ञा दी जाएगी। सदाचार में आस्था, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और मर्यादाओं का विधिवत् पालन ही धर्म की आधारशिला है। सदाचार को धर्म का मूल कहा जा सकता है। मूलोच्छेदन के बाद किसी वृक्ष में लगने वाले फूलों और फलों की आशा करना निरर्थक है।
मध्यकाल के अंधकार युग में यह भ्रांति फैली कि अमुक धार्मिक कर्मकांड करने मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज भी लोग उसी लकीर के फकीर बने हुए हैं। इस प्रकार की निराधार मान्यताएँ फैलाने में तत्कालीन पुरोहित वर्ग का अपना वर्चस्व बनाए रखने वाला स्वार्थ प्रधान था। जिसके माध्यम से जीविकोपार्जन हेतु दान दक्षिणा और पूजा-प्रतिष्ठा यजमानों से सहज रूप में प्राप्त हो जाती थी। जो लाभ सदाचार की कष्टमय कसौटी पर खरा उतरकर उपलब्ध होता है, उसे मात्र बाह्य प्रक्रियाओं से पुण्य-लाभ के प्रलोभन देकर सस्ता बना दिया।
मनुष्य के उत्थान एवं पतन का कारण उसकी भावना होती है, अतएव भावना स्तर को मानवीय आदर्शों के अनुरूप बनाए रहने में धर्म के समस्त क्रियाकलाप सहायक होते हैं। इसी कारण भावना को प्रधानता मिली हुई है। आदर्श जीवन एवं उत्कृष्ट विचार ही सजीव धर्म की शाश्वत साधना है।
प्राचीनकाल में संत, ब्राह्मण और साधु अपरिग्रहशील जीवनयापन करते थे, फलस्वरूप लोकसेवा का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर उठाने में समर्थ होते थे। उनकी त्याग भावना उन्हें लोकश्रद्धा का पात्र बना देती थी। दान-दक्षिणा से प्राप्त धन को वे अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यय न करके लोक-कल्याण के कार्य में लगा देते थे। जिस प्रकार आजकल लोकनायकों को रक्षा कोष आदि के लिए दी जाने वाली थैलियाँ उनकी व्यक्तिगत निधि नहीं मानी जातीं। प्राप्तकर्ता उसे राष्ट्रीय हित के कार्यों में व्यय हेतु समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार प्राचीनकाल में धर्मात्मा, लोकसेवी साधु, ब्राह्मण उदर पूर्ति के उपरांत शेष राशि को सद्ज्ञान, सद्भाव, सदाचार एवं सत्प्रवृतियों के पुण्यप्रसार में लगा देते थे। मंदिर जन-जागरण के केंद्र थे, किंतु आज मठों एवं मंदिर में प्रचुर संपत्ति विद्यमान होने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, जनमानस का परिष्कार एवं उत्कर्ष, सांस्कृतिक लोक-शिक्षण में यदि यह धर्म निधि सुलभ हो सकी होती, तो आज हमारी स्थिति कुछ और होती, तब आज का वातावरण ही भिन्न प्रकार का परिलक्षित होता।
न केवल भारत अपितु अन्य देशों में भी धर्म के विषय में जितना मतभेद देखने में आता है, उतना और किसी विषय में शायद ही मिल सके। यह भेद अज्ञानियों में ही नहीं, समझदार और उन्नतिशील लोगों में भी देखने में आता है। हिंदू गौ का एक रोम भूल से भी दूध के साथ पेट में चले जाने पर घोर पाप समझते हैं, मुसलमान उसी गाय को खुदा के नाम पर काटकर खा जाने पर बड़ा पुण्य बतलाते हैं। ईसाई बिना पाप-पुण्य के झगड़े में पड़े, नित्य ही उसके मांस को एक साधारण आहार की तरह ग्रहण करते हैं। यहूदी भगवान की उपासना करते समय मुँह के बल लेट जाते है, कैथोलिक ईसाई घुटनों के बल झुकते हैं, प्रोटेस्टेंट ईसाई कुरसी पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, मुसलमानों को नमाज में कई बार उठना-बैठना पड़ता है और हिंदुओं की सर्वोच्च प्रार्थना वह है, जिसमें साधक ध्यानमग्न होकर अचल हो जाए। यदि यह कहा जाए कि इन सबमें एक ही उपासना विधि ठीक है, दूसरी सब निकम्मी है तो भी काम नहीं चलता। अन्य धर्मों में भी अनेक व्यक्ति बड़े संत, त्यागी महात्मा हो गए हैं। धार्मिक-क्षेत्र के इसी घोर वैषम्य को देखकर 'ऑरिजिन एण्ड डेवलपपेमेंट ऑफ रिलिजस बिलीफ' (धार्मिक विश्वास की उत्पत्ति और विकास) नामक ग्रंथ के लेखक एस० बैरिंग गाल्ड ने लिखा है-
संसार में समस्त प्राचीन युगों से कई ऐसे धार्मिक विश्वास पाए गए हैं, जो एकदूसरे से सर्वथा विपरीत हैं और जिनकी रस्मों तथा सिद्धांतों में जमीन-आसमान का अंतर है। एक प्रदेश में मंदिर का पुजारी देवमूर्ति को मानव रक्त से लिप्त करता है और दूसरे ही दिन अन्य धर्म का अनुयायी वहाँ आकर उसे तोड़कर गंदगी में फेंक देता है। जिनको एक धर्म वाले भगवान मानते, उन्हीं को दूसरे धर्मानुयायी शैतान कहते हैं। एक धर्म में धर्म-याजक भगवान की पूजा की उद्देश्य से बच्चों को अग्नि में डाल देता है। और दूसरे धर्म वाला अनाथालय स्थापित करके उनकी रक्षा करता है। और इसी को ईश्वर-पूजा समझता है। एक धर्म वालों की देवमूर्ति सौंदर्य का आदर्श होती है और दूसरे की घोर वीभत्स एवं कुरूप। इंगलैण्ड में प्रसव के समय माता को एकांत स्थान में रहना पड़ता है, पर अफ्रीका की 'बास्क' जाति में संतान होने पर पिता को कंबलों से ढंककर अलग रखा जाता है और लपसी' खिलाई जाती है। अधिकांश देशों में माता-पिता की सेवा-सुश्रूषा करके उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति प्रकट की जाती है, पर कहीं पर श्रद्धा की भावना से ही उनको कुल्हाड़े से काट दिया जाता है। अपनी माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से फिजी का मूल निवासी उसके मांस को खा लेता है, जबकि एक यूरोपियन इसी उद्देश्य से उसकी एक सुंदर समाधि बनवाता है।''
विभिन्न धर्मों और मतों के धार्मिक, विश्वासों में अत्यधिक अंतर होने का यह बहुत ही अल्प विवरण है। फ्रेजर नामक विद्वान ने इस विषय पर गोल्डिन वो' नाम की प्रसिद्ध पुस्तक सोलह बड़े-बड़े खंडों में लिखी है, पर उसमें भी पृथ्वी तल पर बसने वाले अनगिनत, जातियों, संप्रदायों में पाई जाने वाली असंख्यों धार्मिक प्रथाओं और रस्मों का पूरा वर्णन नहीं किया जा सका है। ये सिद्धांत, विश्वास और रस्में हर तरह के हैं। इनमें निरर्थक, उपहासास्पद, भयंकर, कठोर, अश्लील प्रथाएँ भी हैं और श्रेष्ठ, भक्तिपूर्ण मानवतायुक्त, विवेकयुक्त और दार्शनिकता के अनुकूल विधान भी पाए जाते हैं।
इन धार्मिक प्रथाओं ने धीरे-धीरे कैसे हानिकारक और निकम्मे अंधविश्वासों का रूप धारण कर लिया है, इस पर विचार करने से चकित हो जाना पड़ता है। डॉ० लैंग ने एक आस्ट्रेलिया के मूल निवासी से उसके किसी मृत सम्बंधी का नाम पूछा। उसने मृतक के बाप का नाम, भाई का नाम, उसकी शक्ल-सूरत, चाल-ढाल, उसके साथियों के नाम आदि सब कुछ बता दिया, पर मृतक का नाम किसी प्रकार उसकी जबान से नहीं निकल सका। इस संबंध में अन्य लोगों से, पूछने पर पता लगा कि ये लोग मृतक का नाम इसलिए नहीं लेते कि ऐसा करने से उसका भूत इनके पास चला आएगा। भारत के गाँवों में जब कोई उल्लू बोल रहा हो तो उसके सामने किसी का नाम नहीं लिया जाता; क्योंकि लोगों का भय होता है कि उस नाम को सुनकर उल्लू उसका उच्चारण करने लगेगा और इससे वह व्यक्ति बहुत शीघ्र मर जाएगा।
हमारे देश में अनेक लोग अब भी स्त्रियों के परदा त्याग करने के बहुत विरुद्ध हैं और जो लड़की विवाह-शादी के मामले में अपनी सम्मति प्रकट करती है या अपनी इच्छानुसार विवाह के लिए जोर देती है तो उसे निर्लज्ज, कुलाँगारिणी आदि कहकर पुकारा जाता है। पर उत्तरी अफ्रीका के 'टौर्गस' प्रदेश में पुरुष बुरका डालकर रहते हैं। और स्त्रियाँ खुले मुँह फिरती हैं। वहाँ पर स्त्रियाँ ही विवाह के लिए पुरुष ढूंढ़ती हैं, प्रेम प्रदर्शित करती हैं और उसे विवाह करके लाती हैं।‘बिली' नाम की जाति में कुमारी कन्याओं को मंदिर के पुजारियों को दान कर दिया जाता है, जिनका वे उपभोग करते हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के मंदिरों में 'देवदासी' की प्रथा का भी लगभग ऐसा ही रूप है। काँगों में कुमारी कन्याओं का मनुष्याकार देवमूर्ति के साथ संपर्क कराया जाता है। ‘बुदा' नामक जाति के समस्त फिरके वाले गाँव की चौपाल में इकट्ठे होते हैं और उनका धर्मगुरु वहाँ चारों हाथ-पैर से चलता हुआ सियार की बोली बोलता है और अन्य सब लोग उसकी नकल करते हैं। मलाया में जिस लड़की को कोई प्यार करता है, वह उसके पदचिह्न के स्थान की धूल को उठा लाता है और उसे आग पर गरम करता है। उसका विश्वास होता है। कि ऐसा करने से उसकी प्रेमिका का हृदय पिघलेगा और वह उसकी पत्नी बनने को राजी हो जाएगी। संसार के कुछ भागों में ऐसी भी प्रथाएँ हैं, जिनमें फिरके के 'भगवान' का ही बलिदान कर दिया जाता है। कुछ फिरके वाले, यदि उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो अपने राजा तथा पुरोहित को ही मार देते हैं। इस प्रकार संसार भर में धर्म के नाम पर अनगिनत अंधविश्वास, हानिकारक और घृणित प्रथाएँ प्रचलित हैं और मानवता के उद्धार के लिए उनका मिटाया जाना आवश्यक है।
किसी मजहब या संप्रदाय में तो भगवान के पुत्र, पौत्र, पत्नी आदि की कल्पना को भी सत्य माना जाता है और दूसरी जाति (रूस, चीन आदि) में ईश्वर की गणना केवल एक 'विश्व नियम के रूप में की जाती है। एक धर्म वाला संगीत और वाद्य को ईश प्रार्थना का आवश्यक अंग मानता है और दूसरा धर्म इसे महापाप बतलाता है। बिहार के सखी संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर-भक्ति के लिए स्त्री की तरह रहना, यहाँ तक कि मासिक धर्म की भी नकल करना बहुत बड़ी साधना समझते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि जिस प्रकार स्त्री अपने पति से प्रेम करके उसमें तन्मय हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर में भी तन्मयता प्राप्त कर ली जाए।
इसी प्रकार देश में ऐसे तांत्रिक संप्रदाय भी पाए जाते हैं-जिनमें मद्यपान, मांस भक्षण, पशु-वध और मैथुन भी धर्म का एक अंग माना जाता है। दूसरी ओर जैन धर्म जैसे मत हैं जिनमें ब्रह्मचर्यपालन के लिए अठारह हजार प्रकार की अश्लीलता से बचने का उपदेश दिया गया है। अगर एक संप्रदाय किसी मानव शरीरधारी को 'भगवान' मानता है (जैसे-बल्लभ संप्रदाय में) तो दूसरा संप्रदाय (जैसे-वेदांती) ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार करता है।
सभी मजहबों या धर्मों के भीतर इतने संप्रदाय या फिरके पाए जाते हैं कि इनको गिनना भी कठिन है। लोगों को प्रायः रहस्यवाद में बड़ा आकर्षण जान पड़ता है। इसलिए सदा नए-नए गुरु उत्पन्न होते रहते हैं, जो साधना या उपासना की एक भिन्न विधि निकालकर एक पृथक संप्रदाय स्थापित कर देते हैं, उनका एक नवीन मंदिर बन जाता है। इस प्रकार के हजारों नए-नए मत और धार्मिक फिरके जंगली कहे जाने वाले प्रदेशों में ही नहीं, वरन् यूरोप, अमेरिका, एशिया के सभ्य और सुसंस्कत देशों में भी पाए जाते हैं। ऐसी कोई पजापद्धति नहीं है, जिसका आविष्कार और प्रचलन संसार में कहीं-न-कहीं हो चुका हो। आप कैसी भी विचित्र अथवा असंगत उपासना पद्धति की कल्पना क्यों न करें, वह इस विस्तृत पृथ्वी पर किसी जगह अवश्य ही क्रिया रूप में होती मिल जाएगी।
हमारा आशय यह नहीं है कि संसार में विभिन्न धर्मों का होना कोई अस्वाभाविक बात है या मनुष्य की गलती है। जिस प्रकार जल, वायु और देश के भेद से मनुष्यों की भाषा और आकृति में अंतर पड़ जाता है, उसी प्रकार परिस्थितियों की भिन्नता के कारण विभिन्न जातियों की संस्कृति में भी अंतर हो सकता है।
विभिन्न धर्मों की उपासनात्मक-प्रक्रिया, विधि-विधानों में काफी भिन्नता होते हुए भी एक तथ्य प्रत्येक धर्म के मूल में काम करता है-वह है व्यक्तित्व का परिष्कार। ऐसा कोई भी धर्म नहीं, जो सदाचरण पर जोर न देता हो। यही वह शाश्वत आधार है, जिसके द्वारा मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हैस्वरूप की भिन्नता होते हुए भी लक्ष्य की एकरूपता प्रत्येक धर्म में देखने में आती है। देश-काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप यह भिन्नता उचित है और उपयोगी भी। धर्म का एक ही उद्देश्य है-मानवीय अंत:करण में सन्निहित श्रेष्ठता को विकसित करना। धर्म परस्पर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, उदारता, संयम एवं सहयोग को बढ़ाता है। धर्म का वास्तविक स्वरूप वस्तुतः सदाचरण एवं कर्तव्यनिष्ठा में ही निहित है।
|
|||||