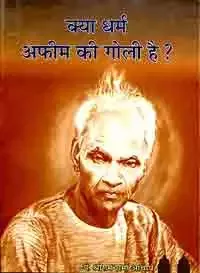|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> क्या धर्म अफीम की गोली है ? क्या धर्म अफीम की गोली है ?श्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
क्या धर्म अफीम की गोली है ?
विज्ञान भावनाशील बने और धर्म तथ्यानुयायी
मोटे तौर से प्रतीत होता है कि विज्ञान और अध्यात्म के आधारभूत सिद्धांतों में मौलिक अंतर है। इसलिए उनका समन्वय कदाचित् कभी भी संभव न हो सकेगा। अंतर को देखकर प्रस्तुत निष्कर्ष पर पहुँचने वाले मनीषियों का कहना यह है कि विज्ञान आग्रही नहीं है, वह तथ्यों को खुले मस्तिष्क से तलाश करता है। पूर्वाग्रहों से मुक्त रहता है और जब जो प्रामाणिक आधार मिलते हैं, उनके सहारे सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इसके विपरीत अध्यात्म में पूर्वाग्रहों की ही भरमार है। तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है। शास्त्र अथवा आप्तपुरुष ही सब कुछ हैं, उन्हीं की खींची रेखाओं की परिधि में घूमने के लिए धार्मिक अथवा अध्यात्मवादी को सीमित रहना पड़ता है। तर्को के झरोखे में झाँकने वालों की धार्मिकता को पतिव्रत को तोड़ने वाला घोषित कर दिया जाता है। ऐसी दशा में तथ्यों का निर्धारण करने को जब तक दोनों की स्थिति एक न हो, तब तक समन्वय कैसे संभव होगा? या तो विज्ञान अपने तथ्यों को प्रमाणिकता देने वाली प्रवृत्ति छोड़े अथवा धर्म को परंपरा आग्रह अपनाए रहने से विरत किया जाए, तभी वह स्थिति बनेगी जिसके आधार पर दोनों को साथ चलने अथवा सहयोग करके सत्य की शोध में समन्वित मार्ग अपनाने की बात बन सके।
कथन को सच मानने का मन तभी करता है, जबकि दोनों की मूलप्रकृति को समझने में भ्रम बना रहे। यह अड़चन उथले चिंतन से सही मालूम पड़ती है और उस समय भी ठीक लगती है जब धर्मपक्ष के विकृत रूप को ही उसका आधारभूत सिद्धांत मान लिया जाए। गहराई में उतरने पर धर्म और विज्ञान दोनों ही ऐसे तथ्यों पर आधारित दीखते हैं, जिन पर अविश्वास करने या मिलजुलकर साथ-साथ न चल सकने की आशंका करने का कोई कारण नहीं हो।
विकृतियाँ तो न्याय और कानून के क्षेत्र में भी बनी रहती हैं। इससे उनकी उपयोगिता या आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्पादन और व्यवसाय में भी आए दिन बदमाशियाँ चलती हैं, इसी कारण उन कार्यों को बंद तो नहीं कर दिया जाता। धार्मिक क्षेत्र में निहित स्वार्थों को घुस पड़ने और अवांछनीय प्रथा-परंपरा चला देने का अवसर मिल जाता है, जब कि उस क्षेत्र के अनुयायी तर्क और तथ्यों को जानने की आवश्यकता नहीं समझते। यदि वे धर्माध्यक्षों के उद्देश्य और प्रतिपादनों के फलितार्थ पर विवेकपूर्वक विचार करना सीखें तो फिर धर्म-क्षेत्र की उपयोगिता भी विज्ञान क्षेत्र की तरह ही अक्षुण्ण बनी रह सकती है। धर्म की मूलप्रवृति अंधविश्वासी या दुराग्रही नहीं है। जिस श्रद्धातत्त्व के आधार पर अंधेरगर्दी फैलती है, उसका भी आधार श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। श्रेष्ठता के प्रति प्यार को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा की अवधारणा जहाँ भी करनी हो, वहाँ सर्वप्रथम श्रेष्ठता है या नहीं, इसको कसौटी पर कसना होता है। यह परख जाग्रत रखी जा सके तो श्रद्धा के शोषण की संभावना न रहेगी और धर्म को अवैधानिक, तर्क विरोधी अथवा अप्रामाणिक कहे जाने का अवसर न आने पाएगा।
धर्म भी एक विज्ञान है। चेतना को अनुशासित रखना और उसे सत्प्रयोजनों में नियोजित करना उसका उद्देश्य है। चेतना की सामर्थ्य प्रकृति-क्षेत्र में भरी पदार्थ-संपदा एवं शक्ति धाराओं से किसी भी प्रकार कम नहीं है। प्रकृति संपदाओं को खोज निकालने और उसका सदुपयोग कर सकने की क्षमता पदार्थों में नहीं है। वह तो चेतना ही कर सकती है। विचारणाएँ, भावनाएँ और प्रवृत्तियाँ चेतना की ही चमत्कारी धाराएँ हैं। पदार्थों की जड़ता को चेतना जैसी सुखद स्थिति में उभार लाने का श्रेय चेतना को ही है। सर्व विदित है कि विचारसंस्थान की उत्कृष्टता से ही व्यक्ति का अंतरंग आनंदित और बहिरंग समुन्नत बन पाता है। उसमें त्रुटि रहेगी तो विकृत चिंतन के फलस्वरूप मनुष्य उद्विग्न और दरिद्र ही बना रहेगा। पिछड़ेपन और शोक-संकट से उसे छुटकारा मिल ही न सकेगा। भले ही परिस्थितियाँ उसके अनुकुल हों अथवा साधनों का बाहुल्य सामने प्रस्तुत हो। व्यक्ति को सुव्यवथित बनाए रहना, इस बात पर निर्भर है कि लोक-चेतना का धारा-प्रवाह किस दिशा में चल रहा है। इन तथ्यों पर ध्यान देने से धर्म चेतना को वैज्ञानिक उपलब्धियों की तरह ही श्रेयस्कर माना जाएगा। इतनी बड़ी उपयोगिता यदि अवैज्ञानिक, अप्रामाणिक मानी जाने की स्थिति में बनी रहे तो उसे मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कहा जाएगा। धर्म को प्रखर बनाए रहने के लिए उसके साथ यथार्थवादी विज्ञान दृष्टि का जुड़ा रहना आवश्यक है। यह कार्य दोनों के समन्वय से ही हो सकता है।
ठीक इसी प्रकार विज्ञान को भाव-संवेदना को अपनाकर चलना होगा जो विचार-संस्थान की नहीं, भाव-संस्थान की उत्पत्ति कही जा सकती है। विज्ञान को मात्र बुद्धिवादी बने रहने से भी उसकी उपलब्धियाँ तो मिलती रह सकती हैं, पर उपयोगिता नष्ट हो जाएगी और वे सूत्र सूख जाएँगे, जहाँ से अन्वेषणों के मूलभूत स्फुरण का उद्भव होता है।
आविष्कारों के बारे में समझा यह जाता है कि वे प्रयोगशालाओं की देन हैं अथवा वे बुद्धिमत्ता के कारण उपलब्ध हुए हैं, पर बात इतनी उथली नहीं है। प्रत्येक आविष्कार की संभावना का आरंभिक विचार अंत:स्फुरण से उठा है। बुद्धि का काम पूर्व प्रचलनों का ऊहापोह करना है। पूर्ववर्ती अस्तित्व के बिना उसकी दौड़ आगे बढ़ती ही नहीं। मस्तिष्कीय संरचना में ऐसे विचारों के उद्भव की गुंजाइश नहीं है जिन्हें मौलिक कहा जा सके। विज्ञान का विस्तार, बुद्धि और साधन-सामग्री के सहारे होने की बात सच है, पर यह सच नहीं है कि आविष्कारों से भी पूर्व अंत:करण में उठने वाली अंत:स्फुरणाएँ भी मस्तिष्क ही उगा सकता है। यदि ऐसा होता तो पूर्ववर्ती बुद्धिमानों ने उन सब अविष्कारों को बहुत पहले ही कर लिया होता, जो अब क्रमश: प्रत्यक्ष होते चले जा रहे हैं। न्यूटन से पहले भी चिरकाल से पेड़ों पर से फल जमीन पर गिरते हुए मूर्खा से लेकर विद्वानों तक सभी देखते रहे हैं, पर उतने भर संकेत से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षणशक्ति का आभास पाना, विश्वास करना और अंततः उसे खोज निकालना न्यूटन की बुद्धि का नहीं अंत:स्फुरणा का आधार है।
इसी प्रकार अन्यान्य सभी आविष्कारक अपने प्रारंभिक रूप में जब चिंतन-क्षेत्र में उतरे, तब उनका अवतरण स्थल उस परत से कहीं गहरा था, जिसे मस्तिष्क संपदा कहते हैं। यह अंत:करण ही है जो न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधारभूत कारण है, वरन् मानवीय व्यक्तित्व की उत्कृष्टता और सामाजिक संगठनों का उद्गम स्रोत भी यही है। यदि अंत:करण तत्त्व को मनुष्य से छीन लिया जाए, तो उसमें न वैज्ञानिक शोधों की आरंभिक अनुभूति पाने की क्षमता रहेगी और न पशु आवरणों से ऊँचे उन आधारों को अपनाने की आशा की जा सकेगी, जिसे मानवीय संस्कृति कहा जाता है। सर्वतोमुखी प्रगति का श्रेय जितना शारीरिक और मानसिक श्रमशीलता को दिया जाता है, उससे भी अधिक संस्कृति को मिलना चाहिए।
संस्कृति भी वैज्ञानिक उपलब्धि है। अंत:स्फुरणा उत्पन्न करने वाला अंतराल प्रकृतिप्रदत्त अनुदान नहीं है, वरन् विज्ञान की तरह ही मानवीय पुरुषार्थ का प्रतिफल है। धर्मतत्त्व को विज्ञान की आत्मा में गुँथा देखा जा सकता है। ऐसा न होता तो वैज्ञानिकों में भी स्वार्थपरता और विलासिता जैसे दुर्गुण छाए रहते और वे शोध-प्रयत्नों में योगियों जैसी तत्परता और तन्मयता का समावेश न कर सके होते। विज्ञानी में योगी और तपस्वी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वह सत्य का शोधक भी होता है और व्यक्तिगत ललक-लिप्साओं से ऊँचा उठकर शोधप्रयत्नों में दत्तचित्त रहने वाला तपस्वी भी होता है। इन प्रयासों में उसे जो संकट सहने और खतरे उठाने पड़ते हैं, वे चेतना की उत्कृष्टता के बिना संभव नहीं हो सकते। विज्ञानी भले ही ईश्वरवादी नहीं, धार्मिक तो निश्चित रूप से होता है। भले ही वह किसी मत-संप्रदाय का अनुसरण न करता हो।
धर्म के बिना विज्ञान अपंग है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। दोनों परस्पर सहयोग न करेंगे, तो वे अपूर्ण ही बने रहेंगे और उतने उपयोगी सिद्ध न हो सकेंगे, जितना कि मिल-जुलकर काम करने पर हो सकते हैं। दोनों के बीच जो दिशा विरोध दीखता है, वह सतही है। गहराई तक उतरने पर भिन्नता घटती और समता बढ़ती जाती है। गंगा और यमुना का मध्यांतर लंबा है, पर गंगोत्री और जमुनोत्री की दूरी कम है। यदि हिमालय की भीतरी जलसंपदा तक पहुँचा जा सके तो प्रतीत होगा कि दोनों के उद्गम भिन्न स्थानों पर होते हुए भी उनकी धाराएँ एक ही विशाल जलाशय से अनुदान प्राप्त करती हैं। धर्म और विज्ञान की प्रवाहमान धाराएँ अलग-अलग हैं, उनके कार्य-क्षेत्र भिन्न हैं। इतने पर भी दोनों के मध्य मौलिक समानता विद्यमान है और दोनों को पूर्ण बनने के लिए पारस्परिक सहयोग की नितांत आवश्यकता है।
अध्यात्म-क्षेत्र में जिन रहस्यमयी उपलब्धियों की चर्चा होती रहती है, उन सिद्धियों और चमत्कारों का आधार विज्ञान की किसी ऐसी धारा के साथ कल नहीं तो परसों जुड़ा हुआ पाया जाएगा, जो प्रकृति के अंतराल में विद्यमान तो है, पर अभी प्रकाश में नहीं आई है। यहाँ अद्भुत का कोई अस्तित्व नहीं। सब कुछ सुव्यवस्थित है। जिस व्यवस्था के कारणों को हम नहीं जान पाते वही अद्भुत लगता है। आरंभ में अग्नि का प्रकटीकरण भी दैवी चमत्कार था। पीछे उसके रहस्य विदित हो जाने पर प्रकृति का एक सामान्य उपक्रम उसे मान लिया गया। ठीक इसी प्रकार वैयक्तिक चेतना की गहरी परतों से जब कभी कोई स्रोत फूट पड़ते हैं, तो दैवी प्रतीत होते हैं। अनुसंधान को अपनाए रहा जाए तो उस सूत्र के सहारे वहाँ पहुँचने में सफलता मिलती है, जहाँ चेतना की किन्हीं गहरी परतों से वैयक्तिक चमत्कारों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार इस विशाल ब्रह्मांड में संव्याप्त चेतना के समुद्र का स्वरूप और उपयोग समझा जा सके तो वह आधार मिल सकता है जिसे दिव्य लोकों से बरसने वाले वरदानों की संज्ञा दी जाती है। वैयक्तिक विभूतियों और दैवी अनुकंपा की चमत्कारी सिद्धियों की चर्चा होती रहती है और उन्हें अभौतिक कहा जाता रहता है, किंतु तथ्य यह है कि जो इंद्रियगम्य या बुद्धिगम्य है वे सभी भौतिक हैं। अध्यात्म के नाम पर चलने वाली साधनाओं को अथवा उपलब्धियों को भौतिक क्षेत्र से बाहर समझना भूल हैं। पदार्थों की सहायता से जो किया जाता है अथवा जिनकी अनुभूति मन समेत ग्यारह इंद्रियों द्वारा होती है। उन्हें अभौतिक कहने का साहस बालबुद्धि तो कर सकती है, पर तत्त्वदर्शन के गले उसे नहीं उतारा जा सकता। इसी प्रकार विज्ञान के उद्भव, अनुसंधान, अभिवर्द्धन और उपयोग में आदर्शों को तिलांजलि नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार धर्म और विज्ञान एक ही उदर से जन्मे दो सहोदर भाइयों की तरह समझे जा सकते हैं और उनमें परस्पर सहयोग से मिलकर काम करने की पूरी गुंजाइश है। देव और दानवों के सहयोग से समुद्र मंथन किए जाने और उसके फलस्वरूप चौदह रत्न मिलने की पौराणिक गाथा को अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए पाया जा सकता है।
विज्ञान अब विगत शताब्दी की तरह अप्रत्यक्ष की सत्ता से इनकार करने में दुराग्रही नहीं रहा है। मेटा-फिजिक्स और पैरासाइकालॉजी की अगणित शाखा-प्रशाखाएँ इस अनुसंधान में संलग्न हैं कि अतींद्रिय अनुभूतियों के मूल में किन तथ्यों का समावेश है। गणितज्ञ सी० ए० डार्विन ने अपने ग्रंथ 'दि न्यू कॉन्सेन्स ऑफ मैटर' में कहा है-"अपने जमाने में वैज्ञानिक क्षेत्र की यह एक बड़ी क्रांति है कि जो अप्रत्यक्ष है, उसकी सत्ता को भी अनुसंधान के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है।''
विज्ञानी हर्बर्ट डिगल ने स्वीकारा है कि वे दिन बीत गए जब विज्ञान का क्षेत्र मात्र तथ्यों तक सीमित था। अब उसका कार्य-क्षेत्र कहीं आगे बढ़ गया है और रहस्यों को भी अनुसंधान के उपयुक्त आधारों का मान लिया गया है। अंतरिक्षविज्ञानी एडिगन के कथनानुसार विज्ञान के रहस्यों को भी तथ्यों में सम्मिलित कर लिया है। इसका अर्थ उनने अपने में अध्यात्म के सुरक्षित सीमा-क्षेत्र तक पहुँचने और उसमें प्रवेश करने की हिम्मत जुटा ली है।
इन दिनों विज्ञान ने विधिवत् रहस्यवाद को अपने कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया है, पर पूर्ववर्ती विज्ञानवेत्ता उस संदर्भ में सर्वथा अनुदार नहीं रहे हैं, वे अपने शोध-प्रयत्न धर्म और विज्ञान-दोनों ही दिशाओं में नियोजित किए रहे हैं और उनके समन्वय की संभावना पर विश्वास करते रहे हैं। पैरासेल्सस, ब्रूनो, पैस्कॉल, न्यूटन आदि की गणना इसी वर्ग के वैज्ञानिकों में की जा सकती है। प्लेटो अपने समय का प्रख्यात समन्वयवादी था। उसने दार्शनिक चर्चा करने के लिए आने वाले जिज्ञासुओं के लिए यह शर्त रखी थी कि उनका गणित का जानकार होना आवश्यक है। उसके दरवाजे पर एक तख्ती टॅगी रहती थी, जिस पर लिखा था-"जिसे गणित न आता हो वह भीतर न आए।''
धर्म को विज्ञान सम्मत अर्थात बुद्धिसंगत बनाने और तथ्यों को कसौटी पर कसने का प्रतिपादन करने वाले अनेक सुधारक समय-समय पर होते रहे हैं। धर्म क्षेत्र में चिरकाल से चली आ रही क्रांतियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि अंधानुसरण नहीं, तथ्यों की कसौटी पर श्रद्धा और परंपरा को कसा जाना आवश्यक है। भगवान बुद्ध की ख्याति इसी रूप में थी कि उनने बुद्धिवाद का प्रतिपादन किया था और तथ्यों की कसौटी पर खरी न उतरने वाली परंपराओं को अस्वीकार करने के लिए जनमानस को भड़काया था। इस श्रृंखला में प्राचीन एवं अर्वाचीन समाज सुधारकों को इसी वर्ग में गिना जा सकता है।
विग्रह का अंत और समन्वय का आरंभ हर क्षेत्र में आवश्यक समझा जा रहा है और उसके लिए सर्वत्र अपने-अपने स्तर के प्रयत्न अपने-अपने ढंग से चल रहे हैं। धर्म और विज्ञान के सहयोग की आवश्यकता भी युग की पुकार है। हमें इच्छा और अनिच्छा से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। विज्ञान को भावनाशील और धर्म को तथ्यानुवर्ती होने की आवश्यकता है। इस यथार्थता को जितनी अच्छी तरह समझा जाने लगेगा, उतनी ही तेजी और मजबूती के साथ दोनों महान शक्तिधाराओं के सुखद समन्वय का दिन निकट आता चला जाएगा।
"पाश्चात्य संस्कृति के पिछले शताब्दी के विचारकों के मतानुसार आदिमकाल से मनुष्य ने पशु के आहार, निद्रा, भय, मैथुन, की सीमित परिधि से आगे बढ़कर जब अपने इर्द-गिर्द के वातावरण को समझने का प्रयत्न किया होगा तो उसे भय लगा होगा। आग का गोला सूर्य, आकाश में चमकने वाले चाँद-तारे, दिन-रात का चक्र, बादलों की घटाएँ, बिजली की कड़क, नदियों की चाल, समुद्र की लहरें, सिंह और सर्पो के उत्पात, जन्म और मरण जैसी विस्मयजनक हलचलों को उसने किन्हीं अदृश्य अतिमानवों की करतूत समझा होगा और उनके कोप से बचने एवं सहायक बनाने के लिए पूजा उपक्रम का कुछ ढंग सोचा होगा। संभवत: यहीं से उपासनात्मक अध्यात्म का आरंभ हुआ है। एकाकी स्वेच्छाचार ने समूह मंय रहने की प्रवृत्ति अपनाई होगी, अन्यथा सहयोग का अभिवर्द्धन और टकराव का समाधान ही संभव न होता। धर्म यहीं से चला है।'' तथ्य और सत्य का मूल स्वरुप क्या था, यह तो साधना-शोध का विष्य है, किंतु सत्य और तथ्य तक पहुँचने के लिए श्रद्धायुक्त जिज्ञासा एवं निरंतर अध्यवसाय का सहारा लेकर ही अध्यात्म-धर्म की खोज की गई थी, ऐसा प्राचीन ग्रंथों को देखकर लगाता है। अब हम धर्म और अध्यात्म को दो धाराओं में बाँटते हैं, पूर्वकाल में दोनों एक थे।
भय के बाद लोभ की प्रवृति पनपी। उसने अतिमानवों से, देवताओं से अभीष्ट लाभ पाने की आशा रखी होगी। उनसे अवरोधों को दूर करने और वांछित फल प्रदान करने का सहयोग माँगा होगा। तब मानव अपने पुरुषार्थ की तुच्छता और आकांक्षाओं की प्रबलता का वह तारतम्य नहीं बिठा पा रहा होगा, जिसे पशु-पक्षी सहज ही बिठा लेते हैं। उपलब्ध परिस्थितियों और निजी आकांक्षाओं का वे सहज ही तालमेल बिठा लेते हैं और जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहकर अपनी प्रकृति को तदनुरूप ढाल लेते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएँ बढ़ीं और समाधान सीमित रहे। ऐसी परिस्थिति में किन्हीं अदृश्य अतिमानवों का, देव-दानवों का पल्ला पकड़ना उसने उचित समझा होगा। देवाराधन का स्वरूप उस विकास युग में भय से थोड़ा-थोड़ा छुटकारा पाने और लोभ-लालच की परिधि में प्रवेश करने का बना होगा। स्वर्ग-नरक, शाप-वरदान, जिन अदृश्य शक्तियों द्वारा दिया जाता है, उनके कोप से बचना और प्रसन्न करके लाभान्वित होना तब एक दिव्य कौशल रहा होगा। उन्हीं दिनों मंत्र-तन्त्र के–देव परिकर के रूप, विधान गढ़े गए। उन्हें देवकृत माना जाता रहा इसी आधार पर अमुक विधान का खंडन अमुक का मंडनक्रम चलता रहा।
धर्म के विकास का इतिहास मनुष्य की चेतना के चिंतन के साथ-साथ कदम मिलाकर चलता आया है। भय और लोभ की व्यक्तिवादी आकांक्षाओं से आगे बढ़कर मनुष्य अधिकाधिक समाज पर निर्भर होते चलने की स्थिति में यह समझने के लिए बाध्य हुआ कि समूहगत हलचलें मनुष्य को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। पारस्परिक सहयोग-असहयोग के, नीति-पालन और उल्लंघन के क्रियाकलाप अधिकाधिक सुविधा-असुविधा उत्पन्न करते हैं। सुख और दु:ख यही परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। अतएव व्यक्ति और समाज की नीति-मर्यादाओं को अधिक सबल अधिक परिष्कृत बनाया जाए। इस मान्यता ने नीति के, उपकार के तत्त्वज्ञान को धर्म में सम्मिलित किया और इसके लिए आचारशास्त्र का विकास हुआ। धर्म की व्याख्या, नीति–पालन एवं उदारता के लिए उत्साह-प्रदर्शन के रूप में की गई। यह और भी अधिक महत्त्वपूर्ण कदम था।
इससे आगे और भी विकसित स्थिति आती है, जब 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की 'सूत्रे मणिगणा इव' की मान्यता की आधारशिला रखी गई। एक ही आत्मा सबमें समाई हुई है-सबमें अपनी ही सत्ता जगमगा रही है-अपने भीतर सब है-सबमें एक ही आत्मा का प्रतिबिंब हैं। सब अपने और अपना सबका है। यह विश्वमानव की, विश्व परिवार की एकात्म अद्वैत बुद्धि सचमुच धर्म की अद्भूत और अति उपयोगी देन है। बढ़ती हुई समाज निर्भरता का संतुलन इसी मान्यता के साथ बैठता है। बढ़ी हुई जनसंख्या-वैज्ञानिक उपलब्धियों ने संचार और द्रुतगामी वाहनों के जो साधन प्रस्तुत किए हैं, उनने सुविस्तृत क्षेत्र में फैली हुई दुनिया का फैलाव सिकोड़कर रख दिया है। अब कुछ घंटों में ही धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचा जा सकता है। कोई देश अपने पड़ोसियों के कारण ही नहीं-दूर देशों की आंतरिक परिस्थितियों के कारण भी प्रभावित होता है। व्यक्ति की प्रगति और अवगति अब उसके निजी पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं, वरन् सामाजिक परिस्थितियाँ उसे बनने, बदलने के लिए विवश करती हैं। व्यक्ति की सत्ता समाज की मुट्ठी में केंद्रित होती चली जा रही है। व्यक्ति पूरी तरह समाज यंत्र का पुरजा मात्र बन गया है। इन परिस्थितियों में यदि व्यक्ति को समाजनिष्ठ बनने के लिए कहा जाए, उसे अपनी प्रगति-अवगति को समाज के उत्थानपतन के रूप में जोड़ने के लिए कहा जाए तो यह सर्वथा उचित और सामयिक है।
जो परिस्थितियाँ आज अनिवार्य हो गई हैं, कुछ समय पहले ही उनकी संभावना दूरदर्शियों ने भाँप ली थी और धर्म एवं अध्यात्म को अधिकाधिक समाजनिष्ठ बनाना आरंभ कर दिया गया। अहंकार को, स्वार्थ को, परिग्रह को, घृणा-वासना को त्यागने के लिए कहने का तात्पर्य व्यक्तिवाद की कड़ी पकड़ से अपनी चेतना को मुक्त करना ही हो सकता है। सेवा, परोपकार, जन-कल्याण, दान-पुण्य, त्याग-बलिदान के आदर्श मनुष्य को समाजनिष्ठ बनाने के लिए विनिर्मित हुए हैं। व्यक्तिवाद को झीना करने और समाजवाद को परिपुष्ट करने के लिए सुविकसित अध्यात्म एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसमें संयम की, तप की, तितिक्षा की, पवित्रता की,मितव्ययता की, शालीनता की, सज्जनता की, संतोष और शांति की वे धाराएँ सम्मिलित की गई हैं, जो मनुष्य को अपने लिए अपनी शक्तियों का न्यूनतम भाग खरच करने की प्रेरणा देती है और तन-मन-धन का जो भाग इस नीति को अपनाने के कारण बचा रहता है, उसे जन-कल्याण में खरच करने की ओर धकेलती हैं।
ईश्वर का स्वरूप भी अब भयंकर, वरदाता, नीति-निर्देशक की क्रमिक भूमिका से आगे बढ़ते-बढ़ते इस स्थिति पर आ पहुँचा है। कि हम विराट ब्रह्म के विश्व दर्शन के रूप में उसकी झाँकी-कर सकें और श्रद्धा-विश्वास जैसे उत्कृष्ट चिंतन को भवानी-शंकर की उपमा दे सकें। अग्निहोत्र की व्याख्या यदि जीवन यज्ञ के-सर्वमेध के साथ जोड़ी जाने लगी है तो यह अत्यंत ही सामयिक परिभाषा का प्रस्तुतीकरण है। क्रियाकांड को यदि भाव-परिष्कार का प्रतीक संकेत कहा जाए, तो वस्तुतः यह प्राचीन ईश्वर की अविकसित मन:स्थिति को आधुनिक ईश्वर की परिष्कृत चेतना ही कहा जाएगा। अब प्रसाद खाकर या प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने वाले ईश्वर की मान्यता का स्वरूप बदल रहा है। प्रतिमाओं का दर्शन करने, नदीतालाबों में नहाने, मंत्रों के जपोच्चार से चित्र-विचित्र कर्मकांडों से ईश्वर के प्रसन्न होने की बात पर केवल बहुत पिछड़े लोग ही विश्वास करते हैं। विचारशील वर्ग का ईश्वर उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व के साथ एकाकार हो गया है और उसकी पूजा श्रेष्ठ व्यक्तित्व एवं समाज के लिए प्रस्तुत किए गए अनुकरणीय अनुदानों के रूप में ही मानी जानी जा रही है। ईश्वर के प्रति यह विकसित धारणा मनुष्य जाति के साथ-साथ प्रगति-पथ पर बढ़ता हुआ साहसिक चरण है।
मध्ययुग में ईश्वर को एक सर्वतंत्र, स्वतंत्र सत्ता रूप में देखा गया। ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि वह जिस पर चाहे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तथा अप्रसन्न होकर जिसे चाहे शाप देना ही उसका काम है। भेंट-पूजा, स्तवन आदि की वह मनुष्य से आकांक्षा करता था। यह मान्यता अब विकसित होकर स्वस्थ रूप में सामने आई है। अब नीति-पालन और परोपकार को ईश्वर की प्रसन्नता का आधार समझा जाने लगा है। ईश्वर को एक नियम-एक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस व्यवस्था में समस्त जड़चेतन जकड़ा है। यहाँ तक कि ईश्वर ने अपने को भी नियमव्यवस्था के बंधनों में बाँध लिया है। आधुनिक मान्यता ईश्वर के प्रति यह बन चली है कि अब उसे पूजा-उपचार मात्र से नहीं, वरन सद्भाव संपन्न एवं सत्कर्मपरायण व्यक्तित्व के आधार पर ही प्रभावित किया और पाया जा सकता है।
धर्म और ईश्वर जिस क्रम से विकास-पथ पर चल रहे हैं उसे देखते हुए अगले दिनों नास्तिक और आस्तिक का झगड़ा दूर हो जाएगा। धर्म और विज्ञान के बीच जो विवाद था उसका हल निकल आएगा। सांप्रदायिक विद्वेष की भी गुंजाइश न रहेगी। पिछले और पिछड़े संप्रदाय अपने-अपने ईश्वरों के अलग-अलग आदेशों को पृथक प्रथा-परंपराओं के रूप में मानते थे और मतभेद रखने वालों को तलवार के घाट उतारते थे। अब वैसी गुंजाइश नहीं रहेगी। सद्भावना एवं सज्जनता की परिभाषाएँ यों अभी भी कई तरह से की जाती हैं, पर उनमें इतना अधिक मतभेद नहीं है, जिसका समन्वय न किया जा सके।
दुनिया अब एक धर्म, एक आचार, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, एक भाषा के आधारों को अपनाकर एकता की ओर चल रही है। ऐसी दशा में एक सर्वमान्य ईश्वर और उसका एक सर्व समर्थित पूजा विधान भी होना ही चाहिए। अब इस दिशा में अधिक आशाजनक स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। लगता है धर्म और ईश्वर अब एक हो जाएँगे। पिछले दिनों ईश्वर अलग था, धर्म उसे प्रसन्न करने की प्रक्रिया थी। अब दोनों मिलकर एक हो जाएँगे। धार्मिक ही ईश्वरभक्त माना जाएगा और ईश्वरभक्त को धार्मिक बनना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इसे अद्वैत सिद्धि कह सकते हैं। अनेकता और बहुरूपता के कारण जो मतिभ्रम और विद्वेष उत्पन्न होता है, वह जब संसार के विविध क्षेत्रों में से मिटाया जा रहा है तो फिर ईश्वर और धर्म का क्षेत्र भी क्यों अछूता रहेगा। धर्म और कर्म का मर्म समझने वाले ब्रह्मपरायण व्यक्ति ईश्वर को निर्विवाद स्थिति तक पहुँचा कर ही रहेंगे।
यही बात विज्ञान के लिए भी है। उसे भी अब मात्र मनुष्य की पार्थिव इंद्रियों की सुख-सुविधा तक ही सीमित न रहकर अंत:करण की शांति को भी एक प्रबल पक्ष के रूप में स्वीकार करना चाहिए तथा अपनी रीति-नीति ही नहीं, गतिविधियाँ भी इस तरह निर्धारित करनी चाहिए जिसमें मूल जीवनसत्ता और उसकी अपेक्षाओंआकांक्षाओं की अवहेलना न हो, यह बात विज्ञान और धर्म के पारस्परिक गठबंधन से ही संभव है।
|
|||||