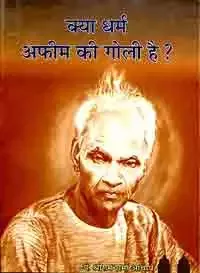|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> क्या धर्म अफीम की गोली है ? क्या धर्म अफीम की गोली है ?श्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
क्या धर्म अफीम की गोली है ?
धर्म एक शास्त्रीय दृष्टिकोण
‘सच्चिदानंद' परमपिता परमात्मा के अनेक संबोधनों में से एक संबोधन है। 'सच्चिदानंद' सत्+चित्+आनंद-इन तीन शब्दों की परस्पर संधि होने से बना है। ये तीनों शब्द परमात्मा के तीन गणों के प्रतीक हैं। सत् उसे कहते हैं जो आदिकाल से लेकर अनंतकाल तक विद्यमान रहता है। कभी नष्ट नहीं होता। यथा हम जल को ही लें। पानी आदिकाल से लेकर आज तक उपलब्ध है और अनंतकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है। यद्यपि पानी का ठोस रूप बरफऔर वायु रूप भाप होता है, जो रूप-परिवर्तन का द्योतक है। इन्हीं तीन रूपों में पानी आदि से लेकर अब तक विद्यमान है। आदि से लेकर अद्यतन चली आ रही प्रवाहमान धारा को ही सनातन कहते हैं।
जगत में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की एक विशेषता होती है। उसका अपना स्वाभाव होता है। उसका अपना गुण होता है। वस्तु की इसी विशेषता, स्वाभाव या गुण को ही धर्म कहते हैं। उदाहरणार्थपानी का गुण या स्वभाव शीतलता प्रदान करना या सृष्टि के प्राणिमात्र की प्यास बुझाना है। इसी प्रकार अग्नि का गुण ताप और प्रकाश प्रदान करना है। सरिता का स्वभाव सतत प्रवाहित रहना है। पक्षियों का स्वभाव सतत चहकते, फुदकते, उड़ते हुए आनंदित होते रहना है। पशुओं का भी स्वभाव चौकड़ी भरते हुए मस्ती भरे जीवन का आनंद उठाना है। केवल मनुष्य के संपर्क में आने वाले पशु-पक्षी जो मनुष्य की अधीनता का जीवन जीते हैं, उन्हें पराधीनता के कारण आनंदमय जीवन से वंचित रह जाना पड़ता है और दुखी जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य का एकमात्र धर्म 'आनंद' ही है। वह सदा आनंद प्राप्ति की दिशा में ही उन्मुख रहता है। यह बात दूसरी है कि परिस्थितियों की पराधीनता के कारण उसे आनंद रहित जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है, परंतु सतत उसकी चिंतन की धारा दु:ख से त्राण पाकर आनंद प्राप्ति की ओर ही प्रवाहित रहती है। मनुष्य समाज के तत्त्वान्वेषी ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, विचारक, चिंतक आदि जितने भी महापुरुष हो गए है तथा जिन्होंने धर्मशास्त्रों का प्रणयन किया है, उन सभी ने एक स्वर से दु:ख से त्राण पाने का उपाय और सुख प्राप्ति का मार्ग धर्म को ही बताया है। सुख प्राप्ति के मार्ग को ही 'धर्म' कहा गया है। व्यक्तिगत सुख के मार्ग को व्यक्ति का धर्म, परिवार को सुखी बनाने वाले मार्ग को ‘कुटुंब धर्म', और जिससे समाज को सुख मिले 'सामाजिक धर्म', जिससे राष्ट्र खुशहाल हो, उसे 'राष्ट्र धर्म', जिससे विश्व सुखी हो, उसे 'सार्वभौम धर्म' और जिससे प्राणिमात्र सुख की अनुभूति करें, ऐसे धर्म को 'सनातन धर्म' कहा गया है।
यों तो 'धर्म' संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसकी शाब्दिक उत्पत्ति ‘धृञ्' 'धारणे' धातु से हुई है। महर्षि व्यास जी ने धर्म की परिभाषा इस प्रकार की है-
धारणाद्धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः।
यत्स्याद् धारणासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥
अर्थ –धारण करने से इसका नाम धर्म है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है। वह निश्चय ही धर्म है। महामुनि कणाद ने कहा है-
यतोऽभ्युदय नि:श्श्रेयससिद्धिः स धर्मः।
अर्थ - जिससे इस लोक और परलोक दोनों स्थानों पर सुख मिले, वही धर्म है।
आधार उसे कहते हैं, जिसके सहारे कुछ स्थिर रह सके, कुछ टिक सके। हम चारों ओर जो गगनचुंबी इमारत देखते हैं, उनके आधार पर नींव के पत्थर होते हैं। इसी पर वे स्थिर हैं। इसी पर वे टिके हुए हैं। प्रत्येक पदार्थ किसी-न-किसी आधार पर ही अवस्थित हैं। यहाँ तक कि ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो अंतरिक्ष में, शून्य में अवस्थित प्रतीत होते हैं, वे भी एकदूसरे की आकर्षण शक्ति को आधार बनाए हुए हैं। आधार रहित कुछ भी नहीं है। बिना आधार के सनातन धर्म भी नहीं है। सनातन धर्म का अपना एक मजबूत आधार है, जिसके ऊपर उसकी भित्ति हजारों वर्षों से मजबूती से खड़ी हुई है।
वह आधार क्या है? वह आधार है- सर्वभूत हितेरताः।
इसे दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि सृष्टि के संपूर्ण जड़-चेतन में अपनी आत्मा का दर्शन करना। अपने समान ही सबको मानना। जैसा कि यजुर्वेद में कहा गया है-
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥
इसी बात को एक अन्य ऋषि ने इस प्रकार कहा है-
न तत्परस्य संदध्यात्प्रतिकूलं यदात्मनः।
एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते।।
अर्थ- जो कार्य अपने विरुद्ध हुँचता हो, दु:खद मालूम होता हो, उसे दूसरों के साथ भी मत करो-संक्षेप में यही धर्म है।
श्रीमद्भागवतकार ने भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कहा है। कि हृदय में सब भूतों के प्रति दया होना तथा यदृच्छ लाभ से संतुष्ट रहना है।
दयया सर्वभूतेषु, संतुष्ट्या येन केन वा।
भगवान कृष्ण कहते हैं-
अहमुच्चावचैर्द्रव्यैर्विषयोत्पन्नयानघे।
नैव तष्येऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः।
अर्थ- जो दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है, वह सब प्रकार की सामग्रियों से विधिपूर्वक मेरा अत्यंत पूजन-भजन भी करे, तो भी मैं उन पर संतुष्ट नहीं होता।
मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है-
धर्मं शनैः निश्चनुयाद् बल्मीकमि व पुत्तिकाः।
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्॥
अर्थ- जैसे दीमक बाँबी को बनाती है वैसे सब प्राणियों को न देकर परलोक के लिए धर्म संग्रह करें। महर्षि व्यास ने कहा है-
श्रूयतां धर्म सर्वस्वं, श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्॥
अर्थ- धर्म का सार सुनो। सुनो और धारण करो। अपने को जो अच्छा न लगे, वह दूसरों के साथ व्यवहार न करो।
‘सर्वभूत दया' ही हमारे सनातन धर्म का आधार है। सब प्राणियों को आत्मवत् मानना ही धर्म का उच्चतम आदर्श है, आधार है। इन्हीं सब कारणों से ही हमारे यहाँ धर्मपालन का निर्देश पग-पग पर दिया गया है, जिससे हम अपने आधार को, अपने आदर्श को कभी भी न भूल सकें। जैसा कि कहा गया है कि-
नापुत्र सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्र दारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः।।
अर्थ- परलोक में न माता, न पिता, न पुत्र, न स्त्री और न संबंधी सहायक होते हैं। केवल धर्म ही सहायक होता है।
चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चले जीवितयौवने।
चला चलति संसारे, धर्म एकोहि निश्चलः॥
अर्थ- लक्ष्मी चलायमान है और जीवन भी चलायमान है। इस चराचर जगत में केवल धर्म ही अचल है। सनातन धर्म कोई मजहब या संप्रदाय नहीं है, जो परस्पर शत्रुता के बीज बो देवे। इस धर्म का आधार अत्यंत मजबूत हैं, जो हमें ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु' का पाठ पढ़ाता है। यही वह धर्म है, जो वसुधैवकुटुंबकम् की ऊँची शिक्षा देता है। यही वह धर्म है जो आत्मानंद और परमानंद की प्राप्ति कराता है। यही वह धर्म है, जो विश्वजनीन है। इसी धर्म से विश्वमानव कल्याण को प्राप्त होगा। धर्म का यह एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है-अवांछनीयताओं, अनाचार, असुरता को निरस्त करना।
असुरता को निरस्त करना और देवत्व का अभिवर्द्धन, यह उभयपक्षीय कर्तव्य कर्म प्रत्येक मनुष्य को निभाने होते हैं। आहार का ग्रहण और मल का विसर्जन दोनों ही क्रियाकलाप जीवनयापन के अविच्छिन्न अंग हैं। भगवान को उद्देश्य लेकर अवतरित होना पड़ता है-(१) धर्म की स्थापना (२) अधर्म का विनाश। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। माली को पौधों में खाद-पानी लगाना पड़ता है, साथ ही बेढंगी टहनियों की काँट-छाँट तथा समीपवर्ती खरपतवार उखाड़ने पर भी सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना पड़ता है। आत्मोन्नति के लिए जहाँ स्वाध्याय, सत्संग, धर्मानुष्ठान आदि करने पड़ते है, वहाँ कुसंस्कारों और दुष्प्रवृतियों के निराकरण के लिए आत्मशोधन की प्रताड़ना-तपश्चर्या भी अपनानी होती है। प्रगति और परिष्कार के लिए सृजन और उन्मूलन की उभयपक्षीय प्रक्रिया अपनानी होती है। धर्माचरण की तरह ही अधर्म के प्रति प्रचंड आक्रोश प्रकट करने पर ही समग्र धर्म की रक्षा हो सकती है। अनीति के प्रति आक्रोश जाग्रत रखने को शास्त्रों में 'मन्यु' कहा गया है और उस प्रखरता को धर्म का अविच्छिन्न अंग माना गया है। अतिवादी, उदार पक्षी, एकांगी धार्मिकता का ही दुष्परिणाम था। जो हजार वर्ष की लंबी राजनैतिक गुलामी के रूप में अपने देश को अभिशाप की तरह भुगतना पड़ा।
सज्जनता का परिपोषण जितना आवश्यक है, उतना ही दुष्टता का उन्मूलन भी परम पवित्र मानवीय कर्तव्य है। यदि यह सनातन सत्य ठीक तरह समझा जा सके तो प्राचीन काल की तरह आज भी हर व्यक्ति न्याय के औचित्य का पोषण और अन्याय के अनौचित्य का निराकरण कर सकता है। शास्त्र कहता है-
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह।
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाऽग्निना।।
हे ब्राह्मण ! तुम अपने विचार उच्च रखना, पर साथ-साथ अपने क्षत्रियत्व को भी जाग्रत किए रखना। विज्ञानी व्यक्ति ही अपनी अग्नि (तेजस्विता) को बनाए रखते हैं। वे ही यज्ञ के ज्ञाता और अधिकारी हैं।
जहाँ ब्रह्मशक्ति और क्षात्रशक्ति साथ-साथ रहती है, जहाँ पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान कायम रहता है, वही देश पुण्य रहता है।
नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्मवर्धते।
ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते॥
न बिना ब्रह्मशक्ति के क्षात्रशक्ति बढ़ सकती है और न बिना क्षात्रशक्ति के ब्रह्मशक्ति बढ़ सकती है, प्रत्युत दोनों के मेल से ही लोक-परलोक की उन्नति होती है।
ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव, तदेकं सन्न व्यभवत्। तच्छ्यो रूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्योः यमो मृत्युरीशान इति।
सृष्टि के पूर्व जगत के स्वरूप में व्यक्त होने के पहले केवल एक ब्रह्म ही था। उस समय एक था, परंतु ब्राह्मण जात्याभिमानी एक ब्रह्म से सृष्टि, स्थिति आदि विश्व से समस्त कार्यों का निर्वाह नहीं हो सकता। एक ब्रह्म सृष्टि, स्थिति आदि निखिल जगत कार्यों को संपादन करने में पर्याप्त समर्थ नहीं है। इसी कारण कर्म करने की इच्छा से परमात्मा प्रशस्त रूप में क्षत्रिय भाव से युक्त हुए। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान रूप में व्यक्त हुए। इंद्राणि देवगण क्षत्रिय जाति के देवता हैं।
ब्राह्मणैः क्षत्रवंधुर्हि द्वारपालो नियोजितः।
ब्राह्मण कर्म वालों ने क्षत्रिय कर्म वाले भाइयों को समाज का चौकीदार नियुक्त किया।
शम प्रधानेषु तपोधनेषु,
गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः।
शम प्रधान तपस्वियों में शत्रुओं को जलाने वाला तेज छिपा हुआ है।''
वीरता ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। ब्राह्मण उसकी साहसिकता का परिचय सत्प्रवृतियों के संवर्द्धन में तन्मय रहकर देता है। क्षत्रिय अपनी शूरता को दुष्टता से जूझने में लगाता है। दोनों का कार्य समान रूप से आवश्यक है। अस्तु, दोनों को ही श्रेयाधिकारी कहा गया है।
वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्यापने रताः
गुरु शुश्रूषया शूरा मातृपितृपरायणाः
आरण्यगृहवासे च शूरा कर्तव्यपालने।
जो वेदाध्ययन में, अध्यापन में, गुरुसेवा में, माता-पिता की सेवा में, कर्तव्यपरायणता में शूर है, वह चाहे वनवासी बने अथवा घर में रहे, समान रूप से प्रशंसनीय है।
प्राचीनकाल में युद्ध धर्मयुद्ध के रूप में ही होते थे। नीति और न्याय की रक्षा के लिए असुरता के विरुद्ध लोहा लिया जाता था। अनीतिपूर्वक स्वार्थसिद्धि करने के लिए आक्रमण करने की देव परंपरा कभी रही ही नहीं। जब भी लड़ना पड़ता तब दुष्टता को निरस्त करना उनका लक्ष्य रहा। अस्तु, भारतीय युद्धों का इतिहास ‘धर्मयुद्ध' के रूप में ही देखा जा सकता है। जिस प्रकार ब्राह्मण तपश्चर्या और लोकसेवा में अपने को तिल-तिल गलाते घुलाते थे। उसी प्रकार क्षत्रिय भी असुरता से जूझने में अपने प्राणों की परवाह न करते थे और जान हथेली पर रखकर अन्याय से जुझते और उसे मिटाकर ही चैन लेते थे। क्षत्रिय धर्म और उसके धर्मयुद्ध की शास्त्रों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है और कायरतावश उससे जी चुराने वालों को निंदनीय ठहराया है।
वेद में भी बताया गया है-
ये युद्धयन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः।
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्॥
जो संग्रामों में लड़ने वाले हैं, जो शूरवीरता से शरीर को त्यागने वाले हैं और जिन्होंने सहस्रों दक्षिणाएँ दी हैं। तू उनको भी प्राप्त हो।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि।
धम्र्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥
स्व धर्म को समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं है; क्योंकि धर्मयुद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता।
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गदारमपावृतम्।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभंते युद्धमीदृशम्॥
हे पार्थ! यों अपने आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्ग का द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है।
यस्तु प्राणान् परित्यज्य प्रविशेदुद्यतायुधः।
संग्राममग्निप्रतियं पतंग इव निर्भयः॥
स्वर्गमाबिशते ज्ञात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्॥
जो अपने प्राणों की चिंता छोड़कर पतंगे की भाँति निर्भय हो हाथ में हथियार उठाए अग्नि के समान विनाशकारी संग्राम में प्रवेश कर जाता है और योद्धा को मिलने वाली निश्चित गति को जानकर उत्साह पूर्वक जूझता है, वह स्वर्गलोक में जाता है।
सलिलादुत्थितोवह्निर्येनव्याप्तंचराचरम्।
दधीचस्यास्थितो वज्रं कृतं दानवसूदनम्॥
पानी से आग पैदा हुई जो सारे जगत को व्याप्त कर रही है। दधीच की हड्डी से सारे दानवों का नाशक वज्र बनाया गया।
भगवान के सभी अवतार धर्म स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुए। दुर्गा का अवतार तो विशेषत: असुरता से जूझने के लिए ही हुआ।
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्थानं भविष्यति।
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यारिसंक्षयम्॥
जब-जब दानव प्रकृति वाले जोर पकड़कर सृष्टिकार्य में, सामाजिक प्रगति में रोड़ा अटकाएँगे, तभी मैं प्रकट होकर उनका नाश करूंगी।
भारतीय धर्म और संस्कृति की जननी गायत्री है। उसे ब्रह्मवर्चस् भी कहते हैं। उसमें ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मतेज दोनों का समावेश है। उन दोनों ही तत्त्वों की उपासना करने वाला ब्रह्मतेज संपन्न हो जाता है। इस तथ्य को शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार कहा गया है-
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं गायत्री।
गायत्र्या तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी भवति॥
“गायत्री ही तेज और ब्रह्मवर्चस् स्वरूप है। उसका सदैव अनुष्ठान करने से तेजस्वी और ब्रह्म वर्चस्वी बनता है।''
सत्प्रवृतियों का प्रसार एवं प्रतिस्थापना एवं दुष्प्रवृतियों का निष्कासन-विनाश ही धर्म का मूलोददेश्य है। इस तथ्य को जो समाज जितना हृदयंगम कर तदनुरूप जीवनशैली में इनका समावेश । करेगा, वह उतना ही सशक्त, समुन्नत एवं शालीन बनेगा। यदि वह इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता तो उसे भी विज्ञान की टेढ़ी आँख का कोपभाजन बनने के लिए तैयार रहना पडेगा। आधारविहीन धर्म थोड़ी देर ठहर सकता है। विज्ञान की कठोर तर्कशक्ति के आगे उसका यथार्थस्वरूप ही टिक पाएगा।
धर्म ऐसे महान तथ्य और जीवन-चेतना का यथार्थ विज्ञान है, उसके बाह्याभ्यांतर दोनों ही स्वरूप व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी होते हैं। ऐसी महान सत्ता को दिमागी बहस नहीं, अपित, श्रद्धा के रूप में देखा-परखा और धारण किया जाना चाहिए।
* * *
|
|||||