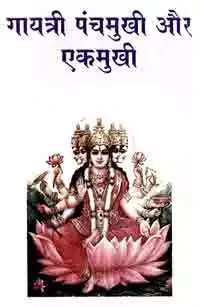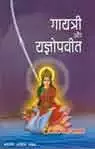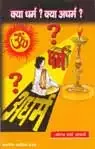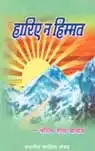|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री पंचमुखी और एकमुखी गायत्री पंचमुखी और एकमुखीश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
गायत्री की पंचमुखी और एकमुखी स्वरूप का निरूपण
(४) विज्ञानमय कोश
अन्नमय, प्राणमय और मनोमय इन तीनों कोशों के उपरान्त आत्मा का चौथा आवरण, गायत्री का चौथा मुख विज्ञानमय कोश है। आत्मोन्नति की चतुर्थ भूमिका में विज्ञानमय कोश की साधना की जाती है।
विज्ञान का अर्थ है-विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोक समस्याओं को समझते हैं। स्कूलों में इसी साधारण ज्ञान की शिक्षा मिलती है। राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, संगीत वकृत्व, लेखन, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, उत्पादन आदि विविध बातों की जानकारी विविध प्रकार से की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर शरीर से सम्बन्ध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है। जिनके पास यह जानकारियाँ जितनी अधिक होंगी, जो लोक-व्यवहार में जितना प्रवीण होगा, उतना ही उनका सांसारिक जीवन उन्नत, यशस्वी, प्रतिष्ठित, सम्पन्न एवं ऐश्वर्यवान् होगा।
ज्ञान का अभिप्राय है जानकारी। विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति। आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु यह जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है सच्चिदानन्द स्वरूप है। परन्तु इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति-भूमिका में नहीं होता। स्वयं, को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो जाता है। शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की उपेक्षा प्रतिक्षण होती रहती है। दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा हर घड़ी सताती रहती है। तब कैसे कहा जाय कि आत्मा की अमरता, शरीर की भिन्नता तथा ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है।
अपने सम्बन्ध में तात्त्विक मान्यता स्थिर करना और उसको पूर्णतया अनुभव करना, यह विज्ञान का उद्देश्य है। आमतौर से लोग अपने को शरीर मानते हैं, स्थूल शरीर से जैसे कुछ हम हैं वही हमारी आत्म मान्यता है, जाति, वंश, प्रदेश, सम्प्रदाय, व्यवसाय, पद, विद्या, धन, आयु, स्थिति, लिंग, आदि के आधार पर यह मान्यता बनाई जाती है कि मैं कौन हूँ? यह प्रश्र पूछने पर कि आप कौन हैं? लोग इन्हीं बातों के आधार पर अपना परिचय देते हैं। अपने को व समझते भी यही हैं। इसी मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थों का निर्धारण होता है। जिस स्थिति में स्वयं हैं, उसी का अहंकार अपने में जागृत होता है और स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति, पुष्टि तथा सन्तुष्टि जिस प्रकार होती सम्भव दिखाई पड़ती है, वही जीवन की अन्तरंग नीति बन जाती है।
विज्ञान इस अज्ञान रूपी अन्धकार से हमें बचाता है। जिस मनोभूमि में पहुँच कर जीव यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं वस्तुतः आत्मा ही हूँ। उस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश में जीव की स्थिति रहती है तब तक वह अपने को स्त्री-पुरुष, मनुष्य, पशु, मोटापतला, पहलवान्, काला-गोरा आदि शरीर संबंधी भेदों से पहिचानता है जब अनामय कोश में जीव की स्थिति होती है, तो गुणों के आधार पर अपनेपन का बोध होता है। शिल्पी, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, मूर्ख, कायर, शूरवीर, वक्ता, धनी, गरीब, आदि की मान्यताएँ प्राण भूमिका में होती हैं। ज्ञानमय कोश का स्थिति में पहुँचने पर अपनेपन की मान्यता स्वभाव के अधार पर होती है। लोभी, दम्भी, चोर, उदार, विषयी, संयमी, नास्तिक, आस्तिक, स्वार्थी, परमार्थी, दयालु, निष्ठुर आदि कर्तव्य और धर्म की, औचित्य और अनौचित्य सम्बन्धी मान्यताएँ जब अपने सम्बन्ध में बनती हों, उन्हीं पर विशेष ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में पहुँचा हुआ है। इससे ऊँची चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका है, जिसमें पहुँचकर जीव अपने को यह अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर, गुणों एवं स्वभाव से ऊपर हूँ। मैं ईश्वर का राजकुमार अविनाशी आत्मा हूँ।
दृष्टिकोण का परिष्कार, उच्चस्तरीय आस्थाओं की अन्तःकरण में स्थापना, यही देवत्व का चिह्न है। देवताओं की आकृति मनुष्य जैसी ही होती है, पर उसका अन्तस्थल ऊँची निष्ठाओं से भरा रहता है। दर्पण के ऊपर जमा मैल साफ हो जाने पर उसमें प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अंगार से राख की पर्त हट जाने पर उसकी तेजस्विता सामने आ जाती है, उसी प्रकार निम्न स्तरीय भोगवादी तृष्णा आदि वासना की हीन वृत्तियाँ जब हट जाती हैं और उनके स्थान पर आत्मज्ञान की तत्व दृष्टि खुल जाती है, तो मनुष्य का देवत्व जाग पड़ता है। देवता जितने दिव्य, सुन्दर होते हैं उतना ही वह शोभायमान बन जाता है। भले ही अष्टावक्र या रामकृष्ण परमहंस की तरह वह चमड़े एवं आँख से कुरूप ही क्यों न दीखे।
मनुष्य के भीतर अगणित दिव्य विभूतियाँ-सिद्धियाँ भरी पड़ी हैं, पर वे निकृष्ट आस्थाओं के कूड़े-कचरे में दबी पड़ी रहती हैं और दीन-दरिद्र की तरह जीवनयापन करने के लिए विवश करती हैं, किन्तु जब विज्ञानमय कोश का अनावरण होता है तो देवत्व की सारी विशेषताएँ मनुष्य में परिलक्षित होती हैं। संसार उसे मस्तक झुकाता है। उसका अनुसरण करता है तथा उसकी तेजस्विता से विविध-विध लाभ उठाता है। विज्ञानमय कोश का जागरण तो साधक को स्वर्ग एवं मुक्ति का आनन्द जीवित रहते हुए ही प्रदान कर देता है, इसके लिए उसे किसी अन्य लोक में जाने या मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।
विज्ञानमय कोश के जागरण का अर्थ है- आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्म लाभ, आत्म दर्शन, आत्म कल्याण। यही तो जीवन लक्ष्य है। इस की प्राप्ति करना पर पुरुषार्थ कहा गया है। इस स्तर को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता।
विज्ञानमय कोश की साधना में (१) सोऽहम् का अजपा जाप, (२) आत्मानुभूति, (३) स्वर संयम और ग्रन्थि आदि, यह चार तपश्चर्यायें करनी पड़ती हैं। व्यावहारिक जीवन के हर पहलू पर उच्चस्तरीय दृष्टिकोण बनाये रखने का आदर्शवादी दृष्टिकोण तो निरन्तर ही साधना क्रम में सम्मिश्रण रखना पड़ता है।
|
|||||