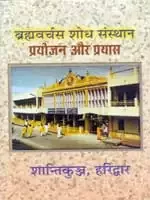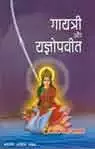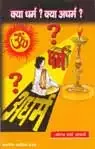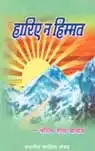|
नई पुस्तकें >> ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान प्रयोजन और प्रयास ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान प्रयोजन और प्रयासश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है ब्रह्मवर्चस् का प्रयोजन और प्रयास
शब्दयोग एवं संगीत की प्रभावोत्पादक सामर्थ्य
अग्रिहोत्र समिधाओं के सहारे अग्रि प्रज्जवलित कर वनौषधियों को जला देने की क्रिया मात्र नहीं है; वरन् इसके साथ मन्त्रोच्चार की अनिवार्य विधा भी जुडी हुई है। यदि ऐसा न होता तो लोग किसी अँगीठी मेंरख कर जड़ी-बूटियों को जला भर दिया करते और उसके धुएँ से वे लाभ उठा लेते, जो अग्रिहोत्र के साथ अतिमहत्वपूर्ण स्तर के बनकर जुड़े हुए हैं।
यज्ञ-कृत्य में वेद मंत्रों का समवेत स्वरों में उच्चारण होता है। वेद मन्त्रों में मात्र शिक्षा ही नहीं है, उनमें स्वर संगीत का भी समावेश है। सामवेद की शाखा प्रशाखाएँ इसी निमित्त रची गयीं थीं कि उन्हीं मन्त्रों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न ध्वनियों में गाया और उनसे तदनुरूप परिणाम उपलब्ध किया जाय। यज्ञों में उद्गाता का महत्त्वपूर्ण पद इसलिए नियत था कि मन्त्रों को आवश्यक्तानुरूप ध्वनियों में विधिपूर्वक गाया जा सके।
यज्ञाग्रि एक प्रकार से विद्युत उत्पादक केन्द्र का काम करती है। उसके साथ निर्धारित ध्वनि का समावेश हो जाने पर उत्पादित शब्द शक्ति की क्षमता एव उपयोगिता अनेक गुनी हो जाती है। रेडियो प्रसारणों में भी यही विधा काम में लायी जाती है। सामान्य रीति से उच्चरित स्वर, विद्युत तरगों के साथ जुड़ कर इस योग्य बन जाते हैं कि एक बहुत व्यापक क्षेत्र तक जा सकें। अग्रिहोत्र प्रक्रिया में उच्चरित वेद मन्त्रों का प्रवाह भी इसी स्तर का शक्तिशाली बन जाता है। यह मनुष्य ही नहीं, आस-पास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीनों शरीरों का उपयोगी परिष्कार होता है। इसके अतिमहत्त्वपूर्ण सत्परिणाम देखने में आते हैं।
ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान में यज्ञ प्रक्रिया का छोटा एवम् आरम्भिक रूप अग्रिहोत्र ही हाथ में लिया गया है। उसे सार्वभौम एवम् सार्वजनिक भी बनाया गया है। इसलिए उसके साथ उन सुगम सगीतों का भी समावेश किया गया है, जो सभी के लिए विशेषतया भारतीय परिस्थितयों के, उसके देशवासियों की मनोदशा के अनुकूल पड़ते हैं। यह संगीत शक्ति, सामर्थ्य से भरी-पूरी है तथा डसकी प्रतिक्रिया सरलतापूर्वक जाँची जा सकती है। वेदमंत्रों के अतिरिक्त संगीत विज्ञान को शोध का विषय बनाया गया है और देखा गया है कि संगीत की-शब्द शक्ति की कितनी विधाएँ मनुष्य के शारीरिक मानसिक रोगों के निवारण में काम आ सकती हैं।
संगीत का सीधा संबंध भावनाओं को तरंगित करने से हैं। वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ-साथ कारण शरीर के उत्कर्ष-उन्नयन का आधार भी बन जाता है। तनाव मिटाने, मनःशक्ति संवर्धन मे उसकी उपयोगिता देखा गयी है। संगीत का प्रभाव जलचर, थलचर, नभचर वर्ग के प्राणियों पर भी पड़ता देखा गया है। वायुमंडल के परिशोधन संबंधी प्रभाव भी उत्पन्न होते हुए देखे गये हैं। गेय मन्त्रों के उच्चारण का जो महल है, उसमें उसकी स्वर लहरी का प्रभाव विशेष रूप से देखा और सरलततापूर्वक जाना जा सकता है। वृक्ष-वनस्पतियों तक पर उसका प्रभाव होता है। संगीत के प्रभाव से अधिक फसल उत्पन्न होने, वृक्षों पर अधिक फल लगने, प्राणिवर्ग में उपयोगी समर्थता बढ़ने की पृष्ठभमि बनती है।
यों संगीत का प्रभाव एक स्वतंत्र विषय है और उसकी सर्वतोमुखी परिणति के सत्परिणाम शोध-उपकरणों तथा अनुभवों के आधार पर देखे-पाये जा सकते हैं। अनेक देशो में इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयोग चल रहे हैं और उनके उपयोगी सत्परिणामों को देखते हुए संगीत को मानव जीवन की एक उपयोगी विधा के रूप मे स्वीकारा जाने लगा है। शान्तिकुञ्ज के शोध-प्रयासों में यह जाँचा-परखा जा रहा है कि किस संगीत से मानव जीवन की किस कठिनाई को घटाया और किस आवश्यकता पूर्ति का सुयोग किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है? संगीत की तरंगों को ऑसीलोस्कोप के माध्यम से देखा-परखा जाता है एवं विभिन्न स्वर लहरियों की पिच, एम्प्लीट्यूड तथा वेवलेन्थ को मापा जाता है। शोर एवं संगीत की ध्वनि तरंगों के स्वरूप के अन्तर के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि शब्द-शक्ति से विकृत रूप के भिन्न-भिन्न प्रभाव होते हैं। इसके लिए बड़ी क्षमता वाले ड्युअलबीम स्टोरेज ऑसीलोस्कोप मे कार्य आरम्भ किया गया है। संगीत के माध्यम से तनाव मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, इसे पॉलीग्राफ यंत्र से दर्शाया तथा बायोफीडबैक द्वारा साधकों को प्रशिक्षित करने की विधा का भी यहाँ समावेश किया गया है।
अग्रिहोत्र से भी संगीत चिकित्सा की संगति इस पकार बैठती है कि जब गायत्री मंत्र को स्टीरियो डेक द्वारा सुनाया जाता है, तब गायन-वादन के माहौल को प्रभावित करने के लिए अग्रिहोत्र के प्रयोग भी चल रहे होते हैं। इस प्रकार ध्वनि के साथ ताप भी जुड जाता है और उच्चारण में ऐसा सूक्ष्म अन्तर विकसित होता है, जिसकी प्रभावोत्पादक शक्ति कहीं अधिक होती है।
शब्द, ताप एवं प्रकाश यही तीन तरंगें प्रकृति का सूक्ष्मरूप है। अग्रिहोत्र में इन तीनों का समुचित समन्वय हो जाता है। इम संतुलित ऊर्जा का प्रभाव मानवी काया, मन, जीव-जगत, पर्यावरण एवं वृक्ष-वनस्पतियों पर बढ़-चढ़कर सत्परिणाम उत्पन्न करते देखा जा सकता है। जहाँ संभव होना है, वहाँ गायन-वादन मंडली-भग्रिहोत्र के सुरभित वातावण में अमुक प्रयोजन के लिए अमुक विधान अपनाये जाने की नीति अपनाती है। जिन्हें उस प्रभाव की विशेष आवश्यकता है वे वहाँ शान्त-चित्त से बैठते हैं। उन्हें केन्द्र बनाया जा सकता है। आज के यान्त्रिक युग में वह प्रयोजन ऑडियो कैसेट द्वास भी पूरा किया जा सकता है।
शान्तिकुञ्ज द्वारा संगीत प्रवाहों के कुछ ऐसे टेप आविष्कृत किये जा रहे हैं जो विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ निबाहते हैं। वनस्पतियों को अधिक बढ़ने और फलने-फूलने में योगदान देने वाले संगीत टेप भी होते हैं, तो थलचये-नभचरों को प्रभावित करने वाले अन्य प्रकार के। मनुष्यों के लिये तीन प्रयोजनों को पूरा करने वाले अलग-अलग प्रवाहों वाले टेप बनाये जा रहे है।
(१) शारीरिक स्वस्थता
(२) मानसिक प्रखरता
(३) भाव-संवेदना क्षेत्र की उत्कृष्टता।
संगीत चिकित्सा को एक स्वतंत्र विषय माना जा सकता है। उसमें अग्रिहोत्र का पुट किसी प्रकार लग जाने से प्रभाव क्षमता का और भी अधिक विस्तार होते देखा गया है। भेद-उपभेदों का ध्यान रखते हुए ऐसे वाद्ययन्त्रों के समुच्चय तैयार किये जा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की व्याधियों के निराकरण में अपना प्रभाव दिखा सकें। कोई व्यक्ति किस दिशा विशेष में अपने व्यक्तित्व को अग्रसर करना, शक्ति-संवर्धन करना चाहता है? यह एक स्वतंत्र प्रयोजन है। संगीत टेपों का अगले दिनों इस प्रकार का प्रयोग-परीक्षण होने जा रहा है, जिसके आधार पर अभीष्ट प्रगति का द्वार खुल सके।
मान्यता है कि सृष्टि के आदि में शब्द उत्पन्न हुआ। उसका ध्वनि प्रवाह ॐकार जैसा था। इसके बाद अन्यान्य तत्त्व उत्पत्र होते गये और सृष्टि की परोक्ष सत्ता प्रत्यक्ष कलेवर धारण करती चली गयी। ओंकार ध्वनि-शास्त्र का बीज है। उस अकेले को ही इतने अनेक प्रवाहों में गाया जा सकता है कि सातों स्वरों का परिचय उस अकेले से ही प्रादुर्भूत हो सके। संगीत चिकित्सा के अनुसंधान में अगले दिनों ऐसे प्रयोग भी चल सकेंगे कि समस्त श्रुति-ऋचाओं का बीज मन्त्र ॐकार ही विभिन्न ध्वनि लहरियों में प्रयुक्त करके संगीत-चिकित्सा का ढाँचा खड़ा किया जा सके।
संगीत की ध्वनि लहरियों शरीर संस्थान, मन:संस्थान और भाव संस्थान के तीनों ही क्षेत्रों को तरंगित करती हैं। ध्वनि प्रवाह शरीर के प्रत्येक अंग-अवयव पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इन तल लहरों में ज्वार-भाटे जैसे गुण पाये जाते हैं। उनमे शमनकारी और उत्तेजक दोनों ही क्षमताएँ प्रचुर परिमाण में विद्यमान पायी जाती हैं। मनुष्य ने विद्युत, लेसर, बारूद, अग्रि आदि का दिव्य वरदानों के रूप में उपयोग किया है। संगीत ऊर्जा का भी सृजनात्मक उपयोग कर उसने मानव मात्र को लाभाविन्त किया है। अब इसकी व्यापक क्षमता का प्रयोग समष्टिगत वातावरण परिशोधन के रूप में होना चाहिए। वातावरण में सौम्य सात्विकता का समावेश करने के लिये संगीत का सामूहिक सहगान-सकीर्तन के रूप में उपयोग किया जा सकता।
शान्तिकुञ्ज की संगीत शोध प्रक्रिया में विभिन्न भाव-सम्बेदनाओं के साथ गाये जाने वाले वाद्यों का क्या प्रभाव चेतना जगत् एवम् जड़जगत् पर होता है, इसका प्रयोग परीक्षण इन दिनों सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके निष्कर्ष सामने आने पर यह सिद्ध होने की सम्भावना है कि विधि विशेष से किये गये सामूहिक दिव्य संकीर्तन, मन्त्रोच्चार अपने माहौल में उत्कृष्टता उत्पन्न करते ही हैं विश्वव्यापी वातावरण पर भी उनका उपयोगी प्रभाव पड़ता है।
|
|||||