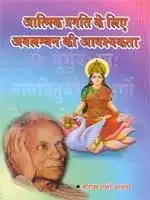|
नई पुस्तकें >> आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकता आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकताश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकता
समर्थ बनना हो, तो समर्थों का आश्रय लें
युग निर्माण योजना मथुरा एवं प्रज्ञा अभियान शान्तिकुञ्ज हरिद्वार के संस्थापक-संचालक लाखों प्रज्ञा परिजनों के गुरु पूज्य पं० श्रीराम शर्मा आचार्य जी कहते रहे हैं कि यदि उन्हें किसी महान मार्गदर्शक का अनुग्रह न मिला होता, तो वे उस स्थिति में न पहुँच सके होते, जिसमें कि पहुँच सकने में वे समर्थ हुए। उन्होंने अपने मार्गदर्शक पर समग्र श्रद्धा एकत्रित करके समर्पित की है। फलतः उदार अनुदानों की अमृत वर्षा होने लगी और उसका लाभ आरंभ से लेकर आज तक अनवरत एवं अविच्छिन्न क्रम से मिलता रहा। यदि इस स्तर पर शिष्य का श्रद्धा समर्पण न रहा होता, तो संभवतः अन्य अनेक चित्र पूजकों की तरह उनके पल्ले भी कुछ न पड़ा होता।
रामकृष्ण परमहंस के तथाकथित अगणित शिष्य थे। सभी को वे आशीर्वाद भी देते रहे, पर जिन्हें निहाल कर दिया, वे विवेकानन्द, बाह्मानन्द, प्रेमानन्द, शारदानन्द आदि थोड़े से ही साधक थे। कुछ के साथ पक्षपात, अन्यों के साथ उपेक्षा का आरोप यहाँ लागू नहीं होता। गड्डा जितना गहरा होता है उतना ही वर्षा का जल उसमें जमा हो जाता है। ऊंचे टीले और चट्टानों पर तो वर्षा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे रूखे के रूखे, प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में देवता की, सिद्ध पुरुषों की सामथ्र्य का जितना महत्व है, उससे अधिक शिष्य की श्रद्धा का है। द्रोणाचार्य को शरीर और मन समेत नौकर रख कर भी कौरव वह न सीख सके, जो एकलव्य ने दूर रहकर भी मिट्टी की प्रतिमा के माध्यम से उपलब्ध कर लिया था। यह श्रद्धा का ही चमत्कार है। आत्मिक प्रगति में इसको आधारभूत कारण माना गया है। मंत्र इसी के आधार पर फलित होते हैं। देवता इसी सीढ़ी के सहारे स्वर्ग से उतर कर साधक के जीवन में प्रवेश करते और कृत-कृत्य बनाते हैं। इस श्रद्धा को जो जिस मात्रा में जमा सका, समझना चाहिए कि उसके लिए अध्यात्म विभूतियाँ उपलब्ध करने का स्वनिर्मित राजमार्ग मिल गया। श्रद्धा विहीनों के द्वारा मंत्र को बकवास और देवता को खिलवाड़ से अधिक और कुछ नहीं समझा जा सकता। इसमें गुरु वरण का श्रद्धा-अभ्यास ही प्रथम सोपान है।
इस रहस्य को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने प्रबल प्रयत्न किए है। यहाँ तक कि गुरु की गोविन्द से भी बढ़कर माना है। उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपमा दी है। इतने पर भी क्यों उसके लिये उत्साह नहीं उठता ? इसका एक ही कारण है कि वैसे समर्थ व्यक्तित्वों का आज एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही हो चला है, जिन्हें गुरु के रूप में वरण किया जा सके।
जिनकी जीवनचर्या में तपश्चर्या आदि से अन्त तक गुंथी नहीं, है, जिसके अध्ययन-अध्यवसाय की ज्ञान-सम्पदा अगाध नहीं है जो लोकमंगल के लिए आत्म-विजर्सन कर सकने में समर्थ नहीं हो सके जिनका चरित्र दूध जैसा धवल नहीं है, उनमें अपनी गाड़ी आप घसीट सकने तक की तो सामथ्र्य होती नहीं, अपने लिए जिस-तिस के सामने पल्लू पसारते फिरते हैं फिर वे अन्यान्यों की, शिष्यों की सहायता कर सकने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं ? ऐसों का आश्रय लेने पर लोभी गुरु लालची चेला वाली उक्ति ही चरितार्थ होती है और एक दूसरे को दोनों नरक में ठेलमठेला का फलितार्थ उत्पन्न करते हैं। जहाँ ऐसी स्थिति हो, वहाँ गुरुता के अभाव में शिष्य की श्रद्धा कैसे उमगे और घनिष्ठता स्थापित करने का सहारा और विश्वास किस आधार पर पनपे?
आज गुरु-शिष्य के क्षेत्र में असमर्थता और अश्रद्धा का बोल बाला है। "गुरुशिष्य अन्ध बधिर कर लेखा, एक न सुनइ, एक नहि देखा” की उक्ति ही इन दिनों चरितार्थ होती दिखती है। तथाकथित गुरु यह नहीं देखते कि शिष्य का जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है और तथाकथित शिष्यों को गुरु के निर्देश सुनकर आचरण करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती हैं। यही कारण है कि वह पुण्य-परम्परा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। लकीर पीटने के लिए कहीं कुछ कर्मकाण्ड होते भी हैं तो उनके बीच वह निर्वाह बनता नहीं, जिसमें गुरु भी यशस्वी होते हैं एवं शिष्य भी मनस्वी बनते हैं। उस सुयोग के फलस्वरूप ही ऐसा वातावरण बन सकता है, जिससे समूचे वातावरण में सत्प्रवृत्तियों का मलयानिल प्रवाहित होता रहे। इन दिनों मन्त्र और देवता, अपनी शक्ति खो चले हैं क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति का कल्पवृक्ष, गुरुशिष्य परम्परा के आधार पर विनिर्मित होने वाली सिचाई से वंचित रहकर कुम्हलाता, मुरझाता और सूखता चला जा रहा है।
यदि आत्म-विज्ञान का महत्व समझ जाय और उस दिशा में बढ़ने का साहस किया जाय तो साथ-साथ इतना और भी होना चाहिए। कि श्रद्धा विश्वास बनाये रहने, उसे बढ़ाते चलने वाले आधार को भी किसी प्रकार उपलब्ध कर लिया जाय। किसी निर्धारित नियुक्त गुरु के अभाव में अपनायी गई गतिविधियों के संबंध में संशय ही बना रहता है। व्यक्तियों के कथनों के और ग्रन्थों के उल्लेखों में असाधारण अन्तर और भारी मतभेद पाया जाता है। उनकी जितनी अधिक टटोल की जाय, उतना ही सन्देह बढ़ेगा। किसे-सही किसे गलत माना जाय इसमें तर्क भी कुछ काम नहीं देते। श्रद्धा को संशय खा जाता है, फलत: अनिश्चय की मन: स्थिति बनी रहती है। एक क्रम अपनाने, दूसरे को छोड़ने का सिलसिला चलता रहता है, फलत: दिग्भ्रान्त की तरह आगे बढ़ते-पीछे हटते, छोड़ते, चक्कर काटते, समय गुजरता है। थकान और खीझ के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इस चक्रव्यूह से निकलना उन्हीं के लिए संभव हो सकता है, जो आत्मिक प्रगति की दिशा में सुनिश्चित विधि-व्यवस्था अपना कर, उसे श्रद्धा एवं दृढ़ता के साथ अविच्छिन्न रूप से अपनाये रह सकें। इसके लिए फिर गुरु-वरण की आवश्यकता, अपनी अनिवार्यता सिद्ध करती हुई सामने आ खड़ी होती है।
सदगुरु की तलाश प्रत्येक श्रेयार्थी साधक को करनी चाहिए। इस पुण्य प्रयोजन के लिए प्रज्ञा अभियान के संचालन तंत्र पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीया माता जी का चयन किया जा सकता है। वे इन दिनों प्रज्ञा परिजनों की तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए युग सन्धि में आत्मशक्ति के व्यापक उत्पादन का महत्व समझते हुए ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं के सृजन में निरत हैं। सूक्ष्म व कारण शरीर से वे स्वयं तथा प्रत्यक्ष रूप में वंदनीया माता भगवती देवी सबकी परोक्ष सहायता करने में पूर्ण सक्षम हैं।
भगवान राम के दो गुरु थे, एक गुरु - वशिष्ठ दूसरे, विश्वामित्र। वशिष्ठ कुल-गुरु थे, योगवाशिष्ट उन्हीं ने पढ़ाया था।
किन्तु बला और अतिबला विद्याएँ प्राप्त करने के लिए उन्हें यज्ञ रक्षा के बहाने विश्वामित्र आश्रम में रहना पड़ा। जो वहाँ सीखा जा सका, वह वशिष्ठ की सीमा से बाहर था। बला और अतिबला सावित्री-गायत्री रूपी भौतिकी एवं आत्मिकी को कहते हैं। प्रथम के द्वारा उन्होंने असुरों को परास्त किया और दूसरे के माध्यम से राम राज्य की स्थापना वाले और कठिन उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर सकने में समर्थ हुए।
एक व्यक्ति के कई गुरु होने में कोई दोष नहीं। पूज्य गुरुदेव को गायत्री मंत्र और उपनयन महामना मालवीय जी ने प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त हिमालय से युगान्तरीय चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रज्ञात्मा को वे सूक्ष्म गुरु मानते और उन्हीं के संकेतों पर अपनी गतिविधियों का ताना-बाना बुनते हैं। ऐसा हर कोई कर सकता है। दत्तात्रेय जी के चौबीस गुरुओं की बात सर्वविदित है। प्राचीनकाल में भी ऐसा होता रहा है। इसकी असंख्य साक्षियाँ विद्यमान हैं।
समर्थ सत्ता के साथ जुड़ जाने पर किसी भी सामान्य को असामान्य बनने का अवसर मिल सकता है। बिजलीघर के साथ सम्बन्ध जुड़ जाने पर ही, बल्ब, पंखे, हीटर, कूलर आदि उपकरण अपना काम करते हैं। टंकी के साथ जुड़े रहने पर नल तब तक पानी देता रहता है, जब तक टंकी खाली नहीं हो जाती। चन्द्रमा, सूर्य की चमक से चमकता है। हिमालय से जुड़ी हुई नदियों का जल सूखता नहीं। पुलिस का अदना सा सिपाही भी अपने को शासन तंत्र का प्रतिनिधि मानता और गर्दन ऊंची उठाकर चलता है। यह सम्बन्ध जुड़ने की बात हुई। समर्थता के साथ जुड़ जाने पर असमर्थता भी समर्थता में बदल जाती है। गन्दे नाले का पानी गंगा में मिल जाने पर गंगा जल की तरह सम्मान पाता है। पेड़ से लिपटने पर बेल उतनी ही ऊंची उठ जाती है, जबकि वह सामान्यतया अपने बल-बूते जमीन पर ही रेंगती है। अशिक्षित और निर्धन घर की बेटी भी किसी विद्वान या सम्पन व्यक्ति की पत्नी बन जाती है तो उसका सम्मान एवं वैभव पति जितना ही हो जाता है।
सामान्यतया यह उदाहरण भक्त और भगवान के बीच संबंध स्थापित होने के सन्दर्भ में दिये जाते हैं पर उन्हें आँशिक रूप से गुरु-शिष्य के मध्य समर्थता और श्रद्धा के संयोग से उत्पन्न घनिष्ठता पर लागू किया जाय, तो वहां भी उदाहरण सटीक बैठ जाता है। गुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन में देवता देवत्व प्राप्त कर सके और शुक्राचार्य के अनुग्रह से असुरों को भौतिक सिद्धियाँ हस्तगत करने का अवसर मिला। यह सब वे दोनों, मात्र अपने बल-बूते नही प्राप्त कर सकते थे। गुरु का मार्गदर्शन एवं शक्ति-अनुदान तथा शिष्यों की श्रद्धा एवं पुरुषार्थ के योग से ही चमत्कारी परिणाम प्रकट होते हैं।
प्राचीन काल में गुरु परम्परा भी वंश परम्परा की तरह गौरावान्वित होती थी। वंश के गोत्र, पूर्वजों से ही नहीं चलते, वरन् गुरु परम्परा से भी चलते हैं। ऋषियों के गोत्र हर जाति वर्ग में पाये जाते हैं। हो सकता है कि उनके पूर्वज भी ऋषि रहे हों और वंश परम्परा के अनुसार उनके गोत्र चले हों। हो सकता है, वे उनके गुरु रहे हों और गुरु परम्परा को ही वंश परम्परा का प्रतीक मान कर उनका गोत्र अपनाया गया हो। यहाँ प्रतीत होता है कि पूर्वजों में, दोनों पक्षों को समान महत्व एवं सम्मान दिया गया है ! तराजू को दो पलड़ों में से एक पर माता-पिता दोनों को, और दूसरे पर अकेले गुरु को रख कर तौला जाता रहा है। कारण स्पष्ट है, शरीर से सम्बन्धित भौतिक साधनों को उपलब्ध कराने में माता-पिता का जितना योगदान है, आत्म कल्याण के लिए व्यक्तित्व में प्रखरता उभारने वाले गुरु का महत्व उनसे-किसी प्रकार कम नहीं है। यह सरकस में विलक्षण काम करने वाले जानवरों को साधने से भी कठिन काम है।
तत्वत: यह मानवी विद्युत को हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया हैं। आग के समीप बैठने से गर्मी आती है, ठंडे तहखाने, बर्फखाने में बैठने से कंप-कंपी छूटती है। चन्दन वृक्ष के नीचे उगे झाड़-झंखाड़ भी सुगंध देने लगते हैं। स्वाति-बूंद का सहयोग पाकर सीप मोती उगलने लगती है। यह समर्थ सान्निध्य का प्रभाव है, जिसकी तुलना पारस, कल्पवृक्ष और अमृत से की जाती है और इसके समीप पहुँचने, घनिष्ठ बनने, आत्मसात् करने का परिणाम कायाकल्प जैसा होता है। इन उदाहरणों को गुरु-शिष्यों के मध्य प्रतिष्ठापित घनिष्ठता, आत्मीयता एवम् प्रत्यावर्तन श्रृंखला के साथ जोड़ा जा सकता है।
यों हर मनुष्य में एक विद्युत धारा विद्यमान है, पर महामानवों में यह प्राणशक्ति अपेक्षाकृत कहीं अधिक होती है। उसे तेजोवलय के रूप में देखा और अनुभव किया जा सकता है। वह अपने क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का प्रभाव छोड़ती है। समीपता-घनिष्टता होने पर महाप्राणों, सशक्तों का प्राण-प्रवाह, न्यून प्राण वालों की ओर अनायास ही चल पड़ता है। प्रत्यक्ष-कथनीपरक न होने पर भी, परोक्ष रूप से प्राणवानों के व्यक्तित्व से निकलने वाली ऊर्जा, अपने समीपवर्ती प्राणियों और पदार्थों को प्रभावित करने लगती है। ऋषि आश्रमों के समीपवर्ती क्षेत्र में सिंह एवं गाय वैर-भाव भूलकर एक घाट पानी पीते और स्नेह-सद्भाव का परिचय देते रहे हैं। वहाँ वे अपने सहज स्वभाव को भूल जाते हैं। यही सब कुछ दीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होता है।
दीक्षा देने का अधिकार मात्र महाप्राणों की है। जिसके पास कुछ वैभव है, वही दूसरे को दान दे सकेगा। जो स्वयं ही खाली हाथ है और याचना पर निर्वाह करता है, उससे कोई अनुदान मिलने की आशा करना व्यर्थ है। दीक्षा दे सकने वाले व्यक्तित्व उपलब्ध होना कठिन है। नाटकीय खिलवाड़ करना हो, तो कोई भी व्यक्ति आपस में गुरु-शिष्य का अभिनय-प्रहसन कर सकते हैं किन्तु पात्रता और यथार्थता न होने पर वह बात बनती नहीं, जिसकी अपेक्षा की गयी है। इसलिए शास्त्रकारों ने यह सम्बन्ध स्थापित करते समय गुरु की समर्थता और शिष्य की श्रद्धा, पात्रता को भलीप्रकार ठोंक बजा लेने की बात कही है अन्यथा मात्र लकीर पीट लेने से बात बनेगी नहीं। निर्धारित अनुशासन के अनुसार चलने पर अनुपम लाभ मिलना सुनिश्चित है।
शास्त्रकारों ने गुरु विहीन की निन्दा की है। कहा गया है कि उसके हाथ से किया श्राद्ध-तर्पण पितरों तक नहीं पहुँचता। कहीं तीर्थफल न मिलने की बात कही है, कहीं उसके हाथ का जल न पीने जैसी प्रताड़ना का उपाय सुझाया गया है। यह कथोपकथन अत्युक्तिपूर्ण, आवेशग्रस्त अथवा आलंकारिक दीखते हैं, तो भी उनके पीछे यह प्रेरणा-प्रतिपादन तो है ही, कि माता-पिता का परिचय दे सकने की तरह हर व्यक्ति को अपने गुरुद्वारे का भी परिचय देना चाहिए।
माता का पता न हो, तो यह समझा जायेगा कि वह अनुचित उत्पादन रहा होगा और लुक-छिपकर कहीं से कहीं पहुँचाया गया होगा। पिता का नाम पता न हो, तो भी माता पर कुलटा होने का आक्षेप आता है और संतान पर अवैध होने का लांछन लगता है। सुसंस्कारिता संवर्धन के लिए गुरु वरण का विधिवत् प्रयास हुआ नहीं किया नहीं गया, तो यह एक कमी है, जिसे दूर करने के लिए शास्त्रकारों ने हर किसी को प्रोत्साहित किया है, इसके लिए लाभ और हानि के दोनों ही पक्ष सुझाये जाते हैं। लगता है 'निगुरा' शब्द निन्दाबोधक शब्दावली में एक गाली की तरह प्रयुक्त हुआ है। जो हो, शास्त्र प्रतिपादनों में इस तथ्य को और उतेजित शब्दों में प्रतिपादित कर गुरु की आवश्यकता समझायी गई है। उसकी पूर्ति की ही जानी चाहिए। दीक्षा और यज्ञोपवीत का परस्पर सम्बन्ध है। यज्ञोपवीत द्विजत्व का-दूसरे जन्म का प्रतीक है। हर माता के गर्भ से नर पशु ही जन्म लेता है, इसे सुसंस्कारी बनाने की प्रक्रिया समर्थ गुरु द्वारा ही सम्पन्न होती है। खदान से मिट्टी मिली धातुएँ ही निकलती हैं। उनका परिशोधन भट्टी में तपाने की प्रक्रिया द्वारा ही सम्पन्न होता है। न तपाने पर वे अनगढ़ ही बनी रहेंगी। मनुष्य के सम्बन्ध में भी यही तथ्य काम करते हैं।
अभिभावक संतान के शरीर उत्पादन एवं परिपोषण भर की प्रक्रिया सम्पन्न कर सकने की स्थिति में होते हैं। सुसंस्कारिता, प्रखरता से संतान को सम्पन्न बनाने के लिए किसी ऐसे महाप्राणों का आश्रय लेना पड़ता है, जो इस दृष्टि से समर्थ हों।
गुरुकुलों में रहकर शिक्षा और प्रखरता उपलब्ध की जाती है। जब यह निकटता संभव नहीं होती, तो पत्राचार विद्यालय, रेडियो पाठ्यक्रम, टेलीफोन वार्ता अथवा समय-समय के वार्तालाप द्वारा भी विचार-विनिमय का, आदान-प्रदान का उपक्रम चलाना पड़ता है। गुरु-शिष्य की दीर्घकालीन समीपता संभव न होने पर अन्यान्य सूत्रों से भी यह संबंध गतिशील रखा जा सकता है। मुर्गी अपने अण्डे को पेट के नीचे रखकर सेती, किन्तु कछुई रेती में अंडे देकर अपने प्राण-प्रवाह से सेती और पकाती रहती है। यदि इसी बीच कछुई मर जाय, तो रेती में छोड़ा गया अंडा भी सड़ जायेगा। ऐसा आदान-प्रदान गुरु-शिष्य के बीच चलता है। राम-विश्वामित्र के कृष्ण-संदीपन के गुरुकुल में पढ़ते थे, किन्तु जब पढ़ने की स्थिति न रही और अलग रहने का अवसर आया, तो भी वह आदान-प्रदान प्रत्यावर्तन सूत्र यथावत् स्थिर रहा। माध्यम बदल गए, तो भी समर्थ मार्गदर्शन और अनुदान-प्रतिदान की श्रृंखला टूटी नहीं। यही क्रम स्नेह-सूत्रों के जुड़े रहने पर अन्यत्र भी चलता-रह सकता है।
साधना से सिद्धि की चर्चा से अध्यात्म शास्त्र भरे पड़े हैं। हर साधना का माहात्म्य एवं विधि-विधान विस्तारपूर्वक लिखा गया है। पग-पग पर यह स्पष्टीकरण किया गया है कि इस पुस्तक को पढ़कर मनमाने ढंग से आरम्भ न कर दिया जाय। गुरु की सहायता से अपनी पात्रता के सम्बन्ध मंह जाँच-पड़ताल होने के उपरान्त ही क्या करना है, किस प्रकार करना है, इसका निर्धारण कराया जाय। चिकित्सा पुस्तकों में हररोग का निदान उपचार का विस्तृत उल्लेख रहता है। उसी प्रकार विक्रेता के यहाँ हर प्रकार की औषधियाँ तैयार मिलती हैं। इतने पर भी चिकित्सक के परामर्श एवं निर्देशन की आवश्यकता रहेगी ही। कोई रोगी निदान के उपचार के लिए स्वेच्छापूर्वक निर्णय लेने लगे, तो उससे भूल एवं हानि होने की आशंका रहेगी। इसी प्रकार साधना के संदर्भ में भी यही उपयुक्त समझा जाना चाहिए। जो भी आकर्षक लगे, उसी को करने लगना अनुचित है। अपनी आन्तरिक स्थिति का पर्यवेक्षण स्वयं नहीं हो पाता। अपनी आँख तक जब अपने को नहीं दिखाई देती, उसके लिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है, तो फिर अन्तःक्षेत्र का विश्लेषण-पर्यवेक्षण अपने आप कैसे संभव हो सकेगा और उसके बिना सही उपचार कैसे बने ? यहाँ चिकित्सक की सूक्ष्म बुद्धि एवं अनुभवशीलता से लाभ उठाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। यही कारण है कि साधनाएँ करने-बढ़ाने के लिए निर्धारित मार्गदर्शक का परामर्श, संरक्षण, सहयोग एवं अनुग्रह-अनुदान उपलब्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। वह न मिले, तो फिर समझना चाहिए कि गाड़ी रुक गई और सफलता की सम्भावना धूमिल हो गई। यही कारण है कि “जो सद्गुरु सो दीक्षा पावें-सो साधन को सफल बनावें” की लोकोक्ति में बहुत कुछ सार सन्निहित दीखता है।
दो जून १९९० को परम्पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ। अपने अन्तिम सन्देश में उन्होंने कहा था कि जो कार्य वे स्थूल शरीर से नहीं कर सके अब कारण शरीर से सम्पन्न करेंगे। विश्व कुण्डलिनी जागृत करेंगे, जिससे स्वाति नक्षत्र के चमकने पर मोती, वंशलोचन, मणिमुक्ता बनने का सौभाग्य उन सभी आत्माओं को मिलेगा जो उनकी कारण सत्ता से जुड़ेंगे। यह क्रम इस शताब्दी के अंत तक निरन्तर चलता रहेगा।
|
|||||