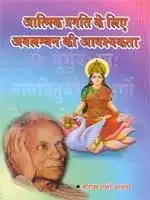|
नई पुस्तकें >> आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकता आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकताश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकता
श्रद्धा का आरोपण - गुरू तत्त्व का वरण
अध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। एक ही मंत्र, एक ही साधना पद्धति एवं एक ही गुरु का अवलम्बन लेने पर भी विभिन्न साधकों की आत्मिक प्रगति की गति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। इस भिन्नता का मूल कारण है - श्रद्धा, समर्पण, इष्ट के प्रति ऐसा लगाव कि दोनों एक रूप हो जाएँ। जहाँ श्रद्धा नहीं होती, वहाँ सभी उपचार बाह्य कर्मकाण्डादि निष्प्राण बने रहते हैं। गीताकार ने ठीक ही कहा है- श्रद्धामये यं पुरुषः यो यच्छ स एव सः। अर्थात् जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह स्वयं भी वही अर्थात् उसके अनुरूप बन जाता है, ढल जाता है। शिष्य और गुरु के मध्य जो श्रद्धा के सूत्रों का सशक्त बन्धन रहता है, वही लक्ष्य तक पहुँचाने में, अध्यात्म क्षेत्र की समस्त विभूतियाँ हस्तगत कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
जिस श्रद्धा के सहारे भीरा ने गिरधर गोपाल को साथ रहने के लिए विवश किया, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी से बनी प्रतिमा को असली द्रोण से भी अधिक समर्थ बनाया था, रामकृष्ण परमहंस ने पत्थर की प्रतिमा को जीवन्त काली जैसा भोग ग्रहण करने के लिए सहमत कर लिया था, वह श्रद्धा तत्व ही आत्मिक प्रगति का आधारभूत कारण है। इसे उपार्जित करने के लिए जीवन्त गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। व्यायामशाला में प्रवेश करके ही बलिष्ठ पहलवान बनने की बात सधती है। डम्बलों /मुगदरों के सहारे भुजदण्ड मजबूत किये जाते हैं। श्रद्धा संवर्धन के लिए गुरु - प्रतीक को सदाशयता की प्रतिमा मानकर चलना होता है। यह भाव निर्धारण प्राय: वैसा ही है जैसा कि मिट्टी के ढेले से कलावा लपेट कर उसे श्रद्धा -आरोपण द्वारा साक्षात् गणेश जैसा समर्थ बनाया जाता है।
जीवन में हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए शिक्षण प्रक्रिया एवं शिक्षक के अवलम्बन की आवश्यकता पड़ती है। अभिभावकों को विशेष रूप से माता की यह भूमिका सर्वप्रथम निभानी व बच्चे में सुसंस्कारिता समाविष्ट करनी होती है। आत्मिक प्रगति की जब भी चर्चा होती है, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए "सद्गुरु” का आश्रय लिये जाने की बात कही जाती है। जन समुदाय की प्रवृत्तियाँ लोक प्रचलन के अनुरूप होने के कारण यह कार्य एक प्रकार से प्रवाह के विरुद्ध चलने के समान है। जैसाकि अधिकांश सोचते व करते रहते हैं उसी का अनुकरण सामान्य स्तर के लोग प्रायः करते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए भिन्न स्तर का सोच अपनाने के लिए व तदनुरूप अपने क्रिया-कलापों को ढालने के लिए एक सशक्त अवलम्बन की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य किन्हें में समर्थ आदर्शवादी, श्रेष्ठ स्तर के व्यक्तित्वों के साथ घनिष्ठता स्थापित करने पर ही बन पड़ता है। इसी व्यवस्था को गुरुवरण या गुरु दीक्षा कहते हैं। गुरु दीक्षा अर्थात् गुरु के रूप में एक ऐसी सत्ता को सम्पूर्ण समर्पण जो उत्कृष्टताओं का, सत्प्रवृतियों का समुच्चय हो। जिसके पद चिन्हों पर चलकर, जिसके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन को अपनाकर अपना जीवन भी वैसा ही श्रेष्ठतम व सार्थक बनाया जा सके। यह समर्पण सघन श्रद्धा के माध्यम से ही बन पड़ता है।
क्या किसी एक गुरु का, सोचसमझ कर, चयनकर, निर्धारण कर गुरुवरण करना आवश्यक है, यह कार्य क्या अनेकों सुयोग्यों से सम्पर्क स्थापित करते रहने पर सम्भव नहीं है। इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए पी.एच.डी. करने वालों, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स की परीक्षा देने वालों, वकीलों तथा डाक्टर बनने के बाद इण्टर्नशिप की प्रक्रिया से गुजरने वालों की सुव्यवस्थित अभ्यास की विधि-व्यवस्था पर दृष्टि डालनी होगी। निश्चित "गाइड” अथवा प्रशिक्षण तंत्र के माध्यम से ही उपरोक्त प्रयोजन पूरे होते हैं। निश्चित निर्धारण के बाद एक सुनिश्चित उतरदायित्व भी बनता है एवं उस सीमा-बंधन के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया की समग्रता की सुनिश्चितता भी रहती है।
अनिश्चय की दशा में जहाँ-तहाँ से चंचु प्रवेश करते रहने से उपर्युक्त कार्यों में से एक भी नहीं सधता। इसलिए परम्परा ऐसी ही बनायी गई है कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विधिवत् एवम् निर्धारित प्रशिक्षण हो, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, एडवोकेट, डॉक्टर आदि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की अवधि में भी किन्हीं विशिष्टों के साथ जुड़े रहने की विधि-व्यवस्था है। इस मर्यादा का उल्लंघन कर, जहाँ-तहाँ से जब तब शिक्षण प्राप्त करते रहने की व्यवस्था करने से भी बात बनती नहीं। यों अन्यों से पूछताछ करके, तदविषयक अनेकानेक पुस्तकें पढ़कर, अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करते रहने पर कोई रोक नहीं हैं, फिर भी निश्चित उत्तरदायित्व में बँधने की प्रचलित विद्या का उल्लंघन करने, उसे निरर्थक मानकर उपेक्षा करने से भी बात बनती नहीं।
अध्यात्म क्षेत्र में भी वही बात इसी तरह लागू होती हैं। आत्मिक क्षेत्र की प्रगति भौतिक प्रगति से कम नहीं, अधिक ही अभीष्ट है। आत्मिक प्रगति से ही व्यक्ति को अनगढ़ से सुगढ़ बनने एवं अपने व्यक्तित्व की गरिमा को असाधारण रूप से बढ़ाने का अवसर मिलता है। उसकी जो फलश्रुतियाँ हैं, अपरिमित उपलब्धियाँ हैं उन्हें देखते हुए गुरु का आश्रय लेना हर दृष्टि से अनिवार्य माना जाना चाहिए।
भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह तीन देवता धरती के माने गये हैं। माता, पिता और गुरु की तुलना उन त्रिदेवों से की गयी है। माता ब्रह्मा क्योंकि वह बालक को पेट में रखती और अपना शरीर काट कर, बालक का शरीर बनाकर जन्म देती है। पिता को विष्णु माना गया है, क्योंकि वह बालक के भरण-पोषण की, शिक्षा, करके उसे समर्थ बनाता है। इस प्रकार पिता विष्णु ठहरता है। गुरु की गरिमा इन दोनों से ऊँची है। माता-पिता तो मात्र शरीर का ही सृजन, और पोषण करते हैं जबकि गुरु आत्मा में व्यक्तित्व में सुसंस्करिता का आरोपण करके, उसे इसी जन्म में दूसरा जन्म प्रदान करता है। द्विजत्व एक उच्चस्तरीय संस्कार है, जिसे यज्ञोपवीत दीक्षा के साथ कर्मकाण्ड के रूप में सम्पन्न किया जाता है। यह प्रतीक पूजा हुई। वस्तुत: इस कृत्य के पीछे गुरु वरण की भूमिका ही काम करती है। माता पिता के सहयोग से मानव शरीर की उपलब्धि जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक गुरु महिमा की सहायता नर-पशु का, नर-नारायण बनने की संभावना के सम्बन्ध में समझी जा सकती है। आत्मिक क्षेत्र का परिशोधन परिष्कार कर सकने वाली गुरु गरिमा को वस्तुत: मूर्तिमान शिव कहा जा सकता है। इसी रूप में वंदना अभ्यर्थना के स्तवन छद भी बने और गाये गये हैं।
गुरुजनों के सान्निध्य अवलम्बन से कितने ही सामान्य व्यक्तियों को असामान्य बनने का अवसर मिला है। बुद्ध के अनुग्रह से हर्षवर्धन, अशोक, आनन्द, कुमारजीव जैसे कितनों को महानता के उच्च शिखर तक पहुँचने का सुयोग मिला। अंगुलिमाल, अम्रपाली जैसे कितने ही हीन व्यक्ति महामानव के रूप में कायाकल्प कर सकने का सौभाग्य अर्जित कर सके। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी की, विरजानन्द और दयानन्द की आत्मिक घनिष्ठता यदि बन न पड़ी होती, तो यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि दोनों ही पक्ष घाटे में रहते। विशेषतया इन युग्मों से सम्बन्धित शिष्य पक्ष को ही अपेक्षाकृत अधिक घाटे में रहना पड़ता। कल्पना की जा सकती है कि यदि स्वराजेन्द्र बाबू, पटेल नेहरू, राजगोपालाचार्य विनोबा आदि की गाँधी जी के साथ घनिष्ठता न जुड़ी होती, वे अपना-अपना अभ्यस्त ढर्रा अपनाये रहे होते, तो निश्चय ही दोनों पक्षों को उतना गौरवान्वित होने का अवसर न मिलता जितना कि संभव हो सका। संभव है उस स्थिति में गाँधी जी अपनी तपश्चर्या को भगीरथ दधीचि, आदि की तरह एकाकी भी चलाते रहते और महानता के उच्च शिखर पर पहुँच जाते किन्तु उनसे सम्बधित अगणित व्यक्तियों की स्थिति सर्वथा भिन्न होती, वे कामकाजी लोगों की तरह मात्र अपना निर्वाह ही चलाते एक छोटे दायरे में ही दिन गुजारते और धनी-निर्धन रहकर जिन्दगी के दिन पूरे करते। उन्हें यह सौभाग्य न मिल पाता जो गाँधी जी की छत्र-छाया का आश्रय लेने पर मिल सका। यह श्रेष्ठता के सान्निध्य, सामीप्य, अवलम्बन का ही चमत्कार है कि साधारण व्यक्ति असाधारण बनता देखा जाता है। गुरुवरण की आवश्यकता व महत्ता इसीलिए बतायी जाती रही है। श्रद्धा इस प्रक्रिया का प्राण है। इतना समझ लेने पर आत्मिक प्रगति के इच्छुकों को वह राजमार्ग मिल जाता है, जिस पर चलकर वे अनुग्रह -अनुदानों से लाभान्वित होते हैं।
|
|||||