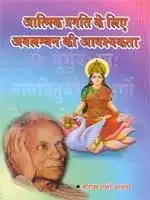|
नई पुस्तकें >> आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकता आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकताश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
आत्मिक प्रगति के लिए अवलम्बन की आवश्यकता
इष्टदेव का निर्धारण
भौतिक प्रगति के लिए भौतिक पुरुषार्थ करने पड़ते हैं और आत्मिक प्रगति के लिए चेतना का स्तर उठाने और प्रखरता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। पेट में भूख लगती है, तो आहार उपार्जन करने के लिए दौड़-धूप करना आवश्यक हो जाता है। शरीर में समर्थता बढ़ने पर कामुकता की तरंगें उठती हैं और साथी ढूँढ़ने, परिवार बसाने का मानसिक ताना-बाना बुना जाने लगता है। प्राणि-जगत का अस्तित्व और पराक्रम, इन्हीं पेट-प्रजनन के दो गति चक्रों के सहारे सरलतापूर्वक लुढ़कता रहता है। आत्मिक प्रगति का प्रसंग दूसरा है। चौरासी लाख योनियों के संगृहीत स्वभाव-संस्कार मनुष्य जीवन के उपयुक्त नहीं रहते, ओछे पड़ जाते हैं। बच्चे के कपड़े बड़ों के शरीर में कहाँ फिट होते हैं ? मानव जीवन की सार्थकता के लिए जिस सद्भाव से अन्त:करण को और सत्प्रवृत्तियों से शरीर को सुसज्जित करना पड़ता है, वे पूर्व अभ्यास एवं प्रभावी प्रचलन न होने के कारण कठिन पड़ते हैं। वह सहज सुलभ नहीं, वरन् प्रयत्न-साध्य हैं। नीचे गिरने में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का क्रम ही निरन्तर सहायता करता रहता है, पर ऊंचा उठने के लिए विशेष साधन जुटाने होते हैं। आन्तरिक अभ्युत्थान के इसी पराक्रम को साधना कहते हैं।
साधना मार्ग पर चलने के लिए प्रथम चरण 'इष्ट निर्धारण' का उठाना पड़ता है। इष्ट अर्थात् लक्ष्य। प्रगति के लिए आन्तरिक महत्त्वाकांक्षा स्वाभाविक है, पर उसका स्वरूप भी तो निश्चित होना चाहिए। उमंगें असीम हैं, उनकी दिशा-धारा भी अनेकों हैं। पानी पर उठने वाली लहरों की तरह महत्त्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं। एक के बाद दूसरी लहरें उठती हैं और हवा के झोंके के साथ अपनी दिशा-धारा बदलता रहती हैं। प्रवाह दिशा धारा न हो, तो पराक्रम अस्त-व्यस्त रहेगा। किसी लक्ष्य तक पहुँच सकना संभव ही न हो सकेगा। दिशाविहीन भगदड़ से मात्र थकान और निराशा ही हाथ लगती है। कस्तूरी के हिरण को अभीष्ट स्थान का पता नहीं होता, फलतः वह भटकता और थकता-खिन्न होता रहता है। मानवी अन्तरात्मा की भूख, प्रगति की दिशा में अग्रसर होने की है, महत्त्वाकांक्षाओं के उभार इसी का परिचय देते हैं। आत्मिक प्रगति का कोई निश्चित लक्ष्य एवम् स्वरूप सामने न रहने से वह कायिक लिप्साओं की ओर ही लुढ़कने लगती है, है। इस स्तर की सफलताएँ काया को भले ही कुछ सुख-सुविधाएँ प्रदान कर सकें, अन्त:करण की उच्चस्तरीय प्रगति में इससे तनिक भी सहायता नहीं मिलती। अनियंत्रित भौतिक महत्वाकांक्षाएँ आतुर होकर कुकर्म करके भी वैभव उपार्जन में जुट पड़ती हैं और उलटे अध:पतन एवं विक्षोभ का कारण बनती हैं।
साधक का कोई न कोई इष्ट देव होता है, साधना का विधि-विधान उसी के अनुरूप चलता है। यों उपास्य केवल एक ही है-दिव्य जीवन, किन्तु उसके लिए पुरुषार्थ करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि उपासनात्मक उपचारों के सहारे बनती हैं। दिव्य जीवन की चरम परिणति ही पूर्णता है। इसी स्थिति को स्वर्ग एवं मुक्ति की प्राप्ति कहते हैं। आत्म-साक्षात्कार एवं ईश्वर-दर्शन भी यही है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसे साधना-विधान के रूप में अपनाना पड़ता है। साधना में शिक्षा और प्रेरणा का समावेश होता है, फलत: उसकी प्रतिक्रिया जीवनोत्कर्ष के रूप में प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है।
प्रगति के किस बिन्दु तक पहुँचना है, इसका सुदृढ़ पूर्वनिश्चय होना आवश्यक है। भव्य भवन बनाने वाले, सर्वप्रथम अभीष्ट निर्माण के नक्शे या मॉडल बनाते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए किस मार्ग से जाना है-किस स्तर के साधन जुटाने हैं इसके लिए कितने ही प्रकार के निर्धारण अपनाये जाते रहे हैं। इन्हें इष्टदेव कहते हैं। राम भक्त बनने के लिए हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सविता को इष्ट बनाने की परम्परा है। इस निर्धारण से मन को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने और तदनुरूप प्रयास करने, साधन जुटाने का मार्ग मिल जाता है। इस निर्धारण से न केवल प्रयास को दिशा मिलती है, वरन् उसी स्तर के अन्तःक्षेत्र की प्रसुप्त शक्तियाँ भी जगने लगती हैं। साथ ही परब्रह्म के शक्ति भण्डार में से उसी स्तर की अनुग्रह-वर्षा भी अनायास ही आरम्भ हो जाती है। आकांक्षाएँ आवश्यकता बनती हैं, आवश्यकता पुरुषार्थ की प्रेरणा जगाती है। प्रेरणा भरे पराक्रम में प्रचण्ड चुम्बकत्व होता है। वह तीन दिशा में काम करता है। प्रथम व्यावहारिक गतिविधियों को अभीष्ट की प्राप्ति के अनुरूप बनाता है। द्वितीय प्रसुप्त क्षमताओं को जगाकर प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए अदृश्य आधार खड़े करता है। तृतीय दिव्य लोक के दैवी अनुदानों के बरसने का विशिष्ट लाभ मिलता है। तीनों के सम्मिलन से त्रिवेणी संगम बनता है।
इष्ट निर्धारण-प्रगति क्रम का सुनिश्चित आधार-पथ निश्चित करना है। ईश्वरीय सत्ता का मनुष्य में अवतरण 'उत्कृष्टता' के रूप में होता है। चिन्तन और चरित्र में उच्च-स्तरीय उमंगें उठने लगती हैं तथा उसी स्तर की गतिविधियाँ चल पड़ती हैं। उत्कृष्टता की उपासना ही ईश्वर उपासना है। यही उपास्य है। लक्ष्य भी इसी को बनाना पड़ता है। इष्टदेव का निर्धारण किस रूप में किया जाय, आज इस संदर्भ में अनेकों विकल्पों के जंजाल बने खड़े हैं। प्राचीनकाल में ऐसा न था। तत्वज्ञानी एक निश्चय पर पहुँचे थे और उन्होंने समस्त साधकों को वही निष्कर्ष अपनाने का परामर्श दिया था। भारतीय संस्कृति जिसे वस्तुः: विश्व संस्कृति कहा जाना चाहिए-साधना के संदर्भ में एक ही निश्चय पर पहुँची है कि आत्मिक प्रगति की साधना के लिए इष्ट रूप में गायत्री का ही वरण होना चाहिए।
गायत्री को इष्ट मानने की अनादि परम्परा है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने कमल पुष्प पर बैठकर आकाशवाणी द्वारा निर्देशित गायत्री उपासना की थी और सूजन की सामथ्र्य प्राप्त की थी। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। त्रिदेवों की उपास्य गायत्री रही है। देव गुरु बृहस्पति ने-दक्षिण मार्गी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने-वाम मार्गी साधनायें गायत्री के ही आत्मिक और भौतिक पक्षों को लेकर प्रचलित की-थी। सप्तऋषि, गायत्री की सप्त व्याहतियों के प्रतीक माने जाते हैं। राम-कृष्ण आदि अवतारों की इष्ट गायत्री रही है। इसी महामंत्र की व्याख्या में चारों वेद तथा अन्यान्य धर्मशास्त्र रचे गये हैं। दत्तात्रेय के चौबीस गुरु गायत्री के चौबीस अक्षर ही हैं। चौबीस योग, चौबीस तप प्रसिद्ध हैं। यह सभी गायत्री के तत्वज्ञान और साधना-विधान का विस्तार है। गायत्री गुरुमंत्र है। दीक्षा में उसी को माध्यम बनाया जाता है। हिन्दू धर्म के दो प्रतीक हैं-शिखा और सूत्र। दोनों ही गायत्री के प्रतीक हैं। गायत्री का ज्ञान पक्ष मस्तिष्क पर शिखा के रूप में और कर्म पक्ष कन्धे पर यज्ञोपवीत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। परम्परागत उपासना-विधि संध्या है। संध्या में गायत्री का समावेश अनिवार्य है। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि गायत्री अनादि धर्म परम्परा एवं अध्यात्म परम्परा का आधार भूत तथ्य है। उपासना में उसी का प्रयोग सर्वोत्तम है।
तत्त्वदर्शन की दृष्टि से गायत्री 'ऋतम्भरा प्रज्ञा' है। ऋतम्भरा अर्थात् विवेक संगत श्रद्धा। प्रज्ञा अर्थात् श्रेय साधक दूरदर्शिता। इस समग्र विवेकशीलता को गायत्री कह सकते हैं। इस बीज मंत्र का विशाल वृक्ष ब्रह्मविद्या है ! अध्यात्म का यह दार्शनिक पक्ष है। साधना प्रयोजन में इसी के विभिन्न उपचार योगाभ्यासों, तप साधनों एवं धर्मानुष्ठानों के रूप में प्रचलित हैं। इष्ट का-लक्ष्य का-उपास्य का निर्धारण, दिव्यदर्शियों ने गायत्री के रूप में गहन अध्यवसाय और अनवरत अनुभव-अध्यास के आधार पर किया है। वह प्राचीनकाल की ही तरह अपनी उपयोगिता यथावत् अक्षुण्ण रखे हुए है।
गायत्री सार्वभौम एवं सर्वजनीन है। इसे किसी देश, धर्म, जाति, सम्प्रदाय तक सीमित नहीं किया जा सकता है। भारत में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम भारतीय संस्कृति पड़ा है, पर उसकी कोई प्रक्रिया इस परिधि में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं रखी जा सकती। गायत्री भारतीय संस्कृति की आत्मा कही जाती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसी देश के निवासी या इसी धर्म के अनुयायी इसका उपयोग कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति वस्तुत: दैवी संस्कृति है, उसे मानवी संस्कृति कह सकते हैं। उसे देश, धर्म, जाति, भाषा सम्प्रदाय आदि के नाम पर अपने-पराये की विभाजन रेखा नहीं बनानी चाहिए।
ऋतम्भरा को इष्ट माना जाये, यही मानव जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। आत्मज्ञान-ब्रह्मज्ञान इसी को कहा गया है। विवेकशीलता-दूरदर्शिता यही है। न्याय और औचित्य इसी के प्रतिफल हैं। परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करने वाले जानते हैं कि वह मात्र मन:स्थिति की ही परिणति होती है। बुरी परिस्थितियों के लिए बुरी मन:स्थिति ही उत्तरदायी होती है। भीतर का परिवर्तन बाहरी परिकर में आश्चर्यजनक हेर-फेर उत्पन्न करता है। दरिद्रता, विपन्नता, विग्रह, विपत्ति एवं विभीषिकाएँ आन्तरिक निकृष्टता की ही प्रतिक्रियाएँ हैं। उत्कृष्ट चिन्तन के कारण बन पड़ने वाले आदर्श क्रिया-कलाप ही मनुष्य को आत्मसंतोष, जन-सम्मान, विपुल सहयोग एवं दैवी अनुग्रह की अनेक सम्पदाएँ एवं विभूतियाँ प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल की सतयुगी परिस्थिति और देवोपम मन:स्थिति की सुखद गाथा गाने वाले जानते हैं कि अतीत की गरिमा का एक मात्र आधार, उस समय अपनाया गया उत्कृष्ट दृष्टिकोण एवं आदर्श चरित्र ही था। इस समस्त वैभव को ऋतम्भरा की देन कह सकते हैं। यह प्रज्ञा की देवी का अजस्र अनुदान ही था, जिसे पाकर भारत भूमि और समस्त विश्व-वसुधा को चिरकाल तक कृत-कृत्य रहने का अवसर मिला।
प्रज्ञा को इष्ट मानकर चलने वाला उन सभी लाभों को प्राप्त करता है, जो गायत्री उपासना के माहात्म्य वर्णन में आकर्षक एवम् आलंकारिक ढंग से बताये गये हैं। “नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते' आत्मा वाऽऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो, जैसे उद्वबोधन वाक्यों में जिस आत्मज्ञान की गरिमा बतायी गयी है, जिसे प्राप्त करके भगवान बुद्ध की तरह अनेकानेक श्रेय-साधक धन्य बनते रहे हैं, वही महाप्रज्ञा आदिशक्ति गायत्री है। उसी का हमें वरण करना चाहिए।
गायत्री का वाहन हंस है- राजहंस-परमहंस, विवेकवान्-प्रज्ञावान्। राजहंस नीर-क्षीर-विवेक से युक्त, कृमि-कीटकों का भक्षण करने से विरत, मुक्ताओं पर निर्भर रहता है। यह चित्रण बताता है कि श्रेय-साधक की मनोभूमि कैसी होनी चाहिए। गायत्री जिस पर कृपा करे, वह प्रज्ञावान् होता है अथवा प्रज्ञावान् को गायत्री का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। दोनों प्रतिपादनों का तात्पर्य एक ही है। गायत्री का इष्टरूप में वरण सर्वोत्तम चयन है। इतना निश्चित निर्धारण करने पर आत्मिक प्रगति का उपक्रम सुनिश्चित रूप से द्रुतगति से अग्रगामी बनने लगता है, तब साधना, से सिद्धि' के सिद्धांत में कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती।
|
|||||