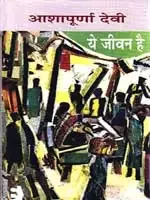|
नई पुस्तकें >> ये जीवन है ये जीवन हैआशापूर्णा देवी
|
5 पाठक हैं |
||||||
इन कहानियों में मानव की क्षुद्र और वृहत् सत्ता का संघर्ष है, समाज की खोखली रीतियों का पर्दाफाश है और आधुनिक युग की नारी-स्वाधीनता के परिणामस्वरूप अधिकारों को लेकर उभर रहे नारी-पुरुष के द्वन्द्व पर दृष्टिपात है।
कैक्टस
निहायत ज़रूरत के समय वांछित वस्तु का हाथ लग जाना मनुष्य के भाग्य में कभी-कभार ही होता है।
भारती के भाग्य में वही दुर्लभ घटनी घट गयी। खबर मिलते ही भाग्य की इस अप्रत्याशित करुणा पर खुशी से पागल हो गयी भारती।
उस खबर को पाने के बाद उस दिन जब तक भी वह कॉलेज में रही सोचती रही कि किस भाषा में, किस ढंग में यह खबर शिशिर को सुनाएगी।
कब सुना सकेगी।
सच ही है, मकान की चिन्ता में जब भारती और उसके पति परेशान हो रहे हें, नये-नये अपमान की ज्वाला, नयी कड़वाहट से मन पीड़ित हो रहा है, हर छुट्टी का दिन दोनों मकान की खोज में ही बिता रहे हैं और अखबार खोलते ही सर्वप्रथम पाठ्य समाचार 'मकान और जमीन' का कॉलम ही होता हे, ऐसे समय में यह समाचार जैसे विधाता के हाथों आशीर्वादी फूल की तरह ही लगता है।
हालाँकि घर में समस्या होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि जिस मकान में वे लोग किराये से रहते थे उस घर में सुविधाएँ ही अधिक थीं। मगर कुछ दिनों से मकान मालिक को ही ये लोग नापसन्द होने लगे थे।
प्रतिदिन बढ़ रहे मकान-किराये की खबर सुन-सुनकर उनके मिजाज भी सातवें आसमान पर पहुँच चुके थे। असर पड़ा था इतने दिनों से रहते आये किरायेदारों पर।
जब भारती की शादी भी नहीं हुई थी, तब से शिशिर यहीं है। शादी के बाद दुल्हन के रूप में इसी घर में आयी। आकर देखा-नीचे मकान मालिक, ऊपर ये लोग रहते हें। मगर मकान मालिक होकर भी अपनों जैसा व्यवहार था उनका।
शिशिर की माँ के साथ मकान मालकिन की गहरी दोस्ती थी। शिशिर की माँ की मृत्यु के बाद वही माँ-मौसी की तरह इनकी देखभाल करती रही, ''बहू बहू," कहकर बीस बार खबर लेती रही। सुख-दुःख में अभिभावक की भूमिका निभाते रहे थे वे लोग।
मगर कालक्रम में वे अभिभावक ही अब पराये-सा बर्तावकर रहे हें। एक साथ दो-दो चूल्हे जलाकर भारती के सोने के कमरे की खिड़की के पास छोड़ जाते, रात के नौ बजते-बजते गेट पर ताला मार देते, भारती के घर के कपड़े बरामदे पर सूखते देखकर ही चिल्लाना शुरू करते-कपड़े माथे पर लग रहे है, भारती के बेटे की गेद अगर आँगन में गिर जाती तो सीधे उठाकर सड़क पर फेक देते। और जब भी मौका मिलता, भारती और शिशिर को लक्ष्य बनाकर जिसे पाते उसे ही बुलाकर उपदेश देने लग जाते-''और चाहे जो कर लो भैया, कभी भी घर को किराये पर मत देना। ये किरायेदार इतने खतरनाक होते हें कि एक बार डेरा गाड़ लिया तो जिन्दगी-भर नहीं हटेगे। पुरखों तक रह जाएँगे।
ऐसे ही कुछ-न-कुछ कहते रहते।
यानी किरायेदार भगाने की हर तरकीब वे आजमा चुके थे भारती और शिशिर के लिए यह स्थिति अत्यन्त पीड़ादायक रही।
विशेषकर सुना-सुनाकर कही गयी बातें हजम नहीं होती। अपमानजनक कार्यों से अपमानजनक बातें और भी पीड़ादायक होती है। और उसी की मात्रा बढ़ती जा रही है।
कारण शायद ही है-विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि। पिछले हफ्ते अखबार में विज्ञापन देखा-''दो कमरे, रसोईघर, बाथरूम-दो सौ पचास रुपये''-इसी हफ्ते वह बढ़कर तीन सौ पचीस, अगले हफ्ते शायद बढ़कर...खैर। इसी बहाने अब तक का सीहार्दपूर्ण वातावरण कटुता में बदल गया, यही अफसोस की बात है। और यह कटुता इतनी निर्लज्ज रूप ले चुकी है कि सच्चे दुश्मन भी शरमा जाएँ।
सुबह-सुबह एक नयी बात और हो गयी।
ऊपर, पता नहीं किस कारण, कटू कुछ ज्यादा ही ऊधम मचा रहा था, अचानक नीचे से मकान-मालकिन व्यग्यपूर्ण शब्दों में बोली, ''बहू ओ बहू, बच्चे को थोडा सँभालकर रखो बेटा, गरीब की टूटी-फूटी झोंपड़ी ढह जाएगी। इस जन्म में खाली भी तो नहीं होगी कि थोड़ी मरम्मत करा लूँ।''
भारती के कॉलेज जाने का समय हो रहा था, इसलिए बात बढ़ायी नहीं उसने। जहाँ तक सम्भव होता वह अपनी तरफ से बढ़ाती भी नहीं। केवल अपने आठ वर्ष के बेटे से मिन्नत कर आयी कि ऊधम नहीं मचाये।
मगर आज पता नहीं किस बात की छुट्टी है स्कूल में और इधर माँ-बाप की छुट्टी नहीं, ऐसा सुनहरा अवसर कभी-कभी उसके हाथ लगता है। अतः बण्टू माँ की मिन्नतों को नजरअन्दाज कर और बाई की परवाह न कर मनमानी करता रहा।
क्या पता, लौटकर कैसी परिस्थिति से सामना हो भारती का। और पहले? जब बन्टू और छोटा था, यही लोग दिन-रात बन्टू को अपने पास रखते थे, नहलाते, खिलाते, सुलाते थे।
शायद उन्हीं के आग्रह और स्नेह के कारण ही कॉलेज की नौकरी बहाल रख सकी थी भारती। कितना प्यार जताकर यही लोग कहा करते थे-''तुम लोग धन्य हो बहू। आजकल की लड़कियाँ...। घर-बार सँभालती, पकाती, खिलाती और उधर मोटी रकम कमाकर भी लाती हो। हम तो कुछ भी नहीं करते, इतना तो कर सकते हैं न?''
चक्का घूम गया।
बदल गया सब कुछ।
अब हवा में बातों के तीर छोड़े जाते हैं। अब बण्टू को छोड़कर जाती तो इस प्रकार के तीर कान पर आकर चुभते-''माँ चली बैग लटकाकर, सज-सँवरकर, अब बेटे की धमाचोकड़ी को भोगें पड़ोसवाले! अच्छी मुसीबत हो गयी है।'' ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करनेवाले वे ही थे जो बण्टू को 'चाँद का टुकड़ा' कहकर प्यार किया करते थे और उसकी जन्म-सम्भावना के दिनों में भारती को अचार खिलाते और हज़ारों उपदेश दिया करते थे।
हो सकता है, बहू बनकर आयी भारती की बढ़ती हुई डिग्रियाँ और फलस्वरूप कॉलेज की अध्यापिका बन जाना ही उनकी निराशा का एक और कारण हो।
खैर, यह भारती के सोचने की बात नहीं है।
भारती के सोचने की बात यह है कि उसकी घर की समस्या के समाधान का एक सुयोग आ गया है। कॉलेज के अधिकारी उसे कॉलेज-हॉस्टल के सुपरिटेण्डेण्ट का काम सौंपना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप उसे एक अच्छा खासा क्वार्टर मिले जाएगा।
कॉलेज पुराना है मगर हॉस्टल की बिल्डिंग बिलकुल नयी। आधुनिक सुख-सुविधा के उपकरणों से सज्जित। एक तरह से अत्यन्त ही आकर्षक, इसमें सन्देह नहीं। जब से यह प्रस्ताव मिला है, वह अत्यन्त प्रसन्न है।
हालाँकि कहा तो उसने यही कि 'सोचकर कल जवाब दूँगी', मगर मन-ही-मन जानती थी सोचने को कुछ है ही नहीं। वह जिम्मेदारी भारती अच्छी तरह निभा सकेगी, इतना आत्मविश्वास था उसमें। ऐसे कामों में सबसे जरूरी है अच्छा बर्ताव। वह हारेगी नहीं। उसके बाद रही परिकल्पना। वह सब हो जाएगा।
घर लौटकर और जवाब देने से पहले ही वह अपनी कार्यप्रणाली ठीक करने लगी।
लौटकर देखा तो बण्टू खेलने निकल गया था। बाई चूल्हा जलाकर दूध गर्मकर रही है। कोयले का चूल्हा। देखते ही भारती को याद आ गया वहाँ गैस स्टोव होगा। कितना साफ-सुथरा, कितना सुन्दर सरल। अब तक पुरानी बची-खुची चीज़ों से ही गृहस्थी चलाती रही, कभी अपनी रुचि के अनुसार आधुनिक ढंग से नहीं चला सकी, अब शायद नसीब का दरवाज़ा खुल जाएगा।
बाई से बोली, ''शारदा, बण्टू को दूध पिलाये बिना ही छोड़ दिया क्या?''
शारदा भारती की मान-मर्यादा की परवाह न करते हुए बोल उठी, ''अच्छा कहा आपने? इतना सीधा लड़का है आपका कि छोड़ने से जाएगा और नहीं छोड़ने से घर में बैठा रहेगा।''
''फिर भी। दूध पीने तक उसे रोककर रखना चाहिए था। उसकी छुट्टी होने से ही यह मुसीबत हो जाती है। दिन-भर खूब शैतानी की उसने?''
''शैतानी!'' आवाज़ को और चढ़ाकर शारदा बोली, ''शैतानी या...। मकान मालकिन तो ऊपर आकर कितना कुछ सुना गयीं।''
यह शिकायत कोई नयी नहीं है।
भारती सुनकर दु:खी होती, लज्जित होती, बेटे को डाँट लगाती।
आज लगा, अजीब बात है। छोटे बच्चे शरारत नहीं करेंगे? इसके लिए वह आकर बुरा-भला सुना जाएँगी? इतनी हिम्मत कैसे होती है, इसीलिए न कि हम अपनी मान-मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ताव दिखाकर सामने से चले नहीं जाते हैं? यही न? ठीक है, अब कोई दुविधा नहीं, कल ही जवाब दे दूँगी।
शिशिर के इन्तजार में बेचैन हो उठी भारती।
और एक बार मन-ही-मन सोचा उसने, किस प्रकार यह खबर सुनाएगी। थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा संकुचित होकर-हाँ, थोड़ा हँसकर, थोड़ा चिन्तित-सा मुँह बनाकर भारती बोल उठी, कॉलेज में तो आज एक काण्ड हो गया।''
शिशिर हँसकर बोला, ''तुम्हारे कॉलेज में तो रोज ही काण्ड होता है। हुआ क्या?''
''नहीं, मतलब और कुछ नहीं, मेरे पास एक प्रस्ताव आया है।''
''अरे, तुम तो एक रहस्य की तरह धीरे-धीरे बात को खोल रही हो। प्रस्ताव है क्या? विदेश भेजना चाहते हैं तुम्हें?''
''तुम तो हमेशा ही मेरा मज़ाक़ उड़ाते हो। सुनो महाशय, बताती हूँ। वे लोग मुझे कॉलेज-हॉस्टल की परिचालिका बनाना चाहते हैं।''
शिशिर हैरान होकर बोला, ''अच्छा, तुम्हें ही अचानक योग्य कैसे समझ लिया?
''योग्यता देखी होगी अवश्य'' गर्दन हिलाकर एक तरुणी की तरह हँसते हुए बोली, ''गुण है अन्दर। केवल तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता।''
''वही देख रहा हूँ। अच्छा तो तुमने फट से 'हाँ' तो नहीं कह दिया न?''
किया तो नहीं था पर शिशिर के कहने के अन्दाज से अचानक थोड़ी नाराज़ हो गई। जितना खुश होना चाहिए था, हुआ तो नहीं। हाँ, असली बात अभी सुनी भी तो नहीं। मतलब जानी हुई बात है पर ध्यान नहीं आया होगा ज़रूर। फिर भी
अपनी नाराज़गी को छिपा नहीं सकी। बोली, ''क्यों? हाँ करने में दोष क्या?''
शिशिर समझ गया कि भारती नाराज़ हो गयी है। मगर पता नहीं क्यों आज शिशिर ने इसकी परवाह नहीं की, अपने आप को रोका भी नहीं, बल्कि उसे मज़ा आने लगा। पर गम्भीर स्वर में बोला, ''नहीं, दोष कुछ नहीं, पर काम इतना सरल नहीं है।''
''मगर कठिन कार्य में ही तो खुशी मिलती है।''
''वह अलग बात है। वह तो गणित के कठिन प्रश्नों को सुलझाने की बात है। यह कुछ और है। काफी गोलमालवाली बात है।''
भारती हँस पड़ी है, ''खुद गोलमाल करनेवाले के साथ ही गोल-माल होता है। खुद ईमानदार रहने से 'माल' को गोल नहीं करने से मुश्किल कहाँ?''
''ऐसा मत सोचो। याद रखना ये लड़कियाँ इस युग की छात्राएँ हैं। 'असन्तोष' जिनके इष्टदेव हैं और 'विरोध' जिनका दीक्षामन्त्र।''
दृढ़ स्वर में भारती बोली, ''यह भी इस युग का एक फैशन है। इन छात्रों की निन्दा करना। ये जो देखते हैं, वही सीखते हैं। हम खुद ही कौन सा धैर्य, स्थिरता, सन्तोष और सभ्यता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं इनके आगे? अगर हम स्वयं शिक्षित, दीक्षित, निर्विकार चित्त होकर दिखा सकते तभी पता चलता दोष कहाँ है। खैर हमारी लड़कियाँ वैसी नहीं हैं। वे मुझे बेहद चाहती हैं।''
''विशेष जगहों पर परिवर्तन भी आता है।'' हँसकर शिशिर बोला, मौसीजी भी तो तुम्हें कितना प्यार देती थीं। दिन-रात बहू-बहू...।''
भारती भी हँस पड़ी। बोली, ''हाँ, वह एक उदाहरण की पराकाष्ठा है, मानती हूँ। फिर भी वह प्रस्ताव मैं हाथ से जाने न दूँगी। इतना बड़ा आकर्षण छोड़ा नहीं जा सकता। कम-से-कम मौसीजी के हाथ से तो छुटकारा मिलेगा, बस इसी खुशी में। यह काम लेने का अर्थ ही है एक सुन्दर, सुदृश्य, सुरम्य वास-भवन।''
हाँ, ऐसे ही बातों में उलझा रखा था। भारती ने। इतनी देर बाद बोलने का अवसर मिला। सोचा उसने, अब रोशनी चमक उठेगी शिशिर के चेहरे पर। मगर कहाँ?
वह आशा किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट आयी।
शिशिर ने व्यंग्य से कहा, ''तो फिर वह वास-भवन ले रही हो क्या?''
अरे! यह कह क्या रहा है? भारती मन-ही-मन हँसकर सम्भावना के पंख पसारे एक असीम सुखद आकाश में सैर करने लगी।
''नही लूँ, जब से सुना है, मैं खुशी से पागल हो रही थी, सोच रही थी कब तुम्हें यह खबर सुना सकूँ! और तुम तो चिन्ता में डूब गये। इतना सोचने का क्या है, मैं अगर काम में खोट रखकर जीतने की कोशिश न कर दिल लगाकर मेहनत
करूँ, तो लड़कियाँ असन्तुष्ट क्यों होंगी? यह सब सोचकर डरो मत। अहा, अगर हमारा वह क्वार्टर तुम देखते। बिलकुल एक तस्वीर है। देखना कैसे सजा लेती हूँ! और मकान छोड़ देने से तुम्हारी मौसीजी भी शायद...'' हँस पड़ी भारती।
बोल उठेंगी, ''तुम लोग जा रहे हो, हम रहेंगे कैसे..., कहकर रो ही पड़ेगी। दुनिया में असम्भव कुछ भी नहीं है।''
भारती की बात शायद सच ही थी। दुनिया में असम्भव कुछ भी नहीं है। तभी तो भारती के साथ सुर मिलाकर शिशिर भी हँसा नहीं, बल्कि फट से बोल उठा, ''मकान एकदम छोड़ देने का सवाल उठता कहाँ है? क्वार्टर तो मिल रहा है तुम्हें।''
''यह क्या बात है। मुझे मिल रहा है का मतलब? सिर्फ मुझे रहने देंगे क्या? मेरे पति और पुत्र को नहीं रहने देंगे?''
''पुत्र की बात नहीं कह सकता,'' शिशिर बोला, ''प्रश्न पति को लेकर है। रहने देने से ही रहा जा सकेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है।''
भारती बोली, ''घुमा-फिराकर नहीं, जरा सीधी तरह से बोलो?''
''सीधा ही तो है सब कुछ। तुम्हारे उस प्रमीला-राज्य में जाकर बसने की मेरी इच्छा नहीं है।''
''यह बात है।'' निश्चिन्त होकर भारती ने साँस छोड़ी, ''प्रमीला-राज्य से कोई सम्पर्क नहीं रहेगा महाशय, बिलकुल स्वयं-सम्पूर्ण व्यवस्था है। प्रवेश-द्वार भी अहाते के भीतर नहीं, बाहर है। और शायद भूले नहीं कि हॉस्टल ही लड़कियों का है, कॉलेज में 'सहशिक्षा' दी जाती है। लड़कों के हॉस्टल के परिचालक के क्वार्टर में उनकी पत्नी बिना किसी भय के रहती है।''
हँस पड़ा शिशिर, ''यह कोई कहने की बात नहीं है। स्त्रियाँ अपने पति के साथ, जंगल, पाताल, पर्वत-शिखर, सभी जगह रह सकती हैं''
भारती अचानक स्तब्ध हो गयी। जिस निश्चिन्त, प्रफुल्लित, सरल मन से अपनी भावी गृहस्थी की सुखद छवि भारती बना रही थी, उस छवि पर जैसे किसी के पंख की छाया पड़ गयी।
धीरे से भारती बोली, ''रह सकती नहीं, रहना ही पड़ता है। यही बात है।''
आपत्ति का कारण समझना कठिन नहीं था अब। पत्नी की योग्यता से मिले उस मकान में जाने की इच्छा नहीं है महाशय को।
वही चिरन्तन पुरुष का अर्थहीन अहंकार! किसी भी तरह अपने आपको पत्नी से श्रेष्ठ सोचे बिना नहीं रह सकते। श्रेष्ठ हर तरह से- मान, मर्यादा, आर्थिक अवस्था। अरे बाबा, जिस युग में दस वर्ष की लड़की को ब्याहकर अपनी गृहस्थी के कारागार में जीवन-भर के लिए बाँदी की तरह भर लेते थे, उस युग की चिन्ता-चेतना-अभ्यास को भूल क्यों नहीं सकते तुम लोग?
इतने दिनों तक स्वामी, प्रभु, वर आदि अनेक श्रेष्ठ विशेषण अपने नाम के साथ जोड़कर राज-पाट तो बहुत किया, अब वह कृत्रिम मोह टूटता क्यों नहीं, एक बार ज्ञान की आँखें खोलकर देखो तो सही - वर बड़ा है या वधू बड़ी है?
अर्थनैतिक मुक्ति के साथ ही क्या स्त्री-पुरुष दोनों एक ही मैदान में आकर खड़े नहीं हुए?
फिर?
मन-ही-मन भारती ने सोचा यह सब, मगर मुँह से कुछ बोली नहीं। बात बदलकर बोली, ''देखो तो, तुम्हारे आते ही बात छेड़ दी मैंने, अभी तक हाथ-मुँह धोया नहीं तुमने, ध्यान ही नहीं रहा। जाओ झटपट। आलोचना, सोच-विचार सब बाद में करना।''
उस समय तो बाँध दे दिया।
मगर फिर तरंग तो उठेगी ही।
फिर वही प्रसंग छिड़ा। तरंग के आघात से ही।
कुछ घण्टे बाद, बण्टू खाकर सोया ही था, ये लोग खाने की तैयारी कर रहे थे कि नीचे की मौसीजी तरंग बनकर आघात कर बैठीं। इन्हें आजकल भारती ने 'मकानवाली मौसी' कहना शुरू किया उनकी आड़ में।
मौसीजी का नाम चारुलता है।
पर उनके नाम को लेकर कभी किसी ने सोचा नहीं। आजकल शिशिर कहता है-एक तरह से सार्थक नाम है उनका। 'नष्टनीड़' की नायिका, हमारे ऐसे सुखद नीड़ का क्या हाल कर दिया।
ऐसे समय आकर उन्होंने एक सम्भावित पल को नष्ट ही कर दिया। खाना खाते-खाते भारती सोच रही थी, प्यार-दुलार दिखाकर शिशिर को उसकी झूठी मर्यादा के मीनार से उतारना पड़ेगा। नहीं तो क्या पता, अचानक कह देगा, 'नहीं, वह काम तुम्हें नहीं लेना है।'' यही सब सोच रहा है, उसकी बातों से पता चल ही रहा है।
भारती भी हर तरह से समझा-बुझाकर उसके मन की दुविधा को दूर कर देगी।
मगर उसके पहले ही कली को तोड़कर फूल को निकाल लिया मौसीजी ने।
एक समय इस घर में उनका बेझिझक आना-जाना था, इसीलिए संकोच नहीं किया उन्होंने। सीढ़ी से उठते ही बोल उठीं, ''बेटा शिशिर, खुलकर ही बोलना पड़ रहा है, बुरा मत मानना, यह मकान अब छोड़ देना होगा। हर तरह से परेशान हो रही हूँ तुम लोगों को रखकर। ऊपर से हमारे नाती साहब। किसदिन गरीब के टूटे-फूटे घर की छत गिरा दें, इसी डर से मरी जाती हूँ। मेरे इस कहने को ही नोटिस मानकर मकान खोजो...''
बराबर 'मौसी' पुकारता आया, इज्जत करता आया, अचानक मुँह पर बेइज्जत तो नहीं कर सकता था। इसीलिए शिशिर मुलायम स्वर में बोलने ही जा रहा था, ''खोज तो रहा हूँ बहुत दिनों से...''
मगर उसकी बात खत्म होते ही भारती बोल उठी, ''आजकल के ज़माने में जो नियमित रूप से किराया दे उसे 'नोटिस' तो नहीं दिया जा सकता मौसीजी।''
मौसीजी जरा चौंक उठीं।
क्योंकि इसकी आशा नहीं की थी उन्होंने।
अब तक जितने तीर थे सब उन्होंने ही छोड़े थे। लगता था पत्थर की दीवार से लगकर गिर पड़ते थे। निशाना ठीक बैठा कि नहीं पता ही नहीं चला?
वह जिस बात को असुविधाजनक बतातीं, वे लोग उस मामले में और सावधानी बरतते। कभी जवाब देते सुना नहीं। और आज एकदम कानून की बात कर बैठी।
चेहरे को विकृत करते हुए बोलीं, ''हम लोग उस ज़माने के आदमी हैं, इस जमाने में क्या चलता है पता नहीं, सीधी बात यह है कि तुम लोग एक मकान का इन्तजाम कर लो, बस। अनिल का ब्याह करना है, कमरे की आवश्यकता है।''
इतना कहने के बाद मौसी नीचे उतर गयीं।
भारती ने स्थिर दृष्टि से शिशिर की ओर देखा और बोली, ''सुन लिया?''
''सुन लिया।'' शिशिर बोला, ''सुनता ही तो रहता हूँ हर समय। पर तुमने भी उनके मुँह पर क़ानून की बात करके अच्छा नहीं किया।''
भारती अपने पति की ऐसी उल्टी बात सुनकर हैरान रह गयी। सच कहा जाए तो मौसीजी के बर्ताव में परिवर्तन आने के बाद से उनसे और उनके परिवार से जो शिष्टता निभाये जा रहे हैं वे लोग, उसका बारह आना श्रेय भारती को ही जाना चाहिए। अकसर ही क्रोधित होकर शिशिर कुछ कहने को मचलता तो भारती ही उसे ठण्डा करती। कहती, ''और जो चाहे कर लो, प्लीज़, झगड़ा मत करो। याद रखना, बाद में फिर मुँह दिखाना पड़ेगा। एक बार आमने-सामने झगड़ा हो जाने से वह पर्दा हट जाता है, फिर तो निर्लज्जता की चरम सीमा तक पहुँचने में भी संकोच नहीं रह जाता है। इससे तो अच्छा है शिष्टता की रक्षा करके यहाँ से निकल जाना।''
शिशिर कहता, ''मगर ये तो उसी कारण बढ़ती ही जा रही है। विरोध करना भी जरूरी है।''
अजीब बात है, आज एक पल के लिए जैसे ही भारती अपनी नीति से हट गयी है, वैसे ही शिशिर ने अपनी नीति बदल ली।
थोड़ी देर चुपचाप पति की ओर देखकर भारती बोली, ''अच्छा नहीं किया क्यों?''
''मुझे तो ऐसा ही लगा।''
''मगर तुम ही कहते हो विरोध करना आवश्यक है।''
''कहता हूँ, तुम ही तो उसपर रोक लगाती हो।''
''आसानी से नहीं लगाती। आज वह ऊपर आकर दोपहर में बण्टू को खूब डाँट गयी हैं, कान मरोड़कर गयी हैं, जानते हो यह बात?
''डाँट गयीं, कान मरोड़ गयीं?
''और क्या कह रही हूँ? बण्टू से सुन लेना कल। उस छोटे से बच्चे से क्या कहा पता है? तुम लोग हमारे इस टूटे घर में पड़े ही क्यों हो? माँ-बाप दोनों कमाते हैं, जाओ न महल बनाकर उस पर उछल-कूद करना।''
शिशिर गम्भीर होकर बोला, ''हूँ।''
''हूँ का मतलब?''
''मतलब दोनों की कमाई ही उनकी आँखों की किरकिरी बन गयी है।'' भारती ने एक बार फिर उस रहस्य भरे चेहरे की ओर तीखी दृष्टि डाली।
क्या कहना चाहता है वह?
दोनों का कमाना बुरा है?
पड़ोसियों को खटकेगी ही?
इसमें पड़ोसियों को दोष नहीं दिया जा सकता।
चेहरे पर गम्भीरता लाकर बोली, ''जब यह भूल हो ही गयी है तो अब चारा क्या है। तुम्हारी मौसी की आँखों से किरकिरी निकालना बस में तो है नहीं? अब आशा करती हूँ कि प्रमीला-राज्य का बहाना बनाकर इस पीड़न से छुटकारा पाने का रास्ता बन्द नहीं कर दोगे। बल्कि अपनी मौसीजी को बोलकर आओ कि अगले महीने से हम मकान छोड़ रहे हैं।''
शिशिर भी गम्भीर हो गया। बोला, ''मैं पागल तो नहीं हो गया।''
भारती अचानक बेहद उत्तेजित हो गयी। बोली, ''इसका अर्थ क्या? क्या तुम सचमुच मेरे क्वार्टर में नहीं जाओगे?''
शिशिर कठोर व्यंग्य के स्वर में बोला, ''एकदम नहीं जाऊँगा, ऐसी प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकता। मान लो अपंग होकर तुम्हारे घर जा पहुँचा।''
''ओह, तुमने आज मुझे नाराज़ करने की ठान ही ली है। मगर मैं नाराज़ नहीं होऊँगी। तुम्हें यह पागलपन करने भी नहीं दूँगी। वह काम मैं ज़रूर लूँगी और सब को जाना ही पड़ेगा। समझे? क्यों, तुम्हारे घर अगर मैं रह सकती हूँ, कोई अपमान नहीं महसूस करती, फिर मेरे घर तुम क्यों नहीं रह सकते?''
''हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है।''
''जवाब है नहीं, इसीलिए नहीं दिया जाता। तुम समझाओ मुझे कि तुम्हें आपत्ति कहाँ पर है?''
अचानक थोड़ा मुस्कुराकर शिशिर ने अपना सीना दिखाकर बोला, ''यहाँ पर।''
''वह मैं समझ रही हूँ। मगर तुम्हें वह पुराना कुसंस्कार त्यागना पड़ेगा। मेरी बात माननी पड़ेगी।'' हल्के स्वर में भारती बोली, ''सुशील बालक की तरह मौसीजी की नाक के सामने से मकान छोड़कर जाना पड़ेगा। सच कहती हूँ तुमसे, जितनी खुशी इस काम के लिए हुई, उससे कहीं अधिक मौसीजी की बात सोचकर हो रही है।''
शिशिर फिर गम्भीर होकर बोला, ''वह बेकार बात है। मकान की खोज तो हो ही रही है।''
''वह तो कब से हो रही है।'' भारती क्रोधित हो गयी, ''शायद अनन्तकाल तक होती रहेगी, उससे लाभ क्या होगा?''
बातों-ही-बातों में तकरार बढ़ती जाती, बढ़ती जाती दोनों तरफ की जिद भी। शिशिर का अड़ियलपन भारती को भी कठोर बना देता।
आखिरकार क्रोध में आकर भारती बोल उठी, ''ठीक है, तुम रहना अपनी पूज्य मौसीजी के घर में, हो सके तो दावत खाना अनिल की शादी में और कमर कसकर काम करना। मैंने अपना भविष्य ठीक कर लिया है।''
हालाँकि कहकर ही वह चौंक गयी।
समझती वह कि ज्यादा ही कठोर हो गयी, पर क्या करे, इनसान ही तो है हाड़-मांस की बनी। शिशिर ने अगर क़सम खा ली है कि जीवन की खुशी, शांति और निश्चिन्तता की ओर कभी नहीं देखेगा, कब तक सहे वह?
क्रमश: उसके मन में भी कुटिल विचार आते। सोचती, ओहो! तुम पुरुष होकर एकदम राजा बन गये। तुम्हारे ही अहंकार की जीत हो। क्यों, मैं इनसान नहीं? अपनी उन्नति, अपना भविष्य, अपनी आर्थिक सुविधा नहीं देखूँ मैं? योग्यता होते हुए भी तुम्हारे तुच्छ अहंकार की तृप्ति के लिए छोड़ दूँ वह सुअवसर?
वही पुराना स्त्री सुलभ आचरण निभाती रही, इसी का नतीजा है कि तुम इस तरह सोचने लगे।
अभी दिन-भर काम कर थक जाती हूँ फिर भी कभी पाँच मिनट आराम करने का नहीं सोचती। कभी आशा नहीं करती कि एक गिलास पानी कोई सामने लाकर दे। घर आते ही कपड़े बदलकर मैं काम में जुट जाती हूँ ताकि घर आकर तुम सब कुछ साफ़-सुथरा देख सको। घर लौटते समय बेटे को स्कूल से लेकर आती हूँ। उसे खिलाती, सँवारती और खेलने भेज देती हूँ ताकि वह तुम्हारे आने से पहले ही खेलकर घर लौट आये, इसके लिए सौ-बार समझती हूँ। क्योंकि जानती हूँ तुम थोड़ी-सी बात पर चिन्तित हो उठते हो। जानती हूँ कि आकर उसे न देखने से तुम्हें बुरा लगता है।
बण्टू की देखभाल करके कभी शायद खड़े-खड़े एक कप चाय पीकर ही चौके में चली जाती हूँ ताकि तुम्हारे आने से पहले खाना पकाने का काम पूरा कर लूँ। मेरे और तुम्हारे घर आने के बीच ढाई घण्टे का अन्तर है, तभी इतना कुछ सँभाल पाती हूँ मैं। उस थोड़े से समय में ही तुम्हारी पसन्द का नाश्ता बना लेती हूँ, ताकि चाय के साथ तुम्हें दे सकूँ। इसी के साथ अपने को भी सँवार लेना पड़ता है कि चाय की मेज पर तुम्हारा साथ दे सकूँ।
ऐसा नहीं कि केवल मुझे ही अव्यवस्थित वेश-भूषा नापसन्द है, तुम्हें भी तो पसन्द नहीं। दिन भर काम करने के बाद इतनी भागदौड़ करने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती क्या?
बहुत तकलीफ़ होती है।
मगर तुम्हें खुशी होगी सोच कर सब सह लेती हूँ मैं। आज तक मेरी जीवन-नैया चलती रही तुम्हारी खुशी की पतवार के अनुकूल।
मगर तुम?
तुमने जीवन में एक बार भी यह नहीं कहा, ''अहा, वह खुश होगी।''
तुम अपने अहंकार में अटल हो।
मैं सभ्य और ममतालु हूँ तभी तुम्हें याद नहीं दिला रही कि-इस काम को लेने से जो अतिरिक्त रुपये आएँगे, उसका अंक तुम्हारे जैसे मामूली क्लर्क के लिए उड़ा देने लायक़ नहीं है। याद नहीं दिला रही हूँ कि महीने भर में जो तुम कमाते हो, वह मेरे बारह दिन की कमाई है।
याद दिलाऊँ भी तो कैसे, खुद ही कभी याद किया क्या? आज तुमने मुझको निराश किया, इतना दुःख दिया, तभी याद आ रहा है।
हाँ, दु:खी भारती के मन में ऐसी उल्टी-सीधी चिन्ता मँडरा रही है।...मगर अगले दिन जब कॉलेज में बात फिर से छिड़ी तो भारती बोली, ''सोचकर देखा मैंने, मैं इस काम के लायक़ नहीं हूँ।''
अध्यक्ष ने कहा, ''योग्यता का विचार करना हमारे हाथ में ही छोड़ दीजिए। झटपट हस्ताक्षर कर दीजिए।''
बाकी अध्यापिकाओं ने भी समझाया। उसकी सहेली लीला घोष बोली, ''तू एक नम्बर की बुद्धू है। जरूर तू अपने रूढ़िवादी पतिदेव के मना करने पर यह मौका छोड़ रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझसे पूछा होता तो मैं खुशी से झूम उठती।''
हँसकर भारती बोली, ''वह तो मैं भी झूम रही हूँ।''
''रहने दे वह बनावटी बातें। 'कर्ता की इच्छा से कर्म' वाला युग अब चला गया, देख नज़र उठाकर दुनिया की ओर।''
अचानक भारती का दिल फिर गया। बोल उठी वह, ''ठीक है।''
''ठीक है?''
मगर ठीक रहा कहाँ? जीवन ही बेतरतीब हो गया भारती का। शिशिर ने भी वही स्वर अपनाया। बोला, ''ठीक है। तुम्हारी बात ही रह जाय। मैं यहाँ रह जाता हूँ, तुम बण्टू को लेकर...''
भारती डर गयी।
बहुत ही असहाय महसूस करने लगी वह। वह विनम्र हो गयी, झुक गयी। देर रात को जब बण्टू सो चुका था, इस कमरे में चली आयी। पति के सीने से लगकर बोली, ''देखो, मेरी बात मानो, मैंने तो जाकर 'ना' ही कर दिया था। बिलकुल। मगर इतनी मिन्नत करने लगे सब कि आखिर-और सच कहो तो कोई तर्क था भी नहीं मेरे पास।''
''पति यहाँ आना नहीं चाहते, यह तर्क काफ़ी नहीं था शायद?''
सीने से लगी पत्नी के दिल की भाषा समझने की कोशिश नहीं की शिशिर ने बल्कि अपने को जरा अलग ही हटा लिया उसने।
भारती फिर भी और झुक गयी। बोली, ''इनसान से बेवकूफी भी तो होती है, गलती भी होती है, यही सोच लो न कि मैंने भी गलती की है, तुम उसे सँभाल लो।'' शिशिर कठोर स्वर में हँस पड़ा।
बोला, ''सँभालूँगा? मैं? क्या कहती हो?''
डेढ़ सौ लड़कियों को सँभालने के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके आयी, अब यह कैसी वाणी?
नहीं होगा, किसी तरह नहीं समझेगा। किसी भी हालत में जीवन को सरल नहीं होने देगा।
मनोरम छवि जैसी सुन्दर गृहस्थी को सजाने का आनन्द वह भारती को नहीं देगा। इस निष्ठुर को क्या पता लड़कियाँ शिक्षा, कर्म या पद-मर्यादा में जितना भी ऊपर उठ जाएँ, उनके हृदय के अन्तर्लोक में एक ही कामना रहती है-अपनी पसन्द का एक घर। उसे सजा-सँवारकर गृहस्थी बसाना।
क्या समझता नहीं वह? जान नहीं पाता?
शायद ठीक ही जान लेता है। सभी पुरुष जान लेते हैं। और लड़कियों की उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ऐसा दिखावा करते हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 'घर' शब्द उनके लिए कोई स्वप्न नहीं, कामना नहीं, साधना नहीं केवल एक आश्रयस्थल है। दिखावा करने, कृपा करके उसने जो 'घर' बसाया है, वह केवल नारी की कामना पूरी करने के लिए है। स्वयं वह निर्लिप्त, उदासीन और फँसा हुआ महज एक प्राणी है। घर-गृहस्थी के साथ उसे जबर्दस्ती बाँधकर रखा गया है।
तभी तो नारीमन के छोट-छोटे सुख, छोटी आशा, छोटी-मोटी चाहतों को अनायास ही अनसुनी कर देते हैं।
शिशिर सो गया। भारती को याद आने लगा-एक बार भारती की बहन की शादी में बारासत गये थे वे लोग। रात हो गयी थी, भारती की माँ ने कितना अनुरोध किया था बाक़ी रात वहीं ठहर जाने के लिए, बोली थी-कल सुबह यहीं से खा-पीकर दफ्तर चले जाना बेटा, आज इतनी रात को...
शिशिर ने भारती की माँ का यह अनुरोध ठुकरा दिया था। अर्थात भारती के अहं को ठेस पहुँचायी थी। फिर भी शिशिर को सुबह खाने की दिक्कत होगी, सोचकर स्वयं भी उतनी रात को शिशिर के साथ भारती लौट गयी थी।
भारती को याद आया, एक दिन-
हाँ, इस तरह एक-एक कर कितने ही दिनों की याद भारती को आयी जिनमें शिशिर की हृदयहीनता साफ-साफ़ उजागर हो रही थी।
शायद ये सब बातें जीवन में कभी भी याद नहीं आतीं भारती को, आज भी पता नहीं मन के किस कोने में छिपी हुई थीं ये यादें। मगर आज सब उठकर सामने आने लगीं अदालत में खड़े हुए एक-एक गवाह की तरह।
भूल गयी भारती कि वह पी-एच.डी. है, भूल गयी कि एक विशिष्ट कॉलेज में वह अध्यापन करती है, भूल गयी अपने कर्मक्षेत्र में उसकी कितनी मान-मर्यादा है। एक कमसिन तरुणी की तरह, नवविवाहित, रूठी हुई वधू की तरह रो-रोकर तकिया भिगोने लगी।...
अच्छा हुआ कि गवाह नहीं रहा कोई। इसी तरह सब कुछ सुरक्षित रहता है, मान सम्मान सब कुछ। निर्जन में आँसू का कोई दशक नहीं होता, एकान्त चिन्ता का कोई साक्षी नहीं होता।
शिशिर का ही कोई एकान्त-लोक नहीं है, कौन कह सकता है। हो सकता है वह भी पीड़ित हो रहा है, दुःखी है, रूठा हुआ है, क्योंकि वह अपनी तरह से सोच रहा है, अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, अपनी चिन्तनधारा के अनुसार राय दे रहा है। इस तरह वह भी शायद भारती को हठी, दुर्विनीत और निष्ठुर समझ रहा है।
दोनों में से किसी का कोई प्रत्यक्ष-प्रमाण नहीं है।
इतने दिनों तक दोनों एक-दूसरे में ऐसे सम्पूर्ण थे कि उनका कोई ऐसा मित्र भी नहीं था, जिसके पास जाकर दिल का बोझ हल्का करें।
इसी वजह से ये दोनों बन्धुहीन अपनी-अपनी दुर्गति से परिचालित होते गये और प्रमाणित करते गये कि दुर्गति का असाध्य कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने एक और उपलब्धि को प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य में कितने ही परिवर्तन आते हैं।
क्योंकि अगला दृश्य कुछ ऐसा है, तस्वीर जैसे उस सुन्दर घर को पौधे, रंगीन मछलियों, कुशन, पर्दे, सोफे आदि से सुन्दर ढंग से सजाकर बण्टू को लेकर अकेले रहती है भारती। एक छोटा-सा नौकर है दिन-रात के लिए जो अपनी छोटी-छोटी बाँहों से घर को धूल-रहित स्वच्छ बनाकर रखता है, एक बाई है जो दोनों शाम आकर मोटे-मोटे काम कर देती है, ऊँची मेज पर रखे गैस के चूल्हे पर खाना पकाती है, बेसिन में साबुन का झाग बनाकर कपड़े धोती है।
कभी-कभी भारती उस बाई की ओर ईर्ष्या की दृष्टि से देखती है, क्योंकि अचानक ही कभी उसे याद आ जाता है चारुलता मौसी के घर का वह कालिख भरा रसोईघर, जिसमें ईंट से बने चूल्हे पर कितने सालों तक वह खाना पकाती रही। याद आ जाता नहाने का वह बाथरूम जिसके फर्श का सीमेण्ट उखड़ा हुआ था। वही तो जगह थी जहाँ भारती कपड़े धोती और एक बेसिनवाले बाथरूम का सपना देखती थी।
मगर अब तो एक रूमाल भी धोने को जी नहीं करता, चौके में जाकर दो आलू की भाजी तक बनाने को जी नहीं करता है।
पता नहीं क्यों।
क्या भारती पैसेवाली हो गयी है इसलिए? या कि शाम होते ही उसके सुन्दर गोल बरामदे में अध्यापिकाओं की जमघट होती है, इसलिए समय नहीं मिलता है?
उस जमघट की प्रधान वक्ता लीला घोष कहती, ''दिखा दिया तेरे उस 'परम गुरु' ने। मैं कह देती हूँ भारती, कहीं कुछ नहीं है, ईर्ष्या है बस। पति-पत्नी के रिश्ते में यह चीज़ कुछ अधिक मात्रा में ही होती है, समझी? मिलकर काम करने से जो लाभ होता है उसी की खातिर अपनी ईर्ष्या को ढँककर रखते हैं।
फीकी हँसी हँसकर भारती बोली, ''इतनी बात कैसे जान गयी?''
''देखकर, वत्स। देखकर।''
''क्या तभी शादी नहीं की?''
''अरे नहीं, इसलिए नहीं,'' लीला घोष हँस पड़ी, ''अभी भी मिले तो कर लूँ।
ऐसे चेहरेवाली से कौन ब्याह करेगा, बोल? तभी तो यह हाल है। पर समझती हूँ सब।''
हँसी का फ़व्वारा छूटता, साथ में चाय की नदी बहती। वह छोटा नौकर सावधानी से ट्रे में उठाकर क़ीमती प्यालों में ले आता सुनहरी चाय।
भारती को उठना भी नहीं पड़ता। शीशे की खिड़की पर लगे गमलों में लगे कैक्टस-कोई सर उठाकर खड़ा रहता, कोई अपनी टेढ़ी-मेढ़ी बाँहें इधर-उधर फैलाकर शीशे पर एक विकृत आदमी जैसी छाया तैयार करता।...
हवा से पर्दा काँप उठता।
उनकी हँसी-ठहाके के बीच भारती की नज़र उधर पड़ती, शायद सोचती, ऐसी भी क्या बुरी हूँ?
फिर एक समय बाई आकर पूछती, ''दीदीजी, मुन्ना को खिला दूँ अभी?''
भारती नाराज़ होकर कहती, ''क्यों? अभी खिला देने से तुम्हारा भागना आसान हो जाएगा, है ना? नौ बजे से पहले नहीं खाएगा, पढ़ेगा नौ बजे तक।''
बाई भारी स्वर में कहती, ''अपने लिए नहीं कह रही थी, पढ़ते-पढ़ते नींद आ रही है, इसीलिए...''
चली जाती गुस्सा दिखाकर।
भारती की सहेलियाँ कहतीं, ''वह बेचारा जरा अकेला महसूस करता है।''
भारती शीशे पर पड़ी टेढ़ी-मेढ़ी छाया की तरफ़ देखकर अनमने भाव से बोलती, ''हाँ, कभी-कभी यही सोचती हूँ कि उसे किसी बोर्डिंग में डाल दूँ। कम-से-कम दूसरे लड़कों के साथ...''
और शिशिर?
सच कहा जाए तो बाहर से शिशिर की हालत भी बुरी नहीं लगती। ऊपर के कमरे छोड़कर वह चारुलता मौसी की बैठक में समा गया है, 'पेइंग गैस्ट' बनकर। देखभाल में कोई कमी नहीं है। मौसीजी स्नेह गद्गद होकर सदा करुणा बरसाती हैं, शिशिर की कमीज़ के बटन लगे हैं या नहीं, यह देखने का जिम्मा भी उन्होंने अपनी बेटियों को दे रखा है। यह ममता केवल दिखाने के लिए है, ऐसा कहना मौसीजी के प्रति अन्याय होगा। ममतावश ही कर रही हैं।
स्नेह ममता की फल्गुधारा बराबर बहती थी, एक तीव्र इच्छा के वशीभूत होकर उनका स्वार्थ उन्हें कठोर, कर्कश और निर्लज्ज बना रहा था। वह बाधा दूर हो गयी, ऊपरवाले कमरों में हल्की रँगाई-पुताई करके किराये में आशानुरूप वृद्धि कर एक किरायेदार को बैठा दिया है, उसके अन्दर से बैठक का भी आधा हिस्सा और दो बार भोजन के लिए शिशिर से मुट्ठी भरकर पैसे ले रही हैं, तो फिर एक बार निर्लज्ज होने में दिक्कत क्या है?
एक बार फिर निर्लज्ज होकर शिशिर के लिए ममता बरसा रही हैं चारुलता मौसी। जिसकी बीवी भाग गयी, उस शिशिर के उदासीन मन पर आगे इस निर्लज्जता की कड़वाहट का असर नहीं होगा, इतना मौसी भी जानती हैं।
मगर क्या शिशिर इतना उदासीन हो गया, कि आधे घर में ही राजी हो गया? हो तो गया। शायद शिष्टाचार के कारण ही। क्योंकि अब तक उस कमरे में जो अविवाहित बेटा सोता था, उसे हटाना ठीक नहीं लगा शिशिर को। इसलिए बोला, ''रहने दीजिए अनिल को सोने दीजिए, जैसे सोता था। कमरा बड़ा है...''
शिशिर के छोटे भाई जैसा ही तो था अनिल। पहले शिशिर के पास कितने हठ करता था, कितना परेशान करता था शिशिर की माँ को।
शिशिर भी अब अधिक जगह लेकर क्या करे? कट ही तो रहे हैं दिन, कट जाती हैं राते। एक थाल भोजन की, एक बिछौना सोने को और नहाने के समय छोड़े धोती, गंजी, तौलिए, सब हाथ के सामने धुले-सूखे मिलते।...इतना तो हो ही जाता है।
इससे अधिक चाहने को है ही क्या, कोई बाधा-बन्धन, कोई उत्तरदायित्व नहीं, ऐसी जिन्दगी का भी एक अलग राग होता है। महीने के प्रारम्भ में रुपये थमा देने के बाद दुबारा सोचना नहीं पड़ता कि खाने के लिए खटना भी पड़ता है। घर चलाने के लिए केवल रुपये ही काफ़ी नहीं है, तेल-नमक-लकड़ी के धन्धे में ही दुनिया छान लेनी पड़ती है।
सच ही तो है, अब तो सुनना नहीं पड़ता-सुना है पावरोटी अब से कूपन के बिना नहीं मिलेगी, क्या आफत है, देखो तो! सुनना नहीं पड़ता, मेरा कोई काम तुम क्यों नहीं करते, जरा सुनो तो। जाओ, एक बार जाकर देख आओ क्या सचमुच बाजार से तेल गायब है? नहीं सुनना पड़ता, ''सैर से लौटते समय एक बार दुकान होकर आना, चाय बिलकुल खत्म है।...देखो, आज तो समय है, बण्टू को लेकर एक बार 'साउथ टेलरिंग' के यहाँ जा सकोगे? कुछ शर्ट-पैण्ट की जरूरत थी उसे।''
उसे आश्रय मिल गया है एक अखण्ड निश्चिन्तता के शब्दहीन जगत में। इस शब्दहीन जगत में बाहर से आ रहे छोटे-मोटे शब्द बुरे नहीं लगते हैं। उन शब्दों में कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। नहीं है कोई गिले-शिकवों का आक्रमण।
ये शब्द केवल कानों पर से गुज़रते हुए शब्द-समूह हैं। पुराने दिनों की तरह बड़े उत्साह के साथ अनिल अपने फुटबाल-टीम की बातें करता, अच्छा ही लगता है शिशिर को।
मौसीजी की बेटियाँ जब-तब बोल उठती, ''उफ् शिशिरदा, कितने अनमने हैं आप, कल से आपकी सुराही में पानी नहीं है, कहा भी नहीं।''
बुरा नहीं लगता सुनने में। और मौसीजी जब खाने के समय सामने पंखा झलतीं और कहतीं, ''कितना कम खाते हो आजकल, देखकर दिल 'हाय-हाय' कर उठता है। दीदी जब थी, घी से सनी रोटी भरकर रख देती थी, बेटा कॉलेज से आकर खाएगा। क्या दिन थे वे सब।''
उस समय खुशी के आवेग से शिशिर की आँखें ही भर आतीं।
घुमा फिराकर शिशिर की माँ की बात ही छेड़ती चारुलता मौसी। कैसी गहरी दोस्ती थी दोनों में, याद दिला देतीं और बीच-बीच में साँस छोड़कर कहतीं, ''क्या जाने, कैसा दिल है बहू का। इस तरह गृहस्थी लुटाकर नौकरी में तरक्की करने चली गयी। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते।''
हो सकता है, यह केवल भारती की निन्दा करने के लिए ही नहीं बोलतीं, शायद सच्चे मन से ही निकलती हों ये बातें।
असहाय, अकेले पुरुष के प्रति ममता,-नारी मन की सहज प्रकृति है, चाहे वह किसी भी उम्र की क्यों न हो।
शिशिर की टूटी हुई गृहस्थी उनकी ममता को और भी छेड़ती और इसी कारण बहू की निन्दा और जमकर करतीं।
भारती की दुर्बुद्धि से मौसी को कितनी ही सुविधा क्यों न मिली हो, उस पर क्रोध बिना नहीं रह पातीं।
मगर उनकी मुलाकात क्या बिलकुल ही नहीं होती? पति-पत्नी की? बाप बेटे की?
नहीं, नहीं। ऐसा हो सकता है क्या?
कानूनन कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई है, केवल अपनी-अपनी सहूलियत के हिसाब से रहते हैं, बस भेंट होती है।
हर रविवार को मुलाकात होती है।
शिशिर नहीं जाता, भारती ही आती है बेटे को लेकर। मौसीजी के घर में ही आकर बैठना पड़ता है। चाय भी पीनी पड़ती है कभी-कभी। प्लेट में लेकर बण्टू भी नाश्ता करता है। कभी अगर देखता उसके पिता नहाने गये हैं या बाहर निकले हैं, चुपके से माँ से पूछता, ''माँ, जरा छत पर जाऊँ?''
छत पर ही उसका अड्डा था। अभी भी टूटी हुई चटाई पानी के टैंक के पास वैसी ही पड़ी है।
भारती को बेटे का यह कँगलापन अच्छा नहीं लगता, आँख से इशारा भी करती, मगर लाभ नहीं होता।
मौसीजी स्नेह-भरे स्वर में बोलतीं, ''अहा जाने दो, बचपन के खेलने की जगह है। नये किरायेदार भले इनसान हैं, कुछ नहीं कहेंगे। जा, चला जा।''
शिशिर नहा लेता। फिर सज-धज लेने के बाद तीनों साथ निकलते। रविवार को अब वे बाहर ही खाते, घर पर नहीं।
जैसे यह एक अलिखित नियम ही बन गया है कि खाने का खर्चा शिशिर ही देगा। भारती कभी अपने बटुए को नहीं छूती।
बाहर घूमते वे लोग इधर-उधर, खाना खाते; सिनेमा देखते, सर्कस आता तो वह भी देखते।
देखने में तो ऐसा लगता कि बण्टू का मनोरंजन ही मुख्य उद्देश्य है। जैसे उसी को खुश करने के लिए निकले हैं दोनों। लौटते समय अकसर खरीदारी करते वे लोग बण्टू के नाम पर, खाने की चीज़, खिलौने, लाल मछली, कैक्टस।
इसका मतलब यह तो नहीं कि ये दोनों बात नहीं करते आपस में, हँसते नहीं? सब कुछ करते हैं।
सामयिक घटनाओं पर छिड़ी हुई बातें भीतर असर नहीं करतीं, बाहर से ही निकल जाती हैं।
शाम होते ही धीरे से दोनों कहते, ''अच्छा।''
शिशिर बण्टू के सर पर हलके से थाप देकर कहता, ''बण्टू बाबू जिस तरह लायक़ होते जा रहे हैं, अब वही हमें घुमाने ले जायेंगे, क्यों बण्टू बाबू?''
बण्टू मुँह फेरकर खड़ा रहता। मुँह नीचा किये रहता।
बण्टू किसी तरह भी अपनी आँखें माँ-बाप को देखने नहीं देता है।
वह बड़ा हो रहा है, क्या यह पता चलता है?
कभी-कभी जब बण्टू इधर-उधर होता, भारती भी अपनी आँखें नीची कर बोलती, ''मेरे घर कभी नहीं आओगे तुम।''
''नहीं आऊँगा, ऐसा कब कहा?''
''कहा नहीं, यह सच है।''
''चला आऊँगा किसी दिन।''
भारती चुप हो जाती।
मन-ही-मन सोचती, ''अच्छा। मैं कभी अस्वस्थ भी तो नहीं होती। कैसा अटूट स्वास्थ्य दिया है भगवान ने।''
कल्पना करती, वह अटूट स्वास्थ्य अब टूट चुका है। कॉलेज के अधिकारी वर्ग खबर भेजते हैं शिशिर को-
मगर कल्पना कल्पना ही रह जाती।
फिर अगले रविवार स्वास्थ्य और शक्ति से भरपूर भारती जा पहुँचती चारुलता मौसी के घर। शायद जानबूझकर कुछ देर से ही पहुँचती ताकि शिशिर तैयार ही मिले। पर यह आशा प्राय: पूरी नहीं होती है। जब तक उन्हें देखता नहीं, शिशिर हिलने का नाम नहीं लेता है।
लाचार होकर उसे मौसीजी के चोके के दरवाजे पर आकर बैठना पड़ता है।
और बण्टू छत पर जाने को बेचैन रहता, मगर पहले की तरह जिद नहीं करता वह। बड़ा शान्त हो गया है बण्टू। शान्त और गम्भीर।
मान लेना पड़ेगा बण्टू भी ठीक ही है। ठीक नहीं होता तो शान्त क्यों हो जाता? हर हफ्ते इसी घटना की पुनरावृत्ति होती। एक ही उत्साह से हर रविवार का प्रारम्भ होता है और एक ही निराशा से उसका अन्त।
मगर आश्चर्य की बात यह है कि यह जीवन अब उन्हें अजीब नहीं लगता है। परिस्थितियों के साथ बिलकुल खप गये हैं वे लोग, अच्छा समझौता हो गया
है उनके साथ।
विनिद्र रातों की अपार क्लान्ति लेकर भी भारती सुबह सहज भाव से लाल मछलियों को खाना देती, कैक्टस के गमलों को धूप की ओर घुमा देती और सोचती कुछ और खरीदने पड़ेंगे।
शिशिर भी रविवार की शाम को घर लौटकर बिस्तर पर हाथ-पैर पसारकर सोचता कि अगले रविवार को क्या उपहार दिया जाए बण्टू को।
इनसान कितना बलशाली है, यही उसका सबूत है। अपने को हर हालत में 'ऐडजस्ट' कर लेता है वह। यही करते-करते उसके जीवन का परिक्रमण चलता है।
फिर भी क्यों अपने आप को लेकर चिन्ता का अन्त नहीं-यही आश्चर्य की बात है, यही सोचने की बात है।
0 0
|
|||||