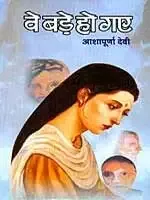|
नारी विमर्श >> वे बड़े हो गए वे बड़े हो गएआशापूर्णा देवी
|
5 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है उत्कृष्ठ उपन्यास...
3
स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरती हैं, तभी तो मोती बनता है।
उदार हृदय समीर सेन कहते हैं, 'जितनी किताब चाहो, ले जाओ। मुझे फिलहाल उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।'
कृतज्ञ सुलेखा विनीत होकर उनके पैर छूकर चली आती है। मगर वे किताबें ही आफत का पहाड़ ढातीं।
चाची कहतीं, 'मुहल्ले भर के बच्चे समीर सेन से डरते हैं। पता नहीं, कैसे तू इतनी किताबें हथियाकर ले आती है।'
समीर सेन की उम्र कुछ खास अधिक नहीं। अतः देवरानी के आश्रय में ठहरी सुलेखा की विधवा माँ डर जाती। गनीमत है कि सुलेखा इस इशारे को समझ नहीं पाती है।
सुलेखा कहती, 'क्यों, डरनेवाली कोई बात तो नहीं है। कितने जतन से ही तो किताबें देते हैं। कभी-कभी पूछते भी हैं, इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेती है। घर में और कोई पढ़ता है या नहीं?'
फिर चाची की जिरह के मारे यह भी बताना पड़ता है कि इन सब बातों का क्या जवाब दिया उसने।।
हालाँकि जवाब सुनकर चाची खुश नहीं होती। कहतीं, 'तुमने इतना ही कहा कि किताबें तुम जल्द ही पढ़ लेती हो, घर में तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, फुरसत-ही-फुरसत है, यह भी तो कह सकती थी। और दूसरा कोई नहीं पढ़ता है-न कहकर उन्हें पढ़ने की फुरसत नहीं होती है, ऐसा भी तो कह सकती थी। सभी तो तुम्हारी माँ जैसे मूरख नहीं हैं। एक उनको छोड़कर किताब पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता है?' ।
अड़ोस-पड़ोस के बारे में भी चाची की टिप्पणियाँ काफी तीखी होती थीं । व्यंग्य भी भरपूर रहता था।
'मुझे पढ़ने में समय लगेगा, तू ही पहले ले जा सुलेखा! बड़ी आई प्यार जतानेवाली मौसी, चाची, ताई कहीं की! परायी लड़की को इस तरह सभी सिर चढ़ा सकते हैं। हुँह ! कुँआरी लड़की का दिन-रात इस तरह नाटक उपन्यास में डूबे रहना ठीक नहीं, ऐसा सदुपदेश नहीं दे सकती क्या वे? दीदी भी तो प्यार में बिलकुल अंधी हैं, कुछ नहीं बोलती। मगर सुलेखा की माँ बोलने में कोई कसर भी तो नहीं रखती। हमेशा कहती है, 'चाची की नजर के सामने किताब लेकर क्यों बैठती है, सुली? इतना अपमान चुभता नहीं तुझे? और छोटी बहू झूठ भी तो नहीं कहती है, अनब्याही लड़की को नाटक-उपन्यास का इतना शौक क्यों? लगता है, यह नशा शराब से बढ़कर है। इस नशे को छोड़ दे, सुली। आखिर पराए घर भी तो जाना है। बहू की ऐसी आदतें कौन भली निगाह से देखेगा, बेटी?'
कहती जरूर थीं, पर निकट भविष्य में वह 'पराए घर' जा सकेगी ऐसी आशा सचमुच नहीं थी उनके मन में।
देवर-देवरानी का ही तो आसरा था।
स्वयं किसी काबिल नहीं थीं - न तन से, न मन से; मगर इतनी डाँट फटकार सहकर भी पढ़ने का नशा छूटा नहीं उसका। दो-चार दिन जरा ठहर जाती थी, फिर मौका पाते ही दो किताब लाकर तकिए के नीचे छिपाकर रख देती थी। रात को चोरी-चोरी पढ़ लेती थी।
मगर उसमें भी चैन कहाँ?
माँ कहती थीं, 'बिजली खर्च कर उपन्यास पढ़ेगी, सुली? चाचा का बिजली का बिल बढ़ेगा, चाची जली-कटी सुनाएगी।'
हर कदम पर माँ इसी तरह डराया करती थीं। अब सुलेखा कभी-कभी सोचती है-उसकी तुलना में उसकी बेटियाँ कितनी सुखी हैं ! कितनी मुक्त-स्वच्छंद हैं! फिर भी उनके चेहरे पर उस सुख की झलक क्यों नहीं दिखाई देती है?
अगर सुलेखा को अपने बचपन में इनके सुखों का एक प्रतिशत भी मिल पाता तो अच्छा, उतने तिरस्कार, उतनी डाँट-फटकार, उतनी दीन दशा में रहकर भी किस प्रसन्नता से पूर्ण रहता था सुलेखा का हृदय! कभी किसी दिन एक पल के लिए भी सुलेखा ने नहीं सोचा था। मन नहीं लगता - धत् , सब बेकार है।
जो उसकी बेटियाँ दिन-रात ही कहती रहती हैं। सुबह से लेकर रात तक उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
सुलेखा आज सोचकर देखती है-उसके जीवन में उन दिनों मन लगाने का साधन ही क्या था? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं।
फिर भी अपने मन की मिठास से ही सुलेखा अपने दिन-रात को सरस कर लेती थी। जिस दिन हाथ में कोई भारी-भरकम नई किताब आ जाती थी, उस दिन तो सुख का कोई अंत नहीं होता था। मन के कलश से खुशी जैसे छलक उठती थी। उस दिन आकाश कितना सुंदर लगता था! हवा कितनी मीठी! घर के काम-काज कितने हलके लगते थे!
चाची चाहे जितना भी डंके की चोट पर कहें, दिन-रात ही तो हाथ-पैर समेटे बैठी रहती हैं, काम तो कुछ होता नहीं है। काम कुछ रहता ही था।
माँ बीमार थीं, इसलिए उनके हिस्से का अधिकतर काम-काज वही करने की कोशिश करती थी; मगर तंदुरुस्त लड़की का काम-काज हँसते खेलते हो जाता था। किताब न होती तो दिन सूना लगता था और उस सूनेपन से थक जाती थी सुलेखा।
जिस दिन लाइब्रेरी से छह महीने या साल भर की पत्रिकाओं का संकलन आता था, वह दिन सुलेखा के लिए यादगार दिन बन जाता था; मगर जो दिन मरुभूमि जैसे होते थे और चाची को उन्ही दिनों विशेष प्रसन्नता होती थी, वैसे दिनों में सुलेखा मन-ही-मन सोचती थी-ठीक है, मुझे पराए घर ही भेज दो। देखूगी वहाँ जाकर, दुलहन को इतनी छूट मिलती है या नहीं।
सोचकर हँसी आती है, कैसा असंभव सपना देखा था उसने । वहाँ तो छपी हुई पुस्तकों का एक प्रकार से प्रवेश निषेध ही था।
मगर उन दिनों सुलेखा सपने देखा करती थी। सपने में देखती थी कि वह बड़ी होकर अपनी गृहस्थी चलाएगी और तब एक साथ चार लाइब्रेरीज की मेंबर बनेगी। एक तरफ से सभी प्रख्यात लेखकों की सारी किताबें पढ़ डालेगी।
शायद इस सपने में ही उसकी प्रसन्नता का बीज छिपा था।
|
|||||