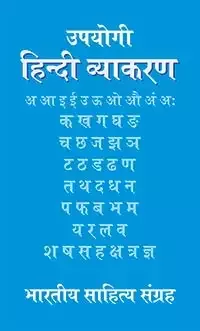उपयोगी हिंदी व्याकरण
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: author_hindi Filename: views/read_books.php Line Number: 21 |
निःशुल्क ई-पुस्तकें >> उपयोगी हिंदी व्याकरण |
|
|
|
हिंदी के व्याकरण को अघिक गहराई तक समझने के लिए उपयोगी पुस्तक
क्रिया के प्रकार
मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है —
क. अकर्मक
ख. सकर्मक।
क. अकर्मक क्रिया : वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की
आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, सोना, हँसना,
रोना, उठना, आना जाना आदि। यहाँ क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है।
जैसे — श्याम मैदान में दौड़ रहा है।
वाक्य में दौड़ना क्रिया का कर्ता श्याम है और दौड़ने
क्रिया के परिणाम या फल या प्रभाव का पात्र भी श्याम है। यह प्रभाव कर्ता से
भिन्न किसी अन्य पर नहीं पड़ता है।
ख. सकर्मक क्रिया: सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म की
आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती
है। जैसे, पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना आदि। यदि वाक्य में कर्म न हो, और
न प्रसंग से कर्म का पता लगता हो, जैसे — मोहन देख रहा है तो अर्थ
में कुछ कमी रहती है, और सहज प्रश्न उठता है कि क्या देख रहा है। यदि कर्म
साफ-साफ हो या प्रसंग से तुरंत मालूम हो जाए, जैसे — मोहन पेड़ देख रहा
है तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।
अकर्मक – सकर्मक के भेद
अकर्मक-सकर्मक के भेद-उपभेद नीचे आरेख में दिए जा रहे हैं और उसके बाद उनका
विवरण दिया जा रहा है:
1. क. स्थित्यर्थक / अवस्था बोधक (पूर्ण) अकर्मक क्रियाएँ :
ये क्रियाएँ अकर्मक हैं अर्थात् इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है; ये
पूर्ण अकर्मक हैं अर्थात् यह अपूर्ण (पूरक के बिना अपूर्ण लगने वाली) नहीं
हैं; और ये कर्ता की अवस्था दशा को बताती हैं। जैसे, सोना. हँसना,
खिलना, रोना, अनुभव होना आदि। उदाहरणार्थ —
श्याम इस समय सो रहा है। (सोने की अवस्था)
मोहन हँस रहा है। (हँसने की अवस्था)
टिप्पणी : अस्तित्ववाची क्रिया होना भी एक विशेष स्थिति (सत्ताभाव दिखाती है,
अतएव वह भी इसी उपभेद के अंतर्गत है। जैसे, ईश्वर है।
ख. गत्यर्थ क (पूर्ण) अकर्मक क्रियाएँ
ये क्रियाएँ भी अकर्मक हैं, अर्थात् इन्हें कर्म की आवश्यकता
नहीं है। ये पूर्ण अकर्मक हैं अर्थात् यह अपूर्ण (पूरक के बिना अपूर्ण लगने
वाली) नहीं हैं; और इन क्रियाओं को करते समय करने वाला गतिमान होता है। जैसे
— जाना, आना, दौड़ना, भागना, घूमना, तैरना, उड़ना, उठना, गिरना आदि। इन
क्रियाओं के साथ स्थान की सूचना देने वाले तत्व प्रायः होते हैं; चाहे
स्थानवाची अधिकरणकारक में, चाहे अपादान कारक में (— से द्वारा प्रकट) चाहे
गंतव्य सूचक में (— तक, की आदि द्वारा प्रकट) उदाहरणार्थ —
मोहन आगरा जा रहा है।
चिड़िया आकाश में उड़ रही है।
सोहन इस समय गेट से निकल रहा है।
2. अपूर्ण (पूरकाकांक्षी) अकर्मक क्रियाएँ:
अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ वे अकर्मक क्रियाएँ हैं, जिनके प्रयोग के समय अर्थ की
पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द विशेष की आवश्यकता पड़ती
है। होना इस कोटि की सबसे प्रमुख क्रिया है, अन्य क्रियाएँ
हैं — बनना, निकलना आदि। उदाहरणार्थ:
मैं बीमार हूँ इसलिए आ नहीं सकूँगा।
मोहन बहुत होशियार है।
श्याम बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा।
मेरा पड़ोसी बहुत चालाक निकला।
यहाँ पूरक (बीमार, होशियार आदि) का लोप करके देंखे कि वाक्य कितना अपूर्ण तथा
अधूरा लगता है। यहाँ बीमार शब्द का संबंध वाक्य के कर्ता “मैं”
से है; होशियार का संबंध वाक्य के कर्ता मोहन
से है; इंजीनियर का संबंध वाक्य के कर्ता, श्याम
से है — इस कारण यह रचना कर्तृपूरक या उद्देश्य पूरक रचना
कही जाती है। कर्तृपूरक शब्द सामान्य तथा विशेषण (जैसे बीमार होते हैं; किंतु
कभी-कभी संज्ञा भी (जैसे इंजीनियर) होते हैं।
3. (क) पूर्ण एककर्मक (सकर्मक) क्रियाएँ
पूर्ण एककर्मक (सकर्मक) क्रियाएँ (सामान्यतया सकर्मक क्रिया
नाम से प्रसिद्ध) वे क्रियाएँ हैं, जो एक कर्म अवश्य लेती हैं, जैसे —
कुत्ते ने बकरी को काट लिया।
सीमा खाना खा रही है।
दर्जी कपड़ा सी रहा है।
(ख) पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएँ
पूर्ण द्विकर्मक वे क्रियाएँ हैं, जिन्हें दो कर्मों की आवश्यकता होती है
देना, लेना, बताना तथा सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ इसी कोटि के अंतर्गत आती
हैं। उदाहरणार्थ :
रेखा ने अपने साथी को अपना पूरा पता बताया।
मालिक ने नौकर से तरह-तरह के सवाल पूछे!
राम ने मोहन को अपनी नई किताब दे दी।
विनोद ने अशोक को अपनी पुरानी कार बेच दी।
देना क्रिया में वस्तुतः दो कर्म नहीं होते — एक संप्रदान
होता है (जिसे दिया जाता है) और एक कर्म होता है (वह वस्तु आदि जो दी जाती
है), किंतु मोटे तौर पर दोनों को कर्म की कोटि के भीतर रखते हुए द्विकर्मक
कहा जा सकता है।
4. अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ: (कर्म पूरकाकांक्षी सकर्मक क्रियाएँ)
ये वे क्रियाएँ हैं, जिन्हें कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है
और उसे पूरा करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले एक अन्य शब्द की आवश्यकता
होती है। चुनना, मानना, समझना, बनाना आदि अनेक क्रियाएँ इस कोटि में आती हैं।
नीचे के उदाहरण देखिए:
अमित श्याम को बिल्कुल मूर्ख समझता है।
रंगरेज ने कपड़े को लाल रंगा।
छात्रों ने दीपक को अपना प्रतिनिधि बनाया/चुना।
मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ।
यहाँ पूरक (मूर्ख, लाल, प्रतिनिधि, भाई आदि) का लोप कर देखें कि वाक्य कितना
अपूर्ण तथा अधूरा लगता है। यहाँ मूर्ख का संबंध कर्म श्याम
से है, लाल का संबंध कर्म कपड़े से है प्रतिनिधि
का संबंध कर्म दीपक से है और भाई का संबंध
कर्मरूप तुम्हें = तुम को से है। इस कारण ये पूरक कर्मपूरक
कहे जाते हैं। ये विशेषण (जैसे – लाल) तथा संज्ञा (जैसे — भाई) हो सकते हैं।
अकर्मक — सकर्मक में परिवर्तन (अंतरण)
क्रियाओँ का अकर्मक अथवा सकर्मक होना, धातु के अर्थ से सीधे न होकर, प्रयोग
पर निर्भर करता है। इस कारण कभी-कभी अकर्मक क्रियाएँ सकर्मक प्रयोग में और
सकर्मक क्रियाएँ अकर्मक प्रयोग में मिलती हैं। जैसे —
पढ़ना (सकर्मक) : श्याम किताब पढ़ रहा है।
पढ़ना (अकर्मक) : श्याम आजकल आठवीं में पढ़ रहा है।
खेलना (सकर्मक) : बच्चे गेंद खेल रहे थे।
खेलना (अकर्मक) : बच्चे दिन भर खेलते रहे।
इसके विपरीत हँसना, लड़ना आदि अकर्मक क्रियाएँ हैं, फिर भी
सजातीय कर्म लगने पर सकर्मक रूप में मिलती हैं, जैसे —
प्रताप ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ीं।
वह बड़ी मस्तानी चाल चल रहा है।
ऐंठना आदि क्रियाओं के दोनों रूप मिलते हैं —
पानी में रस्सी ऐंठती है।
नौकर रस्सी ऐंठ रहा है।
उसका सिर खुजलाता है।
वह अपना सिर खुजलाता है।
To give your reviews on this book, Please Login