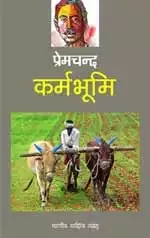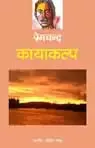|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
|||||||
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
अमर कोठरी से बाहर पाँव न निकाल सका।
मुन्नी ने फिर कहा–‘क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? तुम आज चाहो तो कह सकते हो ख़बरदार, मेरे पास मत आना। और मुँह से चाहे न कहते हो; पर व्यवहार से रोज़ ही कह रहे हो। आज कितने दिनों से देख रही हूँ; लेकिन बेहयाई करके आती हूँ, बोलती हूँ, ख़ुशामद करती हूँ। अगर इस तरह आँखें फेरनी थीं, तो पहले ही से उस तरह क्यों न रहे; लेकिन मैं क्या बकने लगी। तुम्हें देर हो रही, जाओ।’
अमरकान्त ने जैसे रस्सी तुड़ाने का ज़ोर लगाकर कहा–‘तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मुन्नी। मैं तो जैसे पहले रहता था, वैसे ही अब भी रहता हूँ। हाँ, इधर काम अधिक होने से ज़्यादा बातचीत का अवसर नहीं मिलता।’
मुन्नी ने आँखें नीची करके गूढ़ भाव से कहा– ‘तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ लेकिन वह बात नहीं है। तुम्हें भरम हो रहा है।’
अमरकान्त ने आश्चर्य से कहा–‘तुम तो पहेलियों में बातें करने लगीं।’
मुन्नी ने उसी भाव से जवाब दिया–‘आदमी का मन फिर जाता है, तो सीधी बातें भी पहेली–सी लगती हैं।’
फिर वह दूध का खाली कटोरा उठाकर जल्दी से चली गयी।
अमरकान्त का हृदय मसोसने लगा। मुन्नी सम्मोहन-शक्ति से उसे अपनी ओर खींचने लगी। ‘तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें भरम हो रहा है।’ यह वाक्य किसी गहरे खड्ड की भाँति उसके हृदय को भयभीत कर रहा था। उसमें उतरते दिल काँपता था, रास्ता उसी खड्ड में से जाता था।
वह न-जाने कितनी देर अचेत-सा खड़ा रहा। सहसा आत्मानन्द ने पुकारा–‘क्या आज शाला बन्द रहेगी?’
३
इस इलाक़े के ज़मीदार एक महन्तजी थे। कारकून और मुख़्तार उन्हीं के चेले-चापड़ थे। इसलिए लगान बराबर वसूल होता था। ठाकुरद्वारे में कोई-न-कोई उत्सव होता ही रहता था। कभी ठाकुरजी का जन्म है, कभी ब्याह है, कभी यज्ञोपवीत है, कभी झूला है, कभी जल-विहार है। असामियों को इन अवसरों पर बेगार देनी पड़ती थी; भेंट-न्योछावर पूजा-चढ़ावा आदि नामों से दस्तूर चुकानी पड़ती थी; लेकिन धर्म के मुआमले में कौन मुँह खोलता? धर्मसंकट सबसे बड़ा संकट है। फिर इलाके के काश्तकार सभी नीच जातियों के लोग थे। गाँव पीछे दो-चार ब्राह्मण-क्षत्रियों के थे भी, तो उनकी सहानुभूति असामियों की ओर न होकर महन्तजी की ओर थी। किसी-न-किसी रूप में वे सभी महन्तजी के सेवक थे। असामियों को उन्हें प्रसन्न रखना पड़ता था। बेचारे एक तो ग़रीब, ऋण के बोझ से दबे हुए, दूसरे मूर्ख; न क़ायदा जाने, न क़ानून; महन्तजी जितना चाहे इज़ाफ़ा करें, जब चाहें बेदखल करें, किसी में बोलने का साहस न था। अकसर खेतों का लगान इतना बढ़ गया था कि सारी उपज लगान के बराबर भी न पहुँचती थी; किन्तु लोग भाग्य को रोकर, भूके-नंगे रहकर, कुत्तों की मौत मरकर, खेत जोतते जाते थे। करें क्या? कितनों ही ने जाकर शहरों में नौकरी कर ली थी। कितने ही मज़ूरी करने लगे थे। फिर भी असामियों की कमी न थी। कृषि प्रधान देश में खेती केवल जीविका का साधन नहीं है, सम्मान की वस्तु भी है। गृहस्थ कहलवाना गर्व की बात है। किसान गृहस्थी में अपना सर्वस्व खोकर विदेश जाता है, वहाँ से धन कमाकर लाता है और फिर गृहस्थी करता है। मान प्रतिष्ठा का मोह औरों की भाँति उसे घेरे रहता है। वह गृहस्थ रहकर जीना और गृहस्थी ही में मरना भी चाहता है। उसका बाल-बाल कर्ज़ से बंधा हो, लेकिन द्वार पर दो-चार बैला बाँधकर वह अपने को धन्य समझता है। उसे माल में ३६० दिन आधे पेट खाकर रहना पड़े; पुआल में घुसकर रातें काटनी पड़ें, बेबसी से जीना और बेबसी से मरना पड़े, कोई चिन्ता नहीं, वह गृहस्थ तो है। यह गर्व उसकी सारी दुर्गति की पुरौती कर देता है।
|
|||||