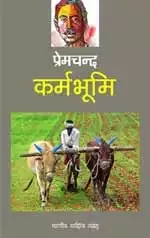|
उपन्यास >> कर्मभूमि (उपन्यास) कर्मभूमि (उपन्यास)प्रेमचन्द
|
31 पाठक हैं |
|||||||
प्रेमचन्द्र का आधुनिक उपन्यास…
‘बड़े हर्ष से! मैं तो तुमसे कई बार कह चुका। तुमने सुनाई ही नहीं।’
‘मैं तुमसे डरती हूँ। तुम मुझे नीच और क्या-क्या समझने लगोगे।’
अमर ने मानो क्षुब्ध होकर कहा–‘अच्छी बात है, मत कहो। मैं तो जो कुछ हूँ, वह रहूँगा, तुम्हारे बनाने से तो नहीं बन सकता।’
मुन्नी ने हारकर कहा–‘तुम तो लाला ज़रा-सी बात पर चिढ़ जाते हो, जभी स्त्री से तुम्हारी नहीं पटती। अच्छा लो, सुनो। जो जी में आये समझना–मैं जब काशी से चली, तो थोड़ी देर तक मुझे होश ही न रहा–कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ। फिर मैं रोने लगी। अपने प्यारों का मोह सागर की भाँति मन में उमड़ पड़ा और मैं उससे डूबने-उतराने लगी। अब मालूम हुआ, क्या कुछ खोकर मैं चली जा रही हूँ। ऐसा जान पड़ता था कि मेरा बालक मेरी गोद में आने के लिए हुमक रहा है। ऐसा मोह मेरे मन में कभी न जागा था। मैं उसकी याद करने लगी। उसका हँसना और रोना, उसकी तोतली बातें, उसका लटपटाते हुए चलना, उसे चुप कराने के लिए चन्दा मामूँ को दिखाना, सुलाने के लिए लोरियाँ सुनाना, एक-एक बात याद आने लगी। मेरा वह छोटा-सा संसार कितना सुखमय था। उस रत्न को गोद में लेकर मैं कितनी निहाल हो जाती थी, मानो संसार की संपत्ति मेरे पैरों के नीचे है। उस मुख के बदले में स्वर्ग का सुख भी न लेती। जैसे मन की सारी अभिलाषाएँ उसी बालक में आकर जमा हो गयी हों। अपना टूटा-झोंपड़ा, अपने मैले-कुचैले कपड़े, अपना नंगा-बूचापन, क़र्ज़-दाम की चिन्ता, अपनी दरिद्रता, अपना दुर्भाग्य–ये सभी पैने काँटे जैसे फूल बन गये। अगर कोई कामना थी तो यह कि मेरे लाल को कुछ न होने पाये। और आज उसी को छोड़कर मैं न जाने कहाँ चली जा रही थी। मेरा चित्त चंचल हो गया। मन की सारी स्मृतियाँ सामने दौड़ने वाले वृक्षों की तरह, जैसे मेरे साथ दौड़ी चली आ रही थीं और उन्हीं के साथ मेरा बालक भी जैसे दौड़ा चला आता था। आख़िर मैं आगे न जा सकी। दुनिया हँसती है, हँसे; बिरादरी मुझे निकालती है, निकाल दे; मैं अपने लाल को छोड़कर न जाऊँगी। मेहनत-मजदूरी करके भी तो अपना निबाह कर सकती हूँ। अपने लाल को आँखों से देखती तो रहूँगी। उसे मेरी गोद से कौन छीन सकता है! मैं उसके लिए मरी हूँ, मैंने उसे अपने रक्त से सिरजा है। वह मेरा है। उस पर किसी का अधिकार नहीं।’
ज्योंही लखनऊ आया, मैं गाड़ी से उतर पड़ी। मैंने निश्चय कर लिया, लौटती हुई गाड़ी से काशी चली जाऊँगी। जो कुछ होना होगा, होगा।
मैं कितनी देर प्लेटफार्म पर खड़ी रही, मालूम नहीं। बिजली की बत्तियों से सारा स्टेशन जगमगा रहा था। मैं बार-बार कुलिया से पूछती थी, काशी की गाड़ी कब आयेगी?
कोई दस बजे मालूम हुआ, गाड़ी आ रही है। मैंने अपना सामान सँभाला। दिल धड़कने लगा। गाड़ी आ गयी। मुसाफिर चढ़ने-उतरने लगे। कुली ने आकर कहा–‘असबाब जनाने डब्बे में रखूँ कि मरदाने में?
|
|||||