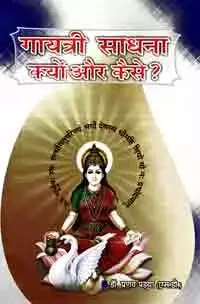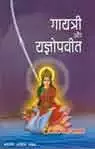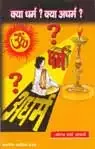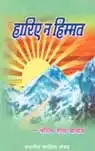|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री साधना क्यों और कैसे गायत्री साधना क्यों और कैसेश्रीराम शर्मा आचार्यडॉ. प्रणव पण्डया
|
5 पाठक हैं |
||||||
गायत्री साधना कैसे करें, जानें....
गायत्री मंत्र का भाव चिंतन
जप- ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन बहुत ही उपयोगी है। इसे दिन के अन्य समय में भी जारी रखा जा सकता है। गायत्री मंत्र का शब्दवार भावार्थ इस तरह से है-ॐ - परमात्मा, भू: - प्राण स्वरूप, मुवः -सुख स्वरूप, स्व: - दुःख नाशक, तत् - उस, सवितु: - तेजस्वी, प्रकाशवान् वरेण्य-वरण करने योग्य, श्रेष्ठ, भर्गः - पाप का नाश करने वाला, देवस्य-देने वाला, देव स्वरूप, धीमहि- धारण करें, धियो- बुद्धि को, यो- जो, न: - हमारी, प्रचोदयात्- प्रेरित करे। अर्थात् उस सुख स्वरूप, दुःख नाशक, श्रेष्ठ-तेजस्वी, पाक नाशक, प्राण स्वरूप परमात्मा को हम धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर प्रेरित करे।
इसके अर्थ पर विचार करते हुए तीन बातें प्रकट होती हैं-
(१) ईश्वर के दिव्य गुणों का चिन्तन,
(२) ईश्वर को अपने अन्दर धारण करने का भाव,
(३) सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। ये तीनों ही बातें अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।
मनुष्य जिस भी दिशा में विचार करता है, जिन वस्तुओं का चिन्तन करता है व जिन बातों पर ध्यान एकाग्र करता है, वे सब धीरे-धीरे उसकी मनोभूमि में स्थिर होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। हमारी मानसिक शक्तियां उसी दिशा में बहने लगती हैं; गुप्त-प्रकद दृश्य-अदृश्य कई तरह के रहस्य उस विषय में प्रकट होने लगते हैं और सफलताओं का तौता लग जाता है।
गायत्री मन्त्र के पहले भाग में ईश्वर के कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख है, जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर के प्राणवान् तेजस्वी,दुःख व पाप नाशक, श्रेष्ठ,आनन्द स्वरूप जैसे गुणों से भरे रूप पर जितना ध्यान एकाग्र किया जाएगा, मस्तिष्क में इनकी उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। मन इनकी ओर आकर्षित होगा, अध्यस्त बनेगा और इसी आधार पर काम करने लगेगा। इस तरह एक नयी अनुभूति, विचार धारा और कार्य पद्धति हमारे जीवन को आतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से दिन-दिन उन्नत व श्रेष्ठ बनाती जाएगी।
दूसरे भाग में, ऊपर बताये गुणों वाले परमात्मा को अपने में धारण करने की प्रतिज्ञा है। इन गुणों वाले परमात्मा का केवल चिन्तन भर किया जाए सो बात नहीं है; वरन यु गायत्री मन्त्र के साधक को सुदृढ़ आदेश है कि उस श्रेष्ठ गुणों वाले परमात्मा को अपने अन्दर धारण करें, उसे अपने रोम-रोम में ओत-प्रोत कर से। ऐसा अनुभव करें कि वह हमारे अन्दर-बाहर भर गया है और हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से उसमें डूब गया है। इस तरह की भाव धारणा से जितने समय व्यक्ति ओत-प्रोत रहेगा, उतने समय तक वह अन्दर-बाहर विकार व दुर्भाव भरे दोषों से मुक्त व हल्का रहेगा।
तीसरे भाग में, भगवान से प्रार्थना की गयी है कि वे सद्बुद्धि की प्रेरणा दें। हमें कुविचारों, नीच वासनाओं व दुष्टभावनाओं से छुड़ा कर सद्बुद्धि व विवेक से भर दें।
इस प्रार्थना में, गायत्री मंत्र के पहले व दूसरे भाग में बताए गये दिव्य गुणों को पाने के लिए उनको धारण करने के लिए उपाय बता दिया गया है, कि हमें वासना-तृष्णा और अंहकार के इशारे पर नाचने वाली दुर्बुद्धि को सही रास्ते पर लाना होगा। इसे शुद्ध-सात्विक बनाना होगा। जैसे-जैसे बुद्धि का दोष व भटकाव दूर होगा वैसे-वैसे सद्गुणों की वृद्धि होगी व उसी अनुपात में हमारा जीवन भीतर शान्ति, आनन्द और बाहर सफलता, समृद्धि से भरता जाएगा।
गायत्री के दो पुण्य प्रतीक-शिखा व यज्ञोपवीत-गायत्री साधना के साथ शिखा एवं यज्ञोपवीत रूपी दो पुण्य प्रतीक अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन्हें गायत्री मंत्र दीक्षा के समय धारण किया जाता है। इस विषय में द्विजता अर्थात् दूसरे जन्म की महत्त्वपूर्ण अवधारणा जुड़ी हुई है। इन सबके बिना साधना नहीं हो सकती या गायत्री उपासना नहीं की जा सकती हो, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर की महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है; किन्तु अपने पुण्य प्रतीकों के साथ विधिवत् एवं अधिकारपूर्ण अपनाई हुई गायत्री उपासना मंजिल को सरल बना देती है।
शिखा एवं यज्ञोपवीत देव संस्कृति के दो पुण्य प्रतीक हैं। हर महत्त्वपूर्ण दायित्त्व संभालने वाले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी और कर्त्तव्य की याद दिलाए रखने के लिए प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। पुलिस डाक्टर वकील, सिपाही आदि सभी के साथ उसके कर्त्तव्य को याद दिलाने वाले, उसका महत्त्व घोषित करने वाले चिन्ह, पोषाक के साथ जुड़े रहते हैं।
भारतीय संस्कृति में मनुष्य के चिंतन व आचरण को पशुता-पिशाचिता में जाने से रोकने और उसे मनुष्यत्व व देवत्त्व की ओर बढ़ाए रखने में ही जीवन की सार्थकता घोषित की गई है और इस महान आदर्श को अपनाने वाले हर व्यक्ति द्वारा चोटी (शिखा) व जनेऊ (यज्ञोपवीत) के रूप में महान प्रतीक चिह्नों को गौरव के साथ धारण करने का विधान रहा है।
शिखा व यज्ञोपवीत न केवल देव संस्कृति के गौरवमय प्रतीक है वरन् ऊंचे उद्देश्य व आदर्शों के जीवन्त प्रतिनिधि भी हैं। देवसंस्कृति की मान्यता है कि जन्म से सभी मनुष्य पशुस्तर के होते हैं और उनमें भी वासना, स्वार्थ, ईर्ष्या-द्वेष जैसी अनेकों पिछड़ी आदतें पाई जाती हैं। बड़े होने पर उन्हें इनसे उबरने और पार होने का पाठ पढ़ाया जाता है। इस प्रयास को ही संस्कार, दीक्षा, द्विजता, यज्ञोपवीत आदि नामों से जाना जाता है।
पहला जन्म माँ के पेट से होता है और दूसरा आचार्य द्वारा किया जाता है। आचार्य अपने शिष्य की मनोभूमि को साफ करता है, उसमें श्रेष्ठ विचारों के बीज बोता है, उन्हें सींचता है, सुधारता है और रखवाली करता है। पहले की जंगली जमीन समय पर सुन्दर बाग बन जाती है। इस भारी परिवर्तन को कायाकल्प या दूसरा जन्म भी कह सकते हैं। पशुता-पिशाचता के नीच व नारकीय जीवन को छोड़कर इन्सानियत के जीवन को अपनाने के संकल्प के साथ आचार्य द्वारा दी गई गायत्री दीक्षा, नए जन्म के समान होती है। इस तरह गायत्री उपासक ''द्विज'' कहलाता है।
अब जीवन आदर्शों के लिए जीने की प्रतिज्ञा के साथ आरम्भ होता है। यज्ञोपवीत धारण इसी द्विजत्व की प्रतिज्ञा, घोषणा एवं आस्था है। जनेऊ पहनने के साथ ही दिजत्व अर्थात् दूसरे जन्म की शुरुआत होती है और संस्कृति की यह महान् परम्परा मनुष्य को उच्च आदर्शों के अनुरूप जीने की प्रेरणा देती है। वस्तुत: यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान् प्रतिमा है। अन्य देवी देवताओं को तो प्रतिमा रूप में किन्ही विशेष स्थानों पर ही स्थापित किया जाता है, किन्तु गायत्री महाशक्ति की सर्वोपरि उपयोगिता को देखते हुए इसे इतना महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि यज्ञोपवीत की प्रतिमा को हर घड़ी छाती से लगाकर रखना, हृदय में धारण किए रहना आवश्यक माना गया।
|
|||||