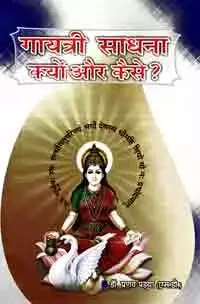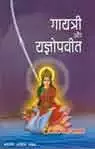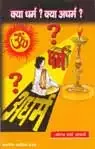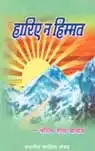|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री साधना क्यों और कैसे गायत्री साधना क्यों और कैसेश्रीराम शर्मा आचार्यडॉ. प्रणव पण्डया
|
5 पाठक हैं |
||||||
गायत्री साधना कैसे करें, जानें....
धरती की कामधेनु गायत्री
पुराणों में उल्लेख आता है कि स्वर्ग में देवताओं के पास कामधेनु गाय है, जो अमृत जैसा दूध देती है, उसे पीकर देवता लोग सदा सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसके समीप जो जाता है, उसकी सभी इच्छाएँ पूरी हो जाती है।
स्वर्ग की इस कामधेनु की सच्चाई तो देवता ही जाने, किन्तु इस धरती पर यह कामधेनु गौ, गायत्री शक्ति ही है। गायत्री उपासना से सभी इष्णाएँ शांत होने लगती हैं। असंभव अनावश्यक और अनुपयोगी कामनाओं का शमन हो जाने से अपने आप वह स्थिति बनने लगती है, जिसे मनोकामना पूर्ति कहते हैं। कामधेनु का दूध पीकर सभी पाप-ताप दूर हो जाते हैं। गायत्री की शरण में जाकर इसके अमृतरस का पान करने वाला भी अपने दुःख कष्टों और पाप-तापों से हस्का होने लगता है।
वास्तव में मनुष्य का असली रूप आनन्द भरा है। आनन्दमग्न रहना ही उसका प्रधान गुण है। दुःख के हटते और मिटते ही वह मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। मनुष्य भी स्वर्ग के देवताओं की तरह आनन्दित रह सकता है, यदि उसके कष्ट कारणों का समाधान हो जाए। गायत्री साधना यही काम करती है।
मनुष्य के दुःखी व परेशान रहने के मूल तीन ही कारण है-
१. अज्ञान अर्थात् नासमझी,
२. अशक्ति अर्थात् दुर्बलता और
३. अभाव- दरिद्रता।
अज्ञानता अर्थात् नासमझी- इसके कारण ही व्यक्ति उल्टा-पुलटा सोचता है। जो नहीं सोचना चाहिए वह सोचता है और उलझनों में फसकर हैरान, परेशान व दुःखी रहता है। अपनी शक्ति व क्षमता का सही ज्ञान न होने केकारण ऐसे असंभव काम हाथ में लेता है जिनमें असफलता और निराशा ही हाथ लगती है। दूसरे व्यक्ति व परिवेश की सच्चाइयों की सही जानकारी न होने के कारण झूठी आशा-अपेक्षा और कल्पनाओं में जीता है, अंतत: खिन्नता और निराशा में चुटता हुआ दुःखी रहता है। अपनी नासमझी के कारण ही दूर के फायदों को न सोचता हुआ क्षणिक सुख व लाभ के चवर में ऐसे काम कर बैठता है कि पीछे दुःख और पश्चात्ताप ही हाथ लगते हैं।
उल्टी सोच के कारण छोटी-छोटी बातें भी बड़ी दुःख भरी लगती है। परिजन अबूझों की मृत्यु साथियों की भिन्न रुचि और परिस्थतियों के उतार-चढ़ाव आदि स्वाभाविक है; किन्तु अपनी अज्ञानता के कारण व्यक्ति इन्हें नकारता है और सोचता है कि मैं जैसा पाएं वैसा ही हो। प्रतिकूलता सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत जब घटना होती है, तो भारी कष्ट होता है।
अशक्ति अर्थात् दुर्बलता- मनुष्य को कदम-कदम पर घोर पीड़ा व यातना भरा जीवन जीने के लिए विवश करती है। ऐसे में व्यक्ति अपने स्वाभाविक व जन्म सिद्ध अधिकारों का भार तक अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं हो पाता और इनसे वंचित ही रह कर दीन-हीन व दरिद्र-दयनीय हालत में पड़े रहने के लिए मजबूर होता है। यदि स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ हो, बीमारी घेरे हुए हो, तो स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, सुन्दर दृश्य, धन-दौलत व जीवन के अन्य सुख-साधन कोई कहने लायक सुख नहीं दे पाते हैं, बल्कि भार स्वरूप और दुःख देने वाले ही लगते हैं।
बौद्धिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति साहित्य, दर्शन काव्य, विज्ञान आदि के अध्ययन व चिंतन-मनन का रस नहीं ले सकता। आत्मिक निर्बलता के कारण स्वाध्याय, सत्संग, भजन-भक्ति आदि का आनन्द दुर्लभ ही रह जाता है। इतना ही नहीं, कमजोरों को मिटाने के लिए प्रकृति का ''उत्तम की रक्षा'' का सिद्धान्त काम करता है। निर्बलों को मिटाने-सताने के लिए अनेकों चीजें प्रकट हो जाती हैं। छोटी-छोटी बातें भी उन पर भारी पड़ती हैं। सर्दी जहाँ खिलाड़ियों को मजबूत बनाती है कमजोर को सर्दी, निमोनिया व गठिया जैसी समस्याएँ खड़ी करती है। कमजोर को दुःख-कष्ट ही नहीं, भले तत्व भी आशाप्रद लाभ नहीं दे पाते, वहीं सबल-वीर दुःख-कष्ट भरी चुनौतियों के बीच ही अपनी शक्ति व गुणों का विकास करता है।
साधनों के अभाव में योग्य व समर्थ व्यक्ति भी बेबस व लुह्म- पुह्म महसूस करते हैं और दुःख उठाते हैं। अन्न-वस्त्र, मित्र-सहयोगी, धन-औषधि व पुस्तक आदि के अभाव में तरह-तरह की पीड़ा व कठिनाई उठानी पड़ती है।
गायत्री रूपी कामधेनु की ही-सद्बुद्धि प्रधान, श्रीं-समृद्धि प्रधान और क्लीं-शक्ति प्रधान, तीन शक्तियां अपने साधक के अज्ञान, अशक्ति और अभाव जन्य कष्टों का समाधान करती हुई, उसके दुःखों को दूर करती है।
हर युग में गायत्री महिमा का गुणगान-अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण ही गायत्री महाशक्ति को भारतीय संस्कृति की जननी होने का गौरव प्राप्त है। हर युग में ऋषि-मुनियों, महापुरुषों एवं विद्वानों ने इसकी महिमा का गुणगान किया है। अन्य विषयों पर उनके मतभेद हो सकते हैं; किन्तु गायत्री के विषय में वैदिक युग से आधुनिक समय तक सभी ने एक मत से गायत्री की महिमा को स्वीकारा है।
अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति में इसे साधक को आयु प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज देने वाला बताया गया है। विश्वामित्र के अनुसार गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। भगवान मनु के अनुसार- गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। योगिराज याज्ञवस्थ्य के अनुसार-यदि एक तराजू में एक ओर समस्त वेदों को और दूसरी ओर गायत्री को तोला जाय, तो गायत्री का पलड़ा भारी रहेगा। अत्रि मुनि के अनुसार- जो व्यक्ति गायत्री तत्त्व को भली-भांति समझ लेता है, उसके लिए संसार में कोई दुःख शेष नहीं रह जाता। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जैसे फल का रस शहद, दूध का सार घी है उसी प्रकार वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। ऋषि भफाज के अनुसार-ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं, वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। नारद जी का कथन है कि गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है, वहाँ नारायण के निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
इसी तरह फे विचार प्रायः सभी ऋषियों के मिलते है। बुद्धि तर्क और प्रत्यक्षवाद के इस युग के दार्शनिकों व आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्त्व को उसी प्रकार स्वीकारा है जैसा कि प्राचीन काल के ऋषि-मुनि लोग मानते थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार भारतवर्ष को जगाने वाला मंत्र इतना सरल है कि उसका एक श्वास में ही उच्चारण किया जा सकता है और वह है गायत्री मंत्र। स्वामी विवेकानन्द इसे सद्बुद्धि का मंत्र होने के नाते मंत्रों का छटमीण मानते थे। रामकृष्ण परमहंस इसकी अद्भुत शक्ति को मानते थे व लम्बी साधनाओं की बजाए इस छोटी सी गायत्री साधना का सुझाव दिया करते थे। मदन मोहन मालवीय ची इसे ऋषियों के द्वारा दिए गए अमूल्य रत्नों में सर्वोपरि मानते थे, जो आत्मा को प्रकाशित कर तमाम बंधनों से मुक्ति देती है और लौकिक अभावों को दूर करती है। लोकमान्य तिलक कहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हमें राजनैतिक संघर्ष के अतिरिक्त आत्मा के अंदर प्रकाश पैदा करना होगा और यह काम करने की प्रचण्ड सामर्थ्य गायत्री मंत्र में भरी हुई है। महात्मा गांधी इसके रोग रक्षक, शान्तिदायक व आत्मा के लिए प्रगतिकारक प्रभाव को मानते थे। योगी अरविन्द इसको आत्मा के विभिन्न स्तरों को प्रकाश्ति करने वाली प्रचण्ड शक्ति मानते थे तथा उन्होंने कइयों को साधना के बतौर गायत्री का जप बताया था।
जगद्गुरु शंकराचार्य के अनुसार गायत्री आदि मंत्र है, इसकी महिमा का गान मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। जीवन लक्ष्य को पाने की समझ जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। स्वामी रामतीर्थ के वचन-राम को पाना सबसे बड़ा काम है और गायत्री से शुद्ध हुई बुद्धि ही राम को पा सकती है। एस. राधाकृष्णन् के अनुसार यह जीवन के स्रोत से जोड़ने वाली सार्वभौम प्रार्थना है, जो ठोस लाभ देती है। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द इसे सबसे श्रेष्ठ मंत्र, वेदों का मूल गुरुमंत्र मानते थे। वे इसके श्रद्धालु उपासक थे व दूसरों को भी इसके जप व पुरश्चरण साधनाओं के लिए प्रेरित करते थे। थियोसॉफिकल सोसायटी के वरिष्ठ साधक प्रो. आर. श्रीनिवास के शब्दों में-गायत्री के अर्थ व रहस्य को मन और हृदय में एकाग्र करके जब कोई शुद्ध उच्चारण करता है तो उसका सम्बन्ध सूर्य में विद्यमान महान् शक्ति से जुड़ जाता है। जिससे उसके अन्दर-बाहर एक विराट् आध्यात्मिक प्रभाव पैदा होता है।
इन सभी उद्गारों से स्पष्ट होता है कि गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास या अंधपरम्परा नहीं है, बल्कि उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाले ठोस तत्त्व छिपे हैं, जो भौतिक दृष्टि से भी व्यक्ति को सम्पन्न बनाने में समर्थ हैं।
गायत्री शक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं-जीवन में सद्बुद्धि के आने पर ही बाहरी सफलता व सुख-समृद्धि का राजमार्ग खुलता है। इस रूप में गायत्री शक्ति का सहारा लिए बिना कोई चारा नहीं है। इसी तरह ईश्वर प्राप्ति, आत्म दर्शन या जीवन मुक्ति आदि को लक्ष्य मानने वालों के लिए भी गायत्री तत्त्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असम्भव है, क्योंकि केवल ईश्वर प्राप्ति को जीवन लक्ष्य बनाने वालों को भी यह जानना चाहिए कि परमात्मा स्वयं में निराकार व गुणों से परे है। वह इन्द्रियों की पकड़ से बाहर और बुद्धि व चिंतन की क्षमता से दूर है। वह न किसी से प्रेम करता है और न द्वेष। उस तक सीधी पहुँच नहीं हो सकती।
जीवात्मा और परमात्मा फे बीच सूस्म प्रकृति का गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। इस पर्दे को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही काम करना होता है। चिंतन-मनन, ध्यान-प्रार्थना, व्रत-अनुष्ठान व साधना आदि सभी आध्यात्मिक उपचार इसी प्रयोजन के लिए हैं। इन सबको छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सतोगुणी माया और चित् शक्ति द्वारा ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन करने वाली शक्ति गायत्री ही है। गायत्री रूपी सीढ़ी को चढ़ते हुए ही परमात्मा रूपी छत तक पहुंच हो सकती है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियों और उनकी अनुभव शक्ति ही लुप्त हो जाती है। इसलिए भक्ति व ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित परमात्मा की, राधे-श्याम सीता-राम, लक्ष्मी-नारायण, पार्वती-शिव की ही उपासना करते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, महामाया सीता राधा सावित्री, पार्वती आदि रूप में गायत्री की ही उपासना की जाती है।
गीता में भगुवान् कृष्ण ने स्वयं कहा है-'गायत्री छन्दसामश्मू' अर्थात् गायत्री मैं ही हूं। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से बड़ा और कोई मंत्र नहीं हो सकता। अतः यह सोच अज्ञानता ही कही जाएगी कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री आवश्यक नहीं है। यह तो अनिवार्य है। नाम से कोई विरोध करे या आपत्ति उठाए यह अलग बात है किन्तु गायत्री शक्ति से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है।
गायत्री माता के रूप में विश्वनारी की पवित्र उपासना-गायत्री उपासना में ईश्वर को माता के रूप में भजने का सुअवसर मिलता है। संसार में मां का प्रेम सबसे पवित्र, निर्मल और उच्च कोटि का होता है। माता अपनी संतान से जितना प्रेम करती है, उतना कोई अन्य सम्बन्धी नहीं कर सकता। जवानी के उफान में पति-पली में भी अधिक प्रेम देखा जाता है; किन्तु अपने असली रूप में यह माता के प्रेम की तुलना में बहुत ही हल्का और उथला बैठता है। यह प्रेम आपसी आदान-प्रदान स्वार्थ, आशा-अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। इसमें कमी या बाधा पड़ते ही इस प्रेम को विरोध में बदलते भी देर नहीं लगती; किन्तु मां का प्रेम इस तरह के दोषों व विघ्न-बाधाओं से मुक्त होता है। शिशु-संतान से प्रतिफल मिलना तो दूर, उल्टे अनेक कष्ट ही होते हैं। इस पर भी वह वात्सल्य की परम सात्विक प्रेमधारा बालक को पिलाती रहती है। कुपुत्र होने पर भी माता की भावनाएँ घटती .नहीं। कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है; किन्तु माता कुमाता नहीं हो सकती।
भगवान को हम जिस भी रूप में मानते हैं, वह उसी रूप में हमें जवाब देते हैं व अनुभूति कराते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनका अनन्य प्रेम पाना चाहते हैं। तब माता के रूप में उन्हें भजना सबसे सही और अनुकूल बैठता है। माता का जैसा वात्सल्य अपने बालक पर होता है, वैसा ही प्रेम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए भगवान से मातृ सम्बन्ध स्थापित करना आत्मविद्या के मनोवैज्ञानिक रहस्यों के आधार पर अधिक उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होता है। प्रभु को माता मानकर जगज्जननी वेदमाता के रूप में उसकी उपासना से भगवान् की ओर से वैसी ही वात्सल्य भरी प्रतिक्रिया होगी, जैसी कि माता को अपने बच्चे के प्रति होती है। माता की गोदी में बालक अपने को सबसे अधिक आनन्दित व सुरक्षित-संतुष्ट अनुभव करता है।
नारी शक्ति पुरुष के लिए सब प्रकार से आदरणीय, पूजनीय और पोषणीय है। पत्नी के रूप में, बहिन एवं माता के रूप में वह मैत्री योग्य, स्नेह करने योग्य एवं गुरुवत् पूजन करने योग्य है। पुरुष के शुष्क अंतर में यदि नारी द्वारा अमृत सिंचन नहीं हो पाता है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार वह बड़ा रूखा, बर्बर कर्कश, कर, निराश संकीर्ण और अविकसित रह जाता है। वर्षा से जैसे पृथ्वी का हृदय हर्षित हो जाता है और उसकी प्रसन्नता ही हरियाली एवं फूल-फलों के रूप में फूट पड़ती है। पुरुष भी नारी की स्नेह वर्षा से इसी प्रकार सिंचन प्राप्त करके अपनी शक्तियों का विकास करता है; किन्तु एक भारी विन्न इस रास्ते में आता है, जो अमृत को विष बना देता है और वह है वासना का विन्न। दुराचार, कुदृष्टि एवं वासना के मिलने से नर-नारी के मिलने से प्राप्त होने वाला अमृत फल विष बीज बन जाता है।
इस विष विकार की भावना के शमन के लिए गायत्री साधना परम उपयोगी है। विश्वनारी के रूप में भगवान की मातृ भाव से, परम पवित्र भावनाओं के साथ उपासना करना, मातृ जाति के प्रति पवित्रता को अधिकाधिक बढ़ाता है। इस दिशा में जितनी सफलता मिलती जाती है, उसी अनुपात में इन्द्रिय संयम, मनोनिग्रह और मनोविकारों का शमन अपने आप होता जाता है। मातृभक्त के हृदय में दुर्भावनाएं अधिक देर नहीं ठहर सकतीं। विश्वनारी के रूप में भगवान की उपासना नर पूजा से श्रेष्ठ ही सिद्ध होती है।
|
|||||