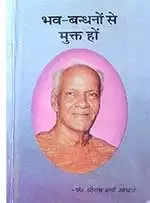|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> भाव बंधनों से मुक्त हों भाव बंधनों से मुक्त होंश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति की आवश्यकता और उपाय
भव-बन्धनों से मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति
बन्धन और मुक्ति कहाँ है? स्वर्ग और नरक कैसा है? यह जानने के लिये किसी स्थान विशेष को तलाश करने की दौड़-धूप पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने भीतर देखा जा सकता है। देखा ही नहीं, अनुभव भी किया जा सकता है।
दोनों का वर्णन-विवरण एक-दूसरे से भिन्न है। तो भी वे इतने सटे हुए हैं कि उनकी दीवार से दीवार मिली है। अन्तर इतना ही है कि एक का मुँह पूरब को है तो दूसरे का उससे उलटी दिशा पश्चिम को है। एक सिरा स्वर्ग जैसे आनन्द और देवतत्वों की भरमार से जुड़ा है, दूसरा उसके ठीक विपरीत है, वह नरक की यातना और असह्य यंत्रणा और सिर चकराने वाली दुर्गन्ध से भरा है।
दोनों में से किसी को चुनने के लिये मनुष्य स्वतंत्र है। किसी पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं है कि कौन किस क्षेत्र में प्रवेश करे। जिसका जिधर मन हो, वह उधर जाने वाली सड़क को स्वेच्छापूर्वक अपना सकता है और उस पर चल सकता है। प्रवेश भी प्रतिबंधित नहीं है। जिसमें भी प्रवेश करना हो खुशी-खुशी घुसा जा सकता है। प्रवेश पाने और निवास करने पर उन परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, जो उस क्षेत्र के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं।
काया और आत्मा यह दोनों ही तत्त्व मिलकर जीवन बनाते हैं। इनके पारस्परिक सहयोग से ही निर्वाह होता है। दोनों के बीच संतुलन बना रहे उनमें से प्रत्येक को उचित स्थान सम्मान और पोषण मिले तो फिर दो पहियों की गाड़ी की तरह जीवन-क्रिया सही दिशा में निर्वाध रूप से चलती रहती है, उसमें न व्यतिक्रम होता है, न व्यवधान पड़ता है।
कठिनाई तब पड़ती है जब भ्रमितों की तरह कुछ की कुछ समझने की भूल होती है। भटकने वाली पगडण्डी पकड़ी जाती है और कुछ ही दूर चलने पर कँटीले झाड़-झंखाड़ों में उलझ जाने की परिस्थिति बन जाती है।
जीवन दो साझीदारों का सम्मिलित व्यवसाय है। दोनों का समान श्रम और समान पूँजी निवेश होना चाहिये। दोनों का अधिकार भी औचित्य की सीमा में रहना चाहिये और लाभांश का बँटवारा भी न्यायोचित होना चाहिये। यदि यह रीति-नीति ठीक प्रकार चलती रहे, तो विग्रह का अवसर खड़ा न हो और हम मानवी गरिमा के उस स्तर पर जमे रहें, जिसे देवोपम कहा जाता है। बात तब बिगड़ती है जब एक पक्ष को सब कुछ बना दिया जाता है और दूसरे पक्ष की अवज्ञा की जाती है। यह भूल आमतौर से इस प्रकार होती है कि दर्पण में दीखने वाले प्रत्यक्ष काय कलेवर को ही सब कुछ मान लिया जाता है और श्रेय-सुविधाओं का सारा परिकर उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। शरीर की सुख-सुविधा आकाश और प्रगति को अतिशय महत्व देने का प्रतिफल यह होता है कि आत्मा को जो पोषण मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। अत: आत्मिक क्षेत्र में दरिद्रता, विपन्नता भर जाती है। शरीर ही अपनी लिप्सा, लालसाओं को उपयोग करता रहता है। उसकी स्वाभाविक प्रकृति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरह अधोगामी है। विलास और वैभव को वह इतनी अधिक मात्रा में चाहने, माँगने लगता है, जो उसकी वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक है। उसे जुटाने में आत्मा का पक्ष विस्मृत एवं उपेक्षित हो जाता है। आदर्शों के प्रतिपालन की बात विस्मृत हो जाती है और लोभ, मोह अहंकार की पूर्ति के लिये वह किया जाने लगता है, जिसमें औचित्य का प्रत्यक्ष व्यतिक्रम है।
शरीर और आत्मा हैं तो सहयोगी और एक ही घर में रहते हैं। वे चाहें, तो सामंजस्य बनाकर भी निर्वाह कर सकते हैं; पर होता इसके विपरीत है। शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा परोक्ष। प्रत्यक्ष में प्रतीति होती है और परोक्ष के बन्धन में मोटी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती। उसका महत्व स्वीकार नहीं करती और जो कुछ उसके निमित्त किया जाना चाहिये, सो भी नहीं करती। ऐसी दशा में शरीर ही सब कुछ बन जाता है और आत्म-पक्ष अभावग्रस्त, हेय, हीन स्थिति में समय गुजारने के लिये विवश होता है।
शरीर की, इन्द्रियों की, वैभव की वासना, तृष्णा जब अनियंत्रित हो जाती है, तो अपनी असीम कामनाओं की पूर्ति के लिये वह करने लगती है, जो उसे नहीं करना चाहिये; वह मानने और चाहने लगती है, जिसकी वस्तुत: उसे कुछ आवश्यकता है नहीं।
यह स्थिति आत्मा को स्वीकार नहीं। वह अपना हक भी माँगती है और जो अनुचित किया जा रहा है उसका विरोभ भी करती है। खींचतान के मूल केन्द्र यही हैं और यहीं से वह अन्तर्द्वन्द खड़ा होता है, जिसका परिणाम आन्तरिक स्वतंत्रता गँवा बैठने और शरीर की गुलामी स्वीकार करने के रूप में सामने आता है। लिप्साओं की पूर्ति की जाती रहती है। साथ ही आत्म हनन भी होता रहता है। तराजू का एक पलड़ा कुछ नीचे झुकाया जाय तो दूसरा हलका पड़ेगा और ऊपर लटकेगा, संतुलन बिगड़ जायेगा। इसी असंतुलन का नाम भ्रष्ट जीवन है। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण आत्मिक बन्धन के चिन्ह हैं। लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी और अहंकार की तौक पहनकर मनुष्य पूरी तरह भव-बन्धनों में आबद्ध हो जाता है। काया को विलास चाहिये और वैभव। वह भी इतनी बड़ी मात्रा में जिसकी कोई सीमा न हो। यह वह प्यास है, जो आग पर घी डालने पर भड़कने वाली अग्नि की तरह कितने ही साधन मिलने पर भी तृप्त नहीं होती। जब कामनाओं का वेग सिर पर असाधारण रूप से सवार होता है तो नीति और मर्यादाओं के सारे बाँध तोड़ देता है और वह सब करने लगता है, जो नहीं करना चाहिये। इसकी परिणति उन परिस्थतियों में होती है, जिन्हे नरक कहते हैं-आन्तरिक असंतोष, सम्पर्क क्षेत्र का अविश्वास और गहन अन्तराल में जमने वाले कुसंस्कारों से भविष्य की अन्धकार भरी परिणति। यही सब मिलकर आधि-व्याधियों के के रूप में सामने आते हैं; अपयश और अविश्वास का वातावरण बनाते हैं; आत्म प्रताड़ना निरन्तर सहनी पड़ती है और समाजदण्ड, राजदण्ड, प्रतिशोध का निरन्तर भय बना रहता हैं। इस सबका सम्मिश्रण ही नरक है। इस प्रताड़ना का एक मात्र कारण है शरीर के प्रति असाधारण आसक्ति। उसे ही अपना स्वरूप मान बैठना। उसी को सुखी बनाने के लिए जघन्य और घृणित कार्य पर उतारू रहना। मनःस्थिति की प्रतिक्रिया ही परिस्थितियों के रूप में सामने आती है और तपते हुए नरक की तरह झुलसाती है।
नरक से बचने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिये दृष्टिकोण बदलने के अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपना आत्म-भाव जगाना पड़ता है और मान्यता को इस गहराई तक पहुँचाना पड़ता है कि अपनी सत्ता आत्मा के रूप में परिलक्षित हो और शरीर मात्र आवरण प्रतीत हो। आवरण की रक्षा करते रहना ही पर्याप्त मालुम पड़े और यह स्मरण जागृत बना रहे कि वह सोचना और वह करना है, जो आत्म-गौरव के अनुरूप और अनुकूल है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना युवराज बनाया और साथ ही यह दायित्व सौंपा है कि अपने को पवित्र और प्रखर बनाते हुए अपूर्णता को दूर करे। साथ ही विश्व उद्यान के माली की तरह उसे वह करने के लिये कहा, जिससे इस विश्व वाटिका में प्रगतिशीलता एवं सुसंस्कारिता बढ़े। इन दोनों कर्तव्यों की पूति में संलग्न रहना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है साथ ही यथार्थता भी।
आत्म-बोध का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य अपने को ईश्वर का वंशधर समझे और चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को इस योग्य बनाये, जो उसकी गौरव-गरिमा के अनुरूप है। दृष्टिकोण का ऐसा परिवर्तन ही स्वर्ग द्वार में प्रवेश पाना है। उत्कृष्टता के लक्ष्य को अपना लेने पर आदर्शवादी क्रियाकलाप ही बन पड़ते हैं। राजमार्ग का अवलम्बन लेने पर भटकाव की कहीं गुजायश नहीं रहती। प्रलोभनों के आकर्षण उसे अपनी ओर खींच नहीं पाते। किसी के विरोधी हो जाने पर हानि पहुँचाने के भय और दबाव भी उसे इस स्थिति में नहीं पहुंचाते, जिसमे उसे अवांछनीय या अनैतिक कार्य करने पर उतारू होना पड़े।
चिन्तन में उत्कृष्टता और आचरण में आदर्शवादिता की समुचित मात्रा भर लेना यही देव जीवन है। जिनने पशुता और पैशाचिकता को निकृष्टता का परित्याग कर दिया, जो ऊँचा सोचता, ऊँचा करता, वह ऊँचा उठता भी है। स्वर्ग ऊर्ध्व दिशा में है। वह किसी स्थान या लोक से संबंधित नहीं है। अपना अन्तःकरण ही वह स्थान है, जिसमें स्वर्ग तो रहता ही है, पर कोई चाहे तो उसे धकेल कर नरक की निकृष्टता को भी प्रतिष्ठित कर सकता है। यह मनुष्य स्वयं ही चुनता और वरण करता है। इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है।
प्रत्येक पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र उसकी परम्परा एवं प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखे। ईश्वर भी अपने युवराज मनुष्य से यही अपेक्षा करता है कि वह देव जीवन जिये, अपनी विचारणा में उत्कृष्टता और क्रियाकलाप में आदर्शवादिता की मात्रा न घटने दे। अपने सम्पर्क क्षेत्र का वातावरण ऐसा बनाये, जिसे स्वर्गोपम कहा जा सके। इसी आधार पर अपना भीतरी और बाहरी ढाँचा सुव्यवस्थित कर लेना हीं-बन्धनों को तोड़कर मोक्ष पाना, नरक से निकलकर स्वर्ग में प्रवेश पाना है। यह सब दृष्टिकोण के परिवर्तन और परिष्कार से ही संभव हो पाता है।
|
|||||