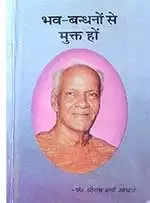|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> भाव बंधनों से मुक्त हों भाव बंधनों से मुक्त होंश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति की आवश्यकता और उपाय
तृष्णा : दुर्गति की गहरी खाई
आवश्कताओं को पूरा करना एक बात है और अपव्यय में उड़ाने, ठाट-बाट बनाने और संग्रह करने की प्रवृत्ति सर्वथा दूसरी। इनमें से प्रथम को उचित और दूसरी को अनुचित ठहराया गया है।
आवश्यकताओं का कोई मापदण्ड होना चाहिये, अन्यथा विलासिता और शेखीखोरी को भी अपनी विशिष्टता बताते हुए आवश्यकताओं की श्रेणी में गिना और गिनाया जा सकता है। अपनी प्रकृति ही ऐसी बन गयी है, अपना स्वभाव ही ऐसा हो गया है, जिसे मजबूरी बताकर अमीरों जैसी सजधज को भी सही बताया जा सकता है, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न कहा जा सकता है। कहीं अदालत में तो जबाव देना नहीं है, अपने मन को समझाना और दूसरों का मुँह बन्द करना भर है। ऐसी दशा में कोई कुछ भी कर सकता है और शान-शौकत को भी आवश्यकता ठहराया जा सकता है।
उचित आवश्यकता का मापदण्ड यह है कि वह औसत नागरिक स्तर की होनी चाहिये। औसत नागरिक का अर्थ है अपने देशवासियों में से मध्यम वर्ग के लोगों जैसा रहन-सहन। अपने देश में भी धन-कुबेर रहते हैं और दरिद्रनारायण भी। इन दोनों वर्गों को अतिवादी या अपवाद कहा जा सकता है। औसत अर्थ होता है-मध्यम वर्ग। अपने देशवासियों का उल्लेख करने का अर्थ यह है कि जिस समुदाय में रहा जा रहा है, उसकी स्थिति का आकलन। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कुबैत जैसे देशों की बात छोड़ी जा सकती है क्योंकि वहाँ का सामान्य व्यक्ति भी यहाँ के असामान्यों से बढ़कर होता है। इसी प्रकार वनवासी कबीलों की बात भी छोड़ी जा सकती है, वे तो कपड़े के अभाव में पत्ती के परिधान बनाकर ही शरीर ढक सकते है। औसत आदमी न दरिद्र होता है, न सम्पन्न। यही है औसत नागरिक की परिभाषा। इसी स्थिति में अपनी, अपने परिवार की स्वस्थता, शिक्षा, चिकित्सा, आतिथ्य जैसी जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। इससे कम की अभावग्रस्त स्थिति में स्थिरता और प्रगति रुकती हैं। इससे अधिक ऊँचा स्तर होने पर अनेक प्रकार की उलझनें उलझती और समस्यायें खड़ी होती हैं।
तृष्णा का परामर्श और दबाव यह है कि अपने पास सम्पदा का बड़ा भण्डार होना चाहिये जिससे बुढ़ापा चैन से कट सके। परिवार को बैठे-ठाले ब्याज-भाड़े की आमदनी से निर्वाह करते रहने का अवसर मिले। उन्हें व्यय की व्यवस्था बनाने के लिये परिश्रम पुरुषार्थ न करना पड़े।
यह दृष्टिकोण आकर्षक और निश्चिन्तता उत्पन्न करने वाला उचित प्रतीत होता है, पर है यह अर्थशास्त्र के सर्वथा विपरीत। संसार में दौलत सीमित मात्रा में है। वह इतनी है कि सभी लोग अपनी जरूरतें पूरी करते रहें, जीवन की नाव खेते रहें। प्रकृति इतना ही उत्पादन करती है। अमीर बनने का अर्थ हैं दूसरे असंख्यों को गरीबी की स्थिति में रहने के लिये विवश करना, स्वयं परिश्रम न करना, अपनों को न करने देना अर्थात् उनके बदले का काम अतिरिक्त रूप से दूसरों पर लादने का माहौल बनाना। उत्पादन के साथ श्रम लड़ा हुआ है। यह श्रम आमतौर से निर्वाह के साधन जुटाने के लिये ही किया जाता है। हर उपभोक्ता को अपनी आवश्यकताये जुटाने के अनुरूप श्रम भी करना चाहिये। अमीरी का दर्शन इस स्वाभाविकता के सर्वथा विपरति है। अमीर उपभोग के लिये ही नही, संग्रह के लिये भी दौलत चाहता हैं। साथ ही उसकी इच्छा यह भी होती है कि उपार्जन के लिये कठोर श्रम न करना पड़े। यह प्रकृति विरुद्ध इच्छा कैसे पूरी हो। इसके लिये उसे जो तरीके अपनाने पड़ते हैं उसमें से अधिकांश अनैतिक होते हैं। साथ ही निष्ठुर व्यक्ति ही अधिकाधिक खर्च करने की बात सोच सकता है, क्योंकि हर किसी के लिए सामाजिक ऋण चुकाना भी आवश्यक है। इसके लिये उदारता अपनाने, पिछड़ों को उठाने के लिये सहायता करने की आवश्यकता पड़ती है। जो उस ओर से आंखें बन्द किये रहेगा, उसी के लिये यह संभव है कि विलासी और संही वने।
व्यक्ति पूर्णतया आत्म-निर्भर नहीं है। उसे दूसरे असंख्यों की सहायता से अपना संतुलन बिठाना पड़ता है। अन्त, वस्त्र, औषधि, शिक्षा शिल्प आदि कोई व्यक्ति मात्र अपने प्रयत्न से प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयुक्त होने वाली प्राय: सभी वस्तुएँ दूसरों द्वारा विनिर्मित होती हैं। उन्हें भले ही मूल्य देकर खरीदा गया हो, पर हैं निश्चित रूप से ऐसी, जिन्हें स्वयं निर्मित नहीं किया जा सकता। सुई से लेकर कलम तक हर वस्तु विनिर्मित होने में असंख्यों का श्रम और कौशल जुड़ा होता हैं। उनकी पूरी कीमत कोई नहीं चुका सकता। खरीदने में जो दिया जाता है, वह तो प्रतीक पात्र है। उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, पर मात्र उतना देकर पूरी तरह कोई उऋण नहीं हो सकता है। इसके लिये समूचे समाज का हमें कृतज्ञ होना चाहिये। अन्य लोगों के कौशल का लाभ तो उठाते रहा जाय, किन्तु अपने अनुदान से समाज का हित करने में कृपणता बरती जाय, तो वह कृतघ्नता भी होगी और निष्ठुरता भी।
कोई व्यक्ति उचित खर्च से अधिक कमाता है, तो विश्व परिवार का सदस्य होने के नाते हर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि उस बचत को उनके लिये खर्च करे, जो अभी भी पिछड़ी हुई स्थिति में पड़े हुए हैं। दो नालियों के बीच यदि एक नीची बना दी जाय. तो ऊँचा पानी नीची की ओर बहने लगेगा और बहाव तब तक जारी रहेगा, जब तक कि सतह एक-सी नहीं हो जाती। मनुष्य जाति में भी यही प्रथा परम्परा चलनी चाहिये कि ऊँची उठी हुई स्थिति वाले अपने साधनों को उन्हें देते रहें, जो नीचे हैं, पिछड़े हैं। यह भी दैनिक आवश्यकताओं में समिलित होना चाहिये। इसे भी कर्तव्य और दायित्व समझना चाहिये।
दूसरे के घर में पली, बढ़ी वयस्क लड़की जब अपने घर वधू रूप में मुफ्त मिल सकती है, तो अपना भी फर्ज हो जाता है कि पुत्री को दूसरे का घर सभालने के लिये उसी प्रकार दे दें। पाने की तरह देना भी आवश्यक है। यही प्रकृति परम्परा है। हमें भी इसका निर्वाह करना चाहिये। समाज के ऋण से ऋणी मनुष्य के लिये यह भी उचित है। उस समुदाय को सुखी समुन्नत बवनाने के लिये अपने उपार्जन का, साधन का एक बड़ा हिस्सा अन्यों के लिये अनुदान स्वरूप प्रदान करें। तृष्णा के दलदल में फँसा हुआ व्यक्ति यह नहीं कर सकता। उसकी निजी हविश ही इतनी बड़ी-चढ़ी होती है कि अपने उपार्जन के अतिरिक्त अन्यों के अधिकार हड़पने के उपरान्त भी उसकी पूर्ति न हो सके। फिर देने का प्रश्न ही कहाँ उठता है?
मनुष्य की संरचना ऐसी है कि वह एक सीमित मात्रा में ही साधनों का उपयोग कर सकता है। पेट भरने के लिये प्राय: सीमित मात्रा में ही आहार लिया जाता है। तन ढकने को कपड़ा भी सीमित मात्रा में ही अभीष्ट होता है। विस्तार की परिधि भी समान होती है। इतना ही हजम भी हो सकता है। जो उग्रर्त मात्रा में हड़पेगा, वह चोर की तरह दण्ड भुगतेगा। अधिक आहार, अधिक वस्त्र, अधिक बिस्तर का प्रयोग करने पर सुविधा के स्थान पर संकट ही खड़ा होगा।
धन के सम्बन्ध में भी यही बात है। र्स्थ साधारण की तुलना में जिसके पास भी अधिक होगा, वह अनेकों मुसबितों में घिरेगा। ईर्ष्यालु इसे चैन से न बैठने देगे और नीचा दिखाने के षड्यंत्र बनाते रहेगे। कर्ज और चन्दा माँगने वाले, हिस्सा बँटाने वाले अपने-अपने ढंग की घात चलेगे। अत्यधिक उपयोग दुर्व्यसनों में हो सकता है। नशेबाजी आवारागर्दी, शेखी जैसी कुटेबें पीछे लगेंगी। व्यभिचार की दिशा में कदम बढ़ेगे। चापलूस, ठग, मित्र बनकर शत्रु जैसी घात करेगे। मुकद्दमेबाजी, बीमारी, अव्याशी जैसे कामों में पैसा पानी की तरह बहेगा। इस प्रकार खोटी कमाई खोटे रास्ते हो अपने आप चले जाने की राह बना लेगी। अपने पल्ले हर घड़ी उद्विग्न रहने को स्थिति ही बनी रहेगी। आन्तरिक अशान्ति से शारारिक और मानसिक क्षेत्र खोखले बनते हैं और गरीबों की अपेक्षा कहीं अधिक जल्दी संसार से बिस्तर गोल करना पड़ता है।
यह सोचना व्यर्थ है कि सन्तान पर अधिक खर्च करने अधिक सुविधा देने से वे समुन्नत बनेगे या देने वाले के प्रति कृतज्ञ रहेगे। तृष्णा अपने तक ही सीमित नहीं रहती, वह उत्तराधिकारियों तक भी चली जाती है। वे प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ पूर्वजों के पास है, वह अधिक जल्दी मिल जाय। इसलिये उन्हें वृद्ध अभिभावकों को निःस्वत्व बनाना पड़ता है ताकि उन्हें मिलने वाली राशि कही अन्यत्र न चली जाय। मन ही मन उनके मरने की कामना करते हैं ताकि जो देर से मिलना है वह जल्दी ही मिल जाय। देखा गया है कि बाप-दादों की सम्पदा के बँटवारे पर आये दिन कलह मचते मुकद्दमे चलते और खून-खराबी तक के षड्यत्र बनते हैं। इस प्रकार जिनके सुख के लिये कठोर परिश्रम ही नहीं, अनाचार भी अपनाया था, परमार्थ हेतु कलेजे को पत्थर जैसा कठोर बनाकर रखा गया था, वे भी उसका अहसान नहीं मानते, वरन् अपना हक कहते हैं और कम देने का अन्यत्र खर्च कर देने का इल्जाम लगाते हैं। उनका स्वभाव और चरित्र भी गये-गुजरे स्तर का बन जाता है, जिसके कारण वे स्वावलम्बी सदाचारी और प्रगतिशील बनने से वंचित ही रह जाते हैं। मुफ्त की सम्पदा किसी को हजम नहीं होती। वह पारे की तरह फूट-फूटकर निकलती है। पचती वही है, जो मेहनत और सही रास्ते से कमायी गयी है। सन्तान को मौज करने की इच्छा से जो सम्पदा जोड़ते हैं, वे अपनी आँखों से ही उसकी व्यर्थता और दुष्परिणति देखते हैं जिनके लिये बचपन में लाड़-दुलार में अन्धाधुन्ध खर्च किया गया है, वे बड़े होने पर फिजूलखर्ची की आदत से इस प्रकार जकड़ जाते हैं कि उन्हें सदा अभावग्रस्त स्थिति ही दीखती रहती है। उस गड्ढे को भरने के लिये उचित-अनुचित सभी कुछ बटोरते और फिजूलखर्ची में उड़ाते हुए सदा खाली हाथ रहते हैं।
तृष्णा का कुचक्र इतना बड़ा, इतना अशान्त और इतना भयानक है कि उसे अपनाकर मौज-मजा करने के दिवास्वप्न निष्फल ही सिद्ध होते रहते हैं।
शरीर के सभी अंग संतुलित हों, तभी सुन्दर-सुडौल बनते है। सब अंग सामान्य हों और कोई एक अवयव क्या हुआ सूजा हुआ बढ़ा हुआ हो, तो वह स्वयं तो कुरूप लगेगा ही, समूचे शरीर की शोभा बिगाड़ देगा। सामान्य लोगों के बीच एक व्यक्ति असामान्य होकर रहे तो वह प्रशंसा का पात्र नहीं बनता और न सम्मान पाता है वरन् निन्दा और ईर्ष्या का भाजन बनता, अनेकों लांछन ओढ़ता है स्वार्थी, कृपण, निष्ठुर आदि समझा जाता है। कोई जमाना था जब अमीरों को भाग्यवान पूर्वजन्म का पुण्यात्मा समझा जाता था, पर अब तो बात बिल्कुल उल्टी हो गयी है। साम्यवादी सिद्धान्तों की पैठ मन में गहराई तक हो गयी है। सम्पन्नों को शोषक-बेईमान आदि के लांछन ही सहने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तृष्णातुर व्यक्ति अपनी समूची सम्पत्ति स्वार्थ सिद्धि में ही लगा देता है। परमार्थ के नाम पर कुछ ठोस कदम उसकी संकीर्णता उठाने ही नहीं देती, झूठी वाहवाही कूटने के लिये कुछ अस्वाद भले ही करता रहे।
|
|||||