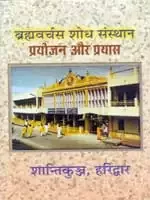|
नई पुस्तकें >> ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान प्रयोजन और प्रयास ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान प्रयोजन और प्रयासश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है ब्रह्मवर्चस् का प्रयोजन और प्रयास
वनौषधि उपचार एक-संजीवनी विद्या
वनस्पतियाँ इस पृथ्वी पर, प्रकृति का भिन्न प्रकार का प्राणवान उत्पादन हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी, उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। आहार के रूप में अन्न, शाक, फल आदि वनस्पतियों के ही भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार हैं। पशु भी घास, दूब आदि के रूप में उन्हीं से आहार पाते हैं। कीड़े आदि भी उन्हीं के सहारे जीवित रहते हैं। माँसाहारी प्राणी भी शाकाहारी जीवों को ही भोजन बनाते हैं। प्रकारान्तर से उनका भोजन भी वनस्पतियों पर ही निर्भर है।
भोजन के अतिरिक्त जमीन को शक्ति देनेवाली खाद भी वनस्पतियों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तरह-तरह के रसायन भी उनसे प्राप्त होते हैं। दुर्बलता दूर करने के लिए उपयोगी रसायन वनस्पतियाँ ही देती हैं। शरीर के रोगाणुओं से निपटने में भी उन्हीं की भूमिका रहती है। इस प्रकार वनस्पतियाँ जीवन निर्वाह का आधार तो हैं ही, दुर्बलता और रुग्णता के निवारण में भी उन्हीं का योगदान है।
पृथ्वी पर वनस्पतियाँ प्राणियों के लिए क्या-क्या योगदान देती हैं? इसका अध्ययन गहराई से किया जाय, तो उनके अनुदानों के प्रति नतमस्तक ही होना पड़ता है। वायु में शुद्धता वाले अंश वनस्पतियों के अनुग्रह से जुड़ते हैं। बादलों को धरती पर बरसने के लिए वही आकर्षित करती हैं। खाद्य को पकाने के लिए आग का ईधन उनसे ही प्राप्त होता है। मकान बनाने में, उपकरण तैयार करने में, अनेक उद्योगों के लिये भी किसी न किसी रूप में उनका उपयोग करना पड़ता है। कागज से लेकर कपड़े तक में वनस्पतियों का ही प्रयोग होता है। यह कहना गलत नहीं है कि वनस्पतियाँ न होतीं तो जीवधारियों का अस्तित्व न रहता।
खाद्य के रूप में कौन प्राणी किस वनस्पति का उपयोग, कब किस रूप में करे, इस जानकारी को आहार-विज्ञान कहते हैं। इस विद्या को जीवन-धारिणी विद्या भी कह सकते हैं। सही प्रयोग होने पर वनस्पतियाँ अमृत-तुल्य बन जाती हैं और दुरुपयोग होने पर विष जैसीं प्रतिक्रिया भी करती हैं। अनुभवों के आधार पर आहार के सूत्र काफी पहले ही खोजे जा चुके हैं। रोग-निवारण के लिए, उपचार के लिए भी वनौधियों के उपयोग के सूत्र आयुर्वेद ने निकाले और प्रयुक्त किए हैं। इसके लिए तत्त्वदर्शी स्तर के शोधकर्ताओं को लम्बे समय तक खोज, प्रयोग, सुधार का क्रम चलाना पड़ा था।
दुर्बलता और रोगों का निवारण मनुष्यों की एक बड़ी समस्या है। दुर्बलता मनुष्य को लाचार बना देती है, वह इच्छित पुरुषार्थ नहीं कर पाता। इसलिए सबकी इच्छा शरीर को स्वस्थ और सुन्दर रखने की होती है। स्वास्थ्य के नियम इसीलिए हर व्यक्ति को सीखने-समझने पड़ते हैं। दुर्बलता से आगे की व्यथा ''रुग्णता'' है। जो रोग शरीरगत होते हैं, उन्हें ''व्याधि'' तथा मानसिक रोगों को ''आधि'' कहा जाता है। दोनों में से कोई भी हो, रुग्णता हर दृष्टि से भयानक होती है। उसके कारण पीड़ा सहनी पड़ती है, परिचर्या के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। कार्य क्षमता घटने से उपार्जन घटता है और अभाव घेर लेते हैं। रोगी के आश्रितों पर विपत्ति टूट पड़ती है। रोगी मौत के पास खिसकता जाता है। इस लिए उपयुक्त चिकित्सा के साधन विकसित करने पड़ते हैं।
आजकल तीव्र प्रतिक्रिया पैदा करने वाले रसायनों से उपचार किया जाने लगा है। इसके लिए विष भी प्रयोग में लाये जाते हैं। मारक, शामक दवाओं की अनेक किस्में हैं पर वो इच्छित क्रिया के साथ प्रतिक्रियाएँ भी उत्पन्न करती हैं। उतावले रोगी और चिकित्सक उनका उपयोग तो करते हैं; परन्तु दूरगामी परिणाम देखने पर लगता है कि लाभ के लिए किए गए उपचारों ने, शरीर को पहले से भी गयी-गुजरी स्थिति में पहुँचा दिया। सही चिकित्सा विधि का जब कभी पता लगाया जाएगा, तब शरीर पोषण को तरह ही, रोगों के उपचार के लिए भी वनस्पतियों को ही आधार बनाया जाएगा।
वनस्पतियों से प्राप्त रसायन और खनिज, शरीर में सहज रूप से रम जाते हैं। अन्य रसायन तथा खनिज शरीर में अधिक समय टिक नहीं पाते, प्रकृति द्वारा बाहर कर दिये जाते हैं। शरीर उन्हें सजातीय मानकर आत्मसात नहीं करता। विजातीय तत्त्वों को अंदर ले जाने, फिर उनकी सफाई करने में शरीर की शक्तियों का क्षय ही होता है। इसलिए शरीर के लिए अनिवार्य समझे जाने वाले तत्वों की पूर्ति, वनस्पतियों के माध्यम से करना अधिक कारगर माना जाता है। जिन दिनों वनौषधि विद्या अपने सही रूप में थी, तब उसे संजीवनी विद्या कहा जाता था। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने से लेकर, वृद्ध च्यवन को युवा बनाने जैसे चमत्कारी प्रतिफल सामने आते रहते थे; किन्तु अब तो उनका प्रचलन मिटने के साथ-साथ पहचान भी नहीं रही। औषधि से मिलती-जुलती कोई भी पत्ती उसके नाम से चला दी जाती है। उखाड़ते समय वह तैयार हो पायी थी? पकी थी या नहीं? यह भी ध्यान नहीं दिया जाता। फिर उसे लम्बे समय तक बोरियों भरकर रख लिया जाता है। वे प्रयोग के समय तक प्राणहीन हो चुकी होती हैं। किस क्षेत्र में कौन सी औषधि अपने पूरे गुण प्राप्त कर पाती है, यह जानकारी भी बहुत महत्त्व की है। हिमालय की संजीवनी बूटी यदि लंका में उगायी जा सकती, तो सुषेण वैद्य हनुमान को इतनी दूर क्यों भेजते? नारियल का पेड़ हर जगह नहीं फलता। मैसूर का चन्दन अन्य स्थानों पर बढ़ता है पर सुगन्धि पैदा नहीं होती। भूमि और जलवायु के संयोग से ही वनस्पतियों के गुणों का विकास होता है।
मनुष्य जिस क्षेत्र में पैदा होता या रहता है, उसके लिए उसी क्षेत्र का उत्पादन उपयोगी होता है। शाक, फल, अन्न सब में यही बात है वनौषधियों के सम्बन्ध में भी यही दृष्टि रखनी पड़ती है। कुछ आपद्कालीन अपवादों को छोड़कर साधारण रूप से यही सिद्धान्त काम करता है। शरीर रचना में जिस जलवायु का योगदान रहा है, उसी जलवायु में उत्पन्न खाद्य और औषधियाँ शरीर के लिए अधिक सजातीय होती हैं। इसलिए उनका उपयोग अधिक कारगर सिद्ध होता है। वनौषधियों के उपयोग में इन दिनों इन सब बातों के प्रति उपेक्षा ही बरती देखी जाती है। इसी कारण उसका वैसा प्रभाव नहीं होता जैसा शास्त्रों में लिखा है।
हमें अपनी भूल सुधारनी होगी। संजीवनी-विद्या के रूप में जानी जाने वाली वनौषधि-चिकित्सा को, उसके वास्तविक रूप में लाने के लिए प्रबल प्रयत्न करना होगा। तभी इस अमोघ कहे जाने वाले 'रामबाण' अस्त्र का सही लाभ जनसाधारण तक पहुँचाया जा सकेगा।
अमीर लोग तो बहुत कीमती दवायें जहाँ-तहाँ से मँगा सकते हैं; परन्तु अपने निर्धन देश की आम जनता के लिए सर्वसुर्लभ जड़ी-बूटी चिकित्सा ही कारगर बैठती है। इसलिए अपने चिकित्सालयों को अधिक खर्चीला न होने देने के लिए जड़ी-बूटियों का व्यापक उत्पादन और सही विधि-विधान जीवन्त बनाना होगा। स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों के पालन का पक्ष भी लोगों को बताया-समझाया जाना आवश्यक है। चिकित्सा-विज्ञान में, इस विद्या का भी समुचित समावेश किया जाना आवश्यक हो गया है।
रसायनों पर आधारित पाश्चात्य चिकित्सा-प्रणाली के विपरीत, वनौषधि उपचार का लक्ष्य होता है-शरीर में स्वस्थ जीवकणों की शक्ति और मात्रा बढ़ाना। बढ़ी हुई स्वस्थता, बीमारियों का कचरा धकेल कर बाहर निकालने में समर्थ हो जाती है। इस पद्धति में रोगों से पूरी तरह पीछा छूटने में कुछ समय लग सकता है; परन्तु जो लाभ होते हैं, वे स्थाई होते हैं। बढ़ी हुई जीवनीशक्ति, रोगों को दूर करने के साथ-साथ समर्थता के हर पक्ष को भी पुष्ट करती है। इसलिए जड़ी-बूटी चिकित्सा से रोग-मुक्ति और सामर्थ्य बढ़ने के दोहरे लाभ मिलते हैं।
रसायनों पर आधारित चिकित्सा जादू के खेलों जैसी सामयिक चमक तो दिखा देती है; परन्तु उसके मारक गुणों के कारण होने वाली जीवनी-शक्ति की हानि को भुला दिया जाता है। ऐसी दवायें चमत्कारी तो दिखती हैं; परन्तु कुछ समय बाद वे अन्य नशों की तरह आदत में शामिल हो जाती हैं। तब उनका प्रभाव होना भी समाप्त हो जाता है।
जड़ी-बूटियाँ सौम्य और हानिरहित होती हैं। उनका प्रभाव शरीर के साथ-साथ मनःस्थिति पर भी पड़ता है। मस्तिष्क के असंतुलन दूर होते हैं। सौम्य-सात्विक विचारों का प्रवाह उठने लगता है। 'जैसा खाये अत्र, वैसा बने मन' की कहावत केवल आहार पर ही नहीं, औषधियों पर भी लागू होती है। सौम्य जड़ी-बूटियों से शरीर के रोगों के साथ मानसिक अस्त-व्यस्तता से भी
छुटकारा मिलता है। बढ़ते हुए सद्विचार, स्वभाव में मिली हुई अवांछनीयताओं को दूर करते हैं। दूरदर्शी विवेकशीलता बढ़ती है। शरीर और मन दोनों को चिरस्थायी लाभ प्राप्त होते हैं।
वनस्पतियाँ ईश्वर-प्रकृति द्वारा विकसित आदर्श सहयोगी हैं। जड़ी-बूटियों के रूप में वे आरोग्य और स्वास्थ्य बढ़ाने की असाधारण शक्ति रखती हैं। उन्हें अपनाया जाना हर दृष्टि से लाभदायक है।
इस विद्या को विज्ञान सम्मत बनाया जाए
सही और शुद्ध रूप में होने पर ही कोई वस्तु अपना ठीक-ठीक प्रभाव दिखा पाती है। नकली वस्तुएँ उपहास का कारण बनती ही हैं, उनसे असफलता और असंतोष भी उत्पन्न होते हैं। नकली सोना, नकली तलवार, नकली आटा, नकली दवा आदि मन बहलाने भर के लिए अपनी झलक दिखला पाते हैं। बाद में तो वे उपेक्षा के गड्डे में फेंक ही दिये जाते हैं। खोटे सिक्कों का भी यही हाल होता है। जानवरों के शकल के खिलौने सस्ते मोल में बिकते हैं; परन्तु उनसे सिर्फ खेला जा सकता है, वे जानवरों जैसे उपयोगी नहीं हो सकते।
इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि जड़ी-बूटियों के नाम पर नकली घास-पात ही बिकता देखा जाता है। मिलती-जुलती शक्ल की कई वनस्पतियाँ होती हैं। दुर्लभ जड़ी-बूटियों के स्थान पर वे रख दी जाती हैं-जिनकी भरमार होती है। आम आदमी उनके बीच फर्क कैसे निकाल सकता है? एलोपैथिक दवाएँ निर्धारित समय के बाद गुणहीन ही नहीं, हानिकारक भी हो जाती हैं। जड़ी- बूटियाँ हानिकारक नहीं होतीं; परन्तु नौ माह से एक वर्ष तक भरकर रखने के बाद निर्जीव- बेकार तो हो ही जाती हैं। परन्तु पन्सारी लोग एक बार भरकर रखी जड़ी-बूटियाँ वर्षों तक बेचते रहते हैं। कुटी-पिसी दवाएँ तो और भी जल्दी बेजान हो जाती हैं; परन्तु उन्हें फेंककर नुकसान उठाना कौन पसंद करता है? ऐसी स्थिति में प्रामाणिकता और गुण कहाँ रह सकते हैं? इस घपले को सुधारना वह पहला चरण है, जिसके बिना जड़ी-बूटियों की उस गरिमा को फिर से जीवित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण आयुर्वेद संसार भर में प्रसिद्ध था। उसका प्रभाव सभी जगह एक स्वर से स्वीकारा जाता था।
उस पुरातन गरिमा को फिर से उभारना है, तो ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि वनौषधियाँ अपने असली रूप में मिलती रहें। उनके उत्पादन पर भी पूरा ध्यान देना होगा। अभी तो इकट्ठा करने वाले उन्हें जड़ से ही खोद लाते हैं। उन्हें फिर से पनपने का मौका ही नहीं मिलता। बीज भी कभी बिखर पाते हैं, कभी नहीं। ऐसी स्थिति में एक वर्ष जहाँ वे काफी मात्रा में होती हैं, वहाँ अगले वर्ष उनका अता-पता ही नहीं रहता। यह उपेक्षा दूर की जानी चाहिए। जिस प्रकार अन्न, सब्जी, मसाले आदि के उत्पादन को महत्त्व, दिया जाता है, उनके लिये जमीन सुरक्षित रखी जाती है, उसी प्रकार जड़ी-बूटियों की भी खेती की जानी चाहिए। उसके विज्ञानसम्मत ढंग अपनाए जाने चाहिए।
आजकल प्रचलन के अनुसार घसियारे किसी जड़ी-बूटी से मिलते-जुलते घास-पात को ले आते हैं और पंसारी के हाथों बेच आते हैं। वैद्य उसी को कूट-पीसकर रोगियों को देते रहते हैं। यही चिन्ह-पूजा चलती रहती है। यह प्रचलन बन्द होना चाहिए। सही जड़ी-बूटियाँ पहचानी और प्रयुक्त की जानी चाहिए। आरम्भ सही हुए बिना परिणाम सही नहीं हो सकते।
भूमि और जलवायु (फ्लोरा) के अनुरूप विभिन्न वनौषधियाँ विभिन क्षेत्रों में उगायी जाएँ। उत्पादन एक केन्द्रीय जगह पर संग्रहीत किया जाय और वहाँ से, जिन्हें जिस वस्तु की, जिस रूप में उपलब्ध कराए जाने की माँग है, उस आवश्यकता को पूरी करते रहा जाय। यह प्रबन्ध सरकार द्वारा भी हो सकता है और निजी स्तर पर भी व्यावसायिक उत्पादन कराया जा सकता है। प्रामाणिक संग्रह व्यवस्था बन जाने पर आधी मात्रा में वह कठिनाई दूर हो जाएगी, जिसके कारण कि आयुर्वेद का प्रगतिरथ एक प्रकार से अड़ा खड़ा है।
शान्तिकुञ्ज ने जनसाधारण को स्वास्थ्य का महत्त्व समझाते हुए और उसे भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त बनाने के लिए अब उपलब्ध अपने नये विस्तृत परिसर में अपनी छोटी सी भूमि में यह उत्प्रादन कार्य सुनियोजित रीति से आरम्भ किया है। अपने प्रभाव क्षेत्र में जहाँ भी बन पड़ा है, वहाँ उस क्षेत्र की भूमि तथा जलवायु के अनुरूप वनौषधियों के उत्पादन का प्रबन्ध किया है। आदान-प्रदान के आधार पर उनका केन्द्रीय संचय भी होता रहता है। यह प्रयत्न फिलहाल छोटे आकार में है पर आशा यह की गई है कि क्रमश: यह एक आयुर्वेदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट का स्वरूप ले लेगा। प्रामाणिकता कि कसौटी पर कसे जाने पर महत्त्व देखते हुए आवश्यकता अनुभव की जायेगी, गुणविहीन-सस्ती वस्तुओं से संतुष्ट होते रहने की आदत छूटेगी। वह किया जाएगा जिसकी जड़ी-बूटी विज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए नितान्त आवश्यकता है। देश-विदेश में आयुर्वेद का गौरव प्राचीन काल की तरह पुनः प्रतिष्ठापित किया जा सकेगा।
इस दिशा में एक कठिनाई और भी है कि समान आकार-प्रकार की कितनी ही वनस्पतियाँ होती हैं। इनमें से कौन असली और कौन नकली है, इसकी पहचान की कसौटी भी अब हाथ से चली गई है। खोदनेवाले, इकट्ठा करने-खरीदने वाले, निर्माता-चिकित्सक तथा सेवनकर्ता, इस संदर्भ में सभी समान रूप से अन्धकार में हैं। कोई भी छाती ठीक कर यह नहीं कह सकता कि हम सही वस्तु के लिए ही श्रम तथा धन खर्च कर रहे हैं। उपेक्षा ने पहचान की आवश्यकता को भी नजर अन्दाज कर दिया है। अब इस दिशा में भी नये प्रयत्न करने होंगे और असली-नकली के अन्तर को सभी समझ सकें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। ऐसा एक सुनियोजित प्रयास, शान्तिकुज्ज की साधन सम्पन्न प्रयोगशाला ने अपनी सीमित क्षमता के आधार पर आरंभ कर दिया है।
इस अनुसंधान के साथ एक असमंजस और भी जुड़ गया है कि एक ही औषधि को अनेक रोगों में प्रयुक्त किये जा सकने का आयुर्वेद में उल्लेख है। सम्भव है उस प्रकार का प्रतिपादन करने वालों ने अनुपान भेद की बात को ध्यान में रखा होगा और सोचा होगा की कम औषधियों से अनेक रोगों की चिकित्सा बन पड़ने की सुगमता बनी रहे तो ठीक है।
वह चिन्तन और प्रबन्धन अपनी जगह पर सही था पर आज की कठिनाई यह है कि हर कोई सरलता चाहता है, उलझन भरे झंझटों में पड़ने से कतराता है। उसके लिए जो विशाल अध्ययन एवं अनुभव चाहिए उसकी कौन प्रतीक्षा करे? आज तो भोजन भी बना-बनाया खरीदने की सोची जाती है। चूल्हा गरम करने के झंझट से जिस प्रकार पाश्चात्य जगत में छुटकारा पाने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसी प्रकार चिकित्सा-क्षेत्र में भी यह चाहा जा रहा है कि रोगों की नियत औषधियाँ निर्धारित हो। अनुपान आदि के झंझटों में न पड़ना पड़े। ऐलोपैथी, होम्योपैथी आदि चिकित्सा विधियों मे ऐसे ही निर्धारण हैं। आयुर्वेद चिकित्सक भी व्यवहार मे इसी सरलता को बरतते हैं। वे एक ही औषधि को अनुपान भेद मे अनेक रोगों मे प्रयुक्त करने के पक्ष में दिखाई नहीं देते। नियत रोग, नियत औषधि की पद्धति ही उन्हें रास आती है। सम्भवतः अगले दिनों यही विधा अधिक सरल जान पड़ेगी और इसी को अपनाये जाने की प्रथा चल पड़ेगी। ऐसी दशा में जड़ी बूटी विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वे अमुक रोग की अमुक दवा निश्रित करने की माँग एवं सुविधा को सरल सम्भव बनाने के लिए नये अनुसंधान करे। देखना यह होगा कि किन औषधियों में पाये जाने वाले कौन से रासायनिक घटक, किन रोगों से निपट लेने में किस सीमा तक समर्थ होते हैं? यह अनुसंधान उसी स्तर का है, जिसे अपनाकर एलोपैथी मैं नई औषधियों का आविष्कार और प्रचलन होता हे। हर नयी औषधि को प्रयोगशालाओं में कठिन परीक्षा देनी होती है। साथ ही उसका प्रयोग अन्य प्राणियों पर करके, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह आविष्कार मनुष्य के लिए किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा? किस रोग के निवारण में किस स्तर का प्रभाव छोड़ सकेगा? आयुर्वेद के क्षेत्र में भी इस स्तर पर नये सिरे से प्रयोग करने की आवश्यकता है इसके बिना तर्क तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करने की बुद्धिवादी जिज्ञासा का समाधान संभव न हो सकेगा।
शान्तिकुञ्ज के ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान ने इस आवश्यकता का महत्त्व गंभीरतापूर्वक अनुभव किया है और अपनी शोध श्रृंखला में इस पक्ष को भी समुचित स्थान दिया है कि वनौषधियों के प्रभाव से किन रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका अन्वेषण उसी स्तर पर किया जाय, जिस प्रकार कि एलोपैथी विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ वनौषधि की जाँच-पड़ताल, सही पहचान हेतु आधुनिक यंत्र प्रयुक्त होते हैं तथा रोग का निदान पैथलॉजी एवं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को आधार बनाकर किया जाता है। यहाँ वात, पित्त, कफ के सिद्धान्त को नकारा नहीं जा रहा, अपितु समय की आवश्यकता, यंत्रों की उपलब्धि और विज्ञान के विकास को दृष्टिगत रखकर एक प्रामाणिक परीक्षण की आवश्यकता समझायी जा रही है।
प्राचीन काल के आयुर्वेद निर्धारण यद्यपि प्रामाणिकता से युक्त हैं, फिर भी नये युग के बढ़ते बुद्धिवाद द्वारा और प्रामाणिकता जानने की माँग को क्या कहा जाय? उसे अमान्य भी नहीं ठहराया जा सकता और शास्त्र-वचन को, पुरातनकथन को सही मान लेने की बात कहकर समझाया भी नहीं जा सकता। इन दिनों हर नियुक्ति में परीक्षा प्रणाली का समावेश है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार काम चलाती रही जड़ी बूटी विद्या के संबंध में सर्वसाधारण को स्वीकारने के लिए किस प्रकार दबाव डाला जाय? उत्तर एक ही है कि समय की माँग को स्वीकारते हुए वनौषधियों की प्रभाव क्षमता को, नये सिरे से विज्ञानसम्मत जाँच की कसौटी पर कसा जाय।
प्रभाव-सामर्थ्य की जाँच पड़ताल के अतिरिक्त, कितने समय उपरान्त किस वनौषधि की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है? इसका शोध-अन्वेषण भी शान्तिकुञ्ज की प्रयोगशाला की साक्षी में किया जाता है। इन निष्कर्षों से यह समझना संभव हो गया है कि कितने समय उपरान्त किस औषधि को गुणहीन घोषित करके उसे व्यवहार के अयोग्य ठहरा दिया जाय। अबतक ऐसे प्रतिबंध ऐलोपैथी में ही देखने को मिलते थे। वनस्पतियों के बारे में भी धारणा इतनी भर थी कि उन्हें एक वर्ष तक ही प्रयोग में लाया जाय पर अब नए शोध अनुसधानों ने इस मान्यता में संशोधन किए हैं कि कुछ जल्दी ही गुणहीन हो जाती हैं। उनपर बदलने मौसम का अधिक प्रभाव पड़ता है। इन सारी खोजबीन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस रूप में, किस औषधि की कच्ची स्थिति में अथवा विनिर्मित होने पर उसकी गुणवत्ता बनी रहती है या चली जाती है? इस निर्धारण से भविष्य में यह बन पड़ेगा कि गुणहीन वस्तुओं को विक्रेताओं या निर्माताओं को अनावश्यक समय तक उपयोग करते रहने की छूट न मिले। उन्हें नष्ट कर दिया जाना अनिवार्य हो। यह ऐसे प्रयास हैं, जिनके आधार पर जड़ी-बूटी उपचार को विज्ञानसम्मत एवं प्रामाणिक मानने के लिए विवश होना पड़ता है। भारत ही नहीं वरन् समस्त पिछड़े विश्व के लिए ऐसी विज्ञानसम्मत उपचार पद्धति सरल, सस्ती और सुविधा भरी सिद्ध हो सकेगी।
|
|||||