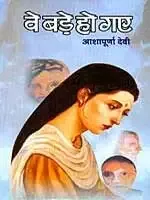|
नारी विमर्श >> वे बड़े हो गए वे बड़े हो गएआशापूर्णा देवी
|
5 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है उत्कृष्ठ उपन्यास...
25
ऐसा लगता है, अब केवल नीरा ही नहीं, सभी विपक्षी शिविर में चले गए हैं। सबकी मनोदशा कुछ ऐसी ही है कि अब लाड़-प्यार की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे घर में लाचार होकर जब रहना ही है, और रहना है तो खाना भी है, इसीलिए खा रहे हैं। और अधिक की क्या आवश्यकता है? हाँ, शायद वे भी रूठ सकते हैं। वे भी शायद सोचते होंगे, जब भाई बहन मिलकर हँसी-मजाक ही सरगर्मी में खाने में रुचि लेते थे, तब तो तुम्हें कोई शौक नहीं था। अभी हमारा मूड खराब है, खाने की मेज तक जाने का दिल ही नहीं करता, अभी तुम्हें रोज अच्छे-अच्छे पकवान बनाने का शौक हो रहा है। झींगा की मलाई करी। यह तो जमाने की बात हो गई। मटन का कोफ्ता करी। अरे बाप रे! यह दुनिया में मिल सकता है, पता ही नहीं था। फिश फ्राई, हिलसा-सरसों, मछली का चॉप, केले के फूल की तरकारी, बंदगोभी की फुलौड़ी-ये सब तो ऐतिहासिक घटनाएँ हो गई थीं।
हाँ, किसी जमाने में यह सब होता जरूर था। जब घर के मालिक का स्वास्थ्य ठीक था, खाने के शौकीन भी थे, खाने की क्षमता भी थी तब हुआ करता था यह सब। सुलेखा के ही हाथों हुआ करता था। जब से घर के मालिक के खाने की क्षमता घट गई तब से तो बच्चों ने यही जान लिया है कि दाल, रसेदार सब्जी और स्टू-इसके अलावा दुनिया में और कुछ बनता ही नहीं है।
अधिक-से-अधिक किसी बदली के दिन खिचड़ी बन गई। 'फ्रायड राइस' की तो बात ही नहीं उठती है। सवाल ही नहीं उठता गरम मुगलई पराँठों का।
मगर अभी युगों के उस पार से सावन के आने की तरह अचानक भोजन की थाली में कभी-कभी इन चीजों से साक्षात्कार हो जाता है।
रूठ ही सकते हैं वे लोग।
नीरा हमेशा से ही खाने-पीने के मामले में झंझट करती है, शौकीन खाना पसंद करती है; मगर जब मिलने पर खुशी होती थी तब तो उनके कान पर जूं नहीं रेंगती थी। तब तो माँ एक बीमार के पथ्य के साथ घर भर के लिए वही पकाकर दिल का चैन अपनी सिलाई लेकर बैठ जाती थी। अब वही नीरा पत्थर हो गई है। खाना, नहीं खाना सब उसके लिए बराबर हो गया है, और इसी समय माँ उसकी पसंद की सारी चीजें पकाकर सामने बढ़ा देती हैं।
वे सोचते हैं-अब माँ को ध्यान आया कि बेटी को खुश करें। अब तुम्हारी 'पत्थर' नीरा उससे पिघलनेवाली नहीं।
वे नहीं समझते हैं कि सुलेखा के दिल में कैसी हलचल मची है। अपने प्रिय संबंधी की निश्चित मौत की खबर सुनकर भी इससे अधिक और क्या हो सकता है? हर शाम ही तो सुलेखा अँगुली पर गिनकर देखती है-नीरा और कितने शाम उसके पास खाएगी। हर पल सुलेखा को यह बात चुभ रही है कि गिनती के कुछ दिनों के बाद नीरा फिर कभी उसके पास नहीं खाएगी।
और तभी अपने मन के तराजू पर इतने दिनों की अपनी त्रुटियों का बोझ पर्वत समान होता जा रहा है।
मगर क्या यह सच है कि समय की कमी ही उसकी त्रुटियों का कारण था? एक और मजबूरी नहीं थी क्या? हमेशा ही भोजन के शौकीन रहे निशीथ को डॉक्टर ने जब सबकुछ खाने पर अंकुश लगा दिया, तब क्या सुलेखा का कलेजा नहीं फट जाता उसी की पसंद के अच्छे-अच्छे पकवान बनाकर औरों को खिलाने में?
तकलीफ से बढ़कर भी एक और बात थी। वह था संकोच। निशीथ से संकोच भी होता था। शायद वही भावना प्रबल थी। निशीथ की जली-कटी टिप्पणियों का डर भी कम नहीं था।
संकोचहीन निशीथ अनायास ही कह सकता था, 'मेरी परवाह किसको है? मेरे लिए हलदी-पानी घोलकर कुछ बन जाता है, बाकियों के तो मजे में कट रहे हैं।'
इसी प्रकार बात करता है वह।
आजकल निशीथ उनके साथ बैठकर नहीं खाता है। अलग खा लेता है। पहले ही खाकर सो जाता है। तभी तो सुलेखा की हिम्मत इतनी बढ़ गई है।
और इतना सामान कहाँ से जुटा रही है? वह भी उसकी हिम्मत बढ़ जाने का एक और नमूना है।
सुलेखा अब खुद बाजार जाकर खरीदारी करना सीख गई है। पहले कभी उसने यह काम किया नहीं। सोचा भी नहीं था कि कभी करेगी। न हिम्मत थी उसे, न समय ही था। शायद हिम्मत की ही कमी थी दरअसल।
औरतों का बाजार जाना निशीथ को बिलकुल नहीं भाता है। जब शुरू शुरू में इसका चलन हुआ था तब बाजार जाती हुई औरतों को व्यंग्य करके निशीथ 'बाजारी औरत' कहता था।
घृणा से होंठ बिचकाकर वह कहता था, 'वह देखो, बाजारी औरतें हाथ में झोले लिये सज-धजकर चली जा रही हैं।'
बात काटना सुलेखा की आदत नहीं है। उसके सारे प्रतिरोध मन के भीतर ही उठते हैं। फिर भी ऐसी बात सुनकर उससे चुप नहीं रहा जाता था।
कहती थी, 'भगवान् ने मुँह दे दिया तो क्या इस मुँह से किसी के लिए कुछ भी कहा जा सकता है? जो बाजार जाती हैं, वे हमारे ही जैसी गृहस्थ घर की बहू-बेटियाँ हैं।'
क्या निशीथ को इस बात पर संकोच महसूस होता था?
नहीं, निशीथ ऐसा आदमी नहीं था। वह कहता था, 'आजकल जो स्टेज पर चढ़कर नाचती हैं, वे भी तुम्हारी तरह गृहस्थ घर की बहू-बेटियाँ हैं ! तो क्या मैं उन्हें शाबाशी देने लगूं?'
मन-ही-मन सुलेखा कहती थी, 'तुम्हारी शाबाशी पाने की आस में ही तो सब बैठी हैं। नहीं मिली तो मर जाएँगी सब। आँखों पर पट्टी बाँधकर घूमते हो, इसीलिए इतनी आसानी से ऐसी असभ्य बात कह देते हो।'
खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं । अब तो यह काम पूरी तरह औरतों के ही जिम्मे आ गया है। अब ऐसी टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
फिर भी एक दिन सुलेखा ने ही एक दुस्साहसपूर्ण काम करके निशीथ की यह आदत छुड़ाई थी।
निशीथ अभी-अभी बाजार से आकर हजामत बनाने बैठा था, तभी सुलेखा ने हड़बड़ाकर उसे आवाज दी, "सुनो जी, इधर खिड़की के पास जल्दी आओ तो।"
"क्यों? क्या हो गया?" "अरे, तुम आओ तो सही।"
ऐसा लगा कि हाथ पकड़कर खींच लाएगी उसे। खिड़की के पास निशीथ के आते ही बोली, "वह जो लड़की आ रही है, पहचानते हो उसे?"
निशीथ जरा मुश्किल में पड़ गया। बोला, "बुली है न?"
बुली निशीथ की ही भानजी है। हाल ही में उसके पति ने भाइयों से अलग होकर इसी मुहल्ले में फ्लैट ले लिया है।
हँसी दबाकर सुलेखा बोली, "हाँ, पहले ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। देखो न ! इतनी तेज धूप में कैसी एक जरी-किनारेवाली मद्रासी साड़ी पहन रखी है।"
निशीथ ने इस बात का दूसरा अर्थ निकाला। उसे लगा कि सुलेखा इसी बहाने उसे साड़ी के लिए ताने दे रही है। इसलिए वह निरुत्साहित होकर ...
|
|||||