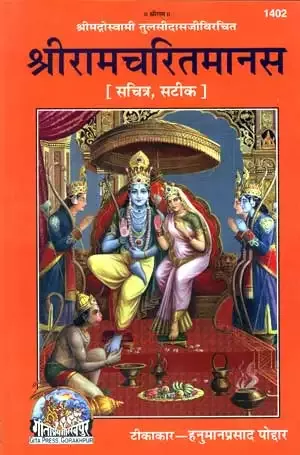श्रीरामचरितमानस (अयोध्याकाण्ड)
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: author_hindi Filename: views/read_books.php Line Number: 21 |
निःशुल्क ई-पुस्तकें >> श्रीरामचरितमानस (अयोध्याकाण्ड) |
|
|
|
वैसे तो रामचरितमानस की कथा में तत्त्वज्ञान यत्र-तत्र-सर्वत्र फैला हुआ है परन्तु उत्तरकाण्ड में तो तुलसी के ज्ञान की छटा ही अद्भुत है। बड़े ही सरल और नम्र विधि से तुलसीदास साधकों को प्रभुज्ञान का अमृत पिलाते हैं।
वसिष्ठ-भरत-संवाद, श्रीरामजी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी
कहत राम गुन सील सुभाऊ।
सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ॥
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी।
सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी॥
सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ॥
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी।
सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी॥
श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके नेत्रोंमें जल भर आया और वे शरीरसे पुलकित हो गये। फिर लक्ष्मणजी और सीताजीके प्रेमकी बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेहमें मग्न हो गये॥४॥
दो०-सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ।
हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ॥१७१॥
हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ॥१७१॥
मुनिनाथने विलखकर (दुःखी होकर) कहा-हे भरत! सुनो, भावी (होनहार) बड़ी बलवान् है। हानि-लाभ, जीवन-मरण और यश-अपयश, ये सब विधाताके हाथ हैं ॥१७१॥
अस बिचारि केहि देइअ दोसू।
ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू॥
तात बिचारु करहु मन माहीं।
सोच जोगु दसरथु नृपु नाहीं॥
ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू॥
तात बिचारु करहु मन माहीं।
सोच जोगु दसरथु नृपु नाहीं॥
ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय? और व्यर्थ किसपर क्रोध किया जाय? हे तात! मनमें विचार करो। राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं हैं ॥१॥
सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना।
तजि निज धरमु बिषय लयलीना॥
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना।
जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥
तजि निज धरमु बिषय लयलीना॥
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना।
जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥
सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिये जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय-भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है॥२॥
सोचिअ बयसु कृपन धनवानू।
जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥
सोचिअ सद्रु बिप्र अवमानी।
मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी॥
जो न अतिथि सिव भगति सुजानू॥
सोचिअ सद्रु बिप्र अवमानी।
मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी॥
उस वैश्यका सोच करना चाहिये जो धनवान् होकर भी कंजूस है, और जो अतिथिसत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्रका सोच करना चाहिये जो ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला, बहुत बोलनेवाला, मान-बड़ाई चाहनेवाला और ज्ञानका घमंड रखनेवाला है॥३॥
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी।
कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी॥
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई।
जो नहिं गुर आयसु अनुसरई॥
कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी॥
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई।
जो नहिं गुर आयसु अनुसरई॥
पुन: उस स्त्रीका सोच करना चाहिये जो पति को छलनेवाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-व्रत को छोड़ देता है और गुरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं चलता॥४॥
सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग।
सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग॥१७२॥
सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग॥१७२॥
उस गृहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहवश कर्ममार्ग का त्याग कर देता है; उस संन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपञ्चमें फँसा हुआ है और ज्ञान वैराग्यसे हीन है॥१७२॥
बैखानस सोइ सोचै जोगू।
तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी।
जननि जनक गुर बंधु बिरोधी॥
तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी।
जननि जनक गुर बंधु बिरोधी॥
वानप्रस्थ वही सोच करनेयोग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिये जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा माता, पिता, गुरु एवं भाई-बन्धुओंके साथ विरोध रखनेवाला है ॥१॥
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी।
निज तनु पोषक निरदय भारी॥
सोचनीय सबहीं बिधि सोई।
जो न छाड़ि छलु हरि जन होई॥
निज तनु पोषक निरदय भारी॥
सोचनीय सबहीं बिधि सोई।
जो न छाड़ि छलु हरि जन होई॥
सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकारसे सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरिका भक्त नहीं होता ॥२॥
सोचनीय नहिं कोसलराऊ।
भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥
भयउ न अहइ न अब होनिहारा।
भूप भरत जस पिता तुम्हारा॥
भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥
भयउ न अहइ न अब होनिहारा।
भूप भरत जस पिता तुम्हारा॥
कोसलराज दशरथजी सोच करनेयोग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट है। हे भरत! तुम्हारे पिता-जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होनेका ही है।।३।।
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा।
बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा॥
बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा॥
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र और दिक्पाल सभी दशरथजीके गुणोंकी कथाएँ कहा करते हैं।॥ ४॥
दो०-- कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु।
राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥१७३॥
राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥१७३॥
हे तात! कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न-सरीखे पवित्र पुत्र हैं? ॥१७३॥
सब प्रकार भूपति बड़भागी।
बादि बिषादु करिअ तेहि लागी।
यह सुनि समुझि सोचु परिहरहू।
सिर धरि राज रजायसु करहू॥
बादि बिषादु करिअ तेहि लागी।
यह सुनि समुझि सोचु परिहरहू।
सिर धरि राज रजायसु करहू॥
राजा सब प्रकारसे बड़भागी थे। उनके लिये विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो॥१॥
रायँ राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा।
पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा॥
तजे रामु जेहिं बचनहि लागी।
तनु परिहरेउ राम बिरहागी॥
पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा॥
तजे रामु जेहिं बचनहि लागी।
तनु परिहरेउ राम बिरहागी॥
राजाने राजपद तुमको दिया है। पिताका वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये, जिन्होंने वचनके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी अग्निमें अपने शरीरकी आहुति दे दी।॥ २॥
नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना।
करहु तात पितु बचन प्रवाना॥
करहु सीस धरि भूप रजाई।
हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई।
करहु तात पितु बचन प्रवाना॥
करहु सीस धरि भूप रजाई।
हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई।
राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिये हे तात! पिताके वचनोंको प्रमाण (सत्य) करो! राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है ॥३॥
परसुराम पितु अग्या राखी।
मारी मातु लोक सब साखी।
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ।
पितु अग्याँ अघ अजसु न भयऊ॥
मारी मातु लोक सब साखी।
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ।
पितु अग्याँ अघ अजसु न भयऊ॥
परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रखी और माताको मार डाला; सब लोक इस बातके साक्षी हैं। राजा ययातिके पुत्रने पिताको अपनी जवानी दे दी। पिताकी आज्ञा पालन करनेसे उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ॥४॥
अनुचित उचित बिचारु तजि जे पालहिं पितु बैन।
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७४॥
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥१७४॥
जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते हैं, वे [यहाँ] सुख और सुयशके पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी (स्वर्ग) में निवास करते हैं ॥१७४॥
अवसि नरेस बचन फुर करहू।
पालहु प्रजा सोकु परिहरहू॥
सुरपुर नृपु पाइहि परितोषू।
तुम्ह कहुँ सुकृतु सुजसु नहिं दोषू॥
पालहु प्रजा सोकु परिहरहू॥
सुरपुर नृपु पाइहि परितोषू।
तुम्ह कहुँ सुकृतु सुजसु नहिं दोषू॥
राजा का वचन अवश्य सत्य करो। शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो। ऐसा करनेसे स्वर्गमें राजा सन्तोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा ॥१॥
बेद बिदित संमत सबही का।
जेहि पितु देइ सो पावइ टीका॥
करहु राजु परिहरहु गलानी।
मानहु मोर बचन हित जानी॥
जेहि पितु देइ सो पावइ टीका॥
करहु राजु परिहरहु गलानी।
मानहु मोर बचन हित जानी॥
यह वेदमें प्रसिद्ध है और [स्मृति-पुराणादि] सभी शास्त्रोंके द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राजतिलक पाता है। इसलिये तुम राज्य करो, ग्लानिका त्याग कर दो। मेरे वचनको हित समझकर मानो॥२॥
सुनि सुखु लहब राम बैदेहीं।
अनुचित कहब न पंडित केहीं॥
कौसल्यादि सकल महतारीं।
तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारी।
अनुचित कहब न पंडित केहीं॥
कौसल्यादि सकल महतारीं।
तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारी।
इस बातको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुख पावेंगे और कोई पण्डित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी॥३॥
परम तुम्हार राम कर जानिहि।
सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि।
सौंपेहु राजु राम के आएँ।
सेवा करेहु सनेह सुहाएँ।
सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि।
सौंपेहु राजु राम के आएँ।
सेवा करेहु सनेह सुहाएँ।
जो तुम्हारे और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धको जान लेगा, वह सभी प्रकारसे तुमसे भला मानेगा। श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना और सुन्दर स्नेहसे उनकी सेवा करना॥४॥
कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि।
रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि॥१७५॥
रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि॥१७५॥
मन्त्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं-गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये। श्रीरघुनाथजीके लौट आनेपर जैसा उचित हो, तब फिर वैसा ही कीजियेगा ॥ १७५ ॥
कौसल्या धरि धीरजु कहई।
पूत पथ्य गुर आयसु अहई॥
सो आदरिअ करिअ हित मानी।
तजिअ बिषादु काल गति जानी।
पूत पथ्य गुर आयसु अहई॥
सो आदरिअ करिअ हित मानी।
तजिअ बिषादु काल गति जानी।
कौसल्याजी भी धीरज धरकर कह रही हैं-हे पुत्र! गुरुजीकी आज्ञा पथ्यरूप है। उसका आदर करना चाहिये और हित मानकर उसका पालन करना चाहिये। कालकी गतिको जानकर विषादका त्याग कर देना चाहिये॥१॥
बन रघुपति सुरपुर नरनाहू।
तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू॥
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा।
तुम्हही सुत सब कहँ अवलंबा।।
तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू॥
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा।
तुम्हही सुत सब कहँ अवलंबा।।
श्रीरघुनाथजी वनमें हैं, महाराज स्वर्गका राज्य करने चले गये। और हे तात! तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र! कुटुम्ब, प्रजा, मन्त्री और सब माताओंके सबके एक तुम ही सहारे हो॥२॥
लखि बिधि बाम कालु कठिनाई।
धीरजु धरहु मातु बलि जाई॥
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू।
प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥
धीरजु धरहु मातु बलि जाई॥
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू।
प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥
विधाताको प्रतिकूल और कालको कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरुकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजाका पालन कर कुटुम्बियोंका दु:ख हरो॥३॥
गुर के बचन सचिव अभिनंदनु।
सुने भरत हिय हित जनु चंदनु॥
सुनी बहोरि मातु मृदु बानी।
सील सनेह सरल रस सानी॥
सुने भरत हिय हित जनु चंदनु॥
सुनी बहोरि मातु मृदु बानी।
सील सनेह सरल रस सानी॥
भरतजी ने गुरु के वचनों और मन्त्रियों के अभिनन्दन (अनुमोदन) को सुना, जो उनके हृदयके लिये मानो चन्दन के समान [शीतल] थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलताके रस में सनी हुई माता कौसल्याकी कोमल वाणी सुनी ॥४॥
छं०-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु ब्याकुल भए।
लोचन सरोरुह स्त्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए।
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की।
तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की॥
लोचन सरोरुह स्त्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए।
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की।
तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की॥
सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये। उनके नेत्र-कमल जल (आँसू) बहाकर हृदय के विरहरूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। (नेत्रों के आँसुओं ने उनके वियोग-दुःखको बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यन्त व्याकुल कर दिया।) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गयी। तुलसीदासजी कहते हैं-स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्रीभरतजीकी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे।
सो०- भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि।
बचन अमि जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि॥१७६॥
बचन अमि जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि॥१७६॥
धैर्यकी धुरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज धरकर, कमलके समान हाथोंको जोड़कर, वचनोंको मानो अमृतमें डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे- ॥ १७६ ॥
मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम
मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका।
प्रजा सचिव संमत सबही का॥
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा।
अवसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा॥
प्रजा सचिव संमत सबही का॥
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा।
अवसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा॥
गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया। [फिर] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही सम्मत है। माताने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ॥१॥
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी।
सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी॥
उचित कि अनुचित किएँ बिचारू।
धरमु जाइ सिर पातक भारू॥
सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी॥
उचित कि अनुचित किएँ बिचारू।
धरमु जाइ सिर पातक भारू॥
[क्योंकि] गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद् (मित्र) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे उसे अच्छी समझकर करना (मानना) चाहिये। उचित-अनुचितका विचार करनेसे धर्म जाता है और सिरपर पापका भार चढ़ता है ॥२॥
तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई।
जो आचरत मोर भल होई॥
जद्यपि यह समझत हउँ नीकें।
तदपि होत परितोषु न जी कें॥
जो आचरत मोर भल होई॥
जद्यपि यह समझत हउँ नीकें।
तदपि होत परितोषु न जी कें॥
आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं, जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बातको भलीभाँति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदयको सन्तोष नहीं होता ॥३॥
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू।
मोहि अनुहरत सिखावनु देहू॥
ऊतरु देउँ छमब अपराधू।
दुखित दोष गुन गनहिं न साधू॥
मोहि अनुहरत सिखावनु देहू॥
ऊतरु देउँ छमब अपराधू।
दुखित दोष गुन गनहिं न साधू॥
अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये और मेरी योग्यताके अनुसार मुझे शिक्षा दीजिये। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिये। साधु पुरुष दुःखी मनुष्यके दोष-गुणोंको नहीं गिनते॥४॥
पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहहु मोहि राजु।
एहि तें जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजु।।१७७॥
एहि तें जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजु।।१७७॥
पिताजी स्वर्गमें हैं, श्रीसीतारामजी वनमें हैं और मुझे आप राज्य करनेके लिये कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [होनेकी आशा रखते हैं] ? ॥ १७७॥
हित हमार सियपति सेवकाईं।
सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाईं।
मैं अनुमानि दीख मन माहीं।
आन उपायँ मोर हित नाहीं॥
सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाईं।
मैं अनुमानि दीख मन माहीं।
आन उपायँ मोर हित नाहीं॥
मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिलताने छीन लिया। मैंने अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा कल्याण नहीं है ॥१॥
सोक समाजु राजु केहि लेखें।
लखन राम सिय बिनु पद देखें।
बादि बसन बिनु भूषन भारू।
बादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचारू॥
लखन राम सिय बिनु पद देखें।
बादि बसन बिनु भूषन भारू।
बादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचारू॥
यह शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोंको देखे बिना किस गिनतीमें है (इसका क्या मूल्य है)? जैसे कपड़ोंके बिना गहनोंका बोझ व्यर्थ है। वैराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यर्थ है।॥ २॥
सरुज सरीर बादि बहु भोगा।
बिनु हरिभगति जायँ जप जोगा।
जायँ जीव बिनु देह सुहाई।
बादि मोर सबु बिनु रघुराई॥
बिनु हरिभगति जायँ जप जोगा।
जायँ जीव बिनु देह सुहाई।
बादि मोर सबु बिनु रघुराई॥
रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं। श्रीहरिकी भक्तिके बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीवके बिना सुन्दर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्रीरघुनाथजीके बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है ॥३॥
जाउँ राम पहिं आयसु देहू।
एकहिं आँक मोर हित एहू॥
मोहि नृप करि भल आपन चहहू।
सोउ सनेह जड़ता बस कहहू॥
एकहिं आँक मोर हित एहू॥
मोहि नृप करि भल आपन चहहू।
सोउ सनेह जड़ता बस कहहू॥
मुझे आज्ञा दीजिये, मैं श्रीरामजीके पास जाऊँ! एक ही आँक (निश्चयपूर्वक) मेरा हित इसीमें है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेहकी जड़ता (मोह) के वश होकर ही कह रहे हैं ॥ ४॥
कैकेई सुअ कुटिलमति राम बिमुख गतलाज।
तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम के राज॥१७८॥
तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम के राज॥१७८॥
कैकेयीके पुत्र, कुटिलबुद्धि, रामविमुख और निर्लज्ज मुझ-से अधमके राज्यसे आप मोहके वश होकर ही सुख चाहते हैं।। १७८ ॥
कहउँ साँचु सब सुनि पतिआहू।
चाहिअ धरमसील नरनाहू॥
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं।
रसा रसातल जाइहि तबहीं।
चाहिअ धरमसील नरनाहू॥
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं।
रसा रसातल जाइहि तबहीं।
मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशीलको ही राजा होना चाहिये। आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पातालमें फँस जायगी ॥१॥
मोहि समान को पाप निवासू।
जेहि लगि सीय राम बनबासू॥
रायँ राम कहुँ काननु दीन्हा।
बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा॥
जेहि लगि सीय राम बनबासू॥
रायँ राम कहुँ काननु दीन्हा।
बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा॥
मेरे समान पापोंका घर कौन होगा, जिसके कारण सीताजी और श्रीरामजीका वनवास हुआ? राजाने श्रीरामजीको वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्गको गमन किया॥२॥
मैं सठु सब अनरथ कर हेतू।
बैठ बात सब सुनउँ सचेतू॥
बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू।
रहे प्रान सहि जग उपहासू॥
बैठ बात सब सुनउँ सचेतू॥
बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू।
रहे प्रान सहि जग उपहासू॥
और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थोंका कारण हूँ, होश-हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ ! श्रीरघुनाथजीसे रहित घरको देखकर और जगत्का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं ॥३॥
राम पुनीत बिषय रस रूखे।
लोलुप भूमि भोग के भूखे॥
कहँ लगि कहौं हृदय कठिनाई।
निदरि कुलिसु जेहिं लही बड़ाई॥
लोलुप भूमि भोग के भूखे॥
कहँ लगि कहौं हृदय कठिनाई।
निदरि कुलिसु जेहिं लही बड़ाई॥
[इसका यही कारण है कि ये प्राण] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रसमें आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगोंके ही भूखे हैं। मैं अपने हृदयकी कठोरता कहाँतक कहूँ ? जिसने वज्रका भी तिरस्कार करके बड़ाई पायी है॥४॥
कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर।
कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७९॥
कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७९॥
कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है।। १७९॥
कैकेई भव तनु अनुरागे।
पावर प्रान अघाइ अभागे॥
जौं प्रिय बिरहँ प्रान प्रिय लागे।
देखब सुनब बहुत अब आगे॥
पावर प्रान अघाइ अभागे॥
जौं प्रिय बिरहँ प्रान प्रिय लागे।
देखब सुनब बहुत अब आगे॥
कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट (पूरी तरह से) अभागे हैं। जब प्रियके वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखू-सुनूँगा ॥१॥
लखन राम सिय कहुँ बनु दीन्हा।
पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा॥
लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू।
दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू॥
पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा॥
लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू।
दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू॥
लक्ष्मण, श्रीरामजी और सीताजीको तो वन दिया; स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया; स्वयं विधवापन और अपयश लिया; प्रजा को शोक और सन्ताप दिया;॥२॥
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू।
कीन्ह कैकईं सब कर काजू॥
एहि तें मोर काह अब नीका।
तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥
कीन्ह कैकईं सब कर काजू॥
एहि तें मोर काह अब नीका।
तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥
और मुझे सुख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया! कैकेयीने सभीका काम बना दिया! इससे अच्छा अब मेरे लिये और क्या होगा? उसपर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं ! ॥३॥
कैकइ जठर जनमि जग माहीं।
यह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं॥
मोरि बात सब बिधिहिं बनाई।
प्रजा पाँच कत करहु सहाई॥
यह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं॥
मोरि बात सब बिधिहिं बनाई।
प्रजा पाँच कत करहु सहाई॥
कैकेयी के पेट से जगत् में जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाताने ही बना दी है। [फिर] उसमें प्रजा और पंच (आप लोग) क्यों सहायता कर रहे हैं? ॥ ४॥
ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार।
तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार॥१८०॥
तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार॥१८०॥
जिसे कुग्रह लगे हों [अथवा जो पिशाचग्रस्त हो], फिर जो वायुरोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी जाय, तो कहिये यह कैसा इलाज है!॥ १८०।।
कैकइ सुअन जोगु जग जोई।
चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई॥
दसरथ तनय राम लघु भाई।
दीन्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई।
चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई॥
दसरथ तनय राम लघु भाई।
दीन्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई।
कैकेयी के लड़के के लिये संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाताने मुझे वही दिया। पर 'दशरथजीका पुत्र' और 'रामका छोटा भाई' होनेकी बड़ाई मुझे विधाताने व्यर्थ ही दी॥१॥
तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका।
राय रजायसु सब कहँ नीका॥
उतरु देउँ केहि बिधि केहि केही।
कहहु सुखेन जथा रुचि जेही॥
राय रजायसु सब कहँ नीका॥
उतरु देउँ केहि बिधि केहि केही।
कहहु सुखेन जथा रुचि जेही॥
आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं! राजाकी आज्ञा सभीके लिये अच्छी है। मैं किस-किसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो, आपलोग सुखपूर्वक वही कहें ॥२॥
मोहि कुमातु समेत बिहाई।
कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई॥
मो बिनु को सचराचर माहीं।
जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं।।
कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई॥
मो बिनु को सचराचर माहीं।
जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं।।
मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर, कहिये, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? जड़-चेतन जगत् में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्रीसीतारामजी प्राणों के समान प्यारे न हों।। ३॥
परम हानि सब कहँ बड़ लाहू।
अदिनु मोर नहिं दूषन काहू॥
संसय सील प्रेम बस अहहू।
सबुइ उचित सब जो कछु कहहू॥
अदिनु मोर नहिं दूषन काहू॥
संसय सील प्रेम बस अहहू।
सबुइ उचित सब जो कछु कहहू॥
जो परम हानि है, उसीमें सबको बड़ा लाभ दीख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है। क्योंकि आप लोग संशय, शील और प्रेम के वश हैं ॥४॥
राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु बिसेषि।
कहइ सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि॥१८१॥
कहइ सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि॥१८१॥
श्रीरामचन्द्रजीकी माता बहुत ही सरलहृदय हैं और मुझपर उनका विशेष प्रेम है। इसलिये मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं।। १८१।।
गुर बिबेक सागर जगु जाना।
जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना॥
मो कहँ तिलक साज सज सोऊ।
भएँ बिधि बिमुख बिमुख सबु कोऊ॥
जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना॥
मो कहँ तिलक साज सज सोऊ।
भएँ बिधि बिमुख बिमुख सबु कोऊ॥
गुरुजी ज्ञानके समुद्र हैं, इस बातको सारा जगत् जानता है, जिनके लिये विश्व हथेलीपर रखे हुए बेरके समान है, वे भी मेरे लिये राजतिलकका साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाताके विपरीत होनेपर सब कोई विपरीत हो जाते हैं ॥१॥
परिहरि रामु सीय जग माहीं।
कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं॥
सो मैं सुनब सहब सुखु मानी।
अंतहुँ कीच तहाँ जहँ पानी॥
कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं॥
सो मैं सुनब सहब सुखु मानी।
अंतहुँ कीच तहाँ जहँ पानी॥
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर जगत्में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थमें मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूँगा और सहूँगा। क्योंकि जहाँ पानी होता है, वहाँ अन्तमें कीचड़ होता ही है ॥२॥
डरु न मोहि जग कहिहि कि पोचू।
परलोकहु कर नाहिन सोचू॥
एकइ उर बस दुसह दवारी।
मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी॥
परलोकहु कर नाहिन सोचू॥
एकइ उर बस दुसह दवारी।
मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी॥
मुझे इसका डर नहीं है कि जगत् मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदयमें तो बस, एक ही दुःसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दु:खी हुए।॥३॥
जीवन लाहु लखन भल पावा।
सबु तजि राम चरन मनु लावा॥
मोर जनम रघुबर बन लागी।
झूठ काह पछिताउँ अभागी॥
सबु तजि राम चरन मनु लावा॥
मोर जनम रघुबर बन लागी।
झूठ काह पछिताउँ अभागी॥
जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्रीरामजीके चरणोंमें मन लगाया। मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था। मैं अभागा झूठ-मूठ क्या पछताता हूँ? ॥ ४॥
आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ।
देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ॥१८२॥
देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ॥१८२॥
सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्रीरघुनाथजीके चरणोंके दर्शन किये बिना मेरे जीकी जलन न जायगी॥१८२॥
आन उपाउ मोहि नहिं सूझा।
को जिय कै रघुबर बिनु बूझा॥
एकहिं आँक इहइ मन माहीं।
प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहीं॥
को जिय कै रघुबर बिनु बूझा॥
एकहिं आँक इहइ मन माहीं।
प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहीं॥
मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्रीरामजीके बिना मेरे हृदयकी बात कौन जान सकता है ? मनमें एक ही आँक (निश्चयपूर्वक) यही है कि प्रात:काल प्रभु श्रीरामजीके पास चल दूंगा ॥१॥
जद्यपि मैं अनभल अपराधी।
भै मोहि कारन सकल उपाधी॥
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी।
छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी॥
भै मोहि कारन सकल उपाधी॥
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी।
छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी॥
यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्रीरामजी मुझे शरणमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझपर विशेष कृपा करेंगे॥२॥
सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ।
कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा।
मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा॥
कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा।
मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा॥
श्रीरघुनाथजी शील, संकोच, अत्यन्त सरल स्वभाव, कृपा और स्नेहके घर हैं। श्रीरामजीने कभी शत्रुका भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही॥३॥
तुम्ह पै पाँच मोर भल मानी।
आयसु आसिष देहु सुबानी॥
जेहिं सुनि बिनय मोहि जनु जानी।
आवहिं बहुरि रामु रजधानी॥
आयसु आसिष देहु सुबानी॥
जेहिं सुनि बिनय मोहि जनु जानी।
आवहिं बहुरि रामु रजधानी॥
आप पंच (सब) लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिये, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्रीरामचन्द्रजी राजधानीको लौट आवें॥४॥
जद्यपि जनमु कुमातु तें मैं सठु सदा सदोस।
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस।।१८३॥
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस।।१८३॥
यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्रीरामजी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं ॥१८३।।
भरत बचन सब कहँ प्रिय लागे।
राम सनेह सुधाँ जनु पागे॥
लोग बियोग बिषम बिष दागे।
मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥
राम सनेह सुधाँ जनु पागे॥
लोग बियोग बिषम बिष दागे।
मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥
भरतजी के वचन सबको प्यारे लगे। मानो वे श्रीरामजी के प्रेमरूपी अमृत में पगे हुए थे। श्रीरामवियोगरूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीजसहित मन्त्रको सुनते ही जाग उठे॥१॥
मातु सचिव गुर पुर नर नारी।
सकल सनेहँ बिकल भए भारी॥
भरतहि कहहिं सराहि सराही।
राम प्रेम मूरति तनु आही॥
सकल सनेहँ बिकल भए भारी॥
भरतहि कहहिं सराहि सराही।
राम प्रेम मूरति तनु आही॥
माता, मन्त्री, गुरु, नगरके स्त्री-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याकुल हो गये। सब भरतजीको सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका शरीर श्रीरामप्रेमको साक्षात् मूर्ति ही है ॥२॥
तात भरत अस काहे न कहहू।
प्रान समान राम प्रिय अहहू॥
जो पावँरु अपनी जड़ताईं।
तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाईं।
प्रान समान राम प्रिय अहहू॥
जो पावँरु अपनी जड़ताईं।
तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाईं।
हे तात भरत! आप ऐसा क्यों न कहें। श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर सन्देह करेगा, ॥३॥
सो सठु कोटिक पुरुष समेता।
बसिहि कलप सत नरक निकेता॥
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई।
हरइ गरल दुख दारिद दहई॥
बसिहि कलप सत नरक निकेता॥
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई।
हरइ गरल दुख दारिद दहई॥
वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित सौ कल्पोंतक नरक के घर में निवास करेगा। साँप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती। बल्कि वह विष को हर लेती है और दुःख तथा दरिद्रताको भस्म कर देती है॥४॥
अवसि चलिअ बन रामु जहँ भरत मंत्रु भल कीन्ह।
सोक सिंधु बूड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥
सोक सिंधु बूड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥
हे भरतजी! वन को अवश्य चलिये, जहाँ श्रीरामजी हैं; आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोकसमुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने [बड़ा] सहारा दे दिया॥१८४॥
भा सब के मन मोदु न थोरा।
जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा॥
चलत प्रात लखि निरनउ नीके।
भरतु प्रानप्रिय भे सबही के॥
जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा॥
चलत प्रात लखि निरनउ नीके।
भरतु प्रानप्रिय भे सबही के॥
सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ (अर्थात् बहुत ही आनन्द हुआ)! मानो मेघोंकी गर्जना सुनकर चातक और मोर आनन्दित हो रहे हों। [दूसरे दिन] प्रात:काल चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय हो गये ॥१॥
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई।
चले सकल घर बिदा कराई।
धन्य भरत जीवन जग माहीं।
सीलु सनेहु सराहत जाहीं॥
चले सकल घर बिदा कराई।
धन्य भरत जीवन जग माहीं।
सीलु सनेहु सराहत जाहीं॥
मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके और भरतजीको सिर नवाकर, सब लोग विदा लेकर अपने-अपने घरको चले। जगत्में भरतजीका जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेहकी सराहना करते जाते हैं ॥२॥
कहहिं परसपर भा बड़ काजू।
सकल चलै कर साजहिं साजू॥
जेहि राखहिं रहु घर रखवारी।
सो जानइ जनु गरदनि मारी॥
सकल चलै कर साजहिं साजू॥
जेहि राखहिं रहु घर रखवारी।
सो जानइ जनु गरदनि मारी॥
आपसमें कहते हैं. बडा काम हआ। सभी चलनेकी तैयारी करने लगे। जिसको भी घरकी रखवालीके लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी ॥३॥
कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू।
को न चहइ जग जीवन लाहू॥
को न चहइ जग जीवन लाहू॥
कोई-कोई कहते हैं—रहने के लिये किसी को भी मत कहो, जगत् में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता?॥४॥
जरउ सो संपति सदन सुखु सुहद मातु पितु भाइ।
सनमुख होत जो राम पद करै न सहस सहाइ॥१८५॥
सनमुख होत जो राम पद करै न सहस सहाइ॥१८५॥
वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाय जो श्रीरामजीके चरणोंके सम्मुख होने में हँसते हुए (प्रसन्नतापूर्वक) सहायता न करे ॥ १८५ ॥
घर घर साजहिं बाहन नाना।
हरषु हृदयँ परभात पयाना॥
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू।
नगरु बाजि गज भवन भंडारू॥
हरषु हृदयँ परभात पयाना॥
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू।
नगरु बाजि गज भवन भंडारू॥
घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं। हृदयमें [बड़ा] हर्ष है कि सबेरे चलना है। भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल खजाना आदि-- ॥१॥
संपति सब रघुपति कै आही।
जौं बिनु जतन चलौं तजि ताही॥
तौ परिनाम न मोरि भलाई।
पाप सिरोमनि साइँ दोहाई॥
जौं बिनु जतन चलौं तजि ताही॥
तौ परिनाम न मोरि भलाई।
पाप सिरोमनि साइँ दोहाई॥
सारी सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीकी है। यदि उसकी [रक्षाकी] व्यवस्था किये बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। क्योंकि स्वामीका द्रोह सब पापोंमें शिरोमणि (श्रेष्ठ) है॥२॥
करइ स्वामि हित सेवकु सोई।
दूषन कोटि देइ किन कोई॥
अस बिचारि सुचि सेवक बोले।
जे सपनेहुँ निज धरम न डोले॥
दूषन कोटि देइ किन कोई॥
अस बिचारि सुचि सेवक बोले।
जे सपनेहुँ निज धरम न डोले॥
सेवक वही है जो स्वामीका हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरतजीने ऐसा विचारकर ऐसे विश्वासपात्र सेवकोंको बुलाया जो कभी स्वप्नमें भी अपने धर्मसे नहीं डिगे थे॥३॥
कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा।
जो जेहि लायक सो तेहिं राखा।
करि सबु जतनु राखि रखवारे।
राम मातु पहिं भरतु सिधारे॥
जो जेहि लायक सो तेहिं राखा।
करि सबु जतनु राखि रखवारे।
राम मातु पहिं भरतु सिधारे॥
भरतजी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया; और जो जिस योग्य था, उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर भरतजी राममाता कौसल्याजीके पास गये॥४॥
आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान।
कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान॥१८६॥
कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान॥१८६॥
स्नेह के सुजान (प्रेम के तत्त्व को जाननेवाले) भरतजीने सब माताओंको आर्त (दुःखी) जानकर उनके लिये पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान (सुखपाल) सजाने के लिये कहा ॥ १८६॥
चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी।
चहत प्रात उर आरत भारी॥
जागत सब निसि भयउ बिहाना।
भरत बोलाए सचिव सुजाना॥
चहत प्रात उर आरत भारी॥
जागत सब निसि भयउ बिहाना।
भरत बोलाए सचिव सुजाना॥
नगर के नर-नारी चकवे-चकवी की भाँति हृदय में अत्यन्त आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते-जागते सबेरा हो गया। तब भरतजी ने चतुर मन्त्रियों को बुलवाया-- ॥१॥
To give your reviews on this book, Please Login