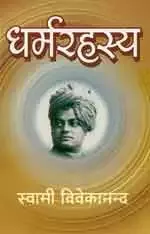|
ई-पुस्तकें >> धर्म रहस्य धर्म रहस्यस्वामी विवेकानन्द
|
13 पाठक हैं |
|||||||
समस्त जगत् का अखण्डत्व - यही श्रेष्ठतम धर्ममत है मैं अमुक हूँ - व्यक्तिविशेष - यह तो बहुत ही संकीर्ण भाव है, यथार्थ सच्चे 'अहम्' के लिए यह सत्य नहीं है।
यहूदियों की भांति हिन्दू भी दूसरे को अपने धर्म में ग्रहण नहीं करते, तथापि धीरे धीरे अन्यान्य जातियाँ हिन्दू धर्म के भीतर चली आ रही हैं और हिन्दुओं के आचार-व्यवहार को ग्रहण कर उनके समश्रेणीभुक्त होती जा रही हैं। ईसाई धर्म ने कैसा विस्तार-लाभ किया है, आप सब जानते हैं; परन्तु मुझे ऐसा मालूम होता है कि फिर भी चेष्टानुरूप फल नहीं हो रहा है। ईसाइयों के धर्मप्रचार के कार्य में एक बड़ा भारी दोष रह गया है और वह दोष पश्चिम की सभी संस्थाओं में है। शक्ति का नब्बे प्रतिशत अंश कल-पुर्जों में ही व्यय हो जाता है - कारण, वहाँ कल-कारखाने बहुत ज्यादा हैं। प्रचार-कार्य तो प्राच्य लोगों का ही काम रहा है। पाश्चात्य लोग संघबद्ध भाव से कार्य, सामाजिक अनुष्टान, युद्ध-सज्जा, राज्यशासन इत्यादि अति सुन्दर रूप से सम्पन्न कर सकते हैं, परन्तु धर्म-प्रचार के क्षेत्र में वे प्राच्य की बराबरी नहीं कर सकते, कारण, प्राच्य के लोग लगातार इसे करते आये हैं, - वे इसमें अभिज्ञ हैं और वे अधिक यन्त्रों का व्यवहार नहीं करते।
अतएव मनुष्य-जाति के वर्तमान इतिहास में यह एक प्रत्यक्ष घटना है कि पूर्वोक्त सब प्रधान प्रधान धर्म ही विद्यमान हैं और वे विस्तारित तथा पुष्ट होते जा रहे हैं। इस तथ्य का अवश्य कोई अर्थ है; और सर्वज्ञ, परम कारुणिक सृष्टिकर्ता की यदि यही इच्छा होती कि इनमें से केवल एक ही धर्म विद्यमान रहे और शेष सब नष्ट हो जायँ, तो वह बहुत पहले ही पूर्ण हो जाती। अथवा यदि इन सब धर्मों में से केवल एक ही सत्य होता और अन्य सब झूठ, तो वह अब तक सारी पृथ्वी में फैल जाता। परन्तु बात ऐसी नहीं है, उनमें से एक ने भी सारे संसार पर अधिकार नहीं कर पाया है। सारे धर्म किसी एक समय उन्नति और किसी एक समय अवनति की ओर जाते हैं। यह भी विचारने की बात है कि तुम्हारे देश में छ: करोड़ मनुष्य हैं; परन्तु उनमें से केवल दो करोड़ दस लाख ही किसी न किसी धर्म के अनुयायी हैं। इसका अर्थ यह है कि सब समय में ही धर्म उन्नति नहीं करता है। गवेषणा करने से सम्भवत: मालूम होगा कि सब देशों में ही धर्म कभी उन्नति और कभी अवनति करता रहा है। उस पर देखा जाता है कि संसार में सम्प्रदायों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। किसी सम्प्रदायविशेष का यह कहना यदि सत्य होता, कि सारा सत्य उसी में भरा है और ईश्वर उस निखिल सत्य को उसी के धर्मग्रन्थ में लिख गये हैं - तो फिर संसार में इतने सम्प्रदाय क्यों हैं? पचास वर्ष के भीतर ही भीतर एक ही पुस्तकविशेष के आधार पर बीसों नये सम्प्रदाय उठ खड़े होते हैं।
|
|||||