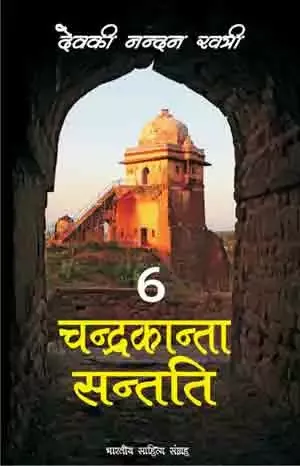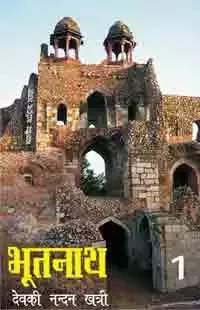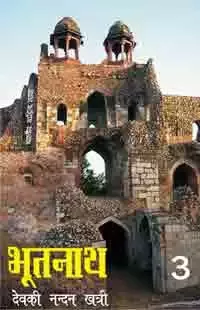|
मूल्य रहित पुस्तकें >> चन्द्रकान्ता सन्तति - 6 चन्द्रकान्ता सन्तति - 6देवकीनन्दन खत्री
|
192 पाठक हैं |
||||||||||||
चन्द्रकान्ता सन्तति 6 पुस्तक का ईपुस्तक संस्करण...
उपसंहार
प्रेमी पाठक महाशय, अब इस उपन्यास में मुझे सिवाय इसके और कुछ कहना नहीं है कि भूतनाथ ने प्रतिज्ञानुसार अपनी जीवनी लिखकर दरबार में पेश की और महाराज ने उसे पढ़-सुनकर उसे खजाने में रख दिया। इस उपन्यास का भूतनाथ की खास जीवनी से कोई सम्बन्ध न था, इसलिए इसमें वह जीवनी नत्थी न की गयी, हाँ खास-खास भेद जो भूतनाथ से सम्बन्ध रखते थे, खोल दिये गये तथापि भूतनाथ की जीवनी, जिसे चन्द्रकान्ता सन्तति का उपसंहार भाग भी कह सकेंगे स्वतन्त्र रूप से लिखकर अपने प्रेमी पाठकों की नजर करूँगा, मगर इसके बदले में अपने प्रेमी पाठकों से इतना जरूर कहूँगा कि इस उपन्यास में जो कुछ भूल-चूक रह गयी हो और जो भेद खुलने से रह गये हों, वह मुझे अवश्य बतायें जिसमें ‘‘भूतनाथ की जीवनी’’ लिखते समय उनपर ध्यान रहे, क्योंकि इतने बड़े उपन्यास में ऐसे अनजान आदमी से किसी तरह की त्रुटि का रह जाना कोई आश्चर्य नहीं है।
प्रिय पाठक महाशय, अब चन्द्रकान्ता सन्तति की लेख-प्रणाली के विषय मंब भी कुछ कहने की इच्छा होती है।
जिस समय मैंने चन्द्रकान्ता लिखनी आरम्भ की थी, उस समय कविवर प्रताप नारायण मिश्र और पण्डितवर अम्बिकादत्त व्यास जैसे धुरन्धर किन्तु अनुद्धत सुकवि और सुलेख विद्यमान थे, तथा राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह जैसे सुप्रतिष्ठित पुरुष हिन्दी की सेवा करने में अपना गौरव समझते थे, परन्तु अब न वैसे मार्मिक कवि हैं और न वैसे सुलेखक। उस समय हिन्दी के लेखक थे, परन्तु ग्राहक न थे, इस समय ग्राहक हैं, पर वैसे लेखक नहीं है। मेरे इस कथन का यह मतलब नहीं है कि वर्तमान समय के साहित्यसेवी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं, बल्कि यह मतलब है कि जो स्वर्गीय सज्जन अपनी लेखनी से हिन्दी के आदि-युग में हमें ज्ञान दे गये हैं, वे हमारी अपेक्षा बहुत बढ़-चढ़कर थे। उनकी लेख-प्रणाली में चाहे भेद रहा हो, परन्तु उन सबका लक्ष्य यही था कि इस भारत-भूमि में किसी तरह की मातृभाषा का एकाधिपत्य हो, लेकिन यह कोई नियम की बात नहीं है कि वैसे लोगों से कुछ भूल हो ही नहीं, उनसे भूल हुई तो यही कि प्रचलित शब्दों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राजा शिवप्रसादजी के राजनीति के विचार चाहे कैसे ही रहे हों पर सामाजिक विचार उनके बहुत ही प्राञ्जल थे और वे समयानुकूल काम करना खूब जानते थे, विशेषतः जिस ढंग की हिन्दी वे लिख गये हैं, उसी से वर्तमान में हिन्दी का रास्ता कुछ साफ हुआ है। चाहे कोई हिन्दू हो, चाहे जैन या बौद्ध हो और चाहे आर्य समाजी या धर्म समाजी ही क्यों न हो, परन्तु जिन सज्जनों के माननीय अवतारों और पूर्वजनों ने इस पुण्य-भूमि का अपने आविर्भाव से गौरव बढ़ाया है, उनमें ऐसा अभागा कौन होगा, जो पुण्यता और मधुरता युक्त संस्कृत-भाषा के शब्दों का प्रचुर प्रचार न चाहेगा? मेरे विचार में किसी विवेकी भारत सन्तान के विषय में केवल यह देखकर कि वह विदेशी भाषा के शब्दों का प्रसार कर रहा है, यह गढ़न्त कर लेना कि वह देववाणी के पवित्र शब्दों का विरोधी है, भ्रम ही नहीं, किन्तु अन्याय भी है। देखना यह चाहिए कि ऐसा करने से उसका मतलब क्या है। भारतवर्ष में आठ सौ वर्ष तक विदेशी यवनों का राज्य रहा है, इसलिए फारसी-अरबी के शब्द हिन्दू-समाज में ‘‘नपठेत् यावनी भाषा’’ की दीवार लाँघकर उसी प्रकार आ घुसे, जिस प्रकार हिमालय के उन्नत मस्तक को लाँघकर वे स्वयं आ गये, यहाँ तक कि महात्मा तुलसीदासजी जैसे भगवद्भक्त कवियों को भी ‘‘गरीबनिवाज’’ आदि शब्दों का बर्ताव दिल खोलके करना पड़ा।
आठ सौ वर्ष के कुसंस्कार को जो गिनती के दिनों में दूर करना चाहते हैं, उनके उत्साह और साहस की प्रशंसा करने पर भी हम यह कहने के लिए मजबूर हैं कि वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं करते, बल्कि जोकुछ वे कर सकते थे, उससे भी दूर हटते हैं। यदि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर सीधे-सादे शब्दों से बँगला में काम न कर लेते तो उत्तरकाल के लेखकों को संस्कृत शब्द के बाहुल्य प्रचार का अवसर न मिलता और यदि ‘‘राजा शिवप्रसादी हिन्दी’’ प्रकट न होती तो सरकारी पाठशालाओं में हिन्दी के चन्द्रमा की चाँदनी मुश्किल से पहुँचती। मेरे बहुत से मित्र हिन्दुओं की अकृतज्ञता का यों वर्णन करते हैं कि उन्होंने हरिश्चन्द्रजी जैसे देश-हितैषी पुरुष की उत्तम-उत्तम पुस्तकें नहीं खरीदीं, पर मैं कहता हूँ कि यदि बाबू हरिश्चन्द्र अपनी भाषा को थोड़ा सरल करते तो हमारे भाइयों को अपने समाज पर कलंक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और स्वाभाविक शब्दों के मेल से हिन्दी की पैसिन्जर भी मेल बन जाती। प्रवाह के विरुद्ध चलकर यदि कोई कृतकार्य हो तो निःसन्देह उसकी बहादुरी है, परन्तु बड़े-बड़े दार्शनिक पण्डितों ने इसको असम्भव ठहराया है। सारसुधानिधि और कविवचनसुधा की भाषा यद्यपि भावुकजनों के लिए आदर की वस्तु थी, परन्तु समय के उपयोगी न थी। हमारे ‘सुदर्शन’ की लेख-प्रणाली को हिन्दी के धुरन्धर लेखकों और विद्वानों ने प्रशंसा के योग्य ठहराया है। परन्तु साधारणजन उससे कितना लाभ उठासकते हैं, यह सोचने की बात है। यदि महाकवि भवभूति के समान किसी भविष्य पुरुष की आशा ही पर ग्रन्थकारों और लेखकों को यत्न करना चाहिए, तब तो मैं सुदर्शन सम्पादक पंडित माधवप्रसाद मिश्र को भी भविष्य की आशा पर बधाई देता हूँ, पर यदि ग्रन्थकारों को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान से अधिक सम्बन्ध है, निःसन्देह इस विषय में मुझे आपत्ति है। किसी दार्शनिक ग्रन्थ या पत्र की भाषा के लिए यदि किसी बड़े कोष को टटोलना पड़े तो कुछ परवाह नहीं, परन्तु साधारण विषयों की भाषा के लिए भी कोष की खोज करनी पड़े, तो निःसन्देह दोष की बात है। मेरी हिन्दी किस श्रेणी की हिन्दी है, इसका निर्धारण मैं नहीं करता, परन्तु मैं यह जानता हूँ कि इसके पढ़ने के लिए कोष की तलाश करनी नहीं पड़ेगी। चन्द्रकान्ता के आरम्भ के समय मुझे यह विश्वास न था कि उसका इतना अधिक प्रचार होगा, यह मनोविनोद के लिए लिखी गयी थी, पर पीछे लोगों का अनुराग देखकर मेरा भी अनुराग हो गया और मैंने अपने उन विचारों को, जिनको मैं अभी तक प्रकाश नहीं कर सका था, फैलाने के लिए इस पुस्तक को द्वार बनाया और सरल भाषा में उन्हीं बातों को लिखा, जिससे मैं उस होनहार मण्डली का प्रियपात्र बन जाऊँ, जिसके हाथ में भारत का भविष्य सौंपकर हमें इस आसार संसार से बिदा होना है। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि मैं इस विषय में सफल हुआ और मुझे ग्राहकों की अच्छी श्रेणी मिल गयी। यह बात बहुत से सज्जनों पर प्रकट है कि ‘चन्द्रकान्ता’ पढ़ने के लिए बहुत से पुरुष नागरी की वर्णमाला सीखते हैं और जिनको कभी हिन्दी सीखना न था, उन लोगों ने भी इसके लिए सीखी।
हिन्दी के हितैषियों में दो प्रकार के सज्जन हैं। एक तो वे जिनका विचार यह है कि चाहे अक्षर फारसी क्यों न हो, पर भाषा विशुद्ध संस्कृत मिश्रित होनी चाहिए और दूसरे वे जो यह चाहते हैं कि चाहे भाषा में फारसी के शब्द मिले भी हों पर अक्षर नागरी होने चाहिए। पहिले में मैं पंजाब के आर्यसमाजियों और धर्मसभावालों को मान लेता हूँ, जिनके लेखों में वर्णमाला के सिवाय फारसी-अरबी को कुछ भी सहारा नहीं, सबकुछ संस्कृत का है, और दूसरे पक्ष में मैं अपने को ठहरा लेता हूँ, जो इसके विपरीत है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि जिस प्रकार फारसी वर्णमाला उर्दू का शरीर और अरबी-फारसी के उपयुक्त शब्द उसके जीवन हैं, ठीक उसी प्रकार नागरी वर्णमाला हिन्दी का शरीर और संस्कृत के उपयुक्त शब्द उसके प्राण कहे जा सकते हैं। यदि यह देश यवनों के अधिकार में न होता और यदि कायस्थादि हिन्दू जातियों में उर्दू भाषा का प्रेम अस्थिमज्जागत न हो गया होता तो हिन्दी का शरीर और जीवन प्रथक दिखलायी देता। उसी प्रकार हमारे ग्रन्थों की सजीव उत्पत्ति होती, जिस प्रकार द्विज बालकों की होती है। शरीर में यदि आत्मा न हो तो वह बेकार है और यदि आत्मा को उपयुक्त शरीर न मिलकर पशु-पक्षी आदि शरीर मिल जाय तो भी वह निष्फल ही है, इसलिए शरीर बनाकर फिर उसमें आत्मदेव की स्थापना करना ही न्याययुक्त और लाभप्रद है। ‘चन्द्रकान्ता’ और ‘सन्तति’ में यद्यपि इस बात का पता नहीं लगेगा कि कब और कहाँ भाषा का परिवर्तन हो गया, परन्तु उसके आरम्भ और अन्त में आप ठीक वैसा ही परिवर्तन पायेंगे, जैसा बालक और वृद्ध में। एकदम से बहुत से शब्दों का प्रचार करते तो कभी सम्भव न था कि उतने संस्कृत शब्द हम उन कुपड़ ग्रामीण लोगों को याद करा देते, जिनके निकट काला अक्षर भैंस बराबर था। मेरे इस कर्तव्य का आश्चर्यमय फल देखकर वे लोग भी बोधगम्य उर्दू के शब्दों को अपनी विशुद्ध हिन्दी में लाने लगे हैं जो आरम्भ में इसीलिए मुझपर कटाक्षपात करते थे। इस प्रकार प्राकृतिक प्रवाह के साथ-साथ साहित्यसेवियों की सरस्वती का प्रवाह बदलता देखकर समय के बदलने का अनुमान करना कुछ अनुचित नहीं है। जो हो, भाषा के विषय में हमारा वक्तव्य यही है कि वह सरल हो और नागरी वाणी में हो, क्योंकि जिस भाषा के अक्षर होते हैं उनका खिंचाव उन्हीं मूल भाषाओं की ओर होता है, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है।
भाषा के सिवाय दूसरी बात मुझे भाव के विषय में कहनी है। मेरे कई मित्र आक्षेप करते हैं कि मुझे देश-हितपूर्ण और धर्मभावमय कोई ग्रन्थ लिखना उचित था, जिससे मेरी प्रसरणशील पुस्तकों के कारण समाज का बहुत कुछ उपकार व सुधार हो जाता। बात बहुत ठीक है, परन्तु एक अप्रसिद्ध ग्रन्थकार की पुस्तक को कौन पढ़ता? यदि मैं चन्द्रकान्ता और सन्तति को न लिखकर अपने मित्रों से भी दो-चार बातें हिन्दी के विषय में कहना चाहता तो कदाचित् वे भी सुनना पसन्द नहीं करते। गम्भीर-विषय के लिए, जैसे एक विशेष भाषा का प्रायोजन होता है, वैसे ही विशेष पुरुष का भी। भारतवर्ष में विशेषता की अधिकता न देखकर मैंने साधारण भाषा में साधारण बातें लिखना ही आवश्यक समझा। संसार में ऐसे भी लोग हुए होंगे जिन्होंने सरल और भावमय एक ही पुस्तक लिखकर लोगों का चित्त अपनी और खैंच लिया हो पर वैसा कठिन काम मेरे ऐसे के करने के योग्य न था। तथापि पात्रों की चाल-चलन दिखाने में जहाँ तक हो सका, ध्यान रक्खा गया है। सब पात्र यथा समय सन्ध्या-तर्पण करते हैं और अवसर पड़ने पर पूजा-प्रकार भी बीरेन्द्रसिंह आदि के वर्णन में जगह-जगह दिखायी देता है।
कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मित्रों ने संवाद-पत्रों में इस विषय का आन्दोलन उठाया था कि इनके कथानक सम्भव हैं या असम्भव, मैं नहीं समझता कि यह बात क्यों उठायी और बढ़ायी गयी? जिस प्रकार पंचतन्त्र, हितोपदेश आदि ग्रन्थ बालकों की शिक्षा के लिए, लिखे गये, उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए, पर यह सम्भव है या असम्भव इस विषय में कोई यह समझे कि ‘चन्द्रकान्ता’ और ‘बीरेन्द्रसिंह’ इत्यादि पात्र और उनके विचित्र स्थानादि सब ऐतिहासिक हैं, तो बड़ी भारी भूल है। कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत है और उसका यह एक छोटा-सा नमूना है। अब रही सम्भव की बात अर्थात् कौन सी बात हो सकती है और कौन नहीं हो सकती है! इसका विचार प्रत्येक मनुष्य की योग्यता और देश-काल पात्र से सम्बन्ध रखता है। कभी ऐसा समय था कि यहाँ के आकाश में विमान उड़ते थे, एक-एक वीर पुरुष के तीरों में यह सामर्थ्य थी कि क्षणमात्र में सहस्त्रों मनुष्यों का संहार हो जाता था, पर अब वह बातें खाली पौराणिक कथा समझी जाती हैं। पर दो सौ वर्ष पहले जो बातें असम्भव थीं आजकल विज्ञान के सहारे वे सब सम्भव हो रही हैं। रेल, तार, बिजली आदि के कार्यों को पहिले कौन मान सकता था? और फिर यह भी है कि साधारण लोगों की दृष्टि में जो असम्भव है, कवियों की दृष्टि में भी वह असम्भव ही रहे, यह कोई नियम की बात नहीं है। संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यास कादम्बरी की नायिका युवती की युवती ही रही पर उसके नायक के तीन जन्म हो गये, तथापि कोई बुद्धिमान पुरुष इसको दोपावहन समझकर गुणधायक ही समझेगा। चन्द्रकान्ता में जो अद्भुत बातें लिखी गयी हैं, वे इसलिए नहीं कि लोग उनकी सच्चाई-झुठलाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि उसका पाठ कौतूहल वर्द्धक हो।
एक समय था कि लोग सिंहासन-बत्तीसी, बैतालपचीसी आदि कहानियों को विश्रामकाल में रुचि से पढ़ते थे, फिर चहारदरवेश और अलिफलैला के किस्सों का समय आया, अब इस ढंग के उपन्यासों का समय है। अब भी वह समय दूर है, जब लोग बिना किसी प्रकार की न्यूनाधिकता और ऐतिहासिक पुस्तकों को रुचि से पढ़ेंगे। अब वह समय आवेगा, उस समय कथा सरत्सागर के समान ‘चन्द्रकान्ता’ बतलावेगी कि एक वह भी समय था जब इसी प्रकार के ग्रन्थों से ही वीरप्रसू भारत भूमि की सन्तान का मनोविनोद होता था। भगवान उस समय को शीघ्र लावें।
|
|||||