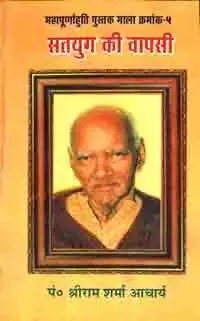|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> सतयुग की वापसी सतयुग की वापसीश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
उज्जवल भविष्य की संरचना....
2
विभीषिकाओं के पीछे झाँकती यथार्थता
वैभव को कमाया तो असीम मात्रा में भी जा सकता है, पर उसे एकाकी पचाया नहीं जा सकता। मनुष्य के पेट का विस्तार थोड़ा-सा ही है। यदि बहुत कमा लिया गया है तो उस सब को उदरस्थ कर जाने की ललक-लिप्सा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह संभव हो नहीं सकेगी। नियत मात्रा से अधिक जो भी खाया गया है, वह दस्त, उल्टी, उदरशूल जैसे संकट खड़े करेगा, भले ही वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों न लगे।
शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षेत्र, भौतिक पदार्थ संरचना के आधार पर विनिर्मित हुए हैं। उनकी भी अन्य पदार्थों की तरह एक सीमा और परिधि है। जीवित रहने और अभीष्ट कृत्यों में निरत रहने के लिए सीमित ऊर्जा, सक्रियता एवं साधन सामग्री ही अभीष्ट है। इसका उल्लंघन करने की ललक तटबंधों को तोड़कर बहने वाली बाढ़ की तरह अपनी उच्छृंखलता के कारण अनर्थ ही अनर्थ करेगी। उस उन्माद के कारण पानी तो व्यर्थ जाएगा ही, खेत खलिहानों, बस्तियों आदि को भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। यों चाहे तो नदी इसे अपने स्वेच्छाचार और अहंकार दर्प-प्रदर्शन के रूप में भी बखान सकती है, पर जहाँ कहीं, जब कभी इस उन्माद की चर्चा चलेगी तब उसकी भर्त्सना ही की जाएगी।
उपयोग की दृष्टि से थोड़े साधनों में भी भली प्रकार काम चल सकता है, पर अपव्यय की कोई सीमा मर्यादा नहीं। कोई चाहे तो लाखों के नोट इकट्ठे करके उनमें माचिस लगाकर, होली जलाने जैसा कौतूहल करते हुए प्रसन्नता भी व्यक्त कर सकता है, पर इस अपव्यय को कोई भी समझदार न तो सराहेगा और न उसका समर्थन करेगा। बेहद चाटुकार तो कुल्हाड़ियों से अपना पैर काटने के लिए उद्यत अतिवादी की भी हाँ में हाँ मिला सकते हैं।
वासना और तृष्णा की खाई इतनी चौड़ी और गहरी है कि उसे पाटने में कुबेर की संपदा और इंद्र की समर्थता भी कम पड़ती है। तृष्णा की रेगिस्तानी जलन को बुझाने के लिए साधन सामग्री का थोड़ा-सा पानी, कुछ काम नहीं करता। अतृप्ति जहाँ की तहाँ बनी रहती है। थोड़े से उपभोग तो उस ललक को और भी तेजी से आग में ईधन पड़ने की तरह भड़का देते हैं।
मन के छुपे रुस्तम का तो कहना ही क्या? वह यक्ष राक्षस की तरह अदृश्य तो रहता है, पर कौतुक-कौतूहल इतने बनाता-दिखाता रहता है कि उस व्यामोह में फँसा मनुष्य दिग्भ्रांत बनजारे की तरह इधर-उधर मारे-मारे फिरने में ही अपनी समूची चिंतन क्षमता गँवा-गुमा दे। तृष्णा तो समुद्र की चौड़ाई और गहराई से भी बढ़कर है। उसे तो भस्मासुर, वृत्रासुर, महिषासुर जैसे महादैत्य भी पूरी न कर सके, फिर बेचारे मनुष्य की तो विसात ही क्या है, जो उसे शांत करके संतोष का आधार प्राप्त कर सके।
दिग्भ्रांत मनुष्य अपने आपे को शरीर तक सीमित मान बैठा है क्योंकि प्रत्यक्ष तो इतना ही कुछ दीख पड़ता है। मन यद्यपि अदृश्य है, पर वह भी शरीर का एक अवयव है। इसे ग्यारहवीं इंद्रिय भी कहा जाता है। वासना, तृष्णा इन्हीं दोनों का मिला-जुला खेल है जो अनंत काल तक चलते रहने पर भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसी उलझन के भवबंधनों में बँधा हुआ जीव, चित्र-विचित्र प्रकार के अभाव अनुभव करता, असंतुलित रहता और उद्विग्नता, चिंता, आशंका के त्रास सहता रहता है। आश्चर्य इस बात का है कि अवांछनीय जाल-जंजालों से अपने को उबारने के लिए कुछ करना तो दूर, सोचने तक का मनुष्य प्रयास नहीं कर पाता, उलटे अनाचारों पर उतारू होकर दूसरों को भी वैसा ही करते रहने के लिए उकसाता रहता है, भले ही वह अनर्थ स्तर का ही घृणित क्यों न हो?
यही है अपने समय के मनुष्य का तात्त्विक पर्यवेक्षण। मूर्खता को कहने सुनने में तो उपहासास्पद बताया जाता है पर वस्तुतः वह इतनी प्रबल एवं आतुर होती है कि उसके आवेश को रोक सकना अच्छे अच्छों के लिए भी कठिन हो जाता है। यह उन्माद जब सामूहिकता के साथ जुड़ जाता है तो फिर स्थिति उस विशालकाय पागलखाने जैसी हो जाती है, जिसमें रोगी एक-दूसरे को उकसाने, भड़काने, गिराने, सताने जैसी विडंबनाओं में ही लगे रहते हैं। वे सभी मात्र हानि-ही-हानि उठाते हैं।
गीताकार ने सच कहा है कि जब दुनिया सोती है, तब योगी जागते हैं। यह अनबूझ पहेली तभी प्रामाणिक सिद्ध हो सकती है, जब यह सोचा जाए कि असंख्यों अवांछनीयताओं की लहरें उठाते चलने वाले प्रस्तुत प्रवाह के साथ-साथ बढ़ते रहने की अपेक्षा, कोई आश्रय दे सकने वाला किनारा खोजा जाए। प्रचलनों से हटकर नए तौर-तरीके अपनाकर, यथार्थता का आश्रय लेने वाली उमंग उमंगे, अन्यथा अच्छे-भले नदी-नालों वाली जल संपदा, खारे समुद्र में गिरकर अपेय ही बनती चली जाएगी।
वर्तमान में तो सर्वत्र कुहासा छाया दीखता है। पतझड़ की तरह सर्वत्र ठूठों-ही-ठूठों का जमघट दीख पड़ता है। पतन और पराभव का नगाड़ा बजता सुनाई देता है। भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है और लगता है कि मनुष्य समुदाय अब सामूहिक आत्महत्या करने पर ही उतारू आवेश से बुरी तरह ग्रसित हो रहा है। चूहों और खरगोशों की, संख्या जब असाधारण रूप से बढ़ जाती है और उनके लिए खाने, पीने, रहने के लिए सहारा शेष नहीं रहता, तो वे किसी बड़े जलाशय में डूब मरने के लिए बेतहाशा दौड़ लगाते देखे जाते हैं। चल रही गतिविधियों की समीक्षा करने पर लगता है मानो एक ऐसा तूफान उभर रहा है कि मानवी सत्ता, महत्ता, संपदा और प्रगति जैसे संचय में से कुछ भी उसकी चपेट से बचकर रह नहीं सकेगा।
अहंकारी यदुवंशी आपस में ही लड़-मरकर खप गए थे। उन पर बाहर से कोई वज्रपात नहीं हुआ था। आग सबसे पहले उसी स्थान को जलाती है, जहाँ से वह प्रकट होती है। उद्दीप्त वासना, अनियंत्रित तृष्णा और उन्माद जैसी अहंकारिता का त्रिदोष, जब महाग्राह की तरह मानवी गरिमा को निगलता-गटकता चला जा रहा हो, तब बच सकने की आशा यत्किंचित् ही शेष रह जाती है। वर्तमान में उफनते तूफानी अनाचार को देखते हुए लगता है कि सचमुच हम महाविनाश की प्रलय-प्रक्रिया की ओर सरपट चाल से दौड़े चले जा रहे हैं।
प्रचंड प्रवाह को रोक सकने वाला बाँध विनिर्मित करने, जलधारा को नहरों के माध्यम से खेत-बगीचे तक पहुँचाने का काम तो निश्चय ही बड़ा कष्टसाध्य और श्रमसाध्य है। पर करने वाले जब प्राणपण से अपने पुरुषार्थ को सृजन की सदाशयता के साथ संबद्ध करते हैं तो उनकी संसाधना भी कम चमत्कारी परिणाम उत्पन्न नहीं करती। फरहाद, शीरी को पाने के लिए पहाड़ खोदकर लंबी नहर निकाल सकने में, एकाकी प्रयासों के बलबूते ही सफल हो गया था। गंगा को स्वर्ग से घसीटकर जमीन पर बहने के लिए बाधित करने में भगीरथ अकेले ही सफल हो गए थे। व्यापक अंधकार पर छोटा दीखने वाला सूरज ही विजय प्राप्त कर लेता है, अस्तु यह आशा भी की जा सकती है कि मनुष्य में उत्कृष्टता का उदय होगा, तो यह वातावरण भी बदल जाएगा, जो हर दृष्टि से भयंकर-ही-भयंकर दीख पड़ रहा है।
|
|||||
- लेने के देने क्यों पड़ रहे हैं?
- विभीषिकाओं के पीछे झाँकती यथार्थता
- महान् प्रयोजन के श्रेयाधिकारी बनें
- संवेदना का सरोवर सूखने न दें
- समस्याओं की गहराई में उतरें
- समग्र समाधान : मनुष्य पर देवत्व के अवतरण से
- बस एक ही विकल्प-भाव-संवेदना
- दानव का नहीं, देव का बरण करें