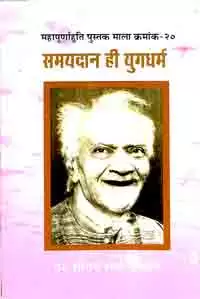|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> समयदान ही युगधर्म समयदान ही युगधर्मश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
प्रतिभादान-समयदान से ही संभव है
1
दान और उसका औचित्य
दान पुण्य शब्द एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं और इनके प्रतिफल भी समानांतर बताए जाते हैं। अध्यात्म भाषा में उसकी महत्ता स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, चमत्कार आदि के रूप में बतायी जाती है और बोल-चाल की भाषा में उसे प्रगति, सफलता, वरिष्ठता प्रदाता तक बताया जाता है।
दान अर्थात् "देना", यही पुण्य है। लेना अर्थात् अधिकारों का अपहरण, यही पाप है। पाप की परिणति लौकिक और पारलौकिक क्षेत्र में अवगति-दुर्गति स्तर की होती है। नरक इसी का अलंकारिक प्रतिपादन है। दोनों में से अपनी गतिविधियाँ किस पक्ष के साथ विनियोजित करना है, यह मनुष्य की अपनी इच्छाओं की बात है। परिस्थितियाँ कई बार इस चयन के विपरीत दबाव भी डालती देखी गई है, पर अततः होता वही है, जिस पर इच्छा शक्ति का संकल्प बनकर केंद्रीभूत होती है।
हरिश्चंद्र, कर्ण, बलि, दधीचि, भामाशाह आदि की कथाएँ इसी तथ्य का प्रतिपादन करती हैं। स्वर्ग जाने वाले और मुक्ति पाने वालों को इससे भी बढ़कर आत्म सपर्मण करना पड़ता है। भक्ति का एक ही स्वरूप है—अपनी इच्छा-आकांक्षाओं को आराध्य के साथ घुला-मिला देना। ईंधन इसी आधार पर तुच्छ होते हुए भी, दावानल बनकर जाज्वल्यमान होता है। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। वह समर्पणकर्ता के हाथों अपने को सौंप देता है और उसके इशारे पर नाचता है। मीरा के साथ सहनृत्य करना, सूर की लकुटी पकड़कर सेवक की तरह कार्यरत रहना, ऐसे ही उदाहरण हैं। सुदामा, चैतन्य, हनुमान, अर्जुन आदि की गणना ऐसे ही भक्तों में होती है, जिन्होंने भगवान के खेत में अपना सर्वस्व उदारतापूर्वक बोया और बीज की तुलना में चार गुना अन्न भंडार अपने कोठे में भरा-सँजोया।
श्रद्धास्पद श्रेष्ठजनों को देव मानव कहा जाता है। उनके अनुदानों के प्रति सृष्टि का कण-कण अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। यहाँ समस्त महामानव मात्र एक ही अवलंबन अपना कर उत्कृष्टता के प्रणेता बन सके हैं, कि उन्होंने संसार में जो पाया, उसकी तुलना में उसके प्रतिफल स्वरूप, असंख्य गुना करने का होते रहने का व्रत निवाहा। यदि कृपणता उन्हें घेरे रही होती, तो प्रेत पिशाचों की पंक्ति में ही गिने जाने योग्य बने रहते; भले ही उनकी संचित-संपदा कितनी ही बढी-चढी क्यों न रही हो ?
सच्चाइयाँ कितनी ही कष्ट साध्य क्यों न हों, अपने स्थान पर अकेले ही समुद्र के बीच अवस्थित प्रकाशस्तंभ की तरह अविचल ही बनी रहती हैं। ऐसी ही सच्चाइयों में से एक यह भी है कि जो जितना देता है, वह उसी अनुपात में पाता है। मसखरी करने वालों को बदले में उपहास ही हाथ लगता है। यह बात इस संदर्भ में कही जा रही है कि देने के नाम पर अँगूठा दिखाने और लेने के लिए कंधे पर बड़ा थैला लादे-फिरने वाले, मात्र निराशा, थकान और खीज ही लेकर लौटते हैं। भले ही उन्होंने मुफ्त में तुर्त-फुर्त बहुत कुछ पाने की शेखचिल्ली जैसा सपना ही क्यों न संजो रखा हो ?
संसार में व्यावहारिकता का ही प्रचलन है। यहाँ इस बाजार में, एक से एक बढ़िया वस्तुएँ भरी और आकर्षक ढंग से सजी पडी हैं. पर उसमें एक को भी मुफ्त में पा सकना कठिन है। जो ऐसी चेष्टा करते हैं, वे चोरों की तरह पकड़े जाते हैं, या फिर भिखारियों की तरह हर द्वार से दुतकारे जाते हैं। इस आधार पर यदि किसी ने कभी कुछ पाया भी होगा, तो वह उसकी आदत और व्यक्तित्व का स्तर गिरा देने के कारण महँगा भी बहुत पड़ा होगा। अनुदान का प्रतिदान ही यहाँ का शाश्वत नियम है।
दुनियाँ का सम्मान और सहयोग उनके लिए सुरक्षित है, जो देते बहुत हैं, पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो प्रवचंकों, पाखंडियों और अना.3क्रम है कि पहले दो, बाद में पाओ। पहले पाने और बाद में उसका एक अंश खैरात कर देने की नीति तो लुटेरे ही अपनाते हैं। उनकी भी घात सदा नहीं लगती।
मन के मोदक न बनाने हों, दिवास्वप्न देखने हों, बिना पंखों के आकाश नापने की योजना न बनानी हो और यथार्थ का अवलंबन करते हुए ठोस उपलब्धियाँ हस्तगत कर लेने की अभिलाषा हो तो वही करना चाहिए जो अब तक के उदारचेता या महामानव अपनाते और उससे प्रेय तथा श्रेय का दुहरा लाभ उठाते रहे हैं। संत, सुधारक, शहीद और सेवाभावी अपनी उदारता के बल पर ही मनुष्यों से लेकर देवताओं तक के वरदान हस्तगत करते रहे हैं। तपश्चर्या अपनाए बिना किसे विभूतियों और सिद्धियों का वरदान हस्तगत हुआ है ?
पूँजी क्या इसी आधार पर जमा होती है कि लिया अधिक और दिया कम जाए ? संसार से हम आए दिन कितना लेते हैं, इसका बही-खाता रखने की किसी को भी फुरसत नहीं है। व्यवसाय के लिए जो पूँजी कहीं से ली जाती है, उसे बाद में ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। यह नियम शाश्वत होते हुए भी हर कोई अपने को इस व्यवस्था से पूरी तरह छूट दिलाना चाहता है। यहाँ हर किसी को हर किसी से कुछ न कुछ लेना ही है। देने के नाम पर अँगूठा दिखा देने या दाँत निपोर देने के अतिरिक्त और कुछ जैसे सूझ ही नहीं पड़ता।
तो क्या सचमुच ही ऐसा है कि कुछ महत्त्वपूर्ण पाने के लिए, वैसा ही कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य किए बिना काम नहीं चल सकता ? इस प्रश्न का प्रत्युत्तर दसों दिशाओं से गूंजते सुना जा सकता है कि "दो और पाओ', "बोओ और काटो", "बाँटो और झोली को कभी खाली होते न पाओ।" इसे शाश्वत सत्य को कृपणता अनादि काल से झुठलाती चली आ रही है, फिर भी यथार्थता को अपने स्थान से एक इंच भी हटाया नहीं जा सका है।
प्रश्न फिर घूमकर वहीं आ जाता है, कि जब अधिकांश लोग अभावों से ग्रसित हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रहकर दिन काटते हैं, तब दान-पुण्य की परंपरा चरितार्थ कैसे हो ? इस प्रश्न में बालकों जैसी भोलेपन की झलक-झाँकी मिलती है। समझा जाता है कि धनदान ही एक मात्र दान है, क्योंकि हर जगह उसी का बोलबाला दीख पड़ता है। चर्चा और प्रशंसा उसी की होती है। प्रचलन को देखते हुए ऐसी मान्यता बन जाना कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है। जो रिश्वत की उपहार की करामात जानते हैं, उनका दावा है कि बेचारा मनुष्य तो चीज ही क्या है ? देवताओं तक को भेंट उपहार के स्तवन, मनुहार के सहारे अपने पक्ष में बनाया जा सकता है। भले ही वह अनुग्रह कितना ही अनैतिक व अवांछनीय क्यों न हो, इस मान्यता वालों का एक बड़ा समुदाय है।
ऐसी दशा में यदि दान शब्द का अर्थ धनदान के साथ जुड़ गया हो और फिर मनोविनोद तक के लिए किए जाने वाले अपव्यय को भी, खर्च की मद में लिखे जाने के कारण दान समझा जाने लगी हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? पूजा पाठ में एक विधि पशुवध की भी सम्मिलित थी और उसे बलिदान कहा जाता था। हरिजनों को कभी जूठन दान दिया जाता था, जिसे अब उन्होंने अपमान माना है। और लेना अस्वीकार कर दिया है। रोगियों के उतरे हुए कपड़े कभी जाति विशेष के लोग खुशी-खुशी ले जाते थे, पर अब इस "उतरन-दान" को स्वाभिमानी-नितांत निर्धन भी स्वीकार नहीं करते। विवाह शादी की धूमधाम में उलीचा गया धन कन्यादान, वागदान आदि नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दान शब्द का दुरुपयोग जहाँ-तहाँ भ्रांतियुक्त रूपों में देखा जा सकता है।
संग्रहित धन को आयकर से बचत हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था को दान देकर दुहरा लाभ उठा लिया जाता है-टेक्स की बचत और दानवीरों की श्रेणी में अपनी गिनती। चंदा माँगने वालों का दबाव, कुटुंबी संबंधियों पर अनुग्रह, तीर्थयात्रा के नाम पर पर्यटन पिकनिक भी दान है। मनोरंजन के लिए उद्यान, पार्क स्विमिंग पूल इत्यादि बना देना भी जनहित कहकर मन को समझाया जा सकता है। रिश्वत में दी गई राशि भी उदारपूर्वक दी जाने के कारण दान ही है। यहाँ तक कि नशा पीने से पहले उसे शंकर भगवान को अर्पण कर दिए जाने पर वह भी भोग प्रसाद बन जाता है। यश के लिए कहीं पैसा देकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना और उस "इमेज" का लाभ किसी दूसरी प्रकार से भुना लेना भी दान की श्रेणी में गिना जा सकता है। इस प्रकार दान शब्द व्यवहार में जिस ढंग से प्रयुक्त होता है, उसे आदान-प्रदान कहा जाए तो अधिक उपयुक्त हो सकता है।
दान को पुण्य उसी आधार पर कहा जा सकता है कि उसको प्रामाणिक माध्यमों से उच्चस्तरीय सत्प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए। इसके विपरीत इस मद में खर्ची गई राशि यदि आलस्य प्रमाद, पाखंड, प्रवंचना, दुर्व्यसन, अंधविश्वासों के विस्तार में निमित्त कारण बनती है, तो उससे ठीक उलटा प्रतिफल भी हो सकता है। परिणाम और प्रयोग के साथ जुड़ी हुई उत्कृष्टता ही पुण्य का आधार बनती है। और उसकी प्रतिक्रिया पुण्य के साथ जुड़ने वाले, अनेक कल्याण कारक रूपों में सामने आती हैं। इसके विपरीत यदि उससे दुर्जनों का, दुष्प्रयोजनों का परिपोषण हुआ, तो समझना चाहिए कि वह देने की तरह खर्च किए जाने पर भी, ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकती है, जो अपने तथा दूसरों के लिए नरक वास जैसे अनेकों संकट खड़े करती है।
प्रवंचनाओं के अतिरिक्त दान क्षेत्र में और भी अनेकों व्यवधान हैं। मुफ्तखोरी की आदत बढाना, किसी के अधःपतन का द्वार खोलना है। आपत्तिग्रस्तों को सामाजिक सहायता देकर उन्हें अपने पैरों खड़े होने की स्थिति तक पहुँचा देना एक बात है, किंतु मुफ्तखोरी की। आदत डालकर वैसा स्वभाव बना देना एक प्रकार से भले चंगे को अपाहिज बना देने के समान है।
ऐसी दशा में यह अति विचारणीय है कि न्यायोपार्जित धन इतनी मात्रा में कहाँ से पाया जाए, जिसे प्रशंसा पाने योग्य स्तर पर दान के नाम पर बिखेरा जा सके। वस्तुतः धनिकों का दान उनके संचित पापों का प्रायश्चित है। फोड़े में भरे स्वाद को निचोड़ देने में, चीरा लगाने वाले की अपेक्षा उसे निकालने देने वाले की भलाई अधिक है।
औचित्य इस बात में है कि हर व्यक्ति औसत नागरिक स्तर का जीवन जिए। "सादा जीवन उच्च विचार" की नीति अपनाए। न्यायोचित पसीने की कमाई पर संतोष करे। चोरी बदमाशी का इस हेतु प्रयोग न करे। यदि अपने खर्च से बच जाता है तो उसे बिना रोके अवांछनीयताओं जैसी अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए खर्च कर दें। सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की व्यवस्था न जुट पाने से ही श्रेष्ठता और प्रगतिशीलता की पौध सूख रही है। उसे सींचने के लिए जो कुछ बन सकता हो करें। यही सत्युगी परंपरा रही है, यही किया भी जाना चाहिए।
|
|||||
- दान और उसका औचित्य
- अवसर प्रमाद बरतने का है नहीं
- अभूतपूर्व अवसर जिसे चूका न जाए
- समयदान-महादान
- दृष्टिकोण बदले तो परिवर्तन में देर न लगे
- प्रभावोत्पादक समर्थता
- प्रामाणिकता और प्रखरता ही सर्वत्र अभीष्ट
- समय का एक बड़ा अंश, नवसृजन में लगे
- प्राणवान प्रतिभाएँ यह करेंगी
- अग्रदूत बनें, अवसर न चूकें