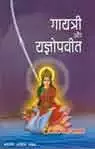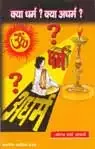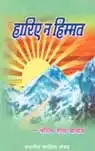|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री प्रार्थना गायत्री प्रार्थनाश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
गायत्री प्रार्थना
प्रार्थना का महत्त्व
गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रकार है :
ॐ (परमात्मा) भू: (प्राण स्वरूप) भुव: (दु:खनाशक) स्व: (सुख स्वरूप) तत् (उस) सवितु: (तेजस्वी) वरेण्य (श्रेष्ठ) भर्ग: (पापनाशक) देवस्य(दिव्य) धीमहि (धारण करे) धियो (बुद्धि) यो (जो) न: (हमारी) प्रचोदयात् (प्रेरित करें)।
अर्थात् उस प्राण स्वरूप, दु:खनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें।
इस अर्थ का विचार करने से उसके अंतर्गत तीन तथ्य प्रकट होते हैं।
१ - ईश्वर का दिव्य चिंतन,
२ - ईश्वर को अपने अंदर धारण करना,
३ - सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। यह तीनों ही बातें असाधारण महत्त्व की है।
(१) ईश्वर के प्राणवान्, दु ख रहित, आनंद स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित, दैवी गुण संपन्न स्वरूप का ध्यान करने का तात्पर्य यह है कि इन्हीं गुणों को हम अपने में लाएं। अपने विचार और स्वभाव को ऐसा बनाएँ कि उपयुक्त विशेषताएँ हमारे व्यावहारिक जीवन में परिलक्षित होने लगें। इस प्रकार की विचारधारा, कार्य पद्धति एवं अनुभूति मनुष्य की आत्मिक और भौतिक स्थिति को दिन-दिन समुन्नत एवं श्रेष्ठ बनाती चलती है।
(२) गायत्री मंत्र के दूसरे भाग में परमात्मा को अपने अंदर धारण करने की प्रतिज्ञा है। उस ब्रह्म, उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को संसार के कण-कण में व्याप्त देखने से मनुष्य को हर घड़ी ईश्वर दर्शन का आनंद प्राप्त होता रहता है और वह अपने को ईश्वर के निकट स्वर्गीय स्थिति में रहता हुआ अनुभव करता है।
(३) मंत्र के तीसरे भाग में सद्बुद्धि का महत्त्व सर्वोपरि होने की मान्यता का प्रतिपादन है। भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी महान् भगवत् कृपा है कि इसके प्राप्त होने पर अन्य सब सुख-संपदाएं अपने आप प्राप्त हो जाती हैं।
इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वरीय दिव्य गुणों को प्राप्त करने, दूसरे भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण धारण करने और तीसरे में बुद्धि को सात्विक बनाने, आदर्शों को ऊँचा रखने, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं में रमण करना और तुच्छ तृष्णाओं एवं वासनाओं के लिए हमें नचाने वाली कुबुद्धि को मानस लोक में से बहिष्कृत करना। जैसे-जैसे कुबुद्धि का कल्मष दूर होगा, वैसे ही वैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों की अपने में वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात से लौकिक और पारलौकिक आनंद की अभिवृद्धि होती जाएगी।
गायत्री मंत्र में सन्निहित उपर्युक्त तथ्य में ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों हैं। सद्गुणों का चिंतन ज्ञानयोग है। ब्रह्म की धारणा भक्तियोग है और बुद्धि की सात्विकता एवं अनासक्ति कर्मयोग है। वेदों में ज्ञान, कर्म, भक्ति ये तीनों ही विषय हैं। गायत्री में बीज रूप से यह तीनों ही तथ्य सर्वांगीण ढंग से प्रतिपादित हैं।
इन भावनाओं का एकांत में बैठकर नित्य अर्थ-चिंतन करना चाहिए। यह ध्यान-साधना मनन के लिए अतीव उपयोगी है। मनन के लिए तीन संकल्प नीचे दिए जाते हैं। इन संकल्पों को शांत चित्त से, स्थिर आसन पर बैठकर, नेत्र बंद रखकर मन ही मन दुहराना चाहिए और कल्पना शक्ति की सहायता से इन संकल्पों का ध्यान मन:क्षेत्र में भली प्रकार अंकित करना चाहिए।
(१) परमात्मा का ही पवित्र अंश-अविनाशी राजकुमार मैं आत्मा हूँ। परमात्मा प्राणस्वरूप है, मैं भी अपने को प्राणवान्
आत्मशक्ति संपन्न बनाऊँगा। प्रभु दु ख रहित है, मैं दु:खदायी मार्ग पर न चलूँगा। ईश्वर आनंद स्वरूप है, अपने जीवन को आनंद स्वरूप बनाना तथा दूसरों के आनंद में वृद्धि करना मेरा कर्त्तव्य है। भगवान् तेजस्वी है, मैं भी निर्भीक, साहसी, वीर, पुरुषार्थी और प्रतिभावान बनूँगा। ब्रह्म श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता, आदर्शवादिता एवं सिद्धांतमय जीवन नीति अपनाकर मैं भी श्रेष्ठ बनूँगा। जगदीश्वर निष्पाप है, मैं भी पापों से, कुविचारों और कुकर्मों से बचकर रहूँगा। ईश्वर दिव्य है, मैं भी अपने को दिव्य गुणों से सुसज्जित करूँगा, संसार को कुछ देते रहने की देव नीति अपनाऊंगा। इसी मार्ग पर चलने से मेरा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है।
(२) उपर्युक्त गुणों वाले परमात्मा को मैं अपने अंदर धारण करता हूँ। इस विश्व ब्रह्माण्ड के कण-कण में प्रभु समाए हैं। वे मेरे चारों ओर, भीतर बाहर सर्वत्र फैले हुए हैं। मैं स्मरण करूँगा। उन्हीं के साथ हँसूँगा और खेलूँगा। वे ही मेरे चिर सहचर हैं। लोभ, मोह, वासना और तृष्णा का प्रलोभन दिखाकर पतन के गहरे गर्त में धकेल देने वाली दुर्बुद्धि से, माया से बचकर अपने को अंतर्यामी परमात्मा की शरण में सौंपता हूँ। उन्हें ही अपने हृदयासन पर अवस्थित करता हूँ अब वे मेरे और मैं केवल उन्हीं का हूँ। ईश्वरीय आदर्शों का पालन करना और विश्वमानव परमात्मा की सेवा करना ही अब मेरा लक्ष्य रहेगा।
(३) सद्बुद्धि से बढ़कर और कोई दैवी वरदान नहीं। इस दिव्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मैं घोर तप करूँगा। आत्मचिंतन करके अपने अंत:करण चतुष्टय में (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में) छिपकर बैठी हुई कुबुद्धि को बारीकी के साथ ढूँढूँगा और उसे बहिष्कृत करने में कोई कसर न रहने दूँगा। अपनी आदतों, मान्यताओं, भावनाओं और विचारधाराओं में जहाँ भी कुबुद्धि पाऊँगा, वहीं से इसे हटाऊंगा। असत्य को त्यागने और सत्य को ग्रहण करने में रत्ती भर भी दुराग्रह नहीं करूँगा। अपनी भूलें मानने और विवेक संगत बातों को मानने में तनिक भी दुराग्रह नहीं करूँगा। अपने स्वभाव, विचार और कर्मों की सफाई करना, सड़े -गले, कूड़े-कचरे को हटाकर सत्य, शिव, सुंदर की भावना से अपनी मनोभूमि को सजाना है। अब मेरी पूजा-पद्धति से प्रसन्न होकर भगवान मेरे अंत करण में निवास करेंगे, तब मैं उनकी कृपा से जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होऊँगा।
इन संकल्पों में अपनी रुचि के अनुसार शब्दों का हेर-फेर किया जा सकता है, पर भाव यही होना चाहिए। नित्य शांत चित्त से भावपूर्वक इन संकल्पों को देर तक अपने हृदय में स्थान दिया जाए, तो गायत्री के मंत्रार्थ की सच्ची अनुभूति हो सकती है। इस अनुभूति से मनुष्य दिन-दिन अध्यात्म मार्ग में ऊँचा उठ सकता है।
|
|||||