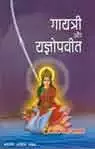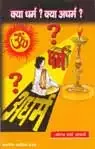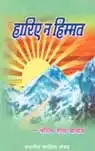|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री की गुप्त शक्तियाँ गायत्री की गुप्त शक्तियाँश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
गायत्री मंत्र की गुप्त शक्तियों का तार्किक विश्लेेषण
गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य
गायत्री की महिमा गाते हुए शास्त्र और ऋषि-महर्षि थकते नहीं। इसकी प्रशंसा तथा महत्ता के सम्बन्ध में जितना कहा गया है, उतना शायद ही और किसी की प्रशंसा में कहा गया हो। प्राचीन काल में बड़े-बड़े तपस्वियों ने प्रधान रूप से गायत्री की ही तपश्चर्यायें, अभीष्ट सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। शाप और वरदान के लिए वे विविध-विधियों से गायत्री का ही उपयोग करते थे।
प्राचीन काल में गायत्री गुरुमंत्र था, आज गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। अधिकांश मनुष्य उसे जानते हैं। अनेक मनुष्य किसी न किसी प्रकार उसको दुहराते या जपते रहते हैं अथवा किसी विशेष अवसर पर स्मरण कर लेते हैं। इतने पर भी देखा गया है कि उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। गायत्री जानने वालों में कोई विशेष स्तर दिखाई नहीं देता। इस आधार पर यह आशंका होने लगती है-कहीं गायत्री की प्रशंसा और महिमा वर्णन करने वालों ने अत्युक्ति तो नहीं की? कई मनुष्य आरम्भ में उत्साह दिखाकर थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ बैठते हैं, वे देखते हैं कि इतने दिन हमने गायत्री की उपासना की, पर लाभ कुछ न हुआ। फिर क्यों इसके लिए समय बरबाद किया जाए। कारण यह है कि प्रत्येक कार्य एक नियत विधि-व्यवस्था द्वारा पूरा होता है। चाहे जैसे, चाहे जिस काम को, चाहे जिस प्रकार करना आरम्भ कर दिया जाए, तो अभीष्ट परिणाम नहीं मिल सकता। मशीनों द्वारा बड़े-बड़े कार्य होते हैं, पर होते तभी हैं जब वे उचित रीति से चलाई जायें। यदि कोई अनाड़ी चलाने वाला मशीन को यों ही अन्धाधुन्ध चालू कर दे, तो लाभ, होना तो दूर, उलटे कारखाने के लिए तथा चलाने वाले के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। मोटर तेज दौड़ने वाला वाहन है। उसके द्वारा एक-एक दिन में कई सौ मील की यात्रा सुखपूर्वक की जा सकती है, पर अगर कोई अनाड़ी आदमी ड्राइवर की जगह जा बैठे और चलाने की विधि तथा कलपुर्जों के उपयोग की जानकारी न होते हुए भी उसे चलाना आरम्भ कर दे; तो यात्रा तो दूर, उलटे ड्राइवर, मोटर यात्रा करने वाले के लिए अनिष्ट खड़ा हो जायगा या यात्रा निष्फल होगी। ऐसी दशा में मोटर को कोसना, उनकी शक्ति पर अविश्वास कर बैठना उचित नहीं कहा जा सकता। अनाड़ी साधकों द्वारा की गई उपासना भी यदि निष्फल हो, तो आश्चर्य की बात नहीं है।
जो वस्तु जितनी अधिक महत्त्वपूर्ण होती है, उसकी प्राप्ति उतनी कठिन भी होती है। सीप-घोंघे आसानी से मिल सकते हैं उन्हें चाहे कोई बीन सकता है, पर मोती जिन्हें प्राप्त करने हैं समुद्र तल तक उतरना पड़ेगा और इस खतरे के काम को किसी से सीखना पड़ेगा। कोई अजनबी आदमी गोताखोरी को बच्चों का खेल समझकर या यों ही समुद्र तल में उतरने के लिए डुबकी लगाये, तो उसे अपनी नासमझी के कारण असफलता पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
यों गायत्री में अन्य समस्त मन्त्रों की अपेक्षा एक खास विशेषता यह है कि नियत विधि से साधना न करने पर भी साधक को कुछ हानि नहीं होती है, परिश्रम भी निष्फल नहीं जाता कुछ न कुछ लाभ ही रहता है, पर उतना लाभ नहीं होता, जितना कि विधिपूर्वक साधना के द्वारा होना चाहिए। गायत्री की तांत्रिक उपासना में तो अविधि साधना से हानि भी होती है, पर साधारण साधना में वैसा कोई खतरा नहीं है। तो भी परिश्रम का पूरा प्रतिफल न मिलना भी तो एक प्रकार की हानि है, इसलिए बुद्धिमान् मनुष्य उतावली, अहमन्यता उपेक्षा के शिकार नहीं होते और साधना मार्ग पर वैसी ही समझदारी से चलते हैं, जैसे हाथी नदी को पार करते समय थाह लगाते हुए, धीरे-धीरे आगे कदम बढ़ाता है।
कुछ औषधियाँ नियत मात्रा में लेकर नियत विधिपूर्वक तैयार करके रसायन बनाई जाए और उसको नियत मात्र में नियत अनुपात के साथ रोगी को सेवन कराया जाए, तो आश्चर्यजनक लाभ होता है; परन्तु यदि उन्हीं औषधियों को चाहे जिस तरह, चाहे जितनी मात्रा में लेकर चाहे जैसे बना डाला जाए और चाहे जिस तरह, चाहे जितनी मात्रा में, चाहे जिस अनुपात से सेवन करा दिया जाए तो निश्चय ही परिणाम अच्छा न होगा। वे औषधियाँ जो विधिपूर्वक प्रयुक्त होने पर अमृतोपम लाभ दिखाती थीं, अविधिपूर्वक प्रयुक्त होने पर निरर्थक सिद्ध होती हैं। ऐसी दशा में उन औषधियों को दोष देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। गायत्री साधना भी यदि अविधिपूर्वक की गई है, तो वैसा लाभ नहीं दिखा सकती जैसा कि विधिपूर्वक साधना से होना चाहिए।
पात्र-कुपात्र हर कोई गायत्री शक्ति का मनमाना प्रयोग न कर सके इसलिए कलियुग से पूर्व ही गायत्री को कीलित कर दिया गया है। जो उसका उत्कीलन जानता है, वही लाभ उठा सकता है। बन्दूक का लाइसेन्स सरकार उन्हीं को देती है, जो उसके पात्र हैं। परमाणु बम का रहस्य थोड़े से लोगों तक सीमित रखा गया, ताकि हर कोई उसका दुरुपयोग न कर डाले। कीमती खजाने की तिजोरियों में बढ़िया चोर-ताले लगे होते हैं, ताकि अनाधिकारी लोग उसे खोल न सकें। इसी आधार पर गायत्री को कीलित किया गया है कि हर कोई उससे अनुपयुक्त प्रयोजन सिद्ध न कर सकें।
पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार गायत्री को वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों ने शाप दिया था कि "उसकी साधना निष्फल होगी।" इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया, तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अन्त में ऐसा मार्ग निकाला गया कि जो शाप-विमोचन की विधि पूरी करके गायत्री साधना करेगा, उसका प्रयत्न सफल होगा और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जाएगा। इस पौराणिक उपाख्यान में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसे न जानने वाले केवल 'शापमुक्तोभव' मन्त्रों को दुहराकर यह मान लेते हैं कि हमारी साधना शाप मुक्त हो गई।
वशिष्ठ का अर्थ - 'विशेष रूप से श्रेष्ठ'। गायत्री साधना में जिसने विशेष रूप से श्रम किया है, जिसने सवा करोड़ का जप किया है, उसे, विशिष्ठ पदवी दी जाती थी। रघुवंशियों के कुल गुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवी धारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लवकुश इन छ: पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं, अलग-अलग थे, पर उपासना के आधार पर उन सभी ने वशिष्ठ पदवी को पाया था। वशिष्ठ का शाप विमोचन करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वशिष्ठ से गायत्री साधना की दीक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ-प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। कारण यह है कि अनुभवी व्यक्ति ही यह जान सकता है कि मार्ग में कहाँ क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है ? जब पानी में तैरने की शिक्षा किसी नये आदमी को दी जाती है, तो कोई कुशल तैराक उसके साथ रहता है, ताकि कदाचित नौसिखिया डूबने लगे तो वह हाथ पकड़कर उसे खींच ले और उसे पार लगा दे तथा तैरते समय जो भूल हो रही हो, उसे समझाता, सुधारता चले। यदि कोई शिक्षक तैराक न हो और तैरना सीखने के लिए बालक मचल रहे हों, तो कोई वृद्ध विनोदी पुरुष उन बालकों को समझाने के लिए ऐसा कह सकता है कि-"बच्चो! तालाब में न उतरना, इसमें तैराक गुरु का शाप है। बिना गुरु का शाप मुक्त हुए तैरना सीखोगे, तो वह निष्फल होगा।" इन शब्दों में अलंकार तो है, शाब्दिक अत्युक्ति भी इसे कह सकते हैं, पर तथ्य बिलकुल सच्चा है। बिना शिक्षक की निगरानी के तैरना सीखने की कोशिश करना एक दुस्साहस ही है।
सवा करोड़ जप की साधना करने वाले गायत्री उपासक की - वशिष्ठ की - संरक्षकता प्राप्त कर लेना, वशिष्ठ का शाप-विमोचन है। इससे साधक निभींक, निधड़क अपने मार्ग पर तेजी से बढ़ता चला जाता है। रास्ते की कठिनाइयों को वह संरक्षक दूर करता चलता है, जिससे नये साधक के मार्ग की बहुत सी बाधाएँ अपने आप दूर हो जाती हैं और अभीष्ट उद्देश्य तक जल्दी ही पहुँच जाता है।
गायत्री को केवल वशिष्ठ का ही शाप नहीं, एक दूसरा शाप भी है, वह है विश्वामित्र का। इस रत्न-कोष पर दुहरे ताले जड़े हुए हैं, ताकि अधिकारी लोग ही खोल सकें और ले भागू, जल्दबाज, अश्रद्धालु, हरामखोरों की दाल न गलने पाए। विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाला परमार्थी, उदार, सत्पुरुष कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन् उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। कठोर साधना और तपश्चर्या द्वारा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। रावण वेदपाठी था, उसने बड़ी-बड़ी तपश्चर्यायें करके आश्चर्यजनक सिद्धियाँ भी प्राप्त की थीं। इस प्रकार वह वशिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता है, पर विश्वामित्र नहीं, क्योंकि संसार की भलाई के, धर्मचर्या एवं परमार्थ के गुण उसमें नहीं थे। स्वार्थी, लालची तथा संकीर्णमनोवृत्ति के लोग चाहे कितने ही बड़े सिद्ध क्यों न हों, शिक्षक नियुक्त किये जाने योग्य नहीं, यही दुहरा शाप विमोचन है। जिसने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला पथप्रदर्शक, गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने दोनों शापों से गायत्री को छुड़ा लिया, उसकी साधना वैसा ही फल उपस्थित करेगी, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है।
यह कार्य सरल नहीं है; क्योंकि एक तो ऐसे व्यक्ति ही मुश्किल से मिलते हैं, जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गुणों से सम्पन्न हों। यदि मिलें भी तो हर किसी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्ति और सामथ्र्य सीमित होती है और उससे वे कुछ थोड़े ही लोगों की सेवा कर सकते हैं। यदि पहले से ही उतने लोगों का भार अपने ऊपर लिया हुआ है, तो अधिक की सेवा करना उनके लिए कठिन है। स्कूलों में एक अध्यापक प्राय: ३० की संख्या तक विद्यार्थी पढ़ा सकता है। यदि वह संख्या ६० हो जाए, तो न अध्यापक पढ़ा सकेगा, न बालक पढ़ सकेंगे, इसलिए ऐसे सुयोग्य शिक्षक सदा ही नहीं मिल सकते। लोभी, स्वार्थी और ठग गुरुओं की कमी नहीं, जो दो रुपया गुरु-दक्षिणा लेने के लोभ से चाहे किसी के गले में कण्ठी बाँध देते हैं। ऐसे लोगों को पथप्रदर्शक नियुक्त करना एक प्रवञ्चना और विडम्बना मात्र है।
गायत्री दीक्षा गुरु-मुख होकर ली जाती है, तभी फलदायक होती है। बारूद को जमीन पर चाहे जहाँ फैलाकर उसमें दियासलाई लगाई जाए, तो वह मामूली तरह से जल जाएगी, पर उसे ही बन्दूक में भरकर विधिपूर्वक प्रयुक्त किया जाए, तो उसमें भयंकर शब्द के साथ एक प्राणघातक शक्ति पैदा होगी। छपे हुए कागजों में पढ़कर या कहीं किसी से भी गायत्री मंत्र सीख लेना ऐसा ही है, जैसा जमीन पर बिछाकर बारूद जलाना और गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना ऐसा है, जैसे बन्दूक के माध्यम से बारूद का उपयोग होना।
गायत्री की विधिपूर्वक साधना करना ही अपने परिश्रम को सफल बनाने का सीधा मार्ग है, इस मार्ग का पहला आधार ऐसे पथ-प्रदर्शक को खोज निकालना है, जो वशिष्ठ एवं विश्वामित्र, गुण वाला हो और जिनके संरक्षण में शाप विमोचन गायत्री-साधना हो सके। ऐसे सुयोग्य संरक्षक सबसे पहले यह देखते हैं कि साधक की मनोभूमि, शक्ति, सामथ्र्य, रुचि कैसी है, उसी के अनुसार वे उसके लिए साधन विधि चुनकर देते हैं। अपने आप विद्यार्थी यह निश्चित नहीं कर सकता कि मुझे किस क्रम से क्या-क्या पढ़ना चाहिए? इसे तो अध्यापक ही जानता है कि यह विद्यार्थी स्तर के कक्षा की योग्यता रखता है और इसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए? जैसे अलग-अलग प्रकृति के एक रोग के रोगियों को भी औषधि अलग-अलग अनुपात तथा मात्रा का ध्यान रख कर दी जाती है। वैसे ही साधकों की आन्तरिक स्थिति के अनुसार उसके साधनों नियमों में हेर-फेर हो जाता है। इसका निर्णय साधक स्वयं नहीं कर सकता। यह कार्य तो सुयोग्य, अनुभवी और सूक्ष्मदर्शी पथ-प्रदर्शक ही कर सकता है।
आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और विश्वास यह दो प्रधान अवलम्बन हैं। इन दोनों का प्रारम्भिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर किया जाता है। जैसे ईश्वर उपासना प्रारम्भिक माध्यम किसी मूर्ति, चित्र या छवि को बनाया जाता है वैसे ही श्रद्धा और विश्वास की उन्नति गुरु नामक व्यक्ति के ऊपर उन्हें दृढ़तापूर्वक जमाने से होती है। प्रेम तो स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र आदि पर भी हो सकता है, पर श्रद्धायुक्त प्रेम का पात्र गुरु ही होता है। माता-पिता भी यदि वशिष्ठ, विश्वामित्र गुणों वाले हों, तो वे सबसे उत्तम गुरु हो सकते हैं। गुरु परम हितचिंतक, शिष्य की मनोभूमि से परिचित और उसकी कमजोरियों को समझने वाला होता है, इसलिए उसके दोषों को जानकर उन्हें धीरे-धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर मोड़ने का प्रयल करता रहता है, ताकि वे दोष अपने आप छूट जायें। योग्य गुरु अपनी साधना द्वारा एकत्रित की आध्यात्मिक शक्ति को धीरे-धीरे शिष्य के अन्त:करण में वैसे ही प्रवेश कराता रहता है, जैसे माता अपने पचाये हुए भोजन को स्तनों में दूध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहती है। माता का दूध पीकर बालक पुष्ट होता है। गुरु का आत्मतेज पीकर शिष्य का आत्म-बल बढ़ता है इस आदान-प्रदान को आध्यात्मिक भाषा में 'शक्तिपात' कहते हैं। ऐसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व संचित शुभ संस्कारों का फल अथवा प्रभु की महती कृपा का चिह्न ही समझना चाहिए।
गुरु का वरण गायत्री उपासना का आरम्भिक किन्तु महत्त्वपूर्ण अंग इसलिए माना गया है कि वह सद्गुरु उपलब्ध कराने का प्रथम सोपान है। सद्गुरु उस निर्मल अन्तरात्मा को कहते हैं, जो हमारा सही मार्गदर्शन करने में समर्थ है। इसी की प्रेरणा और प्रकाश का अनुसरण करके मनुष्य महानता का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हर घड़ी सद्गुरु का ही सत्संग सम्भव है और कुमार्ग से बचने तथा सन्मार्ग पर चलने के हर अवसर पर उचित पथ प्रदर्शन के लिए वही हर समय उपस्थित रह सकता है। जिनके साथ सद्गुरु का मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और उद्बोधन हर घड़ी मौजूद है उसके लिए जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकना अति सरल ही बन जाता है।
आमतौर से मनोभूमि में बसे हुए कुसंस्कार, दुर्भाव, मल, आवरण विक्षेप अन्त:करण को मूछित बना देते हैं और वह उचित मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं होता। दबी जबान से सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता भी है, तो वह इतनी मन्द होती है कि वासना और तृष्णा के नशे में मदोन्मत्त मन उसे ठीक तरह से सुन भी नहीं पाता। आवश्यकता इस बात की है कि अन्तरात्मा में विद्यमान सद्गुरु को स्वच्छ, समर्थ और सक्रिय बनाया जाए। जिसके प्रभाव से प्रभावित चेतना को कुपथ छोड़कर सत्पथ पर चलने का साहस उपलब्ध हो सके। जिसने इतनी सफलता प्राप्त कर ली हो, उसके लिए मानवी महत्ता का लक्ष्य प्राप्त कर लेना कुछ भी कठिन नहीं है।
गुरु का वरण इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। गुरु का प्रत्यक्ष प्रयत्न यह होता है कि शिष्य का प्रसुप्त अन्त:करण और विवेक जाग पड़े। सद्गुरु चैतन्य एवं परिपुष्ट हो जायें। इतना प्रयोजन पूरा कर लेने पर मानव शरीरधारी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कृतज्ञता के नाते उसके वन्दन अभिनन्दन तो तब भी उचित रहते हैं, पर अन्तत: अपने अंतरंग में निवास करने वाला अशरीरी सद्गुरु ही निरन्तर का- जन्मजन्मान्तरों का साथी बनकर नाव को पार लगाने में समर्थ होता है। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए समर्थ, सुयोग्य, चरित्रवान् और विज्ञ, विद्वान् गुरु का वरण करना आवश्यक माना गया है।
कितने ही व्यक्ति सोचते हैं कि अमुक समय पर एक व्यक्ति को गुरु बना चुके, अब हमें दूसरे पथ-प्रदर्शक की नियुक्ति का अधिकार नहीं रहा। उनका यह सोचना वैसा ही है जैसा कोई विद्यार्थी यह कहे कि-"अक्षर आरम्भ करते समय जिस अध्यापक को मैंने अध्यापक माना था, अब वही जीवन भर उसके अतिरिक्त न किसी से शिक्षा ग्रहण करूंगा और न किसी को अध्यापक मानूँगा।" एक ही अध्यापक से संसार भर के सभी विषयों के जान लेने की आशा नहीं की जा सकती। फिर वह अध्यापक मर जाए, रोगी हो जाए, कहीं चला जाए, तो भी उसी से शिक्षा लेने का आग्रह करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है? फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिष्य प्राथमिक गुरु की अपेक्षा कहीं अधिक जानकार हो जाए और उसका जिहास क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाए, ऐसी दशा में उसकी जिज्ञासाओं, का समाधान उस प्राथमिक शिक्षक द्वारा ही करने का आग्रह किया जाए, तो यह किस प्रकार सम्भव है ?
प्राचीनकाल के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर इस उलझन का समाधान हो जाता है। महर्षि दत्तात्रेय ने चौबीस गुरु किये थे। राम और लक्ष्मण ने जहाँ वशिष्ठ से शिक्षा पाई थी, वहाँ विश्वामित्र से भी बहुत कुछ सीखा था। दोनों ही उनके गुरु थे। श्री कृष्ण जी ने सन्दीपन ऋषि से भी विद्यायें पढ़ी थीं और महर्षि दुर्वासा भी उनके गुरु थे। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कृष्ण भी। इन्द्र के गुरु वृहस्पति भी थे और नारद भी। इस प्रकार अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जिससे प्रकट होता है कि आवश्यकतानुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इनमें कोई ऐसी सीमा का बन्धन नहीं, जिसके कारण एक के उपरान्त किसी दूसरे से प्रकाश प्राप्त करने में प्रतिबन्ध हो। वैसे भी एक व्यक्ति के कई पुरोहित, तीर्थ पुरोहित होते हैं। ग्राम्य पुरोहित, कुल पुरोहित, राष्ट्र पुरोहित और दीक्षा पुरोहित आदि। जिसे गायत्री साधना का पथ प्रदर्शक नियुक्त किया है वह साधना पुरोहित या ब्रह्म पुरोहित है। यह सभी पुरोहित अपने-अपने क्षेत्र, अवसर और कार्य में पूछने योग्य तथा पूजन योग्य हैं। यह एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन् पूरक होते हैं।
चौबीस अक्षरों का गायत्री मंत्र सर्व प्रसिद्ध है, उसे आजकल शिक्षित वर्ग के सभी लोग जानते हैं। फिर भी उपासना करनी है, साधना के अन्य लाभों को लेना है, तो गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र का शाप विमोचन कराके, कीलित गायत्री का उत्कीलन करके साधना करनी चाहिए। गुरुमुख होकर गायत्री दीक्षा लेना एक संस्कार है, जिसमें उस दिन गुरु-शिष्य दोनों को उपवास रखना पड़ता है। शिष्य, चन्दन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, अन्न, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि से गुरुपूजन करता है। गुरु-शिष्य को मंत्र देता है और पथ-प्रदर्शक का भार अपने ऊपर लेता है। इस ग्रन्थिबन्धन के उपरान्त अपने उपयुक्त साधना निश्चित कराके जो शिष्य श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ते हैं, वे भगवती की कृपा से अपने अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं।
जब से गायत्री की दीक्षा ली जाए, तब से लेकर जब तक पूर्ण सिद्धि प्राप्त न हो जाए, तब तक साधना गुरु को अपनी साधना के समय समीप रखना चाहिए। गुरु का प्रत्यक्ष रूप से साथ रहना तो सम्भव नहीं हो सकता है, पर उनका चित्र काँच में मढ़वा कर पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है और गायत्री संध्या, जप, अनुष्ठान या कोई और साधना आरम्भ करने से पूर्व उस चित्र का पूजन, धूप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, चन्दन आदि से कर लेना चाहिए। जहाँ चित्र उपलब्ध न हो वहाँ नारियल को गुरु के प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिए। एकलव्य भील की कथा प्रसिद्ध है कि उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उसी को गुरु माना था, उन्हीं से पूछकर बाण विद्या सीखता था। अन्त में वह इतना सफल धनुर्धारी हुआ कि पाण्डवों तक को उसकी विशेषता देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ा था। चित्र या नारियल के माध्यम से गुरु-पूजा करके जो भी गायत्री-साधना आरम्भ की जाएगी वह शाप-मुक्त तथा उत्कीलित होगी।
|
|||||