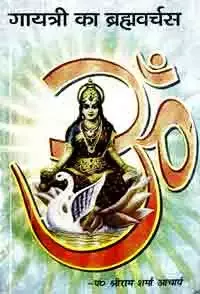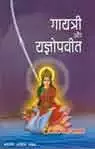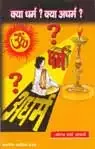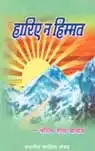|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> गायत्री का ब्रह्मवर्चस गायत्री का ब्रह्मवर्चसश्रीराम शर्मा आचार्य
|
5 पाठक हैं |
||||||
गायत्री और सावित्री उपासना
त्रिविध प्रशिक्षण की त्रिवेणी
आहार के तीन वर्ग हैं-(१) अन्न (२) जल (३) वायु, इन तीनों के सहारे ही मनुष्य जीवित रहता है।
पौधे को बढ़ने के लिए (१) भूमि (२) खाद (३) पानी तीनों की आवश्यकता पड़ती है।
व्यापार के लिए (१) पूँजी (२) उत्पादन (३) विक्रय तीनों साधन जुटाने होते हैं।
आत्मिक प्रगति भी एक उच्चस्तरीय उत्पादन एवं गरिमा सम्पन्न व्यवसाय है। इसके लिए तीन साधन चाहिए (१) भक्तियोग (२) ज्ञानयोग (३) कर्मयोग।
इन तीनों की समन्वित व्यवस्था करने पर ही (१) कारण शरीर (२) सूक्ष्म शरीर (३) स्थूल शरीर को परिष्कृत एवं प्रखर बनाने का अवसर मिलता है। उपरोक्त तीनों साधनाओं में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे अकेले के बलबूते जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इनमें से एक भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसे दोड़कर प्रगति का रथ एक कदम आगे बढ़ सके धुरी और दो पहिए मिलने से ही उसमें गतिशीलता उत्पन्न होती है।
ब्रह्मवर्चस सत्रों की प्रशिक्षण पद्धति में उपरोक्त तीनों तत्वों का समावेश करके उसे साधना क्षेत्र की त्रिवेणी के समतुल्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। उसकी समग्रता यह विश्वास दिलाती है कि साधनों को सर्वागपूर्ण बनाया जा रहा है तो उसका प्रतिफल भी सुनियोजित सत्प्रयत्नों की तरह संतोष जनक ही होना चाहिए।
एक महीने की साधना में भी उस रूप रेखा का समावेश है जिसे अपनाकर अधिक समय टिकने वाले अधिक प्रगति कर सकते हैं। जिन्हें उतने ही समय रुकना है वे अभ्यास कराये गये आधारों को अपनाकर आत्मिक प्रगति के राज मार्ग पर अनवरत गति से चलते हुए परम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं।
प्रशिक्षण के तीन पक्ष हैं (१) साधना (२) ब्रह्मविद्या (३) लोक मंगल।
नित्य कर्म से बंधा हुआ प्राय: सारा ही समय क्रमबद्ध रूप से इन्हीं तीन अभ्यासों में नियोजित रखा जायगा। साधना में गायत्री और सावित्री दोनों की उपासना सम्मिलित है। ब्रह्मवर्चस शब्द का तात्पर्य ही यह है कि उसमें परिष्कार के लिए योगाभ्यास का और प्रखरता के लिए तपश्चर्या का वाममार्गी सावित्री की कुण्डलिनी साधना का समन्वय रहना है। सूर्योदय से पूर्व गायत्री साधना का और सूर्यास्त के उपरान्त कुण्डलिनी जागरण का विधि। विधान हर साधक की स्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखकर कराया जायगा। इस सन्दर्भ में किसे क्या सिखाया जायगा, इनका पूर्व निर्धारण नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की स्थिति और आवश्यकता भिन्न होती है। इसलिए। उच्च स्तरीय साधना का निर्णय उनका तात्विक निरीक्षण करके ही किया जा सकता है।
सामान्यतया प्रातःकालीन गायत्री उपासना में वे अभ्यास कराये जाते हैं जो ब्रह्मलोक, ब्रह्मरन्ध्र, आशाचक्र, सहप्तारचक्र, तालु, मूर्धा श्वास-प्रश्वास के केन्द्र बिन्दु मानकर बने हैं और जिनका प्रभाव शीर्ष भाग में सन्निहित ब्रह्म ज्योति की, आत्म चेतना को प्रभावित करता है। शीर्ष को ब्रह्मलोक माना गया है। इसमें दिव्य चेतना का अधिपत्य है। यही गायत्री लोक है। गायत्री साधना द्वारा जो कुछ पाया जाता है वह सारा विभूति वैभव इसी परिधि में उपार्जित किया जाता है।
सायंकालीन साधना में कुण्डलिनी जागरण की क्रिया प्रतिक्रियाओं का समुच्चय है। जननेन्द्रिय मूल में निवास करने वाली प्राण ऊर्जा का केन्द्र मूलाधार चक्र माना गया है। उसी के योगाग्नि, कालाग्नि, जीवनी शक्ति, काली, कुण्डलिनी आदि अनेक नाम हैं। नाभिचक्र से लेकर जननेन्द्रिय मूल और कटि प्रदेश का सारा क्षेत्र इसी महाशक्ति को ज्वलन्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस क्षेत्र तक साधक की संकल्प शक्ति को पहुँचाने का एक मात्र मार्ग मेरुदण्ड है। उसी को साधना विज्ञान में देवयान कहा गया है। इसमें प्रवाहित होने वाली तीन दिव्य धाराएँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कही जाती हैं। इन्ही का संगम अध्यात्म क्षेत्र का त्रिवेणी संगम कहा गया है।
कुण्डलिनी जागरण की क्रिया प्रक्रिया की समुद्र मन्थन के समतुल्य बताया गया है। समुद्र मन्थन से १४ दिव्य रत्न निकलने की पौराणिक गाथा का संकेत यही है कि इस कुण्डलिनी क्षेत्र का मन्थन करने वाले अपने स्तर के अनुरूप उपयोगी प्रतिफल उपलब्ध कर सकते हैं। मूलाधार की साधना का विशद विज्ञान तन्त्र के अन्तर्गत आता है। सहसार की क्षमताओं से लाभान्वित होने की प्रक्रिया योग कहलाती है। योग से ज्ञान की और तन्त्र से विज्ञान की उपलब्धि होती है। एक की ऋद्धियों का और दूसरे को सिद्धियों का उद्गम माना गया है। तन्त्र का अभ्यास काल रात्रि है और योग के लिए ब्रह्ममुहूर्त सर्वोत्तम माना गया है। यों इन्हें सुविधानुसार अन्य समयों में भी किया जा सकता है।
सामान्य तथा मध्यवर्ती स्तर के साधकों को प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में एक घंटा योगाभ्यास परक गायत्री साधना कराई जाती है। रात्रि को तंत्र प्रक्रिया के अन्तर्गत कुण्डलिनी जागरण के वे अभ्यास कराये जाते हैं जिन्हें वंध, मुद्रा और प्राण संधान की त्रिविध तंत्र प्रक्रियाओं का आधार अंग माना जाता है। यह विधान भी साधक की स्थिति के अनुरूप ही बताये जाते हैं। एक महीने के समय में सब कुछ हल्का ही हल्का रखा गया है। साधना विज्ञान की विशालता और गरिमा को देखते हुए इसे बाल कक्षा जितना ही कहा जा सकता है। अभ्यस्त लोगों के लिए हर नया प्रयोग भारी पड़ता है। ध्यान योग में थोड़ा अधिक गहरा उतरने लगा जाय तो सिर भारी होने लगता है। इस कठिनाई का पूरा-२ ध्यान रखा गया है और पाठ्यक्रम इतना सरल रखा गया है कि उसे बिना किसी प्रकार का खतरा उठाये कोई नया अभ्यासी भी सरलता पूर्वक सम्पन्न कर सके। व्यायमशालाओं और पाठशालाओं में नवागन्तुकों को साहस और उत्साह बढ़ाने की दृष्टि से जो कुछ सिखाया कराया जाता है वह सरलतम ही होता है। अधिक बड़ा पराक्रम एवं दुस्साहस करने की स्थिति तो तब आती है जब अभ्यास में परिपक्वता और प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होने लगे।
प्रातः सार्य साधना के दोनों पक्ष पूरे होते रहेंगे। सवेरे से लेकर मध्यान्ह तक का समय ब्रह्म विद्या के अवगाहन के लिए है और मध्यान्ह से सायंकाल तक लोक शिक्षण में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए मध्यान्ह तक स्वाध्याय और सत्संग का क्रम चलेगा। मध्यान्होत्तर भाषण कला का अभ्यास एवं युग परिवर्तन के लिए आवश्यक रचनात्मक प्रवृत्तियों का क्रियान्वयन करने का व्यवहारिक ज्ञान कराया जायगा।
एक महीने की अवधि में ब्रह्मवर्चस के प्रशिक्षण के सूत्र संचालक द्वारा प्रतिदिन एक प्रवचन किया जाता रहेगा। अध्यात्म तत्वज्ञान और साधना-विज्ञान की जीवन धारा में घुला देने का उपाय सुझाया जाता रहेगा। और बताया जायेगा कि जीवन साधना की प्रक्रिया का शुभ आरम्भ कितनी सरलता से कितने छोटे रूप में किया जा सकता है और उसे क्रमश: बढ़ाते हुए। किस प्रकार सिद्धावस्था तक पहुँचा जा सकता है। साधक के सम्मुख प्रस्तुत कठिनाइयों के समाधान के लिए आवश्यक विचार विनिमय एवं परामर्श की प्रक्रिया भी इसी के साथ जुड़ी रहेगी।
स्वाध्याय के लिए कुछ निर्धारित साहित्य उस अवधि में पढ़ लेने के लिए कहा जायेगा। इस अध्ययन क्रम में वे चुनी हुई पुस्तकें ही रखी गई हैं जो साधक की प्रगति में सहायक हो सकें और उसके सामने प्रस्तुत अवरोधों का निराकरण कर सकें। सामान्य प्रबचन तो सभी के लिए एक होगा पर परामर्श परक विचार विनिमय समय-समय पर साधक की स्थिति के अनुरूप ही होता रहेगा। इसी प्रकार कुछ पुस्तकें सभी के लिए समान रूप से स्वाध्याय में सम्मिलित रहेंगी पर सामान्यतया अधिक समय तक वे पुस्तकें पढ़ने का निर्देश दिया जायेगा जो साधक की मनः स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उपयुक्त आवश्यक समझी जायेंगी। स्वाध्याय साहित्य का निर्धारण भी ब्रह्मवर्चस प्रशिक्षण के सूत्र-संचालक करेंगे। यह स्वाध्याय भी साधना की ही तरह प्रेरणाप्रद एवं भावी जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम कर सके इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा।
मध्यान्होत्तर की कक्षा में युग शिल्पियों के लिए आवश्यक योग्यताओं को विकसित करने तथा कार्य क्षेत्र में जन सम्पर्क में आशाजनक सफलता उपलब्ध करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाये जायेंगे। जो आवश्यक हैं उसका क्रियात्मक अभ्यास भी कराया जायगा। इन योग्यताओं में भाषण कला संभाषण कुशलता को प्रधान माना जाता है।
युग परिवर्तन के लिए जन मानस का परिष्कार करना होगा ज्ञान यज्ञ का युग अनुष्ठान प्रतीक्षित विचार क्रान्ति अभियान के रूप में गतिशील हो रहा है। इसमें जागृत आत्माओं को प्रस्तुत लोक मानस को जगाने में संलग्न होना होगा। यह कार्य सामूहिक रूप में प्रवचनों द्वारा सम्पन्न करना होता है। बड़े जन सम्मेलनों आयोजनों में भाषण करने होते हैं और थोड़े लोगों के साथ ज्ञान गोष्ठियों में विचार विनिमय परामर्श करना होता है। यह दोनों ही कार्य वाणी के प्रयोग उपयोग के द्वारा सम्पन्न होते हैं। कुशल वाणी ही अपने प्रभाव से अभीष्ट प्रयोजन पूरा कर सकती है। जिसे दूसरों के सम्मुख अपने विचार व्यक्त करने में झिझक लगती है उसके लिए युग सृजन में महत्वपूर्ण कर सकना कठिन पड़ेगा। साहित्य का प्रचार करने के लिए भी तो किसी न किसी रूप में वाणी का ही प्रयोग करना होता है। झोला पुस्तकालय, चल पुस्तकालय आदि को गतिशील बनाने में वाणी ही काम आती है।
ब्रह्मवर्चस सत्र में समूह मंच पर भाषण देने और व्यक्तिगत सम्पर्क में प्रभावी संभाषण करने की कला का नियमित अभ्यास मध्यान्तर प्रशिक्षण में कराया जाता है। इसके अतिरिक्त यज्ञ कुत्य सहित पर्व संस्कार आदि के अवसर पर सम्पन्न होने वाले धार्मिक कर्मकाण्डों को कराने का अभ्यास भी साथ-साथ चलता रहेगा। युग निर्माण अभियान में धर्म मंच से लोक शिक्षण की प्रक्रिया को रचनात्मक कार्यक्रम का अंग बनाया गया है। समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए होने वाले आयोजनों में किसी न किसी रूप में यज्ञ कृत्य एवं अन्य पूजा-विधानों का समावेश रहता है। युग शिल्पियों को उसमें प्रवीण होना ही छोटे बड़े सम्मेलनों में यज्ञ कृत्य होते हैं उन विधानों की व्याख्या करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लोक शिक्षण क्रम चलते हैं। इसलिए जहाँ। भाषण संभाषण शैली की कुशलता आवश्यक है वहाँ साथ-साथ जुड़े रहने वाले धर्मानुष्ठान को सम्पन्न कर सकने की प्रवीणता भी रहनी चाहिए। ब्रह्मवर्चस को मध्यान्तर शिक्षण में इन दोनों का अभ्यास कराया जाता है।
सफल जन सम्पर्क, रचनात्मक क्रिया-कलापों का सूत्र संचालन, समायिक समस्याओं के समाधान का सुनिश्चित दृष्टिकोण, सृजन शिल्पियों का, प्रतिभावान व्यक्तित्वों का सहयोग सम्पादन, अवरोधों के निराकरण का दूरदर्शी व्यवहार कौशल जैसे अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनसे हर लोक सेवी को। परिचित होना चाहिए और इतनी पूर्व तैयारी रहनी चाहिए कि किसी भी उतार चढ़ाव पर डगमगाने की आवश्यकता न पड़े। यह कुशलता ब्रह्मवर्चस साधकों को तीसरे पहर के प्रशिक्षण में इसलिए उपलब्ध कराई जाती है कि यह कृत्य भी भावी जीवन में उनकी सामान्य दिनचर्या का ही एक अंग बन कर रहेगा, आत्मिक प्रगति के सेवा धर्म को अपनाये बिना प्राचीन काल के धर्म परायणों का भी काम न चला था और न भविष्य में किसी धर्म प्रेमी को उससे विरत रहने की इच्छा होगी। सिद्धि या मुक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी सेठ या शासक बनने जैसी क्षुद्र ही है। ब्रह्मवर्चस् के साधक उदात्त भूमिका में विकसित होंगे तो उन्हें युग साधना के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को किसी न किसी रूप में नियोजित करना ही होगा। शरीर यात्रा, परिवार, संरक्षण, आजीविका प्रबंध, लोक व्यवहार की तरह ही ब्रह्मवर्चस् के छात्र युग साधना को भी अपने सामान्य जीवन क्रम में सम्मिलित करेंगे। ऐसी दशा में उस सन्दर्भ की आवश्यक ज्ञान अनुभव और अभ्यास रहना ही चाहिए। तीसरे प्रहर की शिक्षण व्यवस्था में इन सभी तत्वों का समावेश रखा गया है जिनके आधार पर ब्रह्मवर्चस साधना सत्र में शिक्षार्थी अपने भावी जीवन क्रम में एक महत्वपूर्ण अंग का सफलता पूर्वक सुसंचालन कर सकें।
हर अंग्रेजी महीने में पहली से तीस तारीख तक चलने वाले एक-एक महीने वाले ब्रह्मवर्चस सत्रों की सुनिश्चित अभिनव श्रृंखला १ जुलाई से आरम्भ होने जा रही है इसके बाद वह लगातार चलती रहेगी। इसकी विशेषता यह है कि हर शिक्षार्थों की परिस्थिति का अलग से विश्लेषण किया जायेगा और तदनुरूप उनके लिए साधना एवं शिक्षण का क्रम निर्धारित किया जायेगा। तपश्चर्या में आहार की सात्विकता और मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जायगा। उस पर जिसके लिए जिस प्रकार, जितना नियंत्रण संभव होगा, तदनुरूप उसे परामर्श दिया जायेगा। मन की सात्विकता स्थिरता के लिए अन्न आहार तप का कोई न कोई स्वरूप हर साधक को अपनाना होगा। इन विशेषताओं के कारण इन सत्रों को विशेष आधार पर खड़ा किया गया और विशेष परिणाम उत्पन्न करने वाला ही कहा जा सकता है। त्रिपदा गायत्री की यह त्रिवेणी साधना युग साधना के अनुरूप होने के कारण नितान्त सामयिक एवं अतीव महत्वपूर्ण समझी जा सकती है।
|
|||||